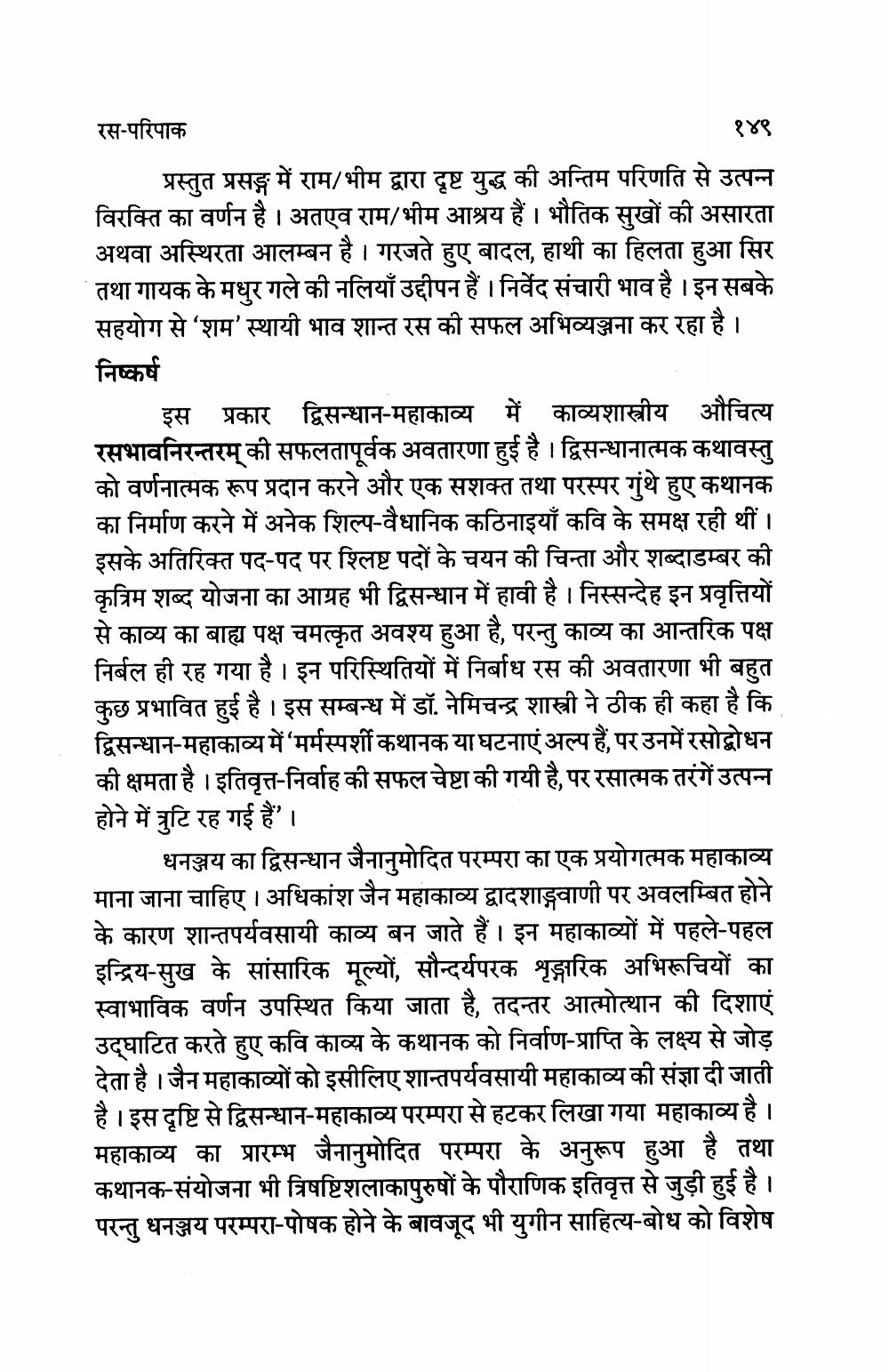________________
रस-परिपाक
१४९
प्रस्तुत प्रसङ्ग में राम / भीम द्वारा दृष्ट युद्ध की अन्तिम परिणति से उत्पन्न विरक्ति का वर्णन है । अतएव राम / भीम आश्रय हैं। भौतिक सुखों की असारता अथवा अस्थिरता आलम्बन है । गरजते हुए बादल, हाथी का हिलता हुआ सिर तथा गायक के मधुर गले की नलियाँ उद्दीपन हैं । निर्वेद संचारी भाव है । इन सबके सहयोग से 'शम' स्थायी भाव शान्त रस की सफल अभिव्यञ्जना कर रहा है । निष्कर्ष
1
इस
प्रकार द्विसन्धान- महाकाव्य में काव्यशास्त्रीय औचित्य रसभावनिरन्तरम् की सफलतापूर्वक अवतारणा हुई है । द्विसन्धानात्मक कथावस्तु को वर्णनात्मक रूप प्रदान करने और एक सशक्त तथा परस्पर गुंथे हुए कथानक का निर्माण करने में अनेक शिल्प- वैधानिक कठिनाइयाँ कवि के समक्ष रही थीं । इसके अतिरिक्त पद-पद पर श्लिष्ट पदों के चयन की चिन्ता और शब्दाडम्बर की कृत्रिम शब्द योजना का आग्रह भी द्विसन्धान में हावी है । निस्सन्देह इन प्रवृत्तियों से काव्य का बाह्य पक्ष चमत्कृत अवश्य हुआ है, परन्तु काव्य का आन्तरिक पक्ष निर्बल ही रह गया है । इन परिस्थितियों में निर्बाध रस की अवतारणा भी बहुत कुछ प्रभावित हुई है । इस सम्बन्ध में डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री ने ठीक ही कहा है कि द्विसन्धान-महाकाव्य में 'मर्मस्पर्शी कथानक या घटनाएं अल्प हैं, पर उनमें रसोद्बोधन की क्षमता है । इतिवृत्त - निर्वाह की सफल चेष्टा की गयी है, पर रसात्मक तरंगें उत्पन्न होने में त्रुटि रह गई हैं' ।
धनञ्जय का द्विसन्धान जैनानुमोदित परम्परा का एक प्रयोगत्मक महाकाव्य माना जाना चाहिए। अधिकांश जैन महाकाव्य द्वादशाङ्गवाणी पर अवलम्बित होने के कारण शान्तपर्यवसायी काव्य बन जाते हैं । इन महाकाव्यों में पहले-पहल इन्द्रिय-सुख के सांसारिक मूल्यों, सौन्दर्यपरक शृङ्गारिक अभिरूचियों का स्वाभाविक वर्णन उपस्थित किया जाता है, तदन्तर आत्मोत्थान की दिशाएं उद्घाटित करते हुए कवि काव्य के कथानक को निर्वाण-प्राप्ति के लक्ष्य से जोड़ देता है । जैन महाकाव्यों को इसीलिए शान्तपर्यवसायी महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है । इस दृष्टि से द्विसन्धान-महाकाव्य परम्परा से हटकर लिखा गया महाकाव्य है । महाकाव्य का प्रारम्भ जैनानुमोदित परम्परा के अनुरूप हुआ है तथा कथानक-संयोजना भी त्रिषष्टिशलाकापुरुषों के पौराणिक इतिवृत्त से जुड़ी हुई है । परन्तु धनञ्जय परम्परा-पोषक होने के बावजूद भी युगीन साहित्य-बोध को विशेष