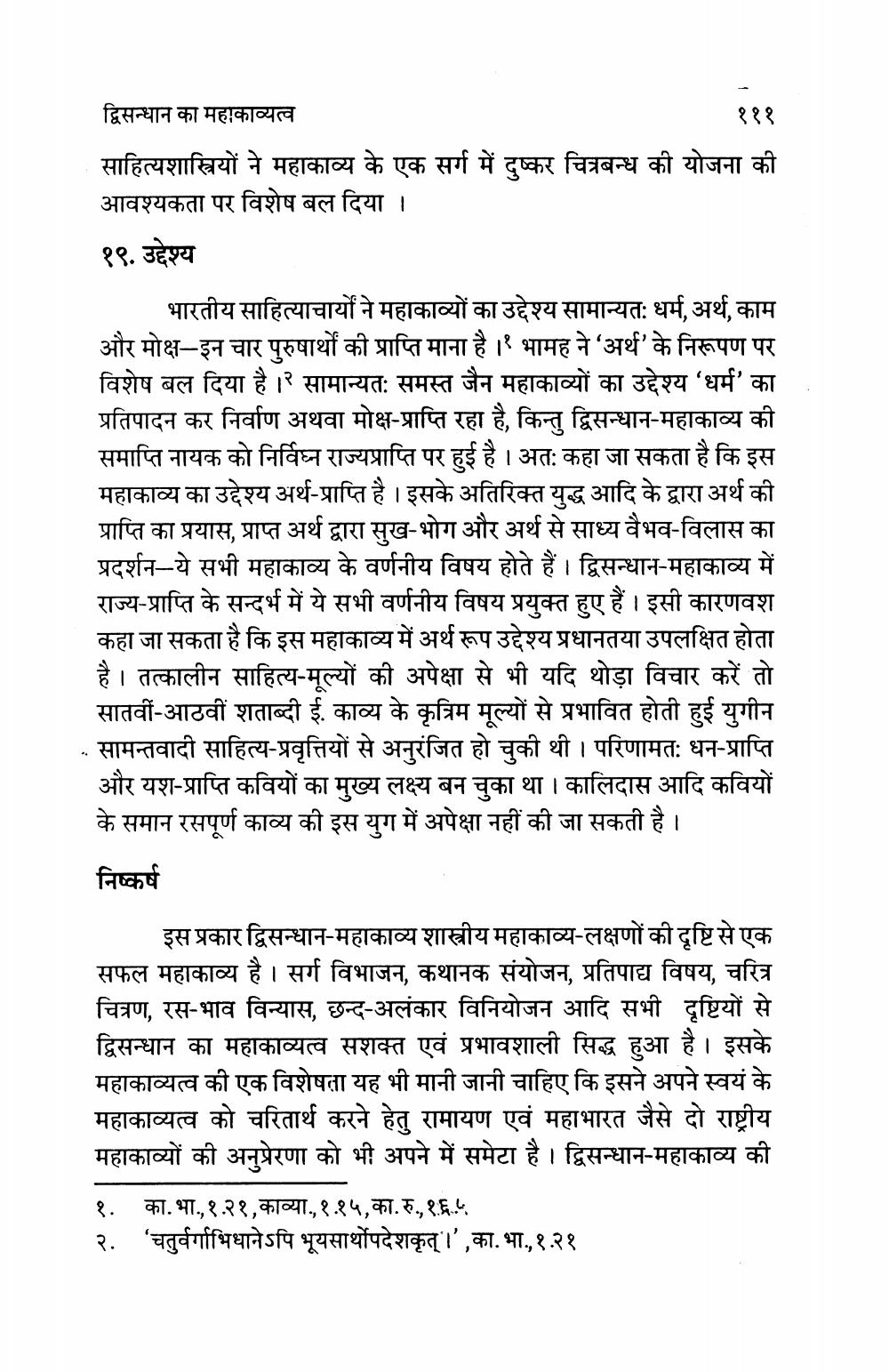________________
द्विसन्धान का महाकाव्यत्व साहित्यशास्त्रियों ने महाकाव्य के एक सर्ग में दुष्कर चित्रबन्ध की योजना की आवश्यकता पर विशेष बल दिया । १९. उद्देश्य ___भारतीय साहित्याचार्यों ने महाकाव्यों का उद्देश्य सामान्यत: धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष-इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति माना है । भामह ने 'अर्थ' के निरूपण पर विशेष बल दिया है। सामान्यत: समस्त जैन महाकाव्यों का उद्देश्य 'धर्म' का प्रतिपादन कर निर्वाण अथवा मोक्ष-प्राप्ति रहा है, किन्तु द्विसन्धान-महाकाव्य की समाप्ति नायक को निर्विघ्न राज्यप्राप्ति पर हुई है । अत: कहा जा सकता है कि इस महाकाव्य का उद्देश्य अर्थ-प्राप्ति है । इसके अतिरिक्त युद्ध आदि के द्वारा अर्थ की प्राप्ति का प्रयास, प्राप्त अर्थ द्वारा सुख-भोग और अर्थ से साध्य वैभव-विलास का प्रदर्शन-ये सभी महाकाव्य के वर्णनीय विषय होते हैं। द्विसन्धान-महाकाव्य में राज्य-प्राप्ति के सन्दर्भ में ये सभी वर्णनीय विषय प्रयुक्त हुए हैं। इसी कारणवश कहा जा सकता है कि इस महाकाव्य में अर्थ रूप उद्देश्य प्रधानतया उपलक्षित होता है। तत्कालीन साहित्य-मूल्यों की अपेक्षा से भी यदि थोड़ा विचार करें तो सातवीं-आठवीं शताब्दी ई. काव्य के कृत्रिम मूल्यों से प्रभावित होती हुई युगीन .. सामन्तवादी साहित्य-प्रवृत्तियों से अनुरंजित हो चुकी थी। परिणामत: धन-प्राप्ति
और यश-प्राप्ति कवियों का मुख्य लक्ष्य बन चुका था। कालिदास आदि कवियों के समान रसपूर्ण काव्य की इस युग में अपेक्षा नहीं की जा सकती है। निष्कर्ष
इस प्रकार द्विसन्धान-महाकाव्य शास्त्रीय महाकाव्य-लक्षणों की द्रष्टि से एक सफल महाकाव्य है । सर्ग विभाजन, कथानक संयोजन, प्रतिपाद्य विषय, चरित्र चित्रण, रस-भाव विन्यास, छन्द-अलंकार विनियोजन आदि सभी दृष्टियों से द्विसन्धान का महाकाव्यत्व सशक्त एवं प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। इसके महाकाव्यत्व की एक विशेषता यह भी मानी जानी चाहिए कि इसने अपने स्वयं के महाकाव्यत्व को चरितार्थ करने हेतु रामायण एवं महाभारत जैसे दो राष्ट्रीय महाकाव्यों की अनुप्रेरणा को भी अपने में समेटा है। द्विसन्धान-महाकाव्य की १. का.भा.,१.२१,काव्या.,१.१५,का.रु.,१६.५ २. 'चतुर्वर्गाभिधानेऽपि भूयसार्थोपदेशकृत् ।',का.भा.,१.२१