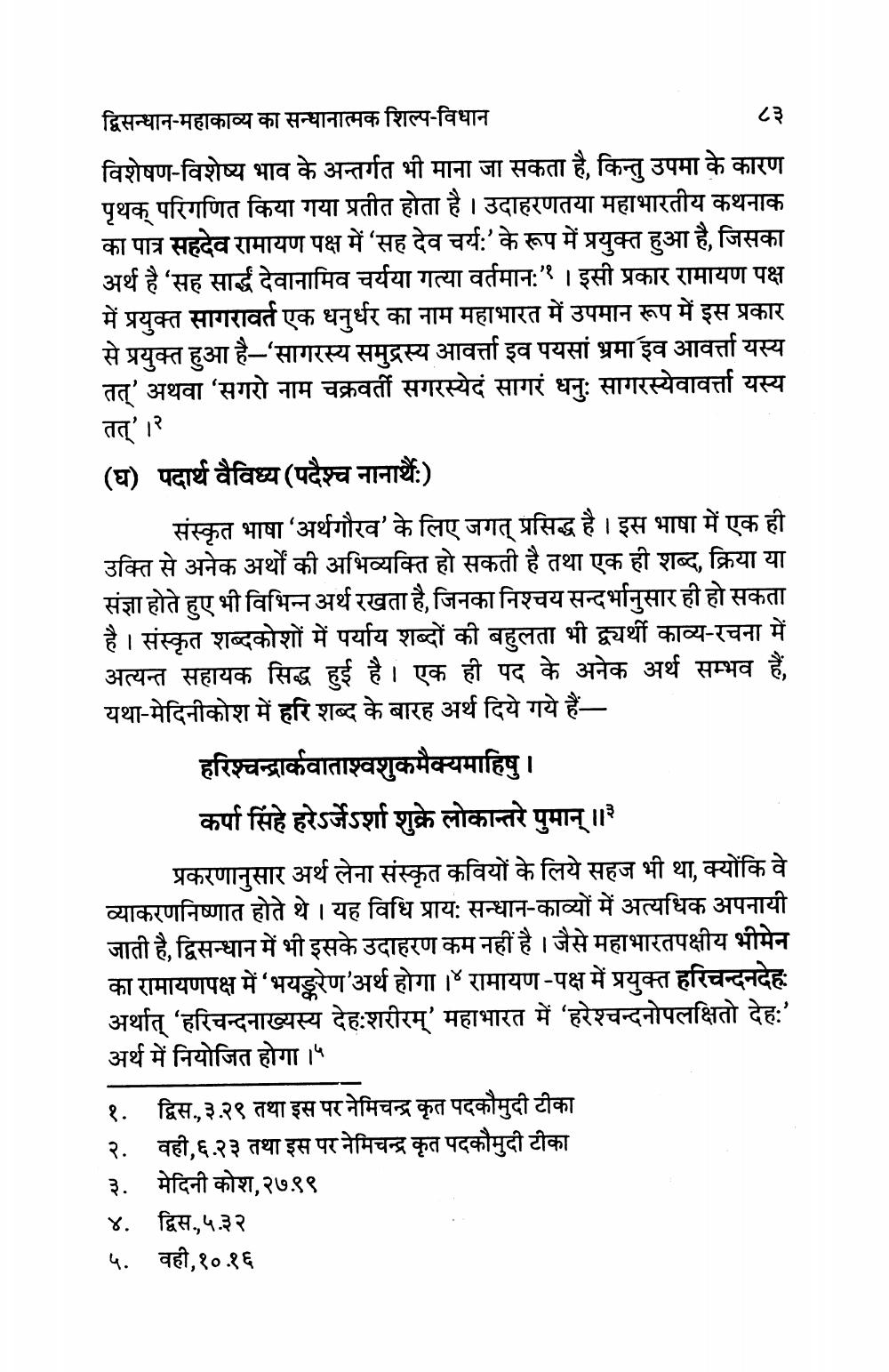________________
८३
द्विसन्धान-महाकाव्य का सन्धानात्मक शिल्प-विधान विशेषण-विशेष्य भाव के अन्तर्गत भी माना जा सकता है, किन्तु उपमा के कारण पृथक् परिगणित किया गया प्रतीत होता है। उदाहरणतया महाभारतीय कथनाक का पात्र सहदेव रामायण पक्ष में 'सह देव चर्य:' के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है 'सह सार्द्ध देवानामिव चर्यया गत्या वर्तमान: । इसी प्रकार रामायण पक्ष में प्रयुक्त सागरावर्त एक धनुर्धर का नाम महाभारत में उपमान रूप में इस प्रकार से प्रयुक्त हुआ है-'सागरस्य समुद्रस्य आवर्ता इव पयसां भ्रमा इव आवर्ता यस्य तत्' अथवा 'सगरो नाम चक्रवर्ती सगरस्येदं सागरं धनुः सागरस्येवावर्ता यस्य तत्' । (घ) पदार्थ वैविध्य (पदैश्च नानाथै:)
संस्कृत भाषा ‘अर्थगौरव' के लिए जगत् प्रसिद्ध है । इस भाषा में एक ही उक्ति से अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति हो सकती है तथा एक ही शब्द, क्रिया या संज्ञा होते हुए भी विभिन्न अर्थ रखता है, जिनका निश्चय सन्दर्भानुसार ही हो सकता है । संस्कृत शब्दकोशों में पर्याय शब्दों की बहुलता भी व्यर्थी काव्य-रचना में अत्यन्त सहायक सिद्ध हई है। एक ही पद के अनेक अर्थ सम्भव हैं, यथा-मेदिनीकोश में हरि शब्द के बारह अर्थ दिये गये हैं
हरिश्चन्द्रार्कवाताश्वशुकमैक्यमाहिषु।
कर्पा सिंहे हरेऽर्जेऽर्शा शुक्रे लोकान्तरे पुमान् ॥२
प्रकरणानुसार अर्थ लेना संस्कृत कवियों के लिये सहज भी था, क्योंकि वे व्याकरणनिष्णात होते थे। यह विधि प्राय: सन्धान-काव्यों में अत्यधिक अपनायी जाती है, द्विसन्धान में भी इसके उदाहरण कम नहीं है । जैसे महाभारतपक्षीय भीमेन का रामायणपक्ष में भयङ्करेण'अर्थ होगा। रामायण-पक्ष में प्रयुक्त हरिचन्दनदेहः अर्थात् 'हरिचन्दनाख्यस्य देहःशरीरम्' महाभारत में 'हरेश्चन्दनोपलक्षितो देहः' अर्थ में नियोजित होगा। १. द्विस,३.२९ तथा इस पर नेमिचन्द्र कृत पदकौमुदी टीका २. वही,६.२३ तथा इस पर नेमिचन्द्र कृत पदकौमुदी टीका ३. मेदिनी कोश,२७.९९ ४. द्विस.,५.३२ ५. वही,१०.१६