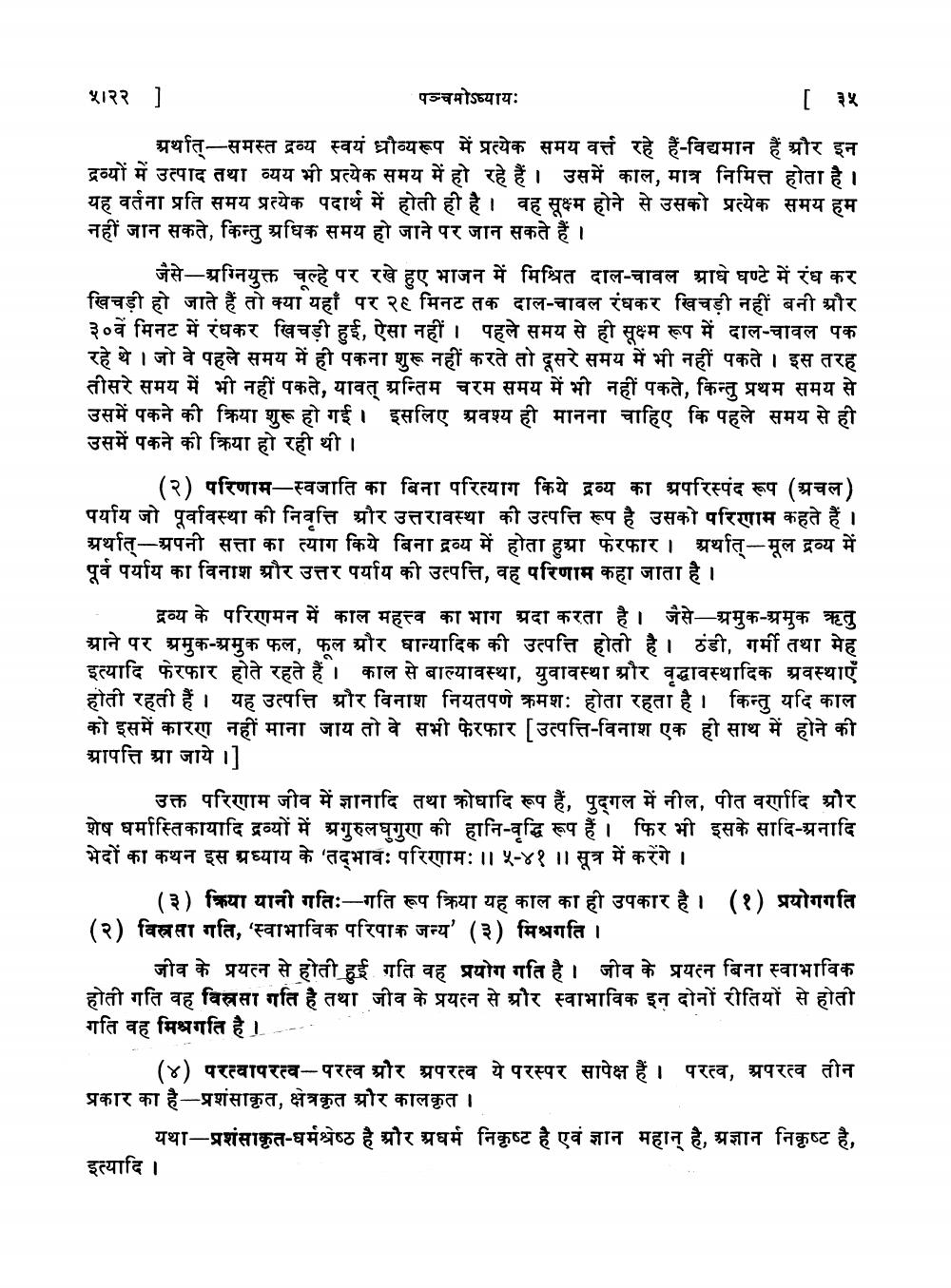________________
५।२२ ] पञ्चमोऽध्यायः
[ ३५ _ अर्थात्-समस्त द्रव्य स्वयं ध्रौव्यरूप में प्रत्येक समय वर्त्त रहे हैं-विद्यमान हैं और इन द्रव्यों में उत्पाद तथा व्यय भी प्रत्येक समय में हो रहे हैं। उसमें काल, मात्र निमित्त होता है। यह वर्तना प्रति समय प्रत्येक पदार्थ में होती ही है। वह सूक्ष्म होने से उसको प्रत्येक समय हम नहीं जान सकते, किन्तु अधिक समय हो जाने पर जान सकते हैं।
जैसे-अग्नियुक्त चल्हे पर रखे हुए भाजन में मिश्रित दाल-चावल आधे घण्टे में रंध कर खिचड़ी हो जाते हैं तो क्या यहाँ पर २६ मिनट तक दाल-चावल रंधकर खिचड़ी नहीं बनी और ३०वें मिनट में रंधकर खिचड़ी हुई, ऐसा नहीं। पहले समय से ही सूक्ष्म रूप में दाल-चावल पक रहे थे । जो वे पहले समय में ही पकना शुरू नहीं करते तो दूसरे समय में भी नहीं पकते । इस तरह तीसरे समय में भी नहीं पकते, यावत अन्तिम चरम समय में भी नहीं पकते. किन्त प्रथम समय उसमें पकने की क्रिया शुरू हो गई। इसलिए अवश्य ही मानना चाहिए कि पहले समय से ही उसमें पकने की क्रिया हो रही थी।
(२) परिणाम-स्वजाति का बिना परित्याग किये द्रव्य का अपरिस्पंद रूप (अचल) पर्याय जो पूर्वावस्था की निवृत्ति और उत्तरावस्था की उत्पत्ति रूप है उसको परिणाम कहते हैं। अर्थात्-अपनी सत्ता का त्याग किये बिना द्रव्य में होता हुआ फेरफार । अर्थात्-मूल द्रव्य में पूर्व पर्याय का विनाश और उत्तर पर्याय की उत्पत्ति, वह परिणाम कहा जाता है । - द्रव्य के परिणमन में काल महत्त्व का भाग अदा करता है। जैसे—अमुक-अमुक ऋतु आने पर अमुक-अमुक फल, फूल और धान्यादिक की उत्पत्ति होती है। ठंडी, गर्मी तथा मेह इत्यादि फेरफार होते रहते हैं। काल से बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्थादिक अवस्थाएँ होती रहती हैं। यह उत्पत्ति और विनाश नियतपणे क्रमशः होता रहता है। किन्तु यदि काल को इसमें कारण नहीं माना जाय तो वे सभी फेरफार [उत्पत्ति-विनाश एक ही साथ में होने की आपत्ति आ जाये।]
उक्त परिणाम जीव में ज्ञानादि तथा क्रोधादि रूप हैं, पुद्गल में नील, पीत वर्णादि और शेष धर्मास्तिकायादि द्रव्यों में अगुरुलघुगुण की हानि-वृद्धि रूप हैं। फिर भी इसके सादि-अनादि भेदों का कथन इस अध्याय के 'तद्भावः परिणामः ।। ५-४१ ।। सूत्र में करेंगे।
(३) क्रिया यानी गतिः-गति रूप क्रिया यह काल का ही उपकार है। (१) प्रयोगगति (२) विनसा गति, 'स्वाभाविक परिपाक जन्य' (३) मिश्रगति ।
जीव के प्रयत्न से होती हुई गति वह प्रयोग गति है। जीव के प्रयत्न बिना स्वाभाविक होती गति वह विनसा गति है तथा जीव के प्रयत्न से और स्वाभाविक इन दोनों रीतियों से होती गति वह मिश्रगति है। ----
(४) परत्वापरत्व-परत्व और अपरत्व ये परस्पर सापेक्ष हैं। परत्व, अपरत्व तीन प्रकार का है-प्रशंसाकृत, क्षेत्रकृत और कालकृत ।
यथा-प्रशंसाकृत-धर्मश्रेष्ठ है और अधर्म निकृष्ट है एवं ज्ञान महान् है, अज्ञान निकृष्ट है, इत्यादि।