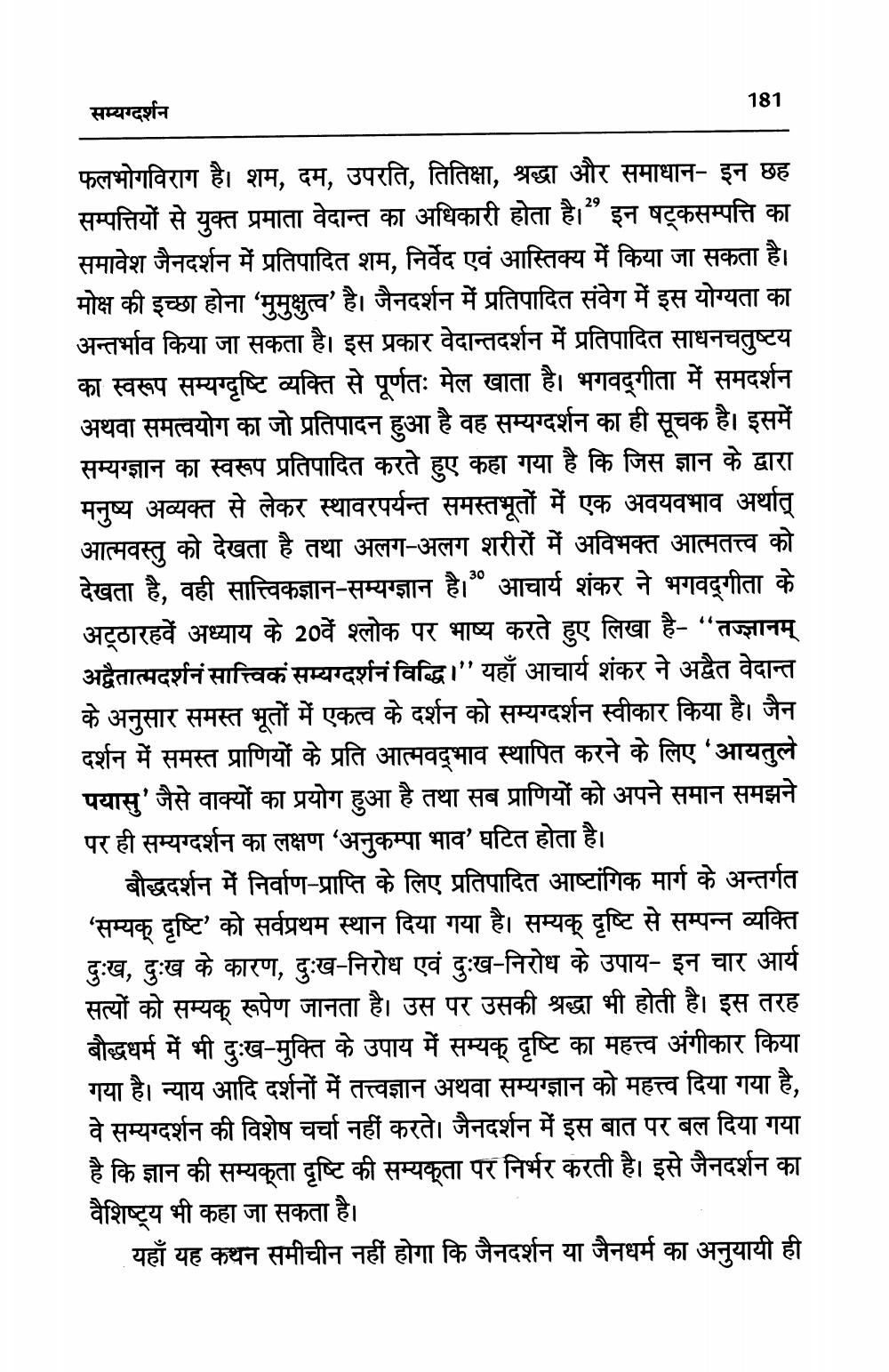________________
सम्यग्दर्शन
181
फलभोगविराग है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान- इन छह सम्पत्तियों से युक्त प्रमाता वेदान्त का अधिकारी होता है।" इन षट्कसम्पत्ति का समावेश जैनदर्शन में प्रतिपादित शम, निर्वेद एवं आस्तिक्य में किया जा सकता है। मोक्ष की इच्छा होना ‘मुमुक्षुत्व' है। जैनदर्शन में प्रतिपादित संवेग में इस योग्यता का अन्तर्भाव किया जा सकता है। इस प्रकार वेदान्तदर्शन में प्रतिपादित साधनचतुष्टय का स्वरूप सम्यग्दृष्टि व्यक्ति से पूर्णतः मेल खाता है। भगवद्गीता में समदर्शन अथवा समत्वयोग का जो प्रतिपादन हुआ है वह सम्यग्दर्शन का ही सूचक है। इसमें सम्यग्ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अव्यक्त से लेकर स्थावरपर्यन्त समस्तभूतों में एक अवयवभाव अर्थात् आत्मवस्तु को देखता है तथा अलग-अलग शरीरों में अविभक्त आत्मतत्त्व को देखता है, वही सात्त्विकज्ञान-सम्यग्ज्ञान है। आचार्य शंकर ने भगवद्गीता के अट्ठारहवें अध्याय के 20वें श्लोक पर भाष्य करते हुए लिखा है- "तज्ज्ञानम् अद्वैतात्मदर्शनं सात्त्विकं सम्यग्दर्शनं विद्धि।" यहाँ आचार्य शंकर ने अद्वैत वेदान्त के अनुसार समस्त भूतों में एकत्व के दर्शन को सम्यग्दर्शन स्वीकार किया है। जैन दर्शन में समस्त प्राणियों के प्रति आत्मवद्भाव स्थापित करने के लिए 'आयतुले पयासु' जैसे वाक्यों का प्रयोग हुआ है तथा सब प्राणियों को अपने समान समझने पर ही सम्यग्दर्शन का लक्षण अनुकम्पा भाव' घटित होता है।
बौद्धदर्शन में निर्वाण-प्राप्ति के लिए प्रतिपादित आष्टांगिक मार्ग के अन्तर्गत 'सम्यक् दृष्टि' को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। सम्यक् दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति दुःख, दुःख के कारण, दुःख-निरोध एवं दुःख-निरोध के उपाय- इन चार आर्य सत्यों को सम्यक् रूपेण जानता है। उस पर उसकी श्रद्धा भी होती है। इस तरह बौद्धधर्म में भी दुःख-मुक्ति के उपाय में सम्यक् दृष्टि का महत्त्व अंगीकार किया गया है। न्याय आदि दर्शनों में तत्त्वज्ञान अथवा सम्यग्ज्ञान को महत्त्व दिया गया है, वे सम्यग्दर्शन की विशेष चर्चा नहीं करते। जैनदर्शन में इस बात पर बल दिया गया है कि ज्ञान की सम्यक्ता दृष्टि की सम्यक्ता पर निर्भर करती है। इसे जैनदर्शन का वैशिष्ट्य भी कहा जा सकता है।
यहाँ यह कथन समीचीन नहीं होगा कि जैनदर्शन या जैनधर्म का अनुयायी ही