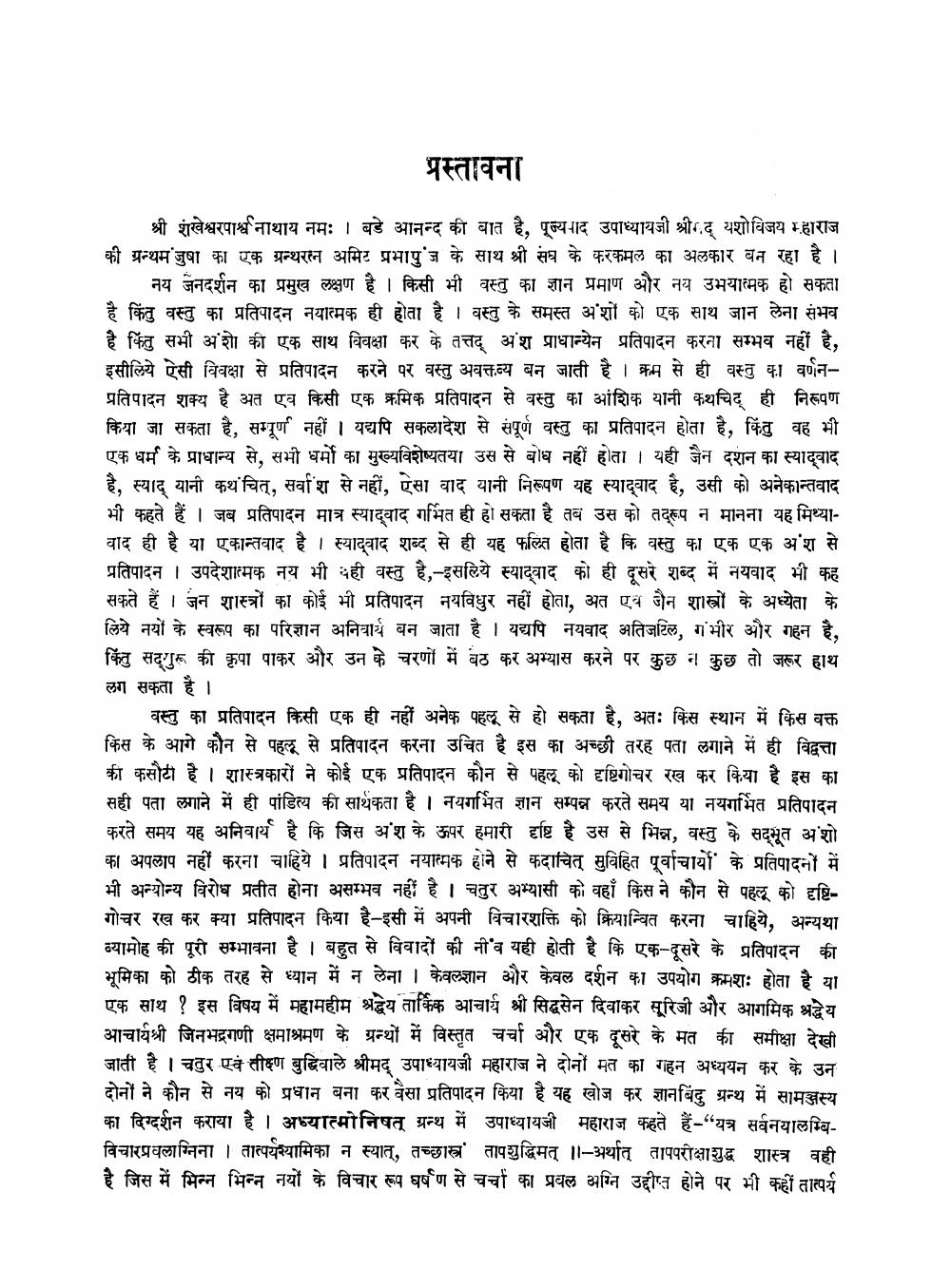________________
प्रस्तावना
श्री शंखेश्वरपार्श्वनाथाय नमः । बडे आनन्द की बात है, पूज्यनाद उपाध्यायजी श्री. द् यशोविजय म्हाराज साथ श्री संघ के करकमल का अलकार बन रहा है । वस्तु का ज्ञान प्रमाण और नय उभयात्मक हो सकता
की ग्रन्थमंजुषा का एक ग्रन्थरस्न अमिट प्रभापु ंज नय जनदर्शन का प्रमुख लक्षण है । किसी भी है किंतु वस्तु का प्रतिपादन नयात्मक ही होता है । वस्तु के समस्त अशों को एक साथ जान लेना संभव है किंतु सभी अंशो की एक साथ विवक्षा कर के तत्तद् अंश प्राधान्येन प्रतिपादन करना सम्भव नहीं है, इसीलिये ऐसी विवक्षा से प्रतिपादन करने पर वस्तु अवक्तव्य बन जाती है । क्रम से ही वस्तु का वर्णनप्रतिपादन शक्य है अत एव किसी एक क्रमिक प्रतिपादन से वस्तु का आंशिक यानी कथचिद् ही निरूपण किया जा सकता है, सम्पूर्ण नहीं । यद्यपि सकलादेश से संपूर्ण वस्तु का प्रतिपादन होता है, किंतु वह भी एक धर्म के प्राधान्य से, सभी धर्मो का मुख्यविशेष्यतया उस से बोध नहीं होता । यही जैन दर्शन का स्यादवाद है, स्याद् यानी कथंचित्, सर्वाश से नहीं, ऐसा वाद यानी निरूपण यह स्याद्वाद है, उसी को अनेकान्तवाद भी कहते हैं । जब प्रतिपादन मात्र स्याद्वाद गर्भित ही सकता है तब उस को तद्रूप न मानना यह मिथ्यावाद ही है या एकान्तवाद है । स्यादवाद शब्द से ही यह फलित होता है कि वस्तु का एक एक अंश से प्रतिपादन । उपदेशात्मक नय भी वही वस्तु है, इसलिये स्यादवाद को ही दूसरे शब्द में नयवाद भी कह सकते हैं । जन शास्त्रों का कोई भी प्रतिपादन नयविधुर नहीं होता, अत एव जैन शास्त्रों के अध्येता के लिये नयों के स्वरूप का परिज्ञान अनिवार्य बन जाता है । यद्यपि नयवाद अतिजटिल, गंभीर और गहन है, किंतु सद्गुरू की कृपा पाकर और उन के चरणों में बैठ कर अभ्यास करने पर कुछ न कुछ तो जरूर हाथ लग सकता है ।
वस्तु का प्रतिपादन किसी एक ही नहीं अनेक पहलू से हो सकता है, अतः किस स्थान में किस वक्त किस के आगे कौन से पहलू से प्रतिपादन करना उचित है इस का अच्छी तरह पता लगाने में ही विद्वत्ता की कसौटी है । शास्त्रकारों ने कोई एक प्रतिपादन कौन से पहलू को दृष्टिगोचर रख कर किया है इस का सही पता लगाने में ही पांडित्य की सार्थकता है । नयगर्भित ज्ञान सम्पन्न करते समय या नयगर्भित प्रतिपादन करते समय यह अनिवार्य है कि जिस अंश के ऊपर हमारी दृष्टि है उस से भिन्न, वस्तु के सद्भूत अशो का अपलाप नहीं करना चाहिये । प्रतिपादन नयात्मक होने से कदाचित् सुविहित पूर्वाचार्यों के प्रतिपादनों में भी अन्योन्य विरोध प्रतीत होना असम्भव नहीं है । चतुर अभ्यासी को वहाँ किस ने कौन से पहलू को दृष्टिगोचर रख कर क्या प्रतिपादन किया है - इसी में अपनी विचारशक्ति को क्रियान्वित करना चाहिये, अन्यथा व्यामोह की पूरी सम्भावना है । बहुत से विवादों की नींव यही होती है कि एक-दूसरे के प्रतिपादन की भूमिका को ठीक तरह से ध्यान में न लेना । केवलज्ञान और केवल दर्शन का उपयोग क्रमशः होता है या एक साथ ? इस विषय में महामहीम श्रद्धेय तार्किक आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरिजी और आगमिक श्रद्धेय आचार्यश्री जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण के ग्रन्थों में विस्तृत चर्चा और एक दूसरे के मत की समीक्षा देखी जाती है । चतुर एवं तीक्ष्ण बुद्धिवाले श्रीमद् उपाध्यायजी महाराज ने दोनों मत का गहन अध्ययन कर के उन दोनों ने कौन से नय को प्रधान बना कर वैसा प्रतिपादन किया है यह खोज कर ज्ञानबिंदु ग्रन्थ में सामञ्जस्य का दिग्दर्शन कराया है । अध्यात्मोनिषत् ग्रन्थ में उपाध्यायजी महाराज कहते हैं- "यत्र सर्वनयालम्बि - विचारप्रवाग्निना । तात्पर्यश्यामिका न स्यात्, तच्छास्त्र तापशुद्धिमत् ॥ अर्थात् तापपरीक्षा शुद्ध शास्त्र वही है जिस में भिन्न भिन्न नयों के विचार रूप घर्षण से चर्चा का प्रबल अग्नि उद्दीप्त होने पर भी कहीं तात्पर्य