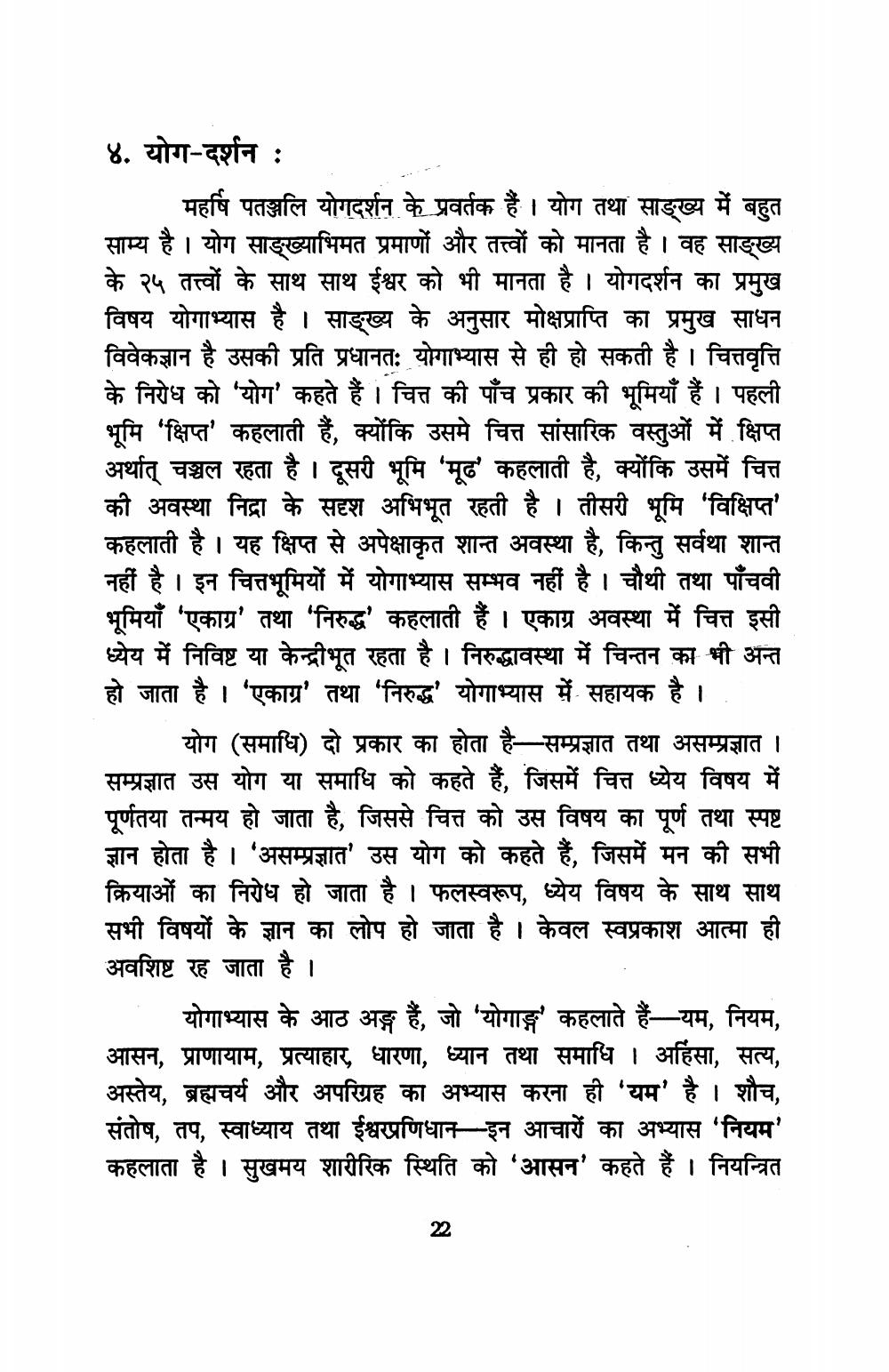________________
४. योग-दर्शन :
I
महर्षि पतञ्जलि योगदर्शन के प्रवर्तक हैं। योग तथा साङ्ख्य में बहुत साम्य है । योग साङ्ख्याभिमत प्रमाणों और तत्त्वों को मानता है । वह साङ्ख्य के २५ तत्त्वों के साथ साथ ईश्वर को भी मानता है । योगदर्शन का प्रमुख विषय योगाभ्यास है । साङ्ख्य के अनुसार मोक्षप्राप्ति का प्रमुख साधन विवेकज्ञान है उसकी प्रति प्रधानतः योगाभ्यास से ही हो सकती है । चित्तवृत्ति के निरोध को 'योग' कहते हैं । चित्त की पाँच प्रकार की भूमियाँ हैं । पहली भूमि 'क्षिप्त' कहलाती हैं, क्योंकि उसमे चित्त सांसारिक वस्तुओं में क्षिप्त अर्थात् चञ्चल रहता है । दूसरी भूमि 'मूढ' कहलाती है, क्योंकि उसमें चित्त की अवस्था निद्रा के सदृश अभिभूत रहती है । तीसरी भूमि 'विक्षिप्त' कहलाती है । यह क्षिप्त से अपेक्षाकृत शान्त अवस्था है, किन्तु सर्वथा शान्त नहीं है । इन चित्तभूमियों में योगाभ्यास सम्भव नहीं है । चौथी तथा पाँचवी भूमियाँ 'एकाग्र' तथा 'निरुद्ध' कहलाती हैं । एकाग्र अवस्था में चित्त इसी ध्येय में निविष्ट या केन्द्रीभूत रहता है । निरुद्धावस्था में चिन्तन का भी अन्त हो जाता है । 'एकाग्र' तथा 'निरुद्ध' योगाभ्यास में सहायक है ।
I
योग (समाधि) दो प्रकार का होता है— सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात । सम्प्रज्ञात उस योग या समाधि को कहते हैं, जिसमें चित्त ध्येय विषय में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, जिससे चित्त को उस विषय का पूर्ण तथा स्पष्ट ज्ञान होता है । 'असम्प्रज्ञात' उस योग को कहते हैं, जिसमें मन की सभी क्रियाओं का निरोध हो जाता है । फलस्वरूप, ध्येय विषय के साथ साथ सभी विषयों के ज्ञान का लोप हो जाता है । केवल स्वप्रकाश आत्मा ही अवशिष्ट रह जाता है ।
योगाभ्यास के आठ अङ्ग हैं, जो 'योगाङ्ग' कहलाते हैं — यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का अभ्यास करना ही 'यम' है । शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान—–इन आचारों का अभ्यास 'नियम' कहलाता है । सुखमय शारीरिक स्थिति को 'आसन' कहते हैं । नियन्त्रित
22