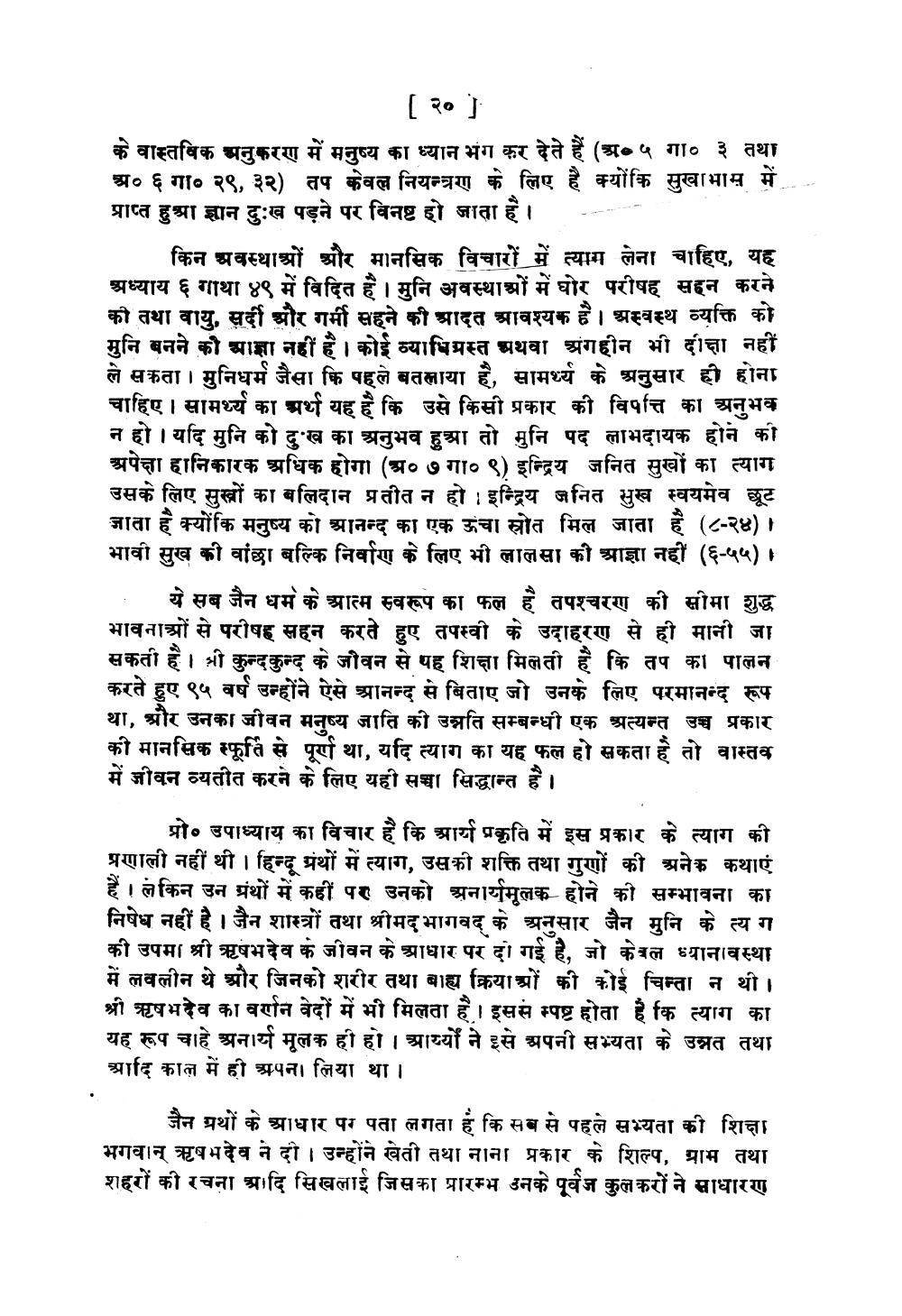________________
[२०] के वास्तविक अनुकरण में मनुष्य का ध्यान भंग कर देते हैं (अ.५ गा० ३ तथा अ० ६ गा० २९, ३२) तप केवल नियन्त्रण के लिए है क्योंकि सुखाभास में प्राप्त हुआ ज्ञान दुःख पड़ने पर विनष्ट हो जाता है।
किन अवस्थाओं और मानसिक विचारों में त्याग लेना चाहिए, यह अध्याय ६ गाथा ४९ में विदित है। मुनि अवस्थाओं में घोर परीषह सहन करने की तथा वायु, सर्दी और गर्मी सहने की आदत आवश्यक है। अस्वस्थ व्यक्ति को मुनि बनने की आज्ञा नहीं है। कोई व्याधिग्रस्त अथवा अंगहीन भी दीक्षा नहीं ले सकता। मुनिधर्म जैसा कि पहले बतलाया है, सामर्थ्य के अनुसार ही होना चाहिए । सामर्थ्य का अर्थ यह है कि उसे किसी प्रकार की विपत्ति का अनुभक न हो । यदि मुनि को दुःख का अनुभव हुआ तो मुनि पद लाभदायक होने की अपेक्षा हानिकारक अधिक होगा (अ०७ गा०९) इन्द्रिय जनित सुखों का त्याग उसके लिए सुखों का बलिदान प्रतीत न हो। इन्द्रिय जनित सुख स्वयमेव छूट जाता है क्योंकि मनुष्य को आनन्द का एक ऊंचा स्रोत मिल जाता है (८-२४)। भावी सुख की वांछा बल्कि निर्वाण के लिए भी लालसा की आज्ञा नहीं (६-५५) ।
ये सब जैन धर्म के आत्म स्वरूप का फल है तपश्चरण की सीमा शुद्ध भावनाओं से परीषह सहन करते हुए तपस्वी के उदाहरण से ही मानी जा सकती है। श्री कुन्दकुन्द के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि तप का पालन करते हुए ९५ वर्ष उन्होंने ऐसे आनन्द से बिताए जो उनके लिए परमानन्द रूप था, और उनका जीवन मनुष्य जाति की उन्नति सम्बन्धी एक अत्यन्त उच्च प्रकार की मानसिक स्फूर्ति से पूर्ण था, यदि त्याग का यह फल हो सकता है तो वास्तव में जीवन व्यतीत करने के लिए यही सच्चा सिद्धान्त है।
प्रो० उपाध्याय का विचार है कि आर्य प्रकृति में इस प्रकार के त्याग की प्रणाली नहीं थी। हिन्दू ग्रंथों में त्याग, उसकी शक्ति तथा गुणों की अनेक कथाएं हैं । लेकिन उन ग्रंथों में कहीं पर उनको अनार्यमूलक होने की सम्भावना का निषेध नहीं है । जैन शास्त्रों तथा श्रीमद भागवद् के अनुसार जैन मुनि के त्य ग की उपमा श्री ऋषभदेव के जीवन के आधार पर दो गई है, जो केवल ध्यानावस्था में लवलीन थे और जिनको शरीर तथा बाह्य क्रियाओं की कोई चिन्ता न थी। श्री ऋषभदेव का वर्णन वेदों में भी मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि त्याग का यह रूप चाहे अनार्य मूलक ही हो । आर्यों ने इसे अपनी सभ्यता के उन्नत तथा आदि काल में ही अपना लिया था।
जैन ग्रथों के आधार पर पता लगता है कि सब से पहले सभ्यता की शिक्षा भगवान ऋषभदेव ने दी। उन्होंने खेती तथा नाना प्रकार के शिल्प, ग्राम तथा शहरों की रचना आदि सिखलाई जिसका प्रारम्भ उनके पूर्वज कुल करों ने साधारण