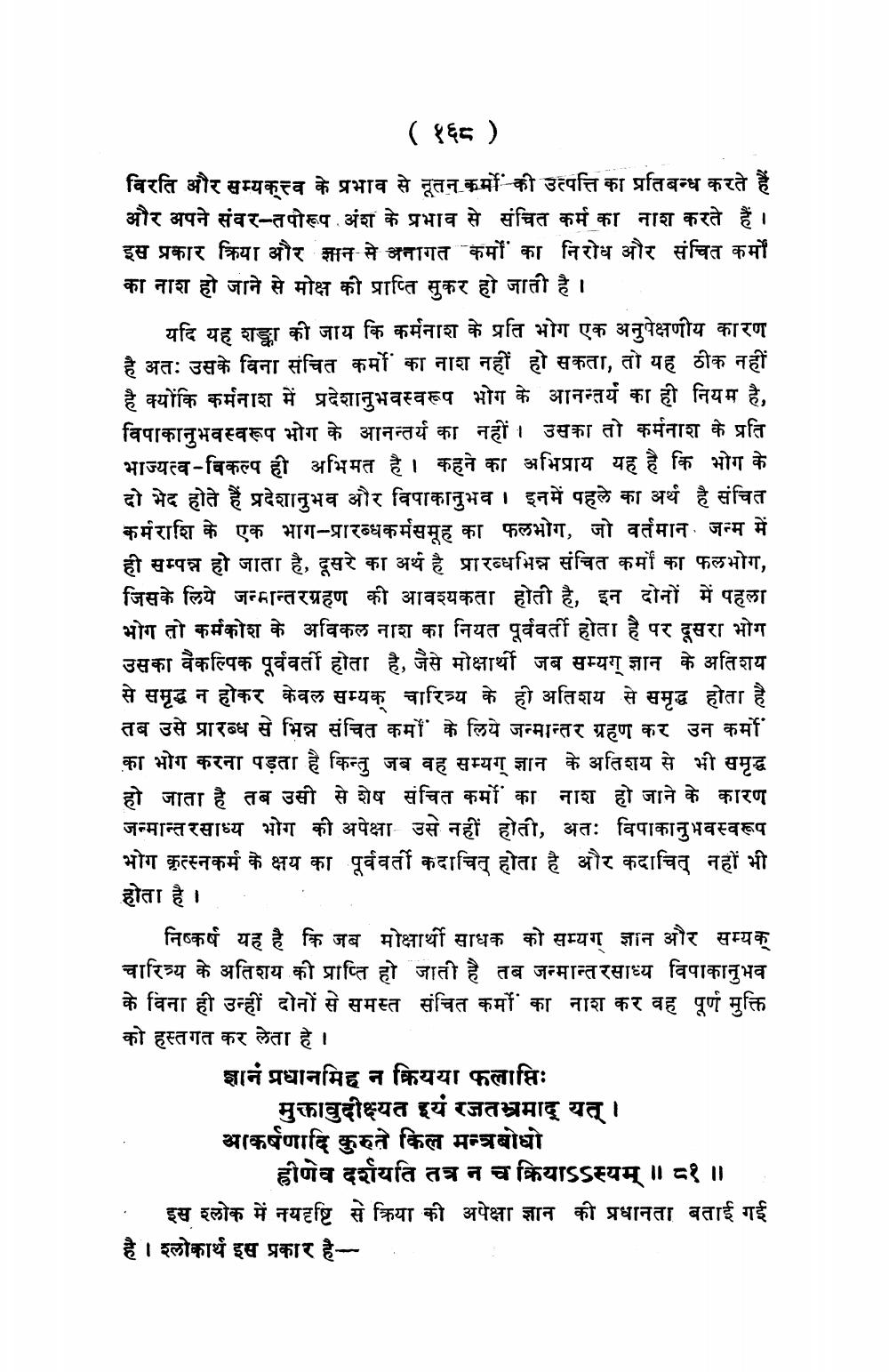________________
( १६८) विरति और सम्यक्त्व के प्रभाव से नूतन कर्मों की उत्पत्ति का प्रतिबन्ध करते हैं
और अपने संवर-तपोरूप अंश के प्रभाव से संचित कर्म का नाश करते हैं। इस प्रकार क्रिया और शान से अनागत कर्मों का निरोध और संचित कर्मों का नाश हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति सुकर हो जाती है ।
यदि यह शङ्का की जाय कि कर्मनाश के प्रति भोग एक अनुपेक्षणीय कारण है अतः उसके विना संचित कर्मों का नाश नहीं हो सकता, तो यह ठीक नहीं है क्योंकि कर्मनाश में प्रदेशानुभवस्वरूप भोग के आनन्तर्य का ही नियम है, विपाकानुभवस्वरूप भोग के आनन्तर्य का नहीं। उसका तो कर्मनाश के प्रति भाज्यत्व-विकल्प ही अभिमत है। कहने का अभिप्राय यह है कि भोग के दो भेद होते हैं प्रदेशानुभव और विपाकानुभव। इनमें पहले का अर्थ है संचित कर्मराशि के एक भाग-प्रारब्धकर्मसमूह का फलभोग, जो वर्तमान जन्म में ही सम्पन्न हो जाता है, दूसरे का अर्थ है प्रारब्धभिन्न संचित कर्मों का फलभोग, जिसके लिये जन्मान्तरग्रहण की आवश्यकता होती है, इन दोनों में पहला भोग तो कर्मकोश के अविकल नाश का नियत पूर्ववर्ती होता है पर दूसरा भोग उसका वैकल्पिक पूर्ववर्ती होता है, जैसे मोक्षार्थी जब सम्यग् ज्ञान के अतिशय से समृद्ध न होकर केवल सम्यक चारित्र्य के ही अतिशय से समृद्ध होता है तब उसे प्रारब्ध से भिन्न संचित कर्मों के लिये जन्मान्तर ग्रहण कर उन कर्मो का भोग करना पड़ता है किन्तु जब वह सम्यग् ज्ञान के अतिशय से भी समृद्ध हो जाता है तब उसी से शेष संचित कर्मों का नाश हो जाने के कारण जन्मान्तरसाध्य भोग की अपेक्षा उसे नहीं होती, अतः विपाकानुभवस्वरूप भोग कृत्स्नकर्म के क्षय का पूर्ववर्ती कदाचित् होता है और कदाचित् नहीं भी होता है।
निष्कर्ष यह है कि जब मोक्षार्थी साधक को सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य के अतिशय की प्राप्ति हो जाती है तब जन्मान्तरसाध्य विपाकानुभव के विना ही उन्हीं दोनों से समस्त संचित कर्मों का नाश कर वह पूर्ण मुक्ति को हस्तगत कर लेता है।
ज्ञानं प्रधानमिह न क्रियया फलाप्तिः
मुक्तावुदीक्ष्यत इयं रजतभ्रमाद् यत् । आकर्षणादि कुरुते किल मन्त्रबोधो
हीणेव दर्शयति तत्र न च क्रियाऽऽस्यम् ॥ ८१॥ इस श्लोक में नयदृष्टि से क्रिया की अपेक्षा ज्ञान की प्रधानता बताई गई है । श्लोकार्थ इस प्रकार है