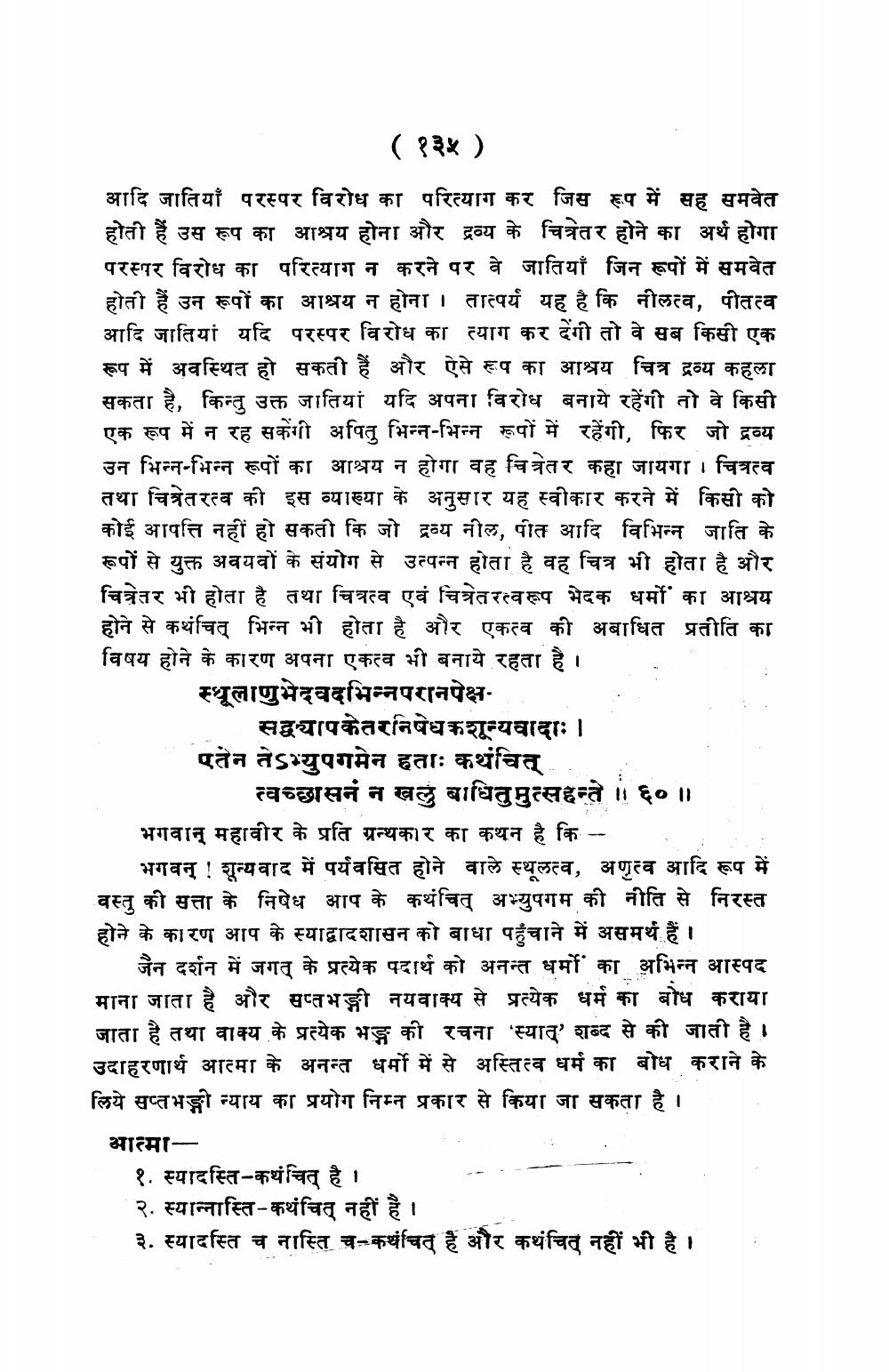________________
(१३५ )
आदि जातियाँ परस्पर विरोध का परित्याग कर जिस रूप में सह समवेत होती हैं उस रूप का आश्रय होना और द्रव्य के चित्रेतर होने का अर्थ होगा परस्पर विरोध का परित्याग न करने पर वे जातियाँ जिन रूपों में समवेत होती हैं उन रूपों का आश्रय न होना। तात्पर्य यह है कि नीलत्व, पीतत्व आदि जातियां यदि परस्पर विरोध का त्याग कर देंगी तो वे सब किसी एक रूप में अवस्थित हो सकती हैं और ऐसे रूप का आश्रय चित्र द्रव्य कहला सकता है, किन्तु उक्त जातियां यदि अपना विरोध बनाये रहेंगी तो वे किसी एक रूप में न रह सकेंगी अपितु भिन्न-भिन्न रूपों में रहेंगी, फिर जो द्रव्य उन भिन्न-भिन्न रूपों का आश्रय न होगा वह चित्रेतर कहा जायगा । चित्रत्व तथा चित्रेतरत्व की इस व्याख्या के अनुसार यह स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि जो द्रव्य नील, पीत आदि विभिन्न जाति के रूपों से युक्त अवयवों के संयोग से उत्पन्न होता है वह चित्र भी होता है और चित्रेतर भी होता है तथा चित्रत्व एवं चित्रेतरत्वरूप भेदक धर्मों का आश्रय होने से कथंचित् भिन्न भी होता है और एकत्व की अबाधित प्रतीति का विषय होने के कारण अपना एकत्व भी बनाये रहता है।
स्थूलाणुभेदवदभिन्नपरानपेक्ष.
सयापकेतरनिषेधकशून्यवादाः । एतेन तेऽभ्युपगमेन हताः कथंचित्
त्वच्छासनं न खलु बाधितुमुत्सहन्ते ।। ६०॥ भगवान् महावीर के प्रति ग्रन्थकार का कथन है कि -
भगवन् ! शून्यवाद में पर्यवसित होने वाले स्थूलत्व, अतृत्व आदि रूप में वस्तु की सत्ता के निषेध आप के कथंचित् अभ्युपगम की नीति से निरस्त होने के कारण आप के स्याद्वादशासन को बाधा पहुंचाने में असमर्थ हैं।
जैन दर्शन में जगत् के प्रत्येक पदार्थ को अनन्त धर्मो का अभिन्न आस्पद माना जाता है और सप्तभङ्गी नयवाक्य से प्रत्येक धर्म का बोध कराया जाता है तथा वाक्य के प्रत्येक भङ्ग की रचना 'स्यात्' शब्द से की जाती है। उदाहरणार्थ आत्मा के अनन्त धर्मों में से अस्तित्व धर्म का बोध कराने के लिये सप्तभङ्गी न्याय का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है । आत्मा१. स्यादस्ति-कथंचित् है । २. स्यान्नास्ति-कथंचित् नहीं है । ३. स्यादस्ति च नास्ति च-कचित् है और कथंचित् नहीं भी है।