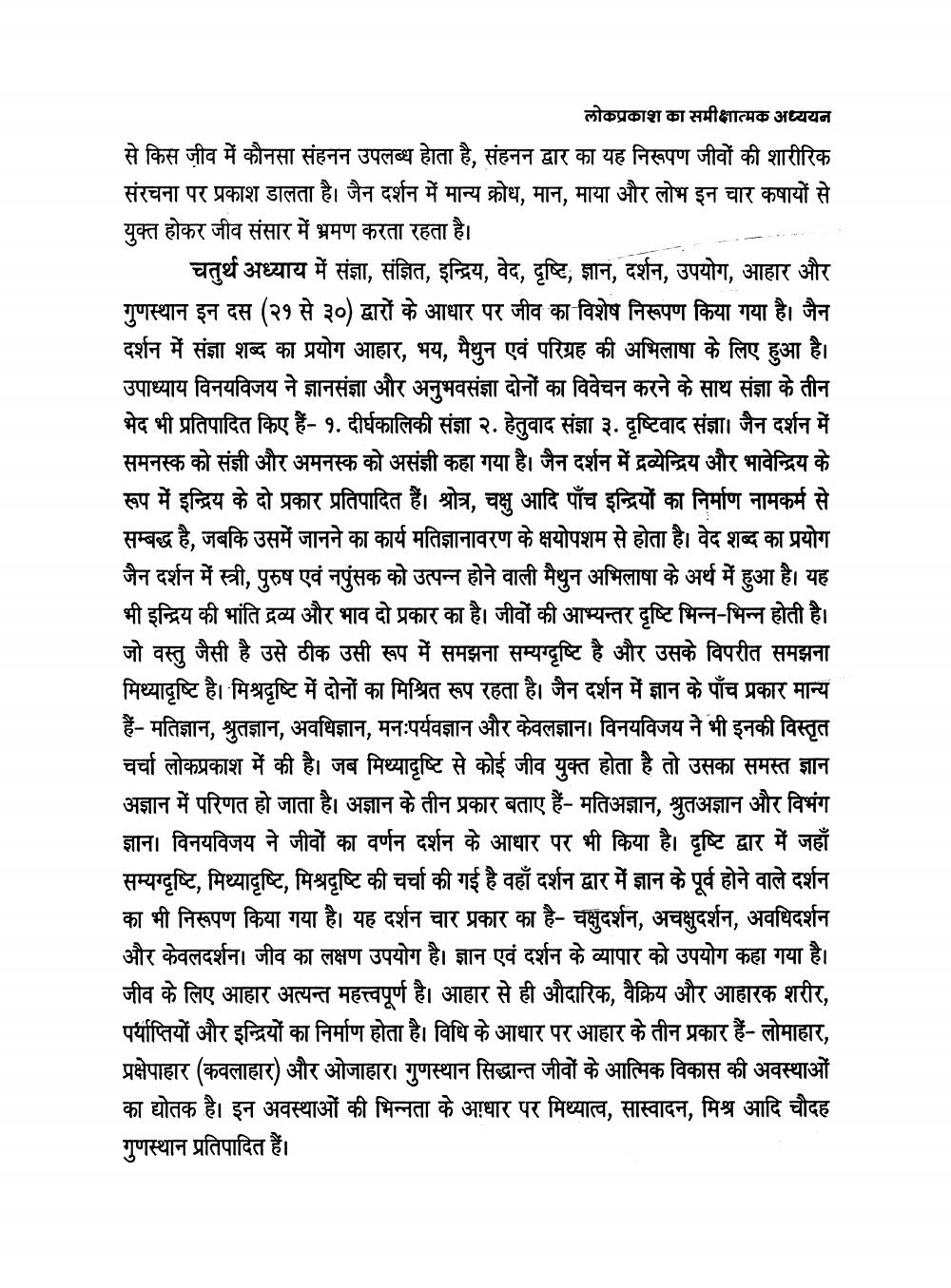________________
लोकप्रकाश का समीक्षात्मक अध्ययन से किस जीव में कौनसा संहनन उपलब्ध होता है, संहनन द्वार का यह निरूपण जीवों की शारीरिक संरचना पर प्रकाश डालता है। जैन दर्शन में मान्य क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायों से युक्त होकर जीव संसार में भ्रमण करता रहता है।
चतुर्थ अध्याय में संज्ञा, संज्ञित, इन्द्रिय, वेद, दृष्टि, ज्ञान, दर्शन, उपयोग, आहार और गुणस्थान इन दस (२१ से ३०) द्वारों के आधार पर जीव का विशेष निरूपण किया गया है। जैन दर्शन में संज्ञा शब्द का प्रयोग आहार, भय, मैथुन एवं परिग्रह की अभिलाषा के लिए हुआ है। उपाध्याय विनयविजय ने ज्ञानसंज्ञा और अनुभवसंज्ञा दोनों का विवेचन करने के साथ संज्ञा के तीन भेद भी प्रतिपादित किए हैं- १. दीर्घकालिकी संज्ञा २. हेतुवाद संज्ञा ३. दृष्टिवाद संज्ञा। जैन दर्शन में समनस्क को संज्ञी और अमनस्क को असंज्ञी कहा गया है। जैन दर्शन में द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय के रूप में इन्द्रिय के दो प्रकार प्रतिपादित हैं। श्रोत्र, चक्षु आदि पाँच इन्द्रियों का निर्माण नामकर्म से सम्बद्ध है, जबकि उसमें जानने का कार्य मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। वेद शब्द का प्रयोग जैन दर्शन में स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक को उत्पन्न होने वाली मैथुन अभिलाषा के अर्थ में हुआ है। यह भी इन्द्रिय की भांति द्रव्य और भाव दो प्रकार का है। जीवों की आभ्यन्तर दृष्टि भिन्न-भिन्न होती है। जो वस्तु जैसी है उसे ठीक उसी रूप में समझना सम्यग्दृष्टि है और उसके विपरीत समझना मिथ्यादृष्टि है। मिश्रदृष्टि में दोनों का मिश्रित रूप रहता है। जैन दर्शन में ज्ञान के पाँच प्रकार मान्य हैं- मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान। विनयविजय ने भी इनकी विस्तृत चर्चा लोकप्रकाश में की है। जब मिथ्यादृष्टि से कोई जीव युक्त होता है तो उसका समस्त ज्ञान अज्ञान में परिणत हो जाता है। अज्ञान के तीन प्रकार बताए हैं- मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान और विभंग ज्ञान। विनयविजय ने जीवों का वर्णन दर्शन के आधार पर भी किया है। दृष्टि द्वार में जहाँ सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, मिश्रदृष्टि की चर्चा की गई है वहाँ दर्शन द्वार में ज्ञान के पूर्व होने वाले दर्शन का भी निरूपण किया गया है। यह दर्शन चार प्रकार का है- चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन। जीव का लक्षण उपयोग है। ज्ञान एवं दर्शन के व्यापार को उपयोग कहा गया है। जीव के लिए आहार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। आहार से ही औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर, पर्याप्तियों और इन्द्रियों का निर्माण होता है। विधि के आधार पर आहार के तीन प्रकार हैं- लोमाहार, प्रक्षेपाहार (कवलाहार) और ओजाहार। गुणस्थान सिद्धान्त जीवों के आत्मिक विकास की अवस्थाओं का द्योतक है। इन अवस्थाओं की भिन्नता के आधार पर मिथ्यात्व, सास्वादन, मिश्र आदि चौदह गुणस्थान प्रतिपादित हैं।