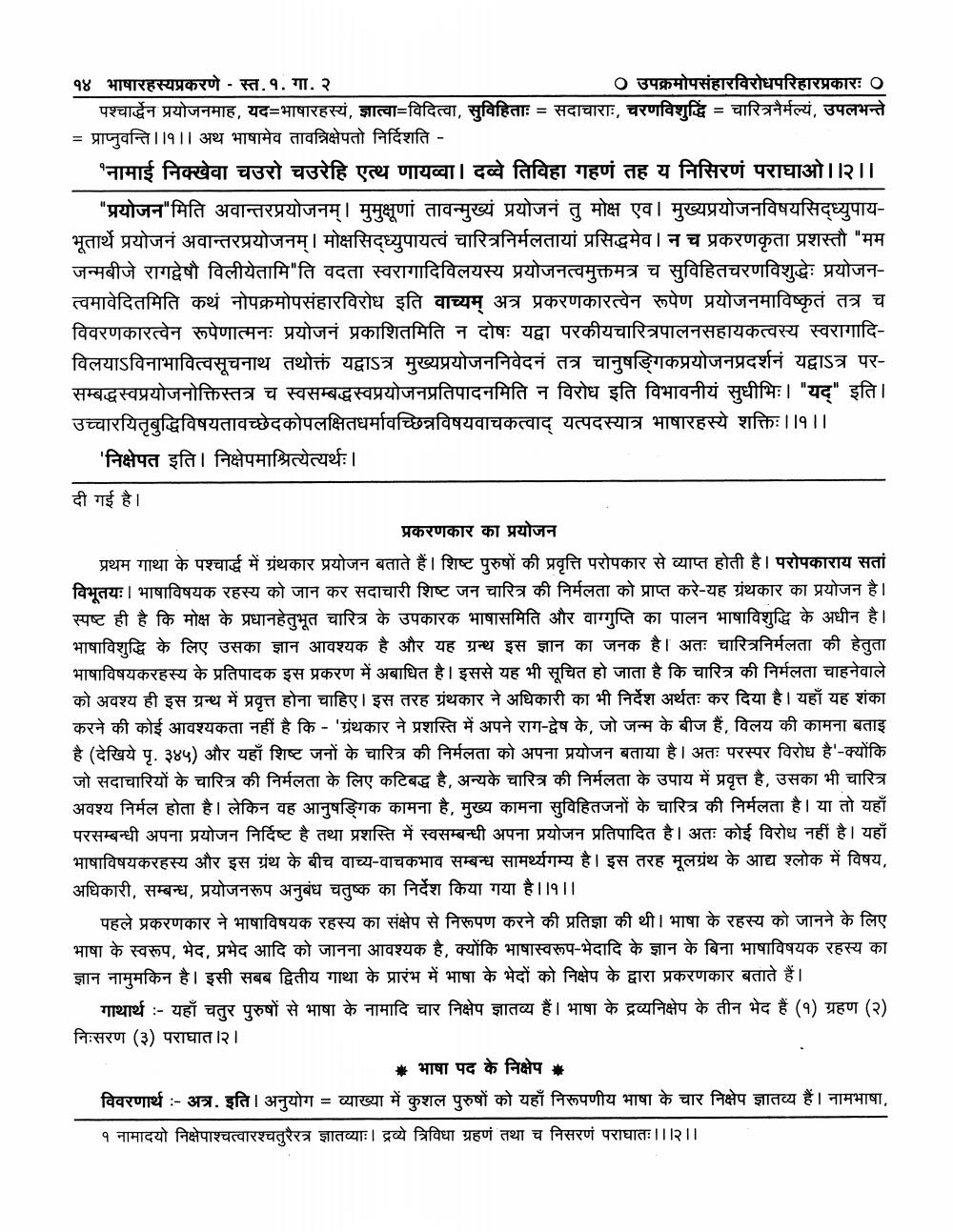________________
१४ भाषारहस्यप्रकरणे - स्त.१. गा. २
० उपक्रमोपसंहारविरोधपरिहारप्रकार: ० पश्चार्द्धन प्रयोजनमाह, यद=भाषारहस्यं, ज्ञात्वा विदित्वा, सुविहिताः = सदाचाराः, चरणविशुद्धिं = चारित्रनैर्मल्यं, उपलभन्ते = प्राप्नुवन्ति ।।१।। अथ भाषामेव तावन्निक्षेपतो निर्दिशति -
'नामाई निक्खेवा चउरो चउरेहि एत्थ णायव्वा। दब्वे तिविहा गहणं तह य निसिरणं पराघाओ।।२।।
"प्रयोजन"मिति अवान्तरप्रयोजनम् । मुमुक्षूणां तावन्मुख्यं प्रयोजनं तु मोक्ष एव । मुख्यप्रयोजनविषयसिद्ध्युपायभूतार्थे प्रयोजनं अवान्तरप्रयोजनम् । मोक्षसिदध्युपायत्वं चारित्रनिर्मलतायां प्रसिद्धमेव । न च प्रकरणकृता प्रशस्तौ "मम जन्मबीजे रागद्वेषौ विलीयेतामि"ति वदता स्वरागादिविलयस्य प्रयोजनत्वमुक्तमत्र च सुविहितचरणविशुद्धेः प्रयोजनत्वमावेदितमिति कथं नोपक्रमोपसंहारविरोध इति वाच्यम् अत्र प्रकरणकारत्वेन रूपेण प्रयोजनमाविष्कृतं तत्र च विवरणकारत्वेन रूपेणात्मनः प्रयोजनं प्रकाशितमिति न दोषः यद्वा परकीयचारित्रपालनसहायकत्वस्य स्वरागादिविलयाऽविनाभावित्वसूचनाथ तथोक्तं यद्वाऽत्र मुख्यप्रयोजननिवेदनं तत्र चानुषङ्गिकप्रयोजनप्रदर्शनं यद्वाऽत्र परसम्बद्धस्वप्रयोजनोक्तिस्तत्र च स्वसम्बद्धस्वप्रयोजनप्रतिपादनमिति न विरोध इति विभावनीयं सुधीभिः | "यद" इति। उच्चारयितबुद्धिविषयतावच्छेदकोपलक्षितधर्मावच्छिन्नविषयवाचकत्वाद् यत्पदस्यात्र भाषारहस्ये शक्तिः ।।१।।
'निक्षेपत इति। निक्षेपमाश्रित्येत्यर्थः । दी गई है।
प्रकरणकार का प्रयोजन प्रथम गाथा के पश्चार्द्ध में ग्रंथकार प्रयोजन बताते हैं। शिष्ट पुरुषों की प्रवृत्ति परोपकार से व्याप्त होती है। परोपकाराय सतां विभूतयः । भाषाविषयक रहस्य को जान कर सदाचारी शिष्ट जन चारित्र की निर्मलता को प्राप्त करे-यह ग्रंथकार का प्रयोजन है। स्पष्ट ही है कि मोक्ष के प्रधानहेतुभूत चारित्र के उपकारक भाषासमिति और वाग्गुप्ति का पालन भाषाविशुद्धि के अधीन है। भाषाविशुद्धि के लिए उसका ज्ञान आवश्यक है और यह ग्रन्थ इस ज्ञान का जनक है। अतः चारित्रनिर्मलता की हेतुता भाषाविषयकरहस्य के प्रतिपादक इस प्रकरण में अबाधित है। इससे यह भी सूचित हो जाता है कि चारित्र की निर्मलता चाहनेवाले को अवश्य ही इस ग्रन्थ में प्रवृत्त होना चाहिए। इस तरह ग्रंथकार ने अधिकारी का भी निर्देश अर्थतः कर दिया है। यहाँ यह शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि - 'ग्रंथकार ने प्रशस्ति में अपने राग-द्वेष के, जो जन्म के बीज हैं, विलय की कामना बताइ है (देखिये पृ. ३४५) और यहाँ शिष्ट जनों के चारित्र की निर्मलता को अपना प्रयोजन बताया है। अतः परस्पर विरोध है'-क्योंकि जो सदाचारियों के चारित्र की निर्मलता के लिए कटिबद्ध है, अन्यके चारित्र की निर्मलता के उपाय में प्रवृत्त है, उसका भी चारित्र अवश्य निर्मल होता है। लेकिन वह आनुषङ्गिक कामना है, मुख्य कामना सुविहितजनों के चारित्र की निर्मलता है। या तो यहाँ परसम्बन्धी अपना प्रयोजन निर्दिष्ट है तथा प्रशस्ति में स्वसम्बन्धी अपना प्रयोजन प्रतिपादित है। अतः कोई विरोध नहीं है। यहाँ भाषाविषयकरहस्य और इस ग्रंथ के बीच वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध सामर्थ्यगम्य है। इस तरह मूलग्रंथ के आद्य श्लोक में विषय, अधिकारी, सम्बन्ध, प्रयोजनरूप अनुबंध चतुष्क का निर्देश किया गया है।।१।।
पहले प्रकरणकार ने भाषाविषयक रहस्य का संक्षेप से निरूपण करने की प्रतिज्ञा की थी। भाषा के रहस्य को जानने के लिए भाषा के स्वरूप, भेद, प्रभेद आदि को जानना आवश्यक है, क्योंकि भाषास्वरूप-भेदादि के ज्ञान के बिना भाषाविषयक रहस्य का ज्ञान नामुमकिन है। इसी सबब द्वितीय गाथा के प्रारंभ में भाषा के भेदों को निक्षेप के द्वारा प्रकरणकार बताते हैं। __गाथार्थ :- यहाँ चतुर पुरुषों से भाषा के नामादि चार निक्षेप ज्ञातव्य हैं। भाषा के द्रव्यनिक्षेप के तीन भेद हैं (१) ग्रहण (२) निःसरण (३) पराघात ।।
* भाषा पद के निक्षेप * विवरणार्थ :- अत्र. इति । अनुयोग = व्याख्या में कुशल पुरुषों को यहाँ निरूपणीय भाषा के चार निक्षेप ज्ञातव्य हैं। नामभाषा, १ नामादयो निक्षेपाश्चत्वारश्चतुरैरत्र ज्ञातव्याः। द्रव्ये त्रिविधा ग्रहणं तथा च निसरणं पराघातः ।।।२।।