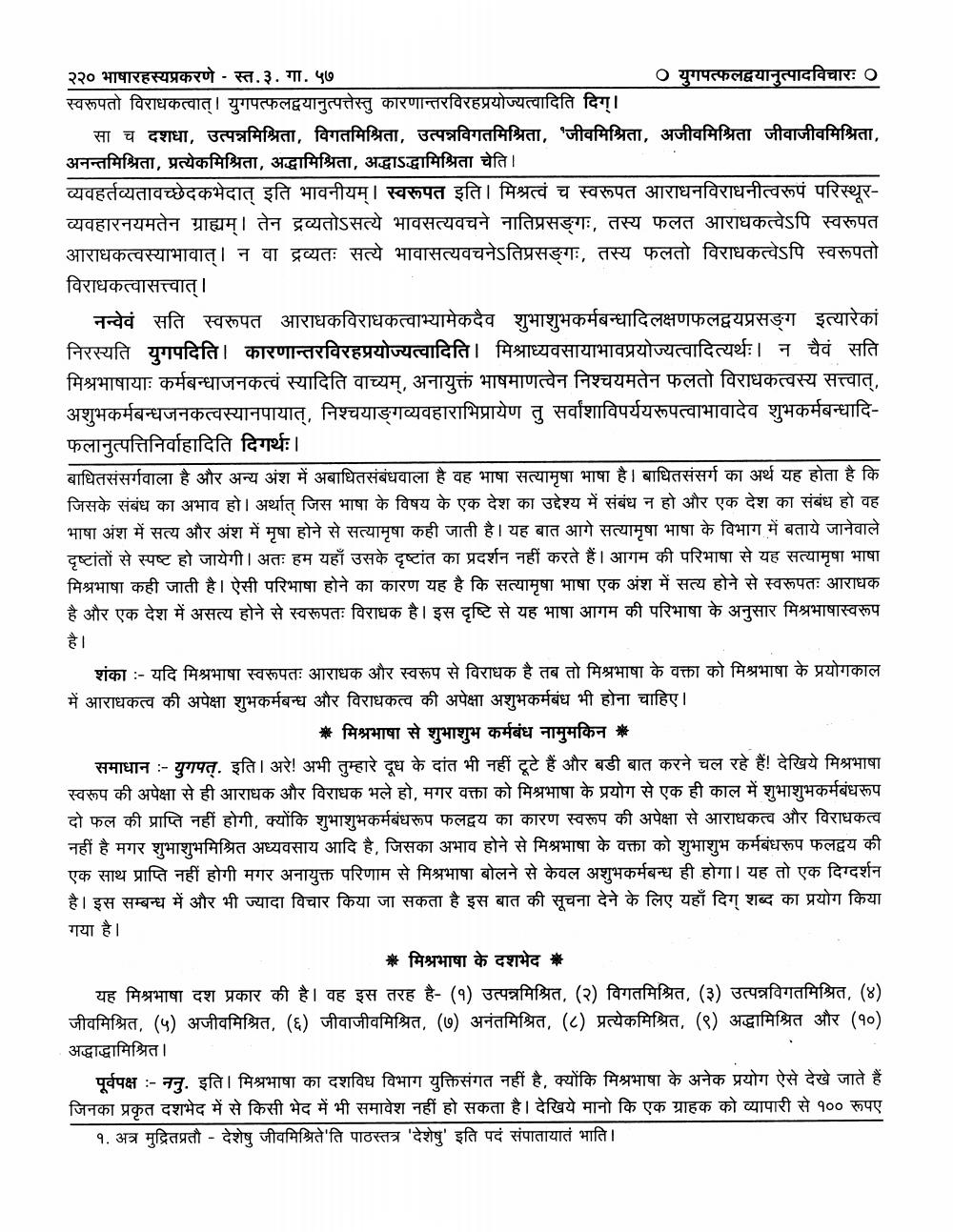________________
२२० भाषारहस्यप्रकरणे - स्त.३. गा. ५७
० युगपत्फलद्वयानुत्पादविचारः ० स्वरूपतो विराधकत्वात्। युगपत्फलद्वयानुत्पत्तेस्तु कारणान्तरविरहप्रयोज्यत्वादिति दिग्।
सा च दशधा, उत्पन्नमिश्रिता, विगतमिश्रिता, उत्पन्नविगतमिश्रिता, 'जीवमिश्रिता, अजीवमिश्रिता जीवाजीवमिश्रिता, अनन्तमिश्रिता, प्रत्येकमिश्रिता, अद्धामिश्रिता, अद्धाऽद्धामिश्रिता चेति। व्यवहर्तव्यतावच्छेदकभेदात इति भावनीयम्। स्वरूपत इति। मिश्रत्वं च स्वरूपत आराधनविराधनीत्वरूपं परिस्थूरव्यवहारनयमतेन ग्राह्यम्। तेन द्रव्यतोऽसत्ये भावसत्यवचने नातिप्रसङ्गः, तस्य फलत आराधकत्वेऽपि स्वरूपत आराधकत्वस्याभावात्। न वा द्रव्यतः सत्ये भावासत्यवचनेऽतिप्रसङ्गः, तस्य फलतो विराधकत्वेऽपि स्वरूपतो विराधकत्वासत्त्वात्।
नन्वेवं सति स्वरूपत आराधकविराधकत्वाभ्यामेकदैव शुभाशुभकर्मबन्धादिलक्षणफलद्वयप्रसङ्ग इत्यारेका निरस्यति युगपदिति। कारणान्तरविरहप्रयोज्यत्वादिति। मिश्राध्यवसायाभावप्रयोज्यत्वादित्यर्थः। न चैवं सति मिश्रभाषायाः कर्मबन्धाजनकत्वं स्यादिति वाच्यम्, अनायुक्तं भाषमाणत्वेन निश्चयमतेन फलतो विराधकत्वस्य सत्त्वात्, अशुभकर्मबन्धजनकत्वस्यानपायात्, निश्चयाङ्गव्यवहाराभिप्रायेण तु सर्वांशाविपर्ययरूपत्वाभावादेव शुभकर्मबन्धादिफलानुत्पत्तिनिर्वाहादिति दिगर्थः । बाधितसंसर्गवाला है और अन्य अंश में अबाधितसंबंधवाला है वह भाषा सत्यामृषा भाषा है। बाधितसंसर्ग का अर्थ यह होता है कि जिसके संबंध का अभाव हो। अर्थात् जिस भाषा के विषय के एक देश का उद्देश्य में संबंध न हो और एक देश का संबंध हो वह भाषा अंश में सत्य और अंश में मृषा होने से सत्यामृषा कही जाती है। यह बात आगे सत्यामृषा भाषा के विभाग में बताये जानेवाले दृष्टांतों से स्पष्ट हो जायेगी। अतः हम यहाँ उसके दृष्टांत का प्रदर्शन नहीं करते हैं। आगम की परिभाषा से यह सत्यामृषा भाषा मिश्रभाषा कही जाती है। ऐसी परिभाषा होने का कारण यह है कि सत्यामृषा भाषा एक अंश में सत्य होने से स्वरूपतः आराधक है और एक देश में असत्य होने से स्वरूपतः विराधक है। इस दृष्टि से यह भाषा आगम की परिभाषा के अनुसार मिश्रभाषास्वरूप
शंका :- यदि मिश्रभाषा स्वरूपतः आराधक और स्वरूप से विराधक है तब तो मिश्रभाषा के वक्ता को मिश्रभाषा के प्रयोगकाल में आराधकत्व की अपेक्षा शुभकर्मबन्ध और विराधकत्व की अपेक्षा अशुभकर्मबंध भी होना चाहिए।
* मिश्रभाषा से शुभाशुभ कर्मबंध नामुमकिन * समाधान :- युगपत्, इति । अरे! अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और बडी बात करने चल रहे हैं! देखिये मिश्रभाषा स्वरूप की अपेक्षा से ही आराधक और विराधक भले हो, मगर वक्ता को मिश्रभाषा के प्रयोग से एक ही काल में शुभाशुभकर्मबंधरूप दो फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि शुभाशुभकर्मबंधरूप फलद्वय का कारण स्वरूप की अपेक्षा से आराधकत्व और विराधकत्व नहीं है मगर शुभाशुभमिश्रित अध्यवसाय आदि है, जिसका अभाव होने से मिश्रभाषा के वक्ता को शुभाशुभ कर्मबंधरूप फलद्वय की एक साथ प्राप्ति नहीं होगी मगर अनायुक्त परिणाम से मिश्रभाषा बोलने से केवल अशुभकर्मबन्ध ही होगा। यह तो एक दिग्दर्शन है। इस सम्बन्ध में और भी ज्यादा विचार किया जा सकता है इस बात की सूचना देने के लिए यहाँ दिग् शब्द का प्रयोग किया गया है।
* मिश्रभाषा के दशभेद * यह मिश्रभाषा दश प्रकार की है। वह इस तरह है- (१) उत्पन्नमिश्रित, (२) विगतमिश्रित, (३) उत्पन्नविगतमिश्रित, (४) जीवमिश्रित, (५) अजीवमिश्रित, (६) जीवाजीवमिश्रित, (७) अनंतमिश्रित, (८) प्रत्येकमिश्रित, (९) अद्धामिश्रित और (१०) अद्धाद्धामिश्रित।
पूर्वपक्ष :- ननु. इति। मिश्रभाषा का दशविध विभाग युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि मिश्रभाषा के अनेक प्रयोग ऐसे देखे जाते हैं जिनका प्रकृत दशभेद में से किसी भेद में भी समावेश नहीं हो सकता है। देखिये मानो कि एक ग्राहक को व्यापारी से १०० रूपए
१. अत्र मुद्रितप्रतौ - देशेषु जीवमिश्रिते'ति पाठस्तत्र 'देशेषु' इति पदं संपातायातं भाति।