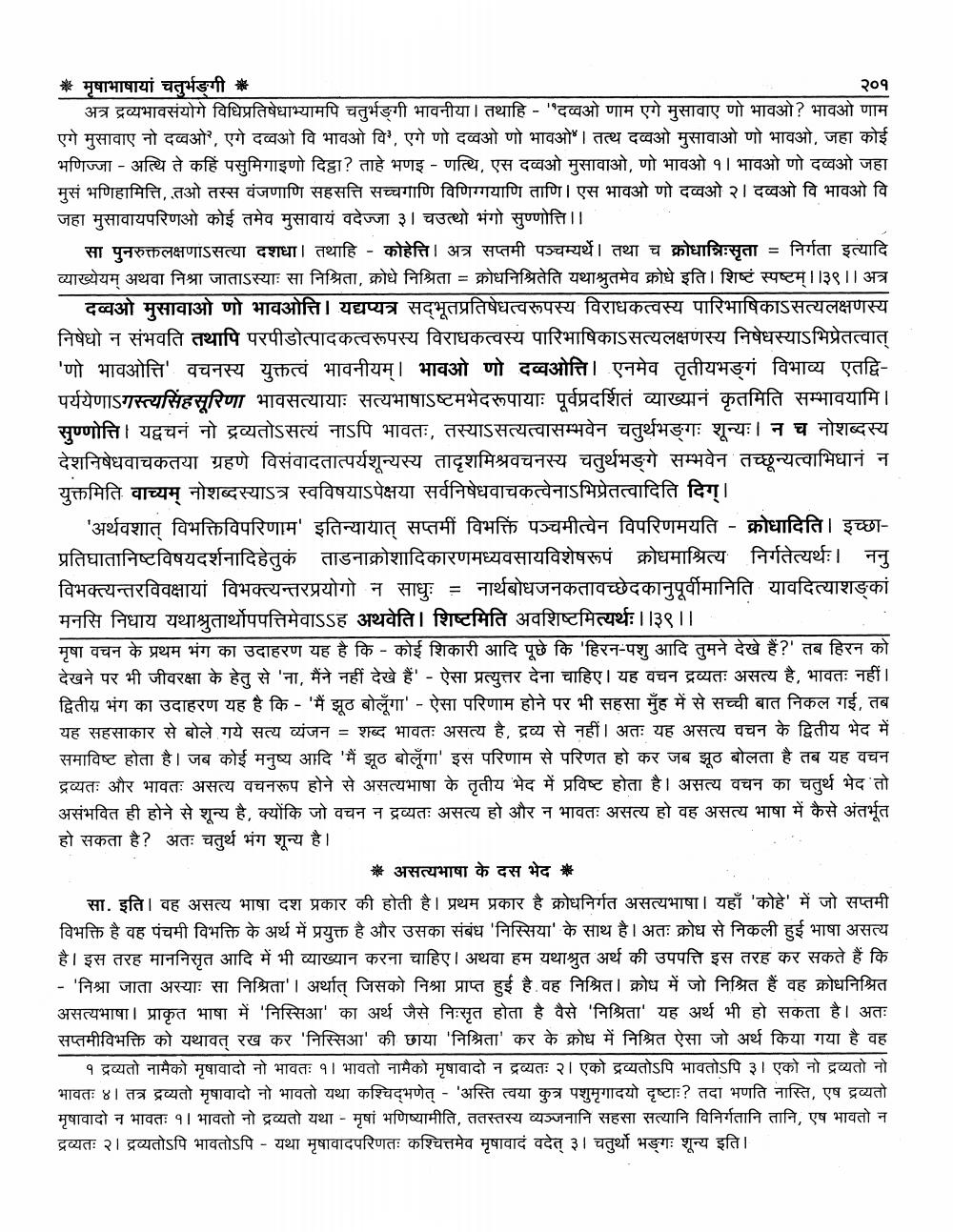________________
* मृषाभाषायां चतुर्भङगी *
२०१ अत्र द्रव्यभावसंयोगे विधिप्रतिषेधाभ्यामपि चतुर्भङ्गी भावनीया । तथाहि - "दव्वओ णाम एगे मुसावाए णो भावओ? भावओ णाम एगे मुसावाए नो दव्वओ, एगे दव्वओ वि भावओ वि', एगे णो दव्वओ णो भावओ । तत्थ दव्वओ मुसावाओ णो भावओ, जहा कोई भणिज्जा - अत्थि ते कहिं पसुमिगाइणो दिट्ठा? ताहे भणइ - णत्थि, एस दव्वओ मुसावाओ, णो भावओ १। भावओ णो दव्वओ जहा मुसं भणिहामित्ति, तओ तस्स वंजणाणि सहसत्ति सच्चगाणि विणिग्गयाणि ताणि । एस भावओ णो दव्वओ २। दव्वओ वि भावओ वि जहा मुसावायपरिणओ कोई तमेव मुसावायं वदेज्जा ३। चउत्थो भंगो सुण्णोत्ति।। ___सा पुनरुक्तलक्षणाऽसत्या दशधा। तथाहि - कोहेत्ति। अत्र सप्तमी पञ्चम्यर्थे । तथा च क्रोधान्निःसृता = निर्गता इत्यादि व्याख्येयम् अथवा निश्रा जाताऽस्याः सा निश्रिता, क्रोधे निश्रिता = क्रोधनिश्रितेति यथाश्रुतमेव क्रोधे इति। शिष्टं स्पष्टम् ।।३९ ।। अत्र
दबओ मुसावाओ णो भावओत्ति। यद्यप्यत्र सद्भूतप्रतिषेधत्वरूपस्य विराधकत्वस्य पारिभाषिकाऽसत्यलक्षणस्य निषेधो न संभवति तथापि परपीडोत्पादकत्वरूपस्य विराधकत्वस्य पारिभाषिकाऽसत्यलक्षणस्य निषेधस्याऽभिप्रेतत्वात् 'णो भावओत्ति' वचनस्य युक्तत्वं भावनीयम्। भावओ णो दव्वओत्ति। एनमेव तृतीयभङ्ग विभाव्य एतद्विपर्ययेणाऽगस्त्यसिंहसूरिणा भावसत्यायाः सत्यभाषाऽष्टमभेदरूपायाः पूर्वप्रदर्शितं व्याख्यानं कृतमिति सम्भावयामि । सुण्णोत्ति। यद्वचनं नो द्रव्यतोऽसत्यं नाऽपि भावतः, तस्याऽसत्यत्वासम्भवेन चतुर्थभङ्गः शून्यः । न च नोशब्दस्य देशनिषेधवाचकतया ग्रहणे विसंवादतात्पर्यशून्यस्य तादृशमिश्रवचनस्य चतुर्थभङ्गे सम्भवेन तच्छून्यत्वाभिधानं न युक्तमिति वाच्यम् नोशब्दस्याऽत्र स्वविषयाऽपेक्षया सर्वनिषेधवाचकत्वेनाऽभिप्रेतत्वादिति दिग्।
'अर्थवशात विभक्तिविपरिणाम' इतिन्यायात सप्तमी विभक्तिं पञ्चमीत्वेन विपरिणमयति - क्रोधादिति। इच्छाप्रतिघातानिष्टविषयदर्शनादिहेतुकं ताडनाक्रोशादिकारणमध्यवसायविशेषरूपं क्रोधमाश्रित्य निर्गतेत्यर्थः। ननु विभक्त्यन्तरविवक्षायां विभक्त्यन्तरप्रयोगो न साधुः = नार्थबोधजनकतावच्छेदकानुपूर्वीमानिति यावदित्याशङ्कां मनसि निधाय यथाश्रुतार्थोपपत्तिमेवाऽऽह अथवेति। शिष्टमिति अवशिष्टमित्यर्थः । ।३९ ।। मृषा वचन के प्रथम भंग का उदाहरण यह है कि - कोई शिकारी आदि पूछे कि 'हिरन-पशु आदि तुमने देखे हैं?' तब हिरन को देखने पर भी जीवरक्षा के हेतु से 'ना, मैंने नहीं देखे हैं' - ऐसा प्रत्युत्तर देना चाहिए। यह वचन द्रव्यतः असत्य है, भावतः नहीं। द्वितीय भंग का उदाहरण यह है कि - 'मैं झूठ बोलूँगा' - ऐसा परिणाम होने पर भी सहसा मुँह में से सच्ची बात निकल गई, तब यह सहसाकार से बोले गये सत्य व्यंजन = शब्द भावतः असत्य है, द्रव्य से नहीं। अतः यह असत्य वचन के द्वितीय भेद में समाविष्ट होता है। जब कोई मनुष्य आदि 'मैं झूठ बोलूँगा' इस परिणाम से परिणत हो कर जब झूठ बोलता है तब यह वचन द्रव्यतः और भावतः असत्य वचनरूप होने से असत्यभाषा के तृतीय भेद में प्रविष्ट होता है। असत्य वचन का चतुर्थ भेद तो असंभवित ही होने से शून्य है, क्योंकि जो वचन न द्रव्यतः असत्य हो और न भावतः असत्य हो वह असत्य भाषा में कैसे अंतर्भूत हो सकता है? अतः चतुर्थ भंग शून्य है।
* असत्यभाषा के दस भेद * सा. इति। वह असत्य भाषा दश प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार है क्रोधनिर्गत असत्यभाषा। यहाँ 'कोहे' में जो सप्तमी विभक्ति है वह पंचमी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त है और उसका संबंध 'निस्सिया' के साथ है। अतः क्रोध से निकली हुई भाषा असत्य है। इस तरह माननिसृत आदि में भी व्याख्यान करना चाहिए। अथवा हम यथाश्रुत अर्थ की उपपत्ति इस तरह कर सकते हैं कि - 'निश्रा जाता अस्याः सा निश्रिता' । अर्थात् जिसको निश्रा प्राप्त हुई है. वह निश्रित। क्रोध में जो निश्रित हैं वह क्रोधनिश्रित असत्यभाषा। प्राकृत भाषा में 'निस्सिआ' का अर्थ जैसे निःसृत होता है वैसे 'निश्रिता' यह अर्थ भी हो सकता है। अतः सप्तमीविभक्ति को यथावत् रख कर 'निस्सिआ' की छाया 'निश्रिता' कर के क्रोध में निश्रित ऐसा जो अर्थ किया गया है वह
१ द्रव्यतो नामैको मृषावादो नो भावतः १। भावतो नामैको मृषावादो न द्रव्यतः २। एको द्रव्यतोऽपि भावतोऽपि ३। एको नो द्रव्यतो नो भावतः ४। तत्र द्रव्यतो मृषावादो नो भावतो यथा कश्चिद्भणेत् - 'अस्ति त्वया कुत्र पशुमृगादयो दृष्टाः? तदा भणति नास्ति, एष द्रव्यतो मृषावादो न भावतः १। भावतो नो द्रव्यतो यथा - मृषां भणिष्यामीति, ततस्तस्य व्यञ्जनानि सहसा सत्यानि विनिर्गतानि तानि, एष भावतो न द्रव्यतः २। द्रव्यतोऽपि भावतोऽपि - यथा मृषावादपरिणतः कश्चित्तमेव मृषावादं वदेत् ३। चतुर्थो भङ्गः शून्य इति।