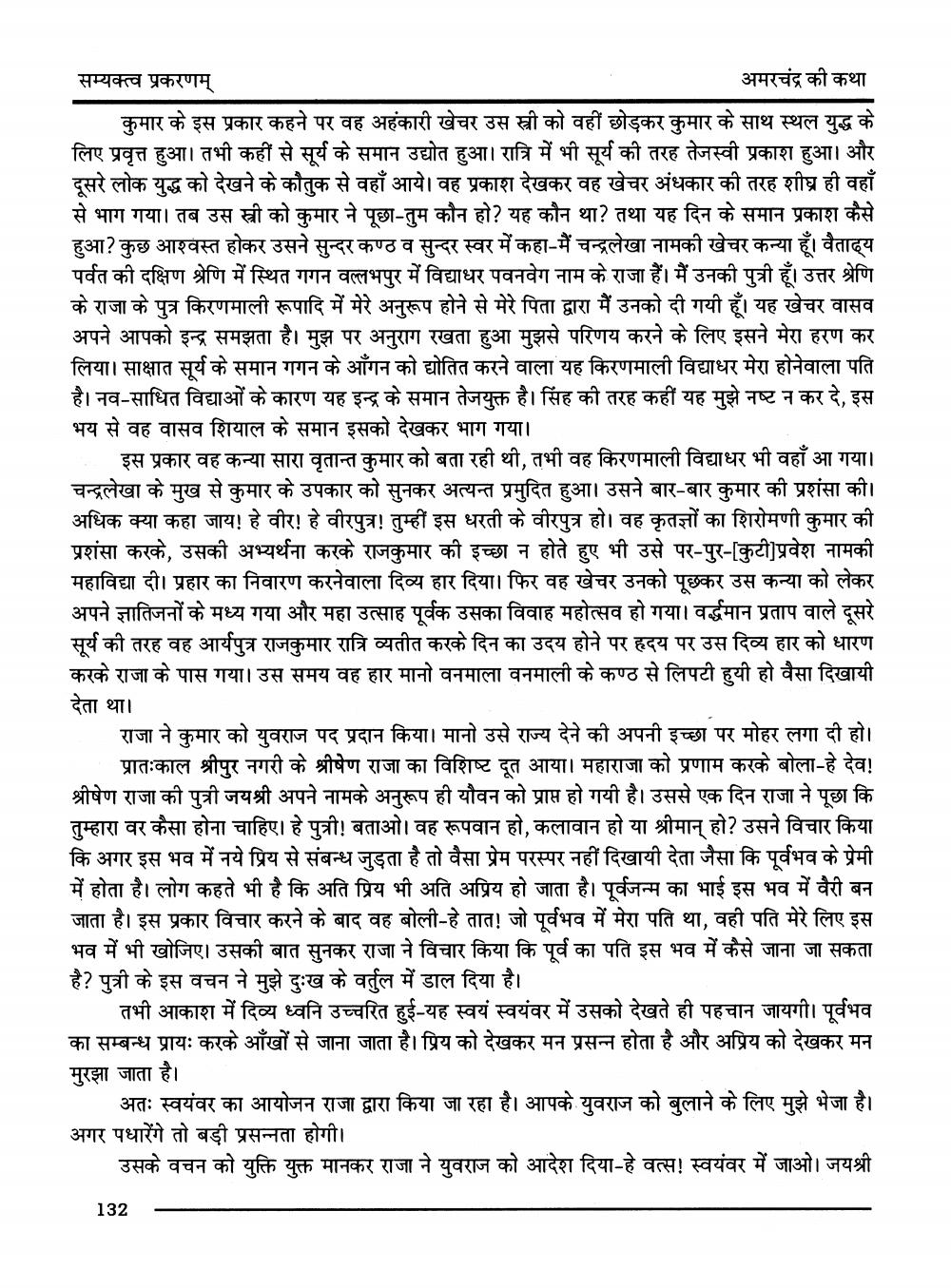________________
सम्यक्त्व प्रकरणम्
अमरचंद्र की कथा
कुमार के इस प्रकार कहने पर वह अहंकारी खेचर उस स्त्री को वहीं छोड़कर कुमार के साथ स्थल युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ। तभी कहीं से सूर्य के समान उद्योत हुआ। रात्रि में भी सूर्य की तरह तेजस्वी प्रकाश हुआ। और दूसरे लोक युद्ध को देखने के कौतुक से वहाँ आये । वह प्रकाश देखकर वह खेचर अंधकार की तरह शीघ्र ही वहाँ से भाग गया। तब उस स्त्री को कुमार ने पूछा- तुम कौन हो ? यह कौन था? तथा यह दिन के समान प्रकाश कैसे हुआ? कुछ आश्वस्त होकर उसने सुन्दर कण्ठ व सुन्दर स्वर में कहा- मैं चन्द्रलेखा नामकी खेचर कन्या हूँ। वैताढ्य पर्वत की दक्षिण श्रेणि में स्थित गगन वल्लभपुर में विद्याधर पवनवेग नाम के राजा हैं। मैं उनकी पुत्री हूँ। उत्तर
राजा के पुत्र किरणमाली रूपादि में मेरे अनुरूप होने से मेरे पिता द्वारा मैं उनको दी गयी हूँ। यह खेचर वासव अपने आपको इन्द्र समझता है। मुझ पर अनुराग रखता हुआ मुझसे परिणय करने के लिए इसने मेरा हरण कर लिया। साक्षात सूर्य के समान गगन के आँगन को द्योतित करने वाला यह किरणमाली विद्याधर मेरा होनेवाला पति है। नव-साधित विद्याओं के कारण यह इन्द्र के समान तेजयुक्त है। सिंह की तरह कहीं यह मुझे नष्ट न कर दे, इस भय से वह वासव शियाल के समान इसको देखकर भाग गया।
इस प्रकार वह कन्या सारा वृतान्त कुमार को बता रही थी, तभी वह किरणमाली विद्याधर भी वहाँ आ गया। चन्द्रलेखा के मुख से कुमार के उपकार को सुनकर अत्यन्त प्रमुदित हुआ । उसने बार- बार कुमार की प्रशंसा की । अधिक क्या कहा जाय! हे वीर! हे वीरपुत्र ! तुम्हीं इस धरती के वीरपुत्र हो । वह कृतज्ञों का शिरोमणी कुमार की प्रशंसा करके, उसकी अभ्यर्थना करके राजकुमार की इच्छा न होते हुए भी उसे पर-पुर- [ कुटी ] प्रवेश नामकी महाविद्या दी। प्रहार का निवारण करनेवाला दिव्य हार दिया। फिर वह खेचर उनको पूछकर उस कन्या को लेकर अपने ज्ञातिजनों के मध्य गया और महा उत्साह पूर्वक उसका विवाह महोत्सव हो गया। वर्द्धमान प्रताप वाले दूसरे सूर्य की तरह वह आर्यपुत्र राजकुमार रात्रि व्यतीत करके दिन का उदय होने पर हृदय पर उस दिव्य हार को धारण करके राजा के पास गया। उस समय वह हार मानो वनमाला वनमाली के कण्ठ से लिपटी हुयी हो वैसा दिखायी देता था।
राजा ने कुमार को युवराज पद प्रदान किया। मानो उसे राज्य देने की अपनी इच्छा पर मोहर लगा दी हो। प्रातः काल श्रीपुर नगरी के श्रीषेण राजा का विशिष्ट दूत आया । महाराजा को प्रणाम करके बोला - हे देव ! श्रीषेण राजा की पुत्री जयश्री अपने नामके अनुरूप ही यौवन को प्राप्त हो गयी है। उससे एक दिन राजा ने पूछा कि तुम्हारा वर कैसा होना चाहिए। हे पुत्री ! बताओ। वह रूपवान हो, कलावान हो या श्रीमान् हो ? उसने विचार किया कि अगर इस भव में नये प्रिय से संबन्ध जुड़ता है तो वैसा प्रेम परस्पर नहीं दिखायी देता जैसा कि पूर्वभव के प्रेमी में होता है। लोग कहते भी है कि अति प्रिय भी अति अप्रिय हो जाता है । पूर्वजन्म का भाई इस भव में वैरी बन जाता है। इस प्रकार विचार करने के बाद वह बोली- हे तात! जो पूर्वभव में मेरा पति था, वही पति मेरे लिए इस भव में भी खोजिए। उसकी बात सुनकर राजा ने विचार किया कि पूर्व का पति इस भव में कैसे जाना जा सकता है ? पुत्री के इस वचन ने मुझे दुःख के वर्तुल में डाल दिया है।
तभी आकाश में दिव्य ध्वनि उच्चरित हुई - यह स्वयं स्वयंवर में उसको देखते ही पहचान जायगी । पूर्वभव का सम्बन्ध प्रायः करके आँखों से जाना जाता है। प्रिय को देखकर मन प्रसन्न होता है और अप्रिय को देखकर मन मुरझा जाता है।
अतः स्वयंवर का आयोजन राजा द्वारा किया जा रहा है। आपके युवराज को बुलाने के लिए मुझे भेजा है। अगर पधारेंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी।
उसके वचन को युक्ति युक्त मानकर राजा ने युवराज को आदेश दिया - हे वत्स ! स्वयंवर में जाओ । जयश्री
132