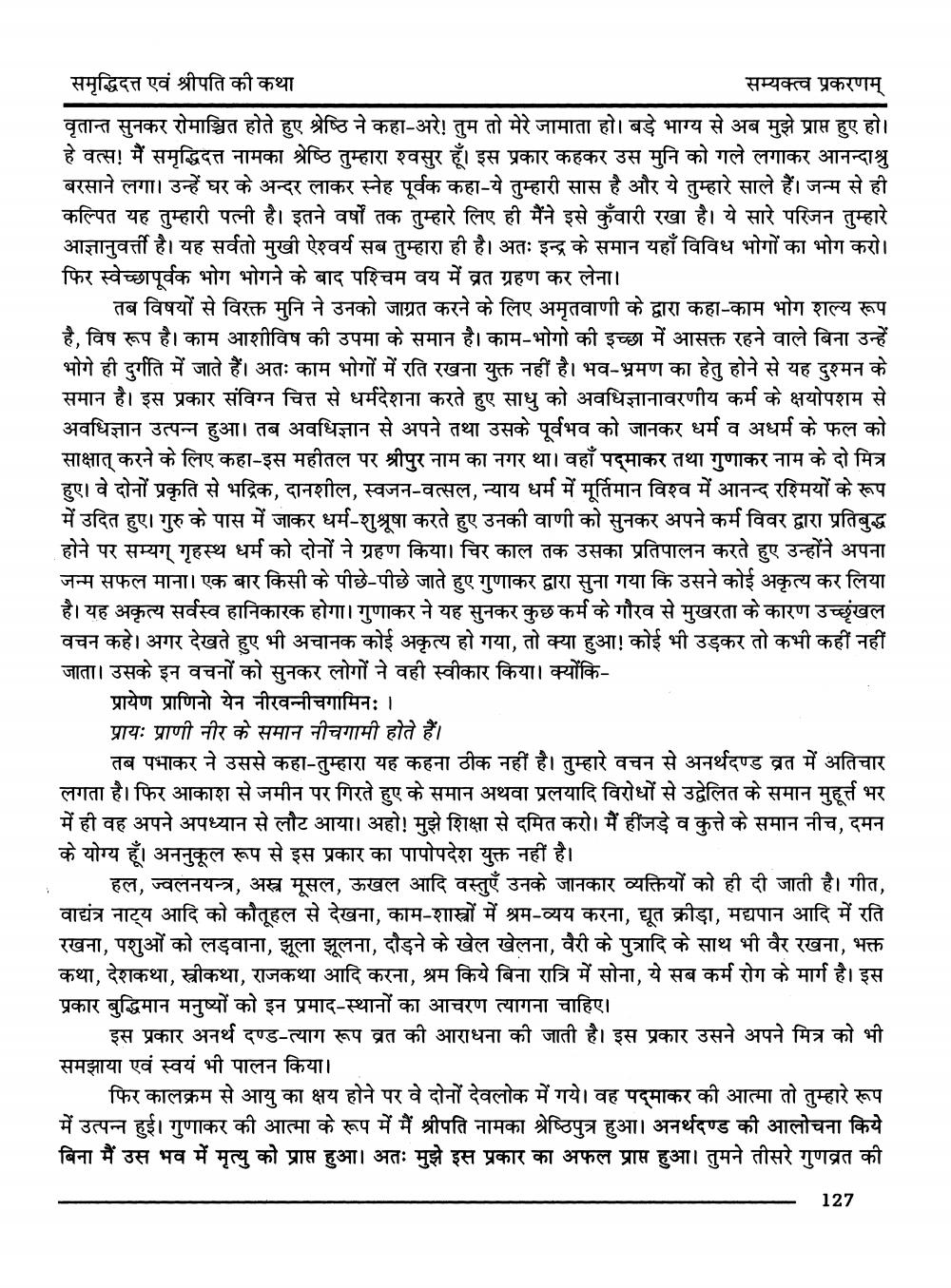________________
समृद्धिदत्त एवं श्रीपति की कथा
सम्यक्त्व प्रकरणम् वृतान्त सुनकर रोमाञ्चित होते हुए श्रेष्ठि ने कहा-अरे! तुम तो मेरे जामाता हो। बड़े भाग्य से अब मुझे प्राप्त हुए हो। हे वत्स! मैं समृद्धिदत्त नामका श्रेष्ठि तुम्हारा श्वसुर हूँ। इस प्रकार कहकर उस मुनि को गले लगाकर आनन्दाश्रु बरसाने लगा। उन्हें घर के अन्दर लाकर स्नेह पूर्वक कहा-ये तुम्हारी सास है और ये तुम्हारे साले हैं। जन्म से ही कल्पित यह तुम्हारी पत्नी है। इतने वर्षों तक तुम्हारे लिए ही मैंने इसे कुँवारी रखा है। ये सारे परिजन तुम्हारे आज्ञानुवर्ती है। यह सर्वतो मुखी ऐश्वर्य सब तुम्हारा ही है। अतः इन्द्र के समान यहाँ विविध भोगों का भोग करो। फिर स्वेच्छापूर्वक भोग भोगने के बाद पश्चिम वय में व्रत ग्रहण कर लेना।
तब विषयों से विरक्त मुनि ने उनको जाग्रत करने के लिए अमृतवाणी के द्वारा कहा-काम भोग शल्य रूप है, विष रूप है। काम आशीविष की उपमा के समान है। काम-भोगो की इच्छा में आसक्त रहने वाले बिना उन्हें भोगे ही दुर्गति में जाते हैं। अतः काम भोगों में रति रखना युक्त नहीं है। भव-भ्रमण का हेतु होने से यह दुश्मन के समान है। इस प्रकार संविग्न चित्त से धर्मदेशना करते हुए साधु को अवधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ। तब अवधिज्ञान से अपने तथा उसके पूर्वभव को जानकर धर्म व अधर्म के फल को साक्षात् करने के लिए कहा-इस महीतल पर श्रीपुर नाम का नगर था। वहाँ पद्माकर तथा गुणाकर नाम के दो मित्र हुए। वे दोनों प्रकृति से भद्रिक, दानशील, स्वजन-वत्सल, न्याय धर्म में मूर्तिमान विश्व में आनन्द रश्मियों के रूप में उदित हुए। गुरु के पास में जाकर धर्म-शुश्रूषा करते हुए उनकी वाणी को सुनकर अपने कर्म विवर द्वारा प्रतिबुद्ध होने पर सम्यग् गृहस्थ धर्म को दोनों ने ग्रहण किया। चिर काल तक उसका प्रतिपालन करते हुए उन्होंने अपना जन्म सफल माना। एक बार किसी के पीछे-पीछे जाते हुए गुणाकर द्वारा सुना गया कि उसने कोई अकृत्य कर लिया है। यह अकृत्य सर्वस्व हानिकारक होगा। गुणाकर ने यह सुनकर कुछ कर्म के गौरव से मुखरता के कारण उच्छृखल वचन कहे। अगर देखते हुए भी अचानक कोई अकृत्य हो गया, तो क्या हुआ! कोई भी उड़कर तो कभी कहीं नहीं जाता। उसके इन वचनों को सुनकर लोगों ने वही स्वीकार किया। क्योंकि
प्रायेण प्राणिनो येन नीरवन्नीचगामिनः । प्रायः प्राणी नीर के समान नीचगामी होते हैं।
तब पभाकर ने उससे कहा-तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं है। तुम्हारे वचन से अनर्थदण्ड व्रत में अतिचार लगता है। फिर आकाश से जमीन पर गिरते हुए के समान अथवा प्रलयादि विरोधों से उद्वेलित के समान मुहूर्त भर में ही वह अपने अपध्यान से लौट आया। अहो! मुझे शिक्षा से दमित करो। मैं हीजड़े व कुत्ते के समान नीच, दमन के योग्य हूँ। अननुकूल रूप से इस प्रकार का पापोपदेश युक्त नहीं है।
हल, ज्वलनयन्त्र, अस्त्र मूसल, ऊखल आदि वस्तुएँ उनके जानकार व्यक्तियों को ही दी जाती है। गीत, वाद्यंत्र नाट्य आदि को कौतूहल से देखना, काम-शास्त्रों में श्रम-व्यय करना, द्यूत क्रीड़ा, मद्यपान आदि में रति रखना, पशुओं को लड़वाना, झूला झूलना, दौड़ने के खेल खेलना, वैरी के पुत्रादि के साथ भी वैर रखना, भक्त कथा, देशकथा, स्त्रीकथा, राजकथा आदि करना, श्रम किये बिना रात्रि में सोना, ये सब कर्म रोग के मार्ग है। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को इन प्रमाद-स्थानों का आचरण त्यागना चाहिए।
इस प्रकार अनर्थ दण्ड-त्याग रूप व्रत की आराधना की जाती है। इस प्रकार उसने अपने मित्र को भी समझाया एवं स्वयं भी पालन किया।
फिर कालक्रम से आयु का क्षय होने पर वे दोनों देवलोक में गये। वह पद्माकर की आत्मा तो तुम्हारे रूप में उत्पन्न हुई। गुणाकर की आत्मा के रूप में मैं श्रीपति नामका श्रेष्ठिपुत्र हुआ। अनर्थदण्ड की आलोचना किये बिना मैं उस भव में मृत्यु को प्राप्त हुआ। अतः मुझे इस प्रकार का अफल प्राप्त हुआ। तुमने तीसरे गुणव्रत की
127