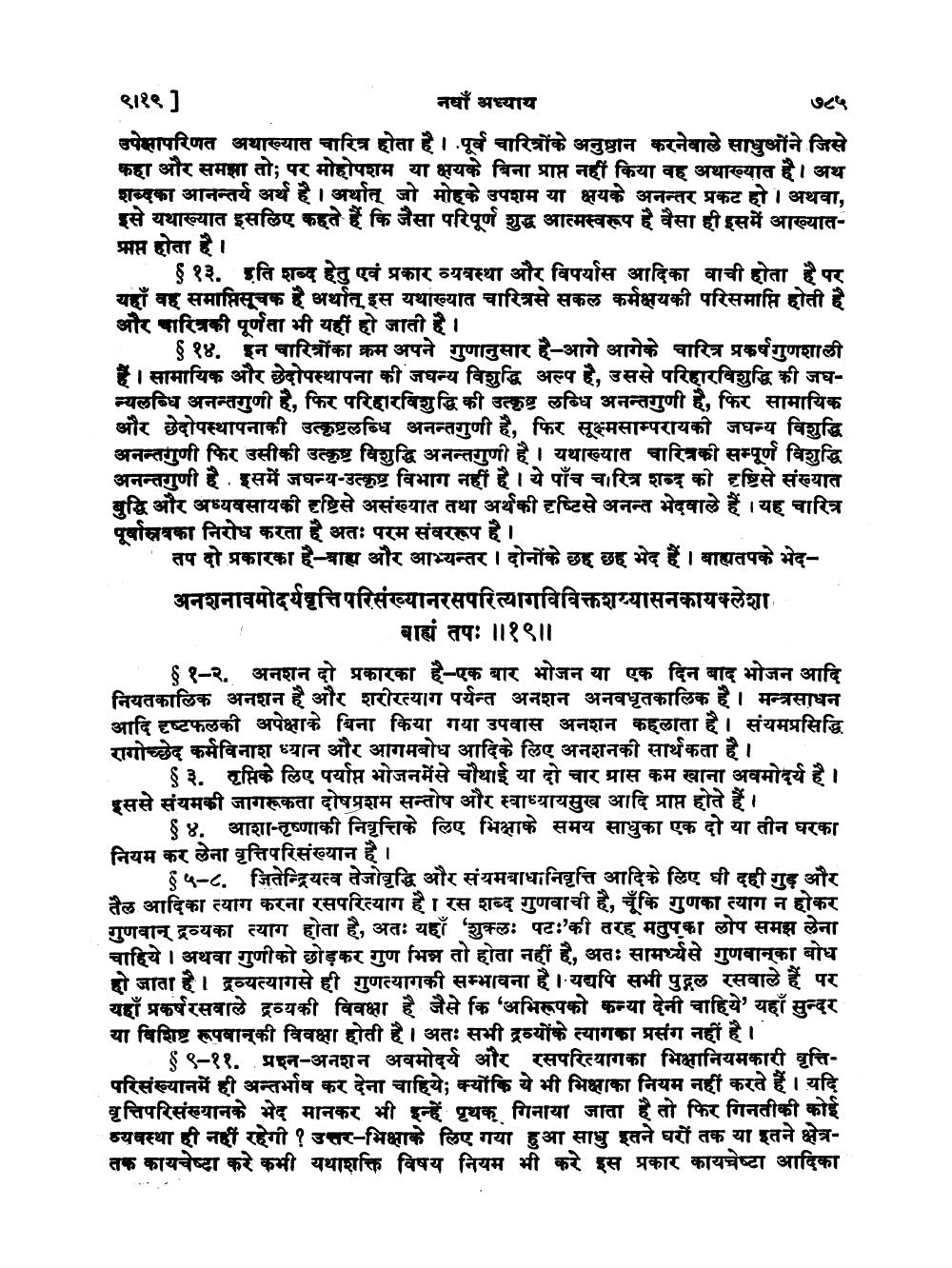________________
९।१९]
नयाँ अध्याय उपेक्षापरिणत अथाख्यात चारित्र होता है। पूर्व चारित्रोंके अनुष्ठान करनेवाले साधुओंने जिसे कहा और समझा तो; पर मोहोपशम या क्षयके बिना प्राप्त नहीं किया वह अथाख्यात है। अथ शब्दका आनन्तर्य अर्थ है । अर्थात् जो मोहके उपशम या क्षयके अनन्तर प्रकट हो । अथवा, इसे यथाख्यात इसलिए कहते हैं कि जैसा परिपूर्ण शुद्ध आत्मस्वरूप है वैसा ही इसमें आख्यातप्राप्त होता है।
६१३. इति शब्द हेतु एवं प्रकार व्यवस्था और विपर्यास आदिका वाची होता है पर यहाँ वह समाप्तिसूचक है अर्थात् इस यथाख्यात चारित्रसे सकल कर्मक्षयकी परिसमाप्ति होती है और चारित्रकी पूर्णता भी यहीं हो जाती है।
६१४. इन चारित्रोंका क्रम अपने गुणानुसार है-आगे आगेके चारित्र प्रकर्षगुणशाली हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना की जघन्य विशुद्धि अल्प है, उससे परिहारविशुद्धि की जघन्यलब्धि अनन्तगुणी है, फिर परिहारविशुद्धि की उत्कृष्ट लब्धि अनन्तगुणी है, फिर सामायिक
और छेदोपस्थापनाकी उत्कृष्टलब्धि अनन्तगुणी है, फिर सूक्ष्मसाम्परायकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी फिर उसीकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है। यथाख्यात चारित्रकी सम्पूर्ण विशुद्धि अनन्तगुणी है . इसमें जघन्य-उत्कृष्ट विभाग नहीं है। ये पाँच चारित्र शब्द को दृष्टिसे संख्यात बुद्धि और अध्यवसायकी दृष्टिसे असंख्यात तथा अर्थकी दृष्टिसे अनन्त भेदवाले हैं । यह चारित्र पूर्वाञवका निरोध करता है अतः परम संवररूप है।
तप दो प्रकारका है-बाह्य और आभ्यन्तर । दोनोंके छह छह भेद हैं । बाह्यतपके भेदअनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा
बाह्यं तपः ॥१९॥ ६१-२. अनशन दो प्रकारका है-एक बार भोजन या एक दिन बाद भोजन आदि नियतकालिक अनशन है और शरीरत्याग पर्यन्त अनशन अनवधृतकालिक है । मन्त्रसाधन
ष्टफलकी अपेक्षाके बिना किया गया उपवास अनशन कहलाता है। संयमप्रसिद्धि रागोच्छेद कर्मविनाश ध्यान और आगमबोध आदिके लिए अनशनकी सार्थकता है।
६३. तृप्तिके लिए पर्याप्त भोजनमेंसे चौथाई या दो चार ग्रास कम खाना अवमोदर्य है। इससे संयमकी जागरूकता दोषप्रशम सन्तोष और स्वाध्यायसुख आदि प्राप्त होते हैं।
६४. आशा-तृष्णाकी निवृत्तिके लिए भिक्षाके समय साधुका एक दो या तीन घरका नियम कर लेना वृत्तिपरिसंख्यान है।
६५-८. जितेन्द्रियत्व तेजोवृद्धि और संयमबाधानिवृत्ति आदिके लिए घी दही गुड़ और तैल आदिका त्याग करना रसपरित्याग है। रस शब्द गुणवाची है, चूँकि गुणका त्याग न होकर गुणवान् द्रव्यका त्याग होता है, अतः यहाँ 'शुक्लः पटः'की तरह मतुपका लोप समझ लेना चाहिये । अथवा गुणीको छोड़कर गुण भिन्न तो होता नहीं है, अत: सामर्थ्यसे गुणवानका बोध हो जाता है। द्रव्यत्यागसे ही गुणत्यागकी सम्भावना है। यद्यपि सभी पुद्गल रसवाले हैं पर यहाँ प्रकर्षरसवाले द्रव्यकी विवक्षा है जैसे कि 'अभिरूपको कन्या देनी चाहिये' यहाँ सुन्दर या विशिष्ट रूपवानकी विवक्षा होती है । अतः सभी द्रव्योंके त्यागका प्रसंग नहीं है।
६९-११. प्रश्न-अनशन अवमोदर्य और रसपरित्यागका भिक्षानियमकारी वृत्तिपरिसंख्यानमें ही अन्तर्भाव कर देना चाहिये। क्योंकि ये भी भिक्षाका नियम नहीं करते हैं । यदि वृत्तिपरिसंख्यानके भेद मानकर भी इन्हें पृथक गिनाया जाता है तो फिर गिनतीकी कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी ? उत्तर-मिक्षाके लिए गया हुआ साधु इतने घरों तक या इतने क्षेत्रतक कायचेष्टा करे कभी यथाशक्ति विषय नियम भी करे इस प्रकार कायचेष्टा आदिका