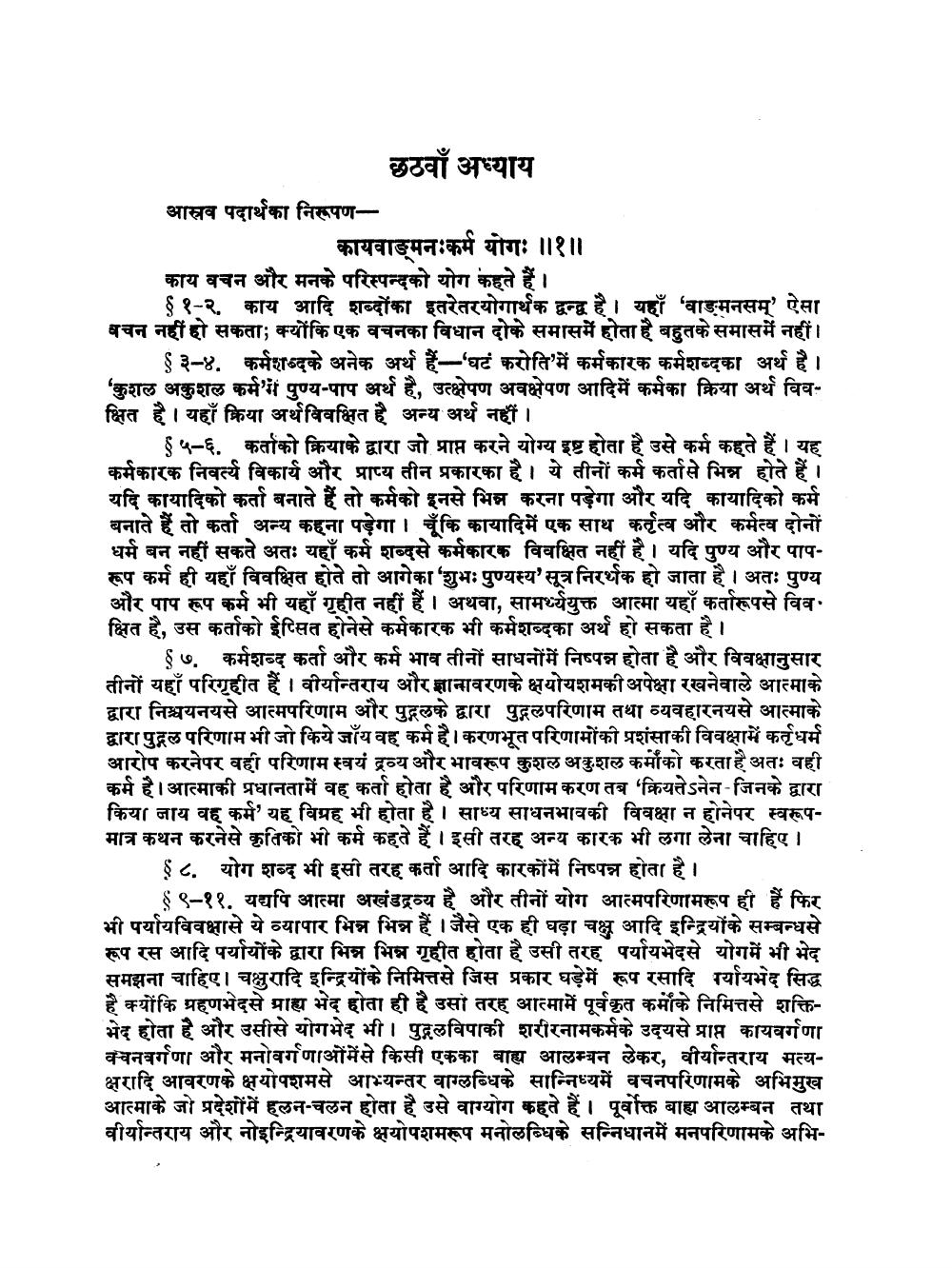________________
छठवाँ अध्याय आस्रव पदार्थका निरूपण
कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥१॥ काय वचन और मनके परिस्पन्दको योग कहते हैं।
६१-२. काय आदि शब्दोंका इतरेतरयोगार्थक द्वन्द्व है। यहाँ 'वाङमनसम्' ऐसा वचन नहीं हो सकता; क्योंकि एक वचनका विधान दोके समासमें होता है बहुतके समासमें नहीं।
३-४. कर्मशब्दके अनेक अर्थ हैं-घटं करोति'में कर्मकारक कर्मशब्दका अर्थ है । 'कुशल अकुशल कर्म में पुण्य-पाप अर्थ है, उत्क्षेपण अवक्षेपण आदिमें कर्मका क्रिया अर्थ विवक्षित है । यहाँ क्रिया अर्थविवक्षित है अन्य अर्थ नहीं।
५-६. कर्ताको क्रियाके द्वारा जो प्राप्त करने योग्य इष्ट होता है उसे कर्म कहते हैं । यह कर्मकारक निवर्त्य विकार्य और प्राप्य तीन प्रकारका है। ये तीनों कर्म कर्तासे भिन्न होते हैं। यदि कायादिको कर्ता बनाते हैं तो कर्मको इनसे भिन्न करना पड़ेगा और यदि कायादिको कर्म बनाते हैं तो कर्ता अन्य कहना पड़ेगा। चूँकि कायादिमें एक साथ कर्तृत्व और कर्मत्व दोनों धर्म बन नहीं सकते अतः यहाँ कर्म शब्दसे कर्मकारक विवक्षित नहीं है। यदि पुण्य और पापरूप कर्म ही यहाँ विवक्षित होते तो आगेका'शुभः पुण्यस्य' सूत्र निरर्थक हो जाता है। अतः पुण्य
र पाप रूप कमें भी यहाँ गृहीत नहीं है। अथवा, सामथ्येयुक्त आत्मा यहाँ कतोरूपसे विव क्षित है, उस कर्ताको ईप्सित होनेसे कर्मकारक भी कर्मशब्दका अर्थ हो सकता है।
६७. कर्मशब्द कर्ता और कर्म भाव तीनों साधनोंमें निष्पन्न होता है और विवक्षानुसार तीनों यहाँ परिगृहीत हैं । वीर्यान्तराय और ज्ञानावरणके क्षयोयशमकी अपेक्षा रखनेवाले आत्माके द्वारा निश्चयनयसे आत्मपरिणाम और पुद्गलके द्वारा पुद्गलपरिणाम तथा व्यवहारनयसे आत्माके द्वारा पुद्गल परिणाम भी जो किये जाँय वह कर्म है। करणभूत परिणामोंकी प्रशंसाकी विवक्षामें कर्तृधर्म आरोप करनेपर वही परिणाम स्वयं द्रव्य और भावरूप कुशल अकुशल कर्मोको करताहै अतः वही कर्म है। आत्माकी प्रधानतामें वह कर्ता होत और परिणाम करण तब 'क्रियतेऽनेन-जिनके द्वारा किया नाय वह कर्म' यह विग्रह भी होता है। साध्य साधनभावकी विवक्षा न होनेपर स्वरूपमात्र कथन करनेसे कृतिको भी कर्म कहते हैं । इसी तरह अन्य कारक भी लगा लेना चाहिए ।
६८. योग शब्द भी इसी तरह कर्ता आदि कारकोंमें निष्पन्न होता है।
६९-११. यद्यपि आत्मा अखंडद्रव्य है और तीनों योग आत्मपरिणामरूप ही हैं फिर भी पर्यायविवक्षासे ये व्यापार भिन्न भिन्न हैं । जैसे एक ही घड़ा चक्षु आदि इन्द्रियोंके सम्बन्धसे रूप रस आदि पर्यायोंके द्वारा भिन्न भिन्न गृहीत होता है उसी तरह पर्यायभेदसे योगमें भी भेद समझना चाहिए। चक्षुरादि इन्द्रियों के निमित्तसे जिस प्रकार घड़ेमें रूप रसादि पर्यायभेद सिद्ध है क्योंकि ग्रहणभेदसे ग्राह्य भेद होता ही है उसी तरह आत्मामें पूर्वकृत काँके निमित्तसे शक्तिभेद होता है और उसीसे योगभेद भी। पुद्गलविपाकी शरीरनामकर्मके उदयसे प्राप्त कायवर्गणा क्वनवर्गणा और मनोवर्गणाओंमेंसे किसी एकका बाह्य आलम्बन लेकर, वीर्यान्तराय मत्यक्षरादि आवरणके क्षयोपशमसे आभ्यन्तर वाग्लब्धिके सान्निध्यमें वचनपरिणामके अभिमुख आत्माके जो प्रदेशोंमें हलन-चलन होता है उसे वाग्योग कहते हैं। पूर्वोक्त बाह्य आलम्बन तथा वीर्यान्तराय और नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमरूप मनोलब्धिके सन्निधानमें मनपरिणामके अभि