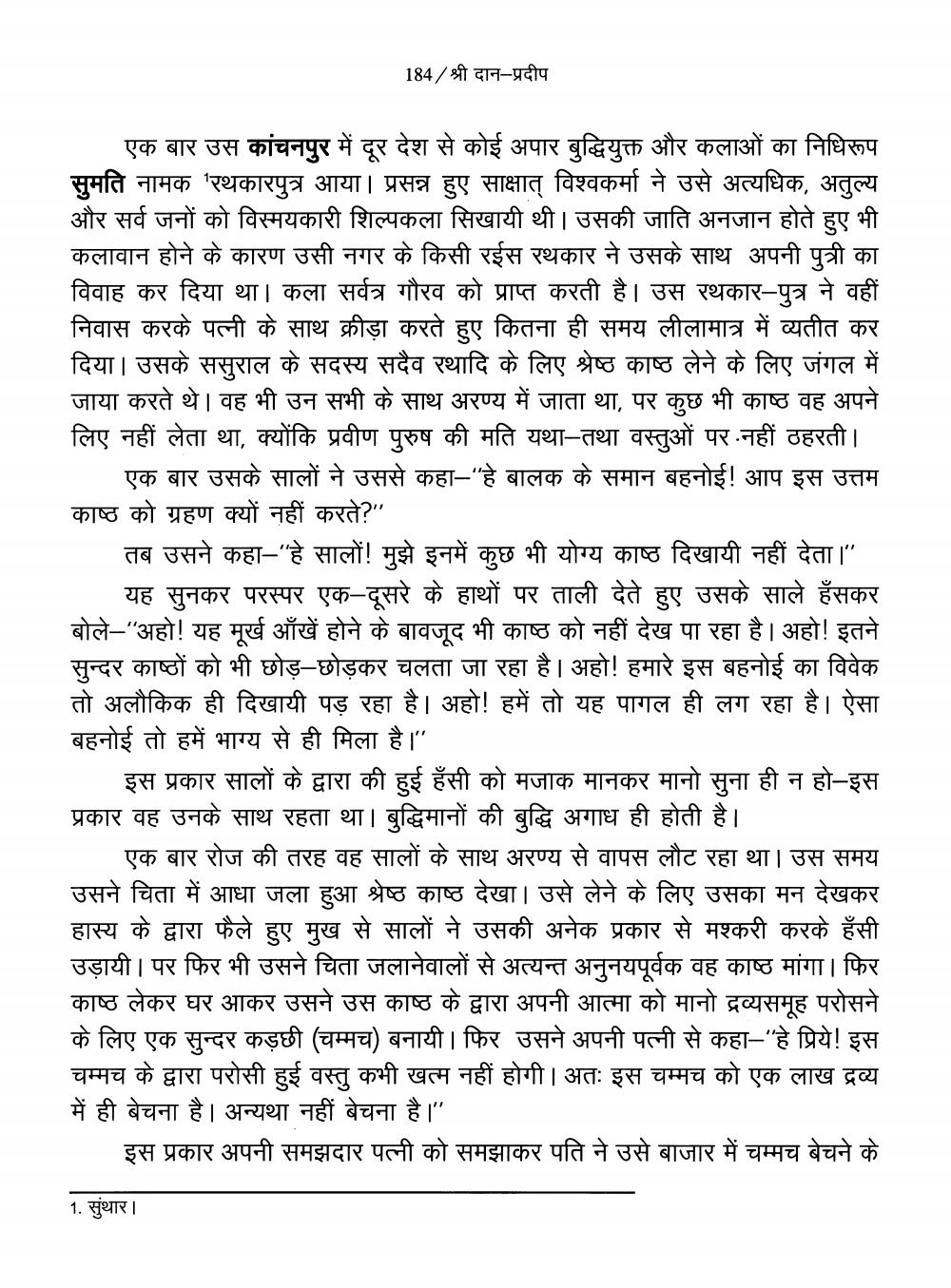________________
184/ श्री दान-प्रदीप
एक बार उस कांचनपुर में दूर देश से कोई अपार बुद्धियुक्त और कलाओं का निधिरूप सुमति नामक 'रथकारपुत्र आया। प्रसन्न हुए साक्षात् विश्वकर्मा ने उसे अत्यधिक, अतुल्य और सर्व जनों को विस्मयकारी शिल्पकला सिखायी थी। उसकी जाति अनजान होते हुए भी कलावान होने के कारण उसी नगर के किसी रईस रथकार ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। कला सर्वत्र गौरव को प्राप्त करती है। उस रथकार-पुत्र ने वहीं निवास करके पत्नी के साथ क्रीड़ा करते हुए कितना ही समय लीलामात्र में व्यतीत कर दिया। उसके ससुराल के सदस्य सदैव स्थादि के लिए श्रेष्ठ काष्ठ लेने के लिए जंगल में जाया करते थे। वह भी उन सभी के साथ अरण्य में जाता था, पर कुछ भी काष्ठ वह अपने लिए नहीं लेता था, क्योंकि प्रवीण पुरुष की मति यथा-तथा वस्तुओं पर नहीं ठहरती।
एक बार उसके सालों ने उससे कहा-“हे बालक के समान बहनोई! आप इस उत्तम काष्ठ को ग्रहण क्यों नहीं करते?"
तब उसने कहा-“हे सालों! मुझे इनमें कुछ भी योग्य काष्ठ दिखायी नहीं देता।"
यह सुनकर परस्पर एक-दूसरे के हाथों पर ताली देते हुए उसके साले हँसकर बोले-"अहो! यह मूर्ख आँखें होने के बावजूद भी काष्ठ को नहीं देख पा रहा है। अहो! इतने सुन्दर काष्ठों को भी छोड़-छोड़कर चलता जा रहा है। अहो! हमारे इस बहनोई का विवेक तो अलौकिक ही दिखायी पड़ रहा है। अहो! हमें तो यह पागल ही लग रहा है। ऐसा बहनोई तो हमें भाग्य से ही मिला है।"
इस प्रकार सालों के द्वारा की हुई हँसी को मजाक मानकर मानो सुना ही न हो इस प्रकार वह उनके साथ रहता था। बुद्धिमानों की बुद्धि अगाध ही होती है।
एक बार रोज की तरह वह सालों के साथ अरण्य से वापस लौट रहा था। उस समय उसने चिता में आधा जला हुआ श्रेष्ठ काष्ठ देखा। उसे लेने के लिए उसका मन देखकर हास्य के द्वारा फैले हुए मुख से सालों ने उसकी अनेक प्रकार से मश्करी करके हँसी उड़ायी। पर फिर भी उसने चिता जलानेवालों से अत्यन्त अनुनयपूर्वक वह काष्ठ मांगा। फिर काष्ठ लेकर घर आकर उसने उस काष्ठ के द्वारा अपनी आत्मा को मानो द्रव्यसमूह परोसने के लिए एक सुन्दर कड़छी (चम्मच) बनायी। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा-“हे प्रिये! इस चम्मच के द्वारा परोसी हुई वस्तु कभी खत्म नहीं होगी। अतः इस चम्मच को एक लाख द्रव्य में ही बेचना है। अन्यथा नहीं बेचना है।"
इस प्रकार अपनी समझदार पत्नी को समझाकर पति ने उसे बाजार में चम्मच बेचने के
1. सुथार।