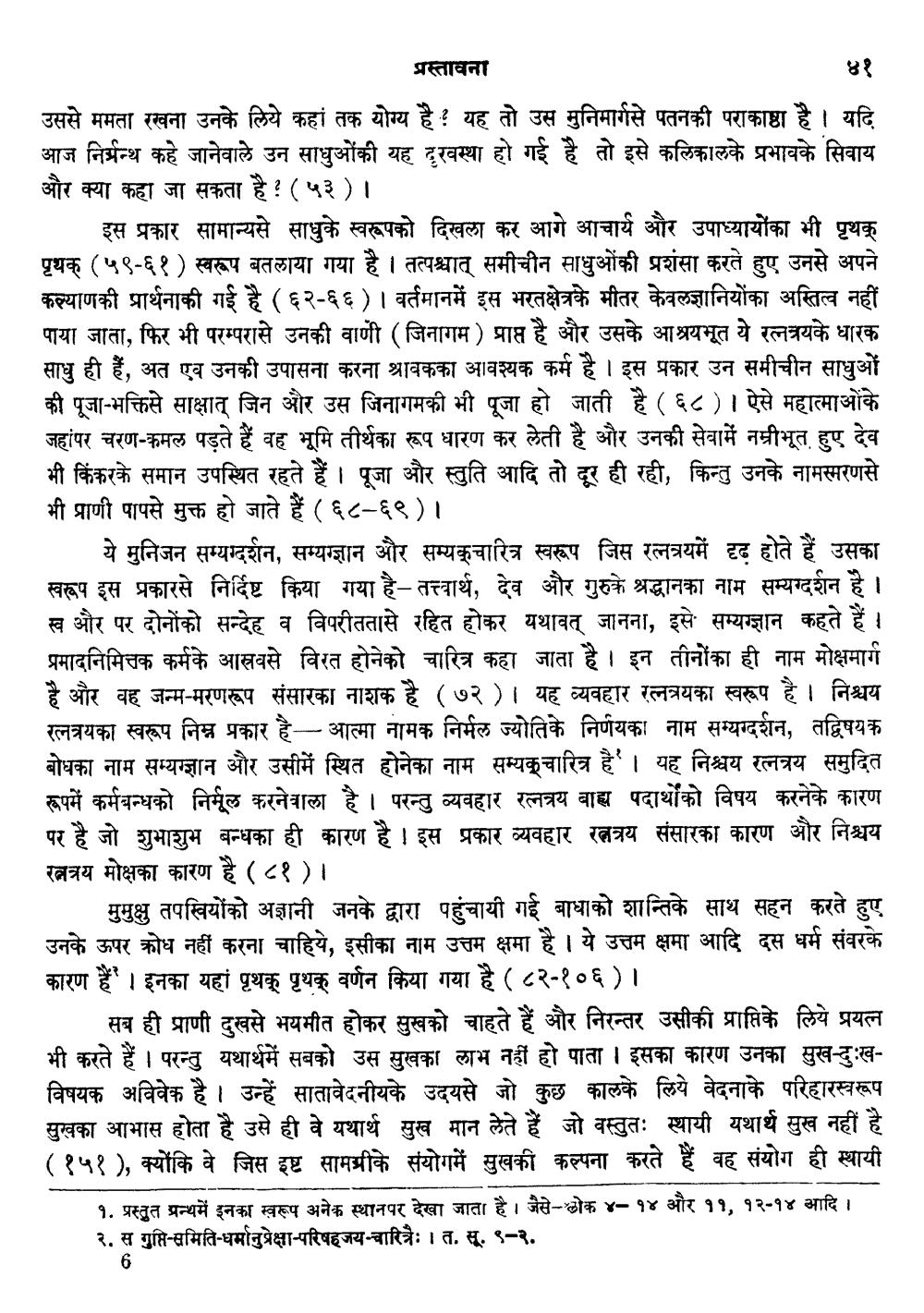________________
प्रस्तावना
४१
उससे ममता रखना उनके लिये कहां तक योग्य है ? यह तो उस मुनिमार्गसे पतनकी पराकाष्ठा है । यदि आज निर्मन्थ कहे जानेवाले उन साधुओंकी यह दुरवस्था हो गई है तो इसे कलिकालके प्रभाव के सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? ( ५३ ) ।
इस प्रकार सामान्यसे साधुके स्वरूपको दिखला कर आगे आचार्य और उपाध्यायोंका भी पृथक् पृथक् (५९-६१ ) स्वरूप बतलाया गया है । तत्पश्चात् समीचीन साधुओंकी प्रशंसा करते हुए उनसे अपने कल्याणकी प्रार्थना की गई है ( ६२-६६ ) । वर्तमानमें इस भरतक्षेत्रके मीतर केवलज्ञानियोंका अस्तित्व नहीं पाया जाता, फिर भी परम्परासे उनकी वाणी (जिनागम) प्राप्त है और उसके आश्रयभूत ये रत्नत्रयके धारक साधु ही हैं, अत एव उनकी उपासना करना श्रावकका आवश्यक कर्म है । इस प्रकार उन समीचीन साधुओं की पूजा - भक्ति से साक्षात् जिन और उस जिनागमकी भी पूजा हो जाती है ( ६८ ) । ऐसे महात्माओं के जहां पर चरण-कमल पड़ते हैं वह भूमि तीर्थका रूप धारण कर लेती है और उनकी सेवामें नम्रीभूत हुए देव भी किंकरके समान उपस्थित रहते हैं । पूजा और स्तुति आदि तो दूर ही रही, किन्तु उनके नामस्मरणसे भी प्राणी पापसे मुक्त हो जाते हैं ( ६८-६९ ) ।
ये मुनिजन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र स्वरूप जिस रत्नत्रयमें दृढ़ होते हैं उसका स्वरूप इस प्रकार से निर्दिष्ट किया गया है- तत्त्वार्थ, देव और गुरुके श्रद्धानका नाम सम्यग्दर्शन है । स्व और पर दोनोंको सन्देह व विपरीतता से रहित होकर यथावत् जानना, इसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं । प्रमादनिमित्तक कर्मके आस्रवसे विरत होनेको चारित्र कहा जाता है । इन तीनोंका ही नाम मोक्षमार्ग है और वह जन्म-मरणरूप संसारका नाशक है ( ७२ ) । यह व्यवहार रत्नत्रयका स्वरूप है । निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप निम्न प्रकार है- - आत्मा नामक निर्मल ज्योतिके निर्णयका नाम सम्यग्दर्शन, तद्विषयक बोधका नाम सम्यग्ज्ञान और उसीमें स्थित होनेका नाम सम्यक् चारित्र है' । यह निश्चय रत्नत्रय समुदित रूपमें कर्मबन्धको निर्मूल करनेवाला है । परन्तु व्यवहार रत्नत्रय बाह्य पदार्थोंको विषय करनेके कारण पर है जो शुभाशुभ बन्धका ही कारण है । इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय संसारका कारण और निश्चय रत्नत्रय मोक्षका कारण है ( ८१ ) ।
मुमुक्षु तपस्वियोंको अज्ञानी जनके द्वारा पहुंचायी गई बाधाको शान्तिके साथ सहन करते हुए उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिये, इसीका नाम उत्तम क्षमा है । ये उत्तम क्षमा आदि दस धर्म संवरके कारण हैं । इनका यहां पृथक् पृथक् वर्णन किया गया है ( ८२ - १०६ ) ।
सब ही प्राणी दुखसे भयभीत होकर सुखको चाहते हैं और निरन्तर उसीकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न भी करते हैं । परन्तु यथार्थमें सबको उस सुखका लाभ नहीं हो पाता । इसका कारण उनका सुख-दुःखविषयक अविवेक है । उन्हें सातावेदनीयके उदयसे जो कुछ कालके लिये वेदनाके परिहारस्वरूप सुखका आभास होता है उसे ही वे यथार्थ सुख मान लेते हैं जो वस्तुतः स्थायी यथार्थ सुख नहीं है ( १५१ ), क्योंकि वे जिस इष्ट सामग्रीके संयोगमें सुखकी कल्पना करते हैं वह संयोग ही स्थायी
१. प्रस्तुत ग्रन्थमें इनका स्वरूप अनेक स्थानपर देखा जाता है। जैसे-छोक ४- १४ और ११, १२-१४ आदि । २. स गुप्ति-समिति-धर्मानुप्रेक्षा परिषहजय चारित्रैः । त. सू. ९-२.
6