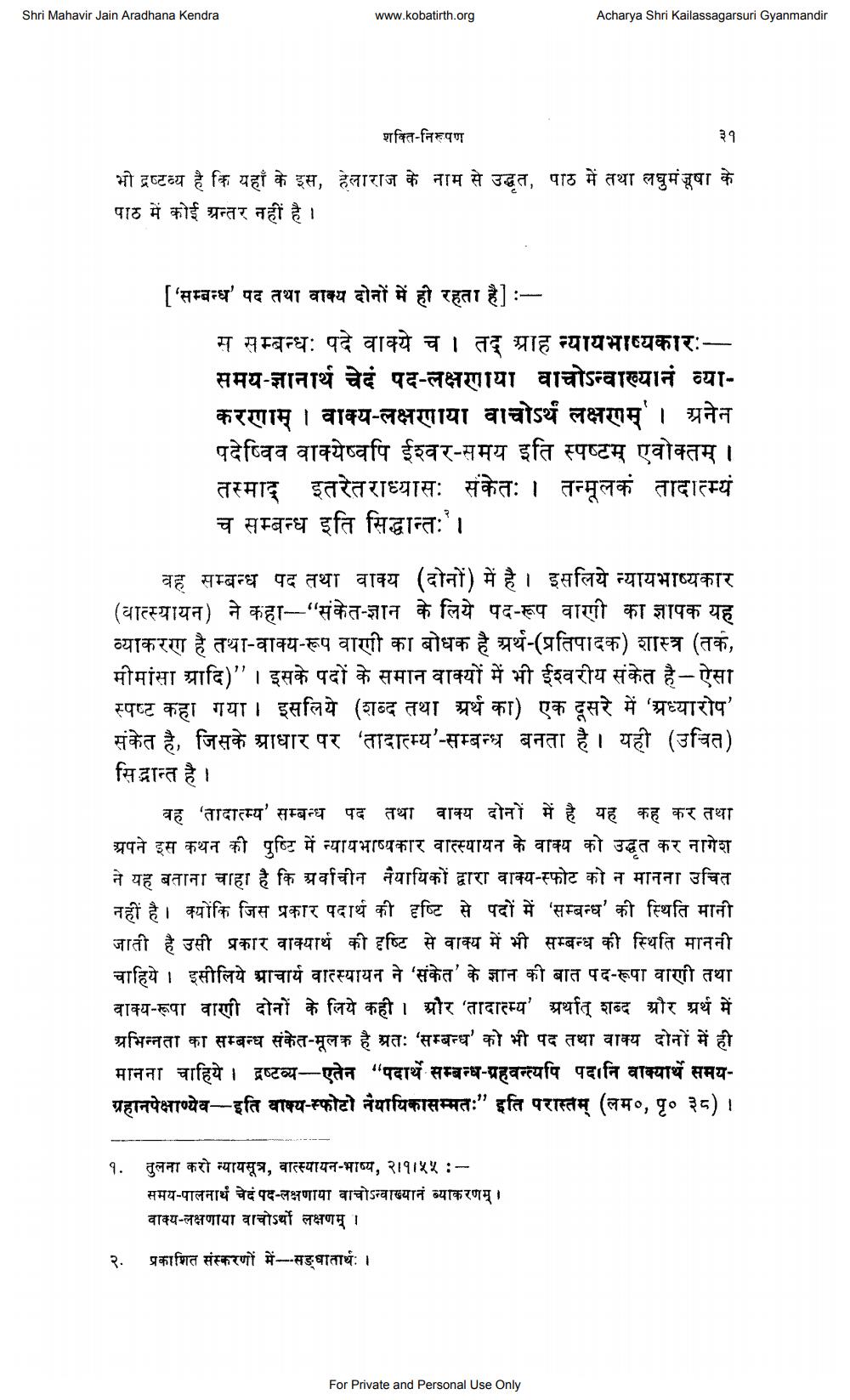________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
शक्ति-निरूपण
भी द्रष्टव्य है कि यहाँ के इस, हेलाराज के नाम से उद्धृत, पाठ में तथा लघुमंजूषा के पाठ में कोई अन्तर नहीं है।
['सम्बन्ध' पद तथा वाक्य दोनों में ही रहता है] :
स सम्बन्धः पदे वाक्ये च। तद् प्राह न्यायभाष्यकार:समय-ज्ञानार्थ चेदं पद-लक्षणाया वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणाम् । वाक्य-लक्षणाया वाचोऽर्थं लक्षरणम्। अनेन पदेष्विव वाक्येष्वपि ईश्वर-समय इति स्पष्टम् एवोक्तम् । तस्माद् इतरेतराध्यासः संकेतः । तन्मूलकं तादात्म्यं च सम्बन्ध इति सिद्धान्तः'।
वह सम्बन्ध पद तथा वाक्य (दोनों) में है। इसलिये न्यायभाष्यकार (वात्स्यायन) ने कहा- "संकेत-ज्ञान के लिये पद-रूप वाणी का ज्ञापक यह व्याकरण है तथा-वाक्य-रूप वाणी का बोधक है अर्थ-(प्रतिपादक) शास्त्र (तर्क, मीमांसा आदि)" । इसके पदों के समान वाक्यों में भी ईश्वरीय संकेत है- ऐसा स्पष्ट कहा गया । इसलिये (शब्द तथा अर्थ का) एक दूसरे में 'अध्यारोप' संकेत है, जिसके आधार पर 'तादात्म्य'-सम्बन्ध बनता है। यही (उचित) सिद्धान्त है।
वह 'तादात्म्य' सम्बन्ध पद तथा वाक्य दोनों में है यह कह कर तथा अपने इस कथन की पुष्टि में न्यायभाष्यकार वात्स्यायन के वाक्य को उद्धृत कर नागेश ने यह बताना चाहा है कि अर्वाचीन नैयायिकों द्वारा वाक्य-स्फोट को न मानना उचित नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार पदार्थ की दृष्टि से पदों में 'सम्बन्ध' की स्थिति मानी जाती है उसी प्रकार वाक्यार्थ की दृष्टि से वाक्य में भी सम्बन्ध की स्थिति माननी चाहिये । इसीलिये प्राचार्य वात्स्यायन ने 'संकेत' के ज्ञान की बात पद-रूपा वाणी तथा वाक्य-रूपा वाणी दोनों के लिये कही। और 'तादात्म्य' अर्थात् शब्द और अर्थ में अभिन्नता का सम्बन्ध संकेत-मूलक है अतः ‘सम्बन्ध' को भी पद तथा वाक्य दोनों में ही मानना चाहिये। द्रष्टव्य-एतेन "पदार्थे सम्बन्ध-ग्रहवन्त्यपि पदानि वाक्यार्थे समयग्रहानपेक्षाण्येव-इति वाक्य-स्फोटो नैयायिकासम्मतः" इति परास्तम् (लम०, पृ० ३८) ।
१. तुलना करो न्यायसूत्र, वात्स्यायन-भाष्य, २।१९५५ :
समय-पालनार्थ चेदं पद-लक्षणाया वाचोऽन्वाख्यानं ब्याकरणम् । वाक्य-लक्षणाया वाचोऽर्थो लक्षणम् ।
२. प्रकाशित संस्करणों में-सरातार्थः ।
For Private and Personal Use Only