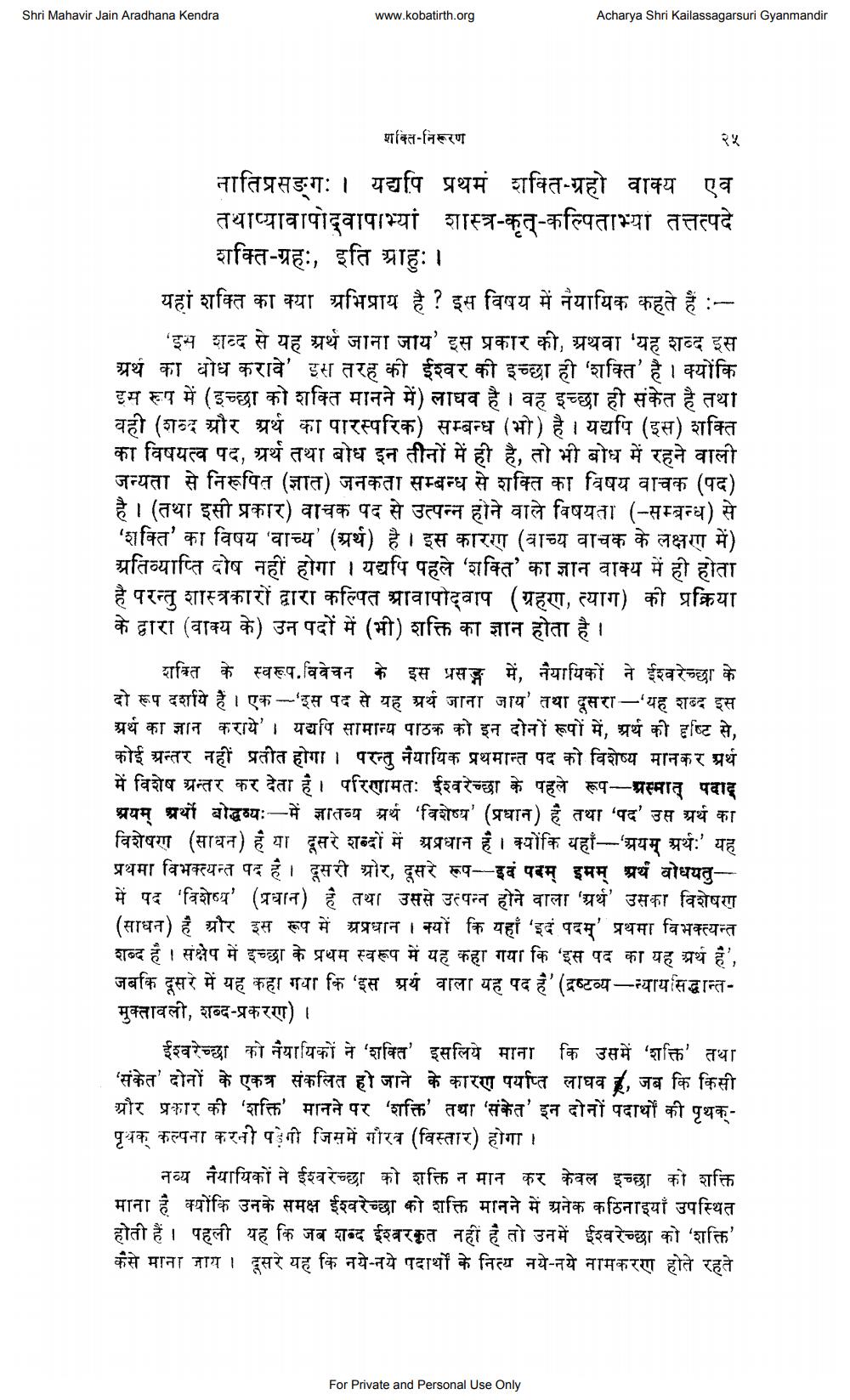________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
शक्ति-निरूरण
२५
नातिप्रसङ्गः । यद्यपि प्रथमं शक्ति-ग्रहो वाक्य एव तथाप्यावापोद्वापाभ्यां शास्त्र-कृत्-कल्पिताभ्या तत्तत्पदे
शक्ति-ग्रहः, इति पाहुः। यहां शक्ति का क्या अभिप्राय है ? इस विषय में नैयायिक कहते हैं :_ 'इस शब्द से यह अर्थ जाना जाय' इस प्रकार की, अथवा 'यह शब्द इस अर्थ का बोध करावे' इस तरह की ईश्वर की इच्छा ही 'शक्ति' है। क्योंकि इस रूप में (इच्छा को शक्ति मानने में) लाघव है। वह इच्छा ही संकेत है तथा वही (शब्द और अर्थ का पारस्परिक) सम्बन्ध (भो) है। यद्यपि (इस) शक्ति का विषयत्व पद, अर्थ तथा बोध इन तीनों में ही है, तो भी बोध में रहने वाली जन्यता से निरूपित (ज्ञात) जनकता सम्बन्ध से शक्ति का विषय वाचक (पद) है । (तथा इसी प्रकार) वाचक पद से उत्पन्न होने वाले विषयता (-सम्बन्ध) से 'शक्ति' का विषय 'वाच्य' (अर्थ) है। इस कारण (वाच्य वाचक के लक्षण में) अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा । यद्यपि पहले 'शक्ति' का ज्ञान वाक्य में ही होता है परन्तु शास्त्रकारों द्वारा कल्पित आवापोद्वाप (ग्रहण, त्याग) की प्रक्रिया के द्वारा (वाक्य के) उन पदों में (भी) शक्ति का ज्ञान होता है।
शक्ति के स्वरूप.विवेचन के इस प्रसङ्ग में, नैयायिकों ने ईश्वरेच्छा के दो रूप दर्शाये है । एक 'इस पद से यह अर्थ जाना जाय' तथा दूसरा-'यह शब्द इस अर्थ का ज्ञान कराये'। यद्यपि सामान्य पाठक को इन दोनों रूपों में, अर्थ की दृष्टि से, कोई अन्तर नहीं प्रतीत होगा। परन्तु नैयायिक प्रथमान्त पद को विशेष्य मानकर अर्थ में विशेष अन्तर कर देता है। परिणामतः ईश्वरेच्छा के पहले रूप-अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो बोद्धव्यः–में ज्ञातव्य अर्थ 'विशेष्य' (प्रधान) है तथा 'पद' उस अर्थ का विशेषण (साधन) है या दूसरे शब्दों में अप्रधान है। क्योंकि यहाँ-'अयम् अर्थः' यह प्रथमा विभक्त्यन्त पद है। दूसरी ओर, दूसरे रूप-इदं पदम् इमम् अर्थ बोधयतुमें पद 'विशेष्य' (प्रधान) है तथा उससे उत्पन्न होने वाला 'अर्थ' उसका विशेषण (साधन) है और इस रूप में अप्रधान । क्यों कि यहाँ 'इदं पदम्' प्रथमा विभक्त्यन्त शब्द है । संक्षेप में इच्छा के प्रथम स्वरूप में यह कहा गया कि 'इस पद का यह अर्थ है', जबकि दूसरे में यह कहा गया कि 'इस अयं वाला यह पद है' (द्रष्टव्य-न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, शब्द-प्रकरण) ।
ईश्वरेच्छा को नैयायिकों ने 'शक्ति' इसलिये माना कि उसमें 'शक्ति' तथा 'संकेत' दोनों के एकत्र संकलित हो जाने के कारण पर्याप्त लाघव ई, जब कि किसी
और प्रकार की 'शक्ति' मानने पर 'शक्ति' तथा 'संकेत' इन दोनों पदार्थों की पृथकपृथक कल्पना करनी पड़ेगी जिसमें गौरव (विस्तार) होगा ।
नव्य नैयायिकों ने ईश्वरेच्छा को शक्ति न मान कर केवल इच्छा को शक्ति माना है क्योंकि उनके समक्ष ईश्वरेच्छा को शक्ति मानने में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। पहली यह कि जब शब्द ईश्वरकृत नहीं है तो उनमें ईश्वरेच्छा को 'शक्ति' कैसे माना जाय । दूसरे यह कि नये-नये पदार्थों के नित्य नये-नये नामकरण होते रहते
For Private and Personal Use Only