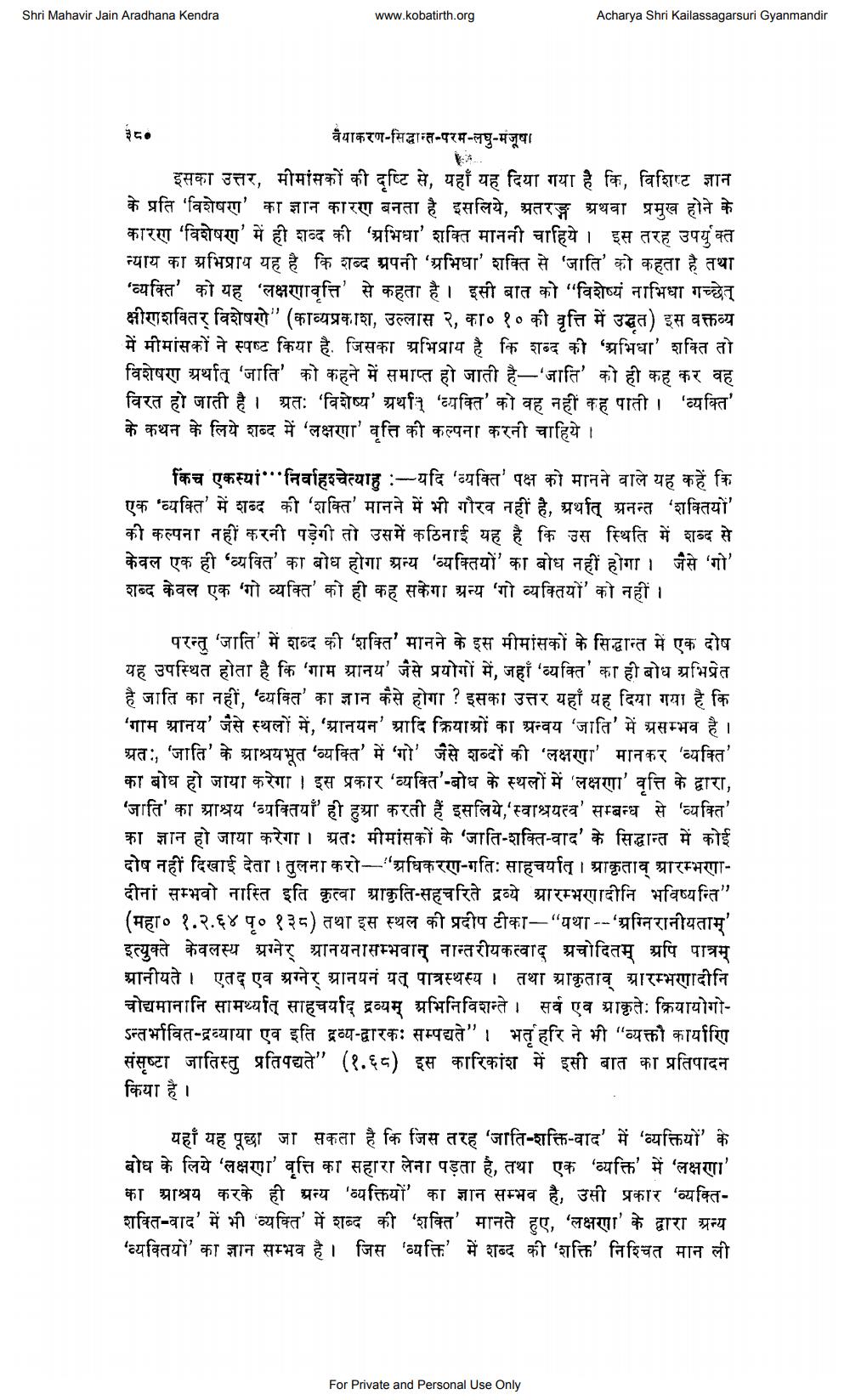________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
३८.
वैयाकरण-सिद्धान्त-परम-लघु-मंजूषा
इसका उत्तर, मीमांसकों की दृष्टि से, यहाँ यह दिया गया है कि, विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण' का ज्ञान कारण बनता है इसलिये, अतरङ्ग अथवा प्रमुख होने के कारण 'विशेषण' में ही शब्द की 'अभिधा' शक्ति माननी चाहिये। इस तरह उपर्युक्त न्याय का अभिप्राय यह है कि शब्द अपनी 'अभिधा' शक्ति से 'जाति' को कहता है तथा 'व्यक्ति' को यह 'लक्षणावृत्ति' से कहता है। इसी बात को "विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्ति विशेषणे" (काव्यप्रकाश, उल्लास २, का० १० की वृत्ति में उद्धृत) इस वक्तव्य में मीमांसकों ने स्पष्ट किया है. जिसका अभिप्राय है कि शब्द की 'अभिधा' शक्ति तो विशेषण अर्थात 'जाति' को कहने में समाप्त हो जाती है—'जाति' को ही कद्र कर वद्र विरत हो जाती है। अत: 'विशेष्य' अर्थात 'व्यक्ति' को वह नहीं कह पाती। 'व्यक्ति' के कथन के लिये शब्द में 'लक्षणा' वृत्ति की कल्पना करनी चाहिये ।
किंच एकस्यां 'निर्वाहश्चेत्याहु :यदि 'व्यक्ति' पक्ष को मानने वाले यह कहें कि एक 'व्यक्ति' में शब्द की 'शक्ति' मानने में भी गौरव नहीं है, अर्थात् अनन्त 'शक्तियों' की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी तो उसमें कठिनाई यह है कि उस स्थिति में शब्द से केवल एक ही 'व्यक्ति' का बोध होगा अन्य व्यक्तियों' का बोध नहीं होगा। जैसे 'गो' शब्द केवल एक 'गो व्यक्ति' को ही कह सकेगा अन्य 'गो व्यक्तियों को नहीं।
परन्तु 'जाति' में शब्द की 'शक्ति' मानने के इस मीमांसकों के सिद्धान्त में एक दोष यह उपस्थित होता है कि 'गाम प्रानय' जैसे प्रयोगों में, जहाँ 'व्यक्ति' का ही बोध अभिप्रेत है जाति का नहीं, 'व्यक्ति' का ज्ञान कैसे होगा ? इसका उत्तर यहाँ यह दिया गया है कि 'गाम आनय' जैसे स्थलों में, 'पानयन' आदि क्रियाओं का अन्वय 'जाति' में असम्भव है । अत:, 'जाति' के आश्रयभूत 'व्यक्ति' में 'गो' जैसे शब्दों की 'लक्षणा' मानकर 'व्यक्ति' का बोध हो जाया करेगा। इस प्रकार 'व्यक्ति'-बोध के स्थलों में 'लक्षणा' वत्ति के द्वारा, 'जाति' का आश्रय 'व्यक्तियाँ ही हया करती हैं इसलिये, स्वाश्रयत्व' सम्बन्ध से 'व्यक्ति' का ज्ञान हो जाया करेगा। अतः मीमांसकों के 'जाति-शक्ति-वाद' के सिद्धान्त में कोई दोष नहीं दिखाई देता। तुलना करो-"अधिकरण-गतिः साहचर्यात् । प्राकृताव् प्रारम्भरणादीनां सम्भवो नास्ति इति कृत्वा प्राकृति-सहचरिते द्रव्ये प्रारम्भणादीनि भविष्यन्ति" (महा० १.२.६४ पृ० १३८) तथा इस स्थल की प्रदीप टीका- “यथा -- 'अग्निरानीयताम्' इत्युक्ते केवलस्य अग्नेर् अानयनासम्भवान् नान्तरीयकत्वाद् अचोदितम् अपि पात्रम् आनीयते । एतद् एव अग्नेर् प्रानयनं यत् पात्रस्थस्य । तथा प्राकृताव् प्रारम्भरणादीनि चोद्यमानानि सामर्थ्यात् साहचर्याद् द्रव्यम् अभिनिविशन्ते। सर्व एव आकृतेः क्रियायोगोऽन्तर्भावित-द्रव्याया एव इति द्रव्य-द्वारकः सम्पद्यते"। भर्तृहरि ने भी "व्यक्तौ कार्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते” (१.६८) इस कारिकांश में इसी बात का प्रतिपादन किया है।
यहाँ यह पूछा जा सकता है कि जिस तरह 'जाति-शक्ति-वाद' में 'व्यक्तियों' के बोध के लिये 'लक्षणा' वृत्ति का सहारा लेना पड़ता है, तथा एक 'व्यक्ति' में 'लक्षणा' का आश्रय करके ही अन्य व्यक्तियों' का ज्ञान सम्भव है, उसी प्रकार 'व्यक्तिशक्ति-वाद' में भी व्यक्ति' में शब्द की 'शक्ति' मानते हुए, 'लक्षणा' के द्वारा अन्य 'व्यक्तियों का ज्ञान सम्भव है। जिस व्यक्ति' में शब्द की 'शक्ति' निश्चित मान ली
For Private and Personal Use Only