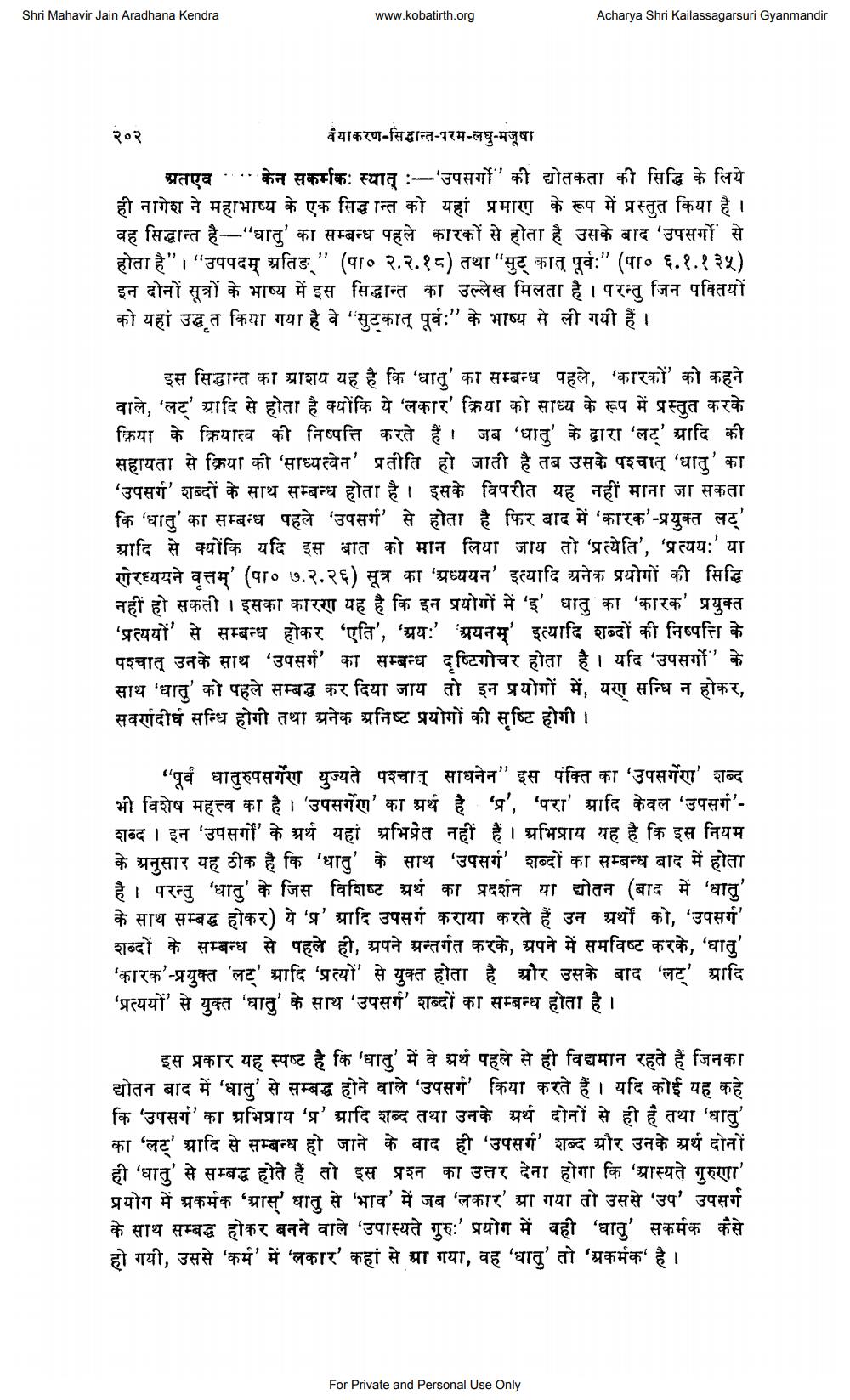________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
२०२
वैयाकरण- सिद्धान्त-परम- लघु-मंजूषा
अतएव
केन सकर्मकः स्यात् :- 'उपसर्गो" की द्योतकता की सिद्धि के लिये ही नागेश ने महाभाष्य के एक सिद्धान्त को यहां प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है । वह सिद्धान्त है - " धातु' का सम्बन्ध पहले कारकों से होता है उसके बाद 'उपसर्गों से होता है" । "उपपदम् प्रतिङ " ( पा० २.२.१८) तथा "सुट् कात् पूर्वः " ( पा० ६.१.१३५) इन दोनों सूत्रों के भाष्य में इस सिद्धान्त का उल्लेख मिलता है । परन्तु जिन पक्तियों को यहां उद्धृत किया गया है वे "सुटकात् पूर्वः " के भाष्य से ली गयी हैं ।
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
इस सिद्धान्त का प्राय यह है कि 'धातु' का सम्बन्ध पहले, 'कारकों' को कहने वाले, 'लट्' आदि से होता है क्योंकि ये 'लकार' क्रिया को साध्य के रूप में प्रस्तुत करके क्रिया के क्रियात्व की निष्पत्ति करते हैं । जब 'धातु' के द्वारा 'लट्' आदि की सहायता से क्रिया की 'साध्यत्वेन' प्रतीति हो जाती है तब उसके पश्चात् 'धातु' का ' उपसर्ग' शब्दों के साथ सम्बन्ध होता है । इसके विपरीत यह नहीं माना जा सकता कि 'धातु' का सम्बन्ध पहले 'उपसर्ग' से होता है फिर बाद में 'कारक' - प्रयुक्त लट्' आदि से क्योंकि यदि इस बात को मान लिया जाय तो 'प्रत्येति', 'प्रत्ययः' या
रध्ययने वृत्तम्' (पा० ७.२.२६) सूत्र का 'अध्ययन' इत्यादि अनेक प्रयोगों की सिद्धि नहीं हो सकती । इसका कारण यह है कि इन प्रयोगों में 'इ' धातु का 'कारक' प्रयुक्त 'प्रत्ययों' से सम्बन्ध होकर 'एति', 'अय:' अयनम्' इत्यादि शब्दों की निष्पत्ति के पश्चात् उनके साथ ' उपसर्ग' का सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता है । यदि ' उपसर्गो' के साथ 'धातु' को पहले सम्बद्ध कर दिया जाय तो इन प्रयोगों में, यरण सन्धि न होकर, सवर्णदीर्घ सन्धि होगी तथा अनेक अनिष्ट प्रयोगों की सृष्टि होगी ।
" पूर्वं धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन" इस पंक्ति का ' उपसर्गेरण' शब्द भी विशेष महत्त्व का है। 'उपसर्गेण' का अर्थ है 'प्र', 'परा' आदि केवल ' उपसर्ग'शब्द । इन ' उपसर्गों के अर्थ यहां अभिप्रेत नहीं हैं । अभिप्राय यह है कि इस नियम के अनुसार यह ठीक है कि 'धातु' के साथ ' उपसर्ग' शब्दों का सम्बन्ध बाद में होता है । परन्तु 'धातु' के जिस विशिष्ट अर्थ का प्रदर्शन या द्योतन (बाद में 'धातु ' के साथ सम्बद्ध होकर) ये 'प्र' आदि उपसर्ग कराया करते हैं उन अर्थों को, 'उपसर्ग' शब्दों के सम्बन्ध से पहले ही, अपने अन्तर्गत करके, अपने में समविष्ट करके, 'घातु' 'कारक' - प्रयुक्त 'लट्' आदि 'प्रत्यों' से युक्त होता है और उसके बाद 'लट्' प्रादि 'प्रत्ययों' से युक्त 'धातु' के साथ 'उपसर्ग' शब्दों का सम्बन्ध होता है ।
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'धातु' में वे अर्थ पहले से ही विद्यमान रहते हैं जिनका द्योतन बाद में 'धातु' से सम्बद्ध होने वाले 'उपसर्ग किया करते हैं । यदि कोई यह कहे कि ' उपसर्ग' का अभिप्राय 'प्र' आदि शब्द तथा उनके अर्थ दोनों से ही है तथा 'धातु' का 'लट्' आदि से सम्बन्ध हो जाने के बाद ही 'उपसर्ग' शब्द और उनके अर्थ दोनों ही 'धातु' से सम्बद्ध होते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि 'प्रास्यते गुरुणा ' प्रयोग में अकर्मक 'आस्' धातु से 'भाव' में जब 'लकार' आ गया तो उससे 'उप' उपसर्ग के साथ सम्बद्ध होकर बनने वाले 'उपास्यते गुरुः' प्रयोग में वही 'धातु' सकर्मक कैसे हो गयी, उससे 'कर्म' में 'लकार' कहां से आ गया, वह 'धातु' तो 'अकर्मक' है ।
For Private and Personal Use Only