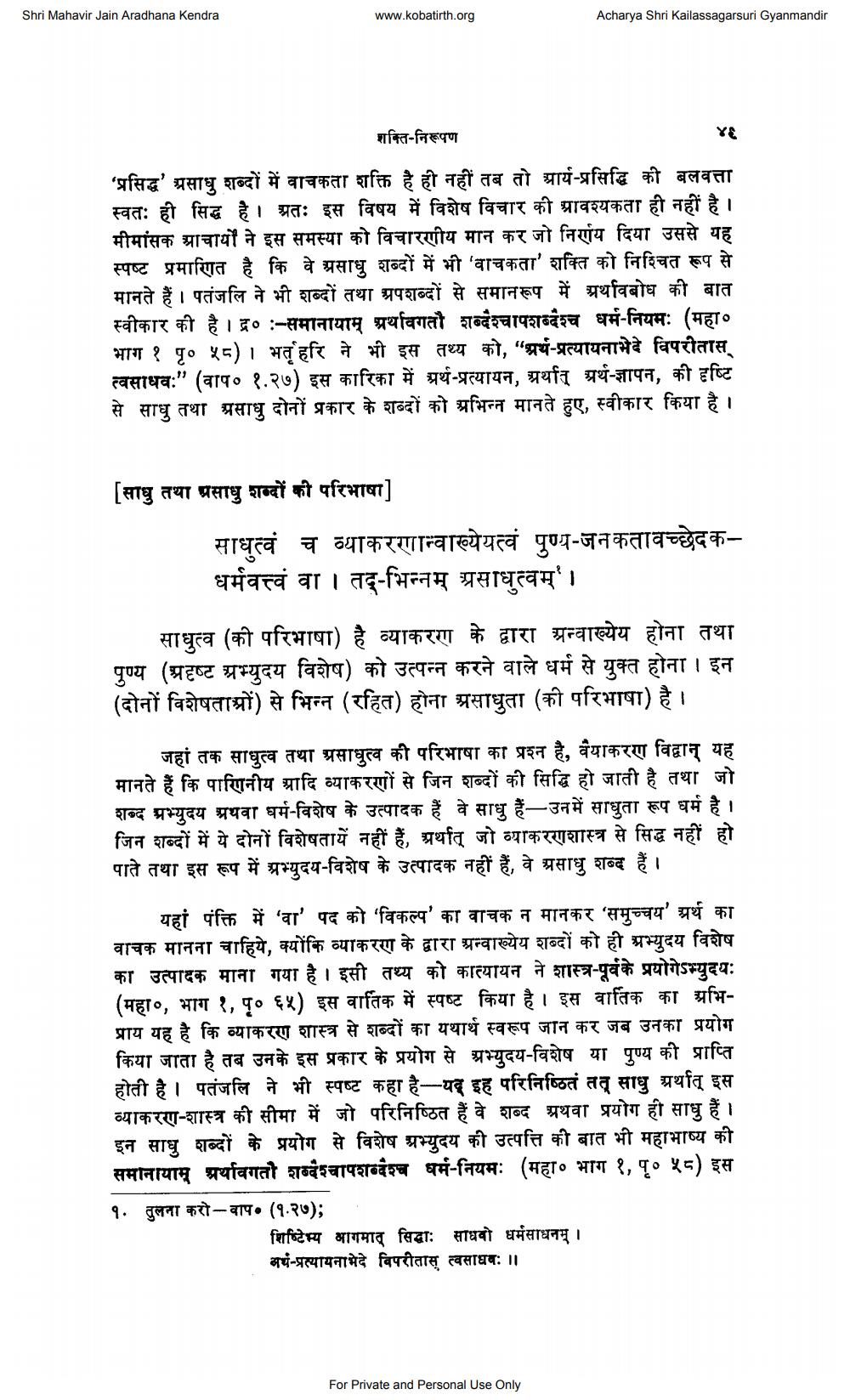________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
शक्ति-निरूपण
'प्रसिद्ध' असाधु शब्दों में वाचकता शक्ति है ही नहीं तब तो आर्य-प्रसिद्धि की बलवत्ता स्वतः ही सिद्ध है। अतः इस विषय में विशेष विचार की आवश्यकता ही नहीं है। मीमांसक आचार्यों ने इस समस्या को विचारणीय मान कर जो निर्णय दिया उससे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि वे असाधु शब्दों में भी 'वाचकता' शक्ति को निश्चित रूप से मानते हैं । पतंजलि ने भी शब्दों तथा अपशब्दों से समानरूप में अर्थावबोध की बात स्वीकार की है। द्र० :-समानायाम् अर्थावगतौ शब्दश्चापशब्देश्च धर्म-नियमः (महा. भाग १ पृ० ५८)। भर्तृहरि ने भी इस तथ्य को, "अर्थ-प्रत्यायनाभेदे विपरीतास त्वसाधवः" (वाप० १.२७) इस कारिका में अर्थ-प्रत्यायन, अर्थात् अर्थ-ज्ञापन, की दृष्टि से साधु तथा असाधु दोनों प्रकार के शब्दों को अभिन्न मानते हुए, स्वीकार किया है।
[साधु तथा प्रसाधु शब्दों की परिभाषा]
साधुत्वं च व्याकरणान्वाख्येयत्वं पुण्य-जनकतावच्छेदक
धर्मवत्त्वं वा । तद्-भिन्नम् असाधुत्वम् । साधुत्व (की परिभाषा) है व्याकरण के द्वारा अन्वाख्येय होना तथा पुण्य (अदृष्ट अभ्युदय विशेष) को उत्पन्न करने वाले धर्म से युक्त होना । इन (दोनों विशेषताओं) से भिन्न (रहित) होना असाधुता (की परिभाषा) है।
जहां तक साधुत्व तथा असाधुत्व की परिभाषा का प्रश्न है, वैयाकरण विद्वान् यह मानते हैं कि पाणिनीय आदि व्याकरणों से जिन शब्दों की सिद्धि हो जाती है तथा जो शब्द अभ्युदय अथवा धर्म-विशेष के उत्पादक हैं वे साधु हैं-उनमें साधुता रूप धर्म है। जिन शब्दों में ये दोनों विशेषतायें नहीं हैं, अर्थात् जो व्याकरणशास्त्र से सिद्ध नहीं हो पाते तथा इस रूप में अभ्युदय-विशेष के उत्पादक नहीं हैं, वे असाधु शब्द हैं।
यहां पंक्ति में 'वा' पद को 'विकल्प' का वाचक न मानकर 'समुच्चय' अर्थ का वाचक मानना चाहिये, क्योंकि व्याकरण के द्वारा अन्वाख्येय शब्दों को ही अभ्युदय विशेष का उत्पादक माना गया है। इसी तथ्य को कात्यायन ने शास्त्र-पूर्वके प्रयोगेऽभ्युदयः (महा०, भाग १, पृ० ६५) इस वार्तिक में स्पष्ट किया है। इस वार्तिक का अभिप्राय यह है कि व्याकरण शास्त्र से शब्दों का यथार्थ स्वरूप जान कर जब उनका प्रयोग किया जाता है तब उनके इस प्रकार के प्रयोग से अभ्युदय-विशेष या पुण्य की प्राप्ति होती है। पतंजलि ने भी स्पष्ट कहा है-यद् इह परिनिष्ठितं तत् साधु अर्थात् इस व्याकरण-शास्त्र की सीमा में जो परिनिष्ठित हैं वे शब्द अथवा प्रयोग ही साधु हैं। इन साधु शब्दों के प्रयोग से विशेष अभ्युदय की उत्पत्ति की बात भी महाभाष्य की समानायाम् अर्थावगतो शब्दश्चापशब्देश्च धर्म-नियमः (महा० भाग १, पृ० ५८) इस १. तुलना करो-वाप० (१.२७);
शिष्टेिभ्य भागमात् सिद्धा: साधवो धर्मसाधनम् । अर्थ-प्रत्यायनाभेदे विपरीतास् त्वसाधवः ।।
For Private and Personal Use Only