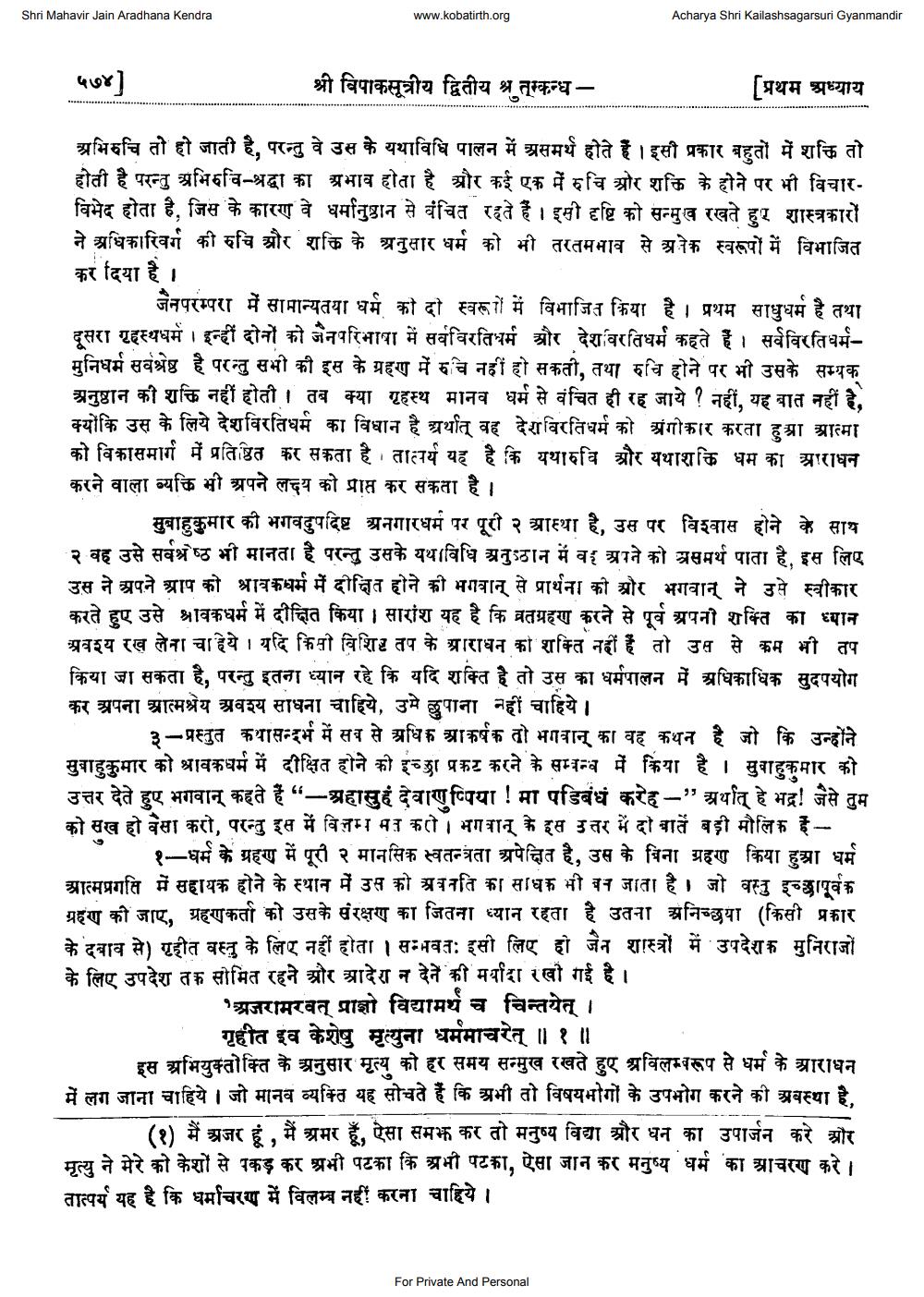________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailashsagarsuri Gyanmandir
५७४ ]
श्री विपाकसूत्रीय द्वितीय श्र तुम्कन्ध
[प्रथम अध्याय
अभिरुचि तो हो जाती है, परन्तु वे उस के यथाविधि पालन में असमर्थ होते हैं । इसी प्रकार बहुतों में शक्ति तो होती है परन्तु अभिरुचि श्रद्धा का अभाव होता है और कई एक में रुचि ओर शक्ति के होने पर भी विचारविभेद होता है, जिस के कारण वे धर्मानुष्ठान से वंचित रहते हैं। इसी दृष्टि को सन्मुख रखते हुए शास्त्रकारों अधिकारिवर्ग की रुचि और शक्ति के अनुसार धर्म को भी तरतमभाव से अनेक स्वरूपों कर दिया है ।
विभाजित
जैनपरम्परा में सामान्यतया धर्म को दो स्वरूपों में विभाजित किया है। प्रथम साधुधर्म है तथा दूसरा गृहस्थधर्मे । इन्हीं दोनों को जैनपरिभाषा में सर्वविरतिधर्म और देशविरतिधर्म कहते हैं । सर्वविरतिधर्मधर्म सर्वश्रेष्ठ है परन्तु सभी की इस के ग्रहण में रुचि नहीं हो सकती, तथा रुचि होने पर भी उसके सम्यक अनुष्ठान की शक्ति नहीं होती। तब क्या गृहस्थ मानव धर्म से वंचित ही रह जाये ? नहीं, यह बात नहीं है, क्योंकि उस के लिये देशविरतिधर्म का विधान है अर्थात् वह देशविरतिधर्म को अंगीकार करता हुआ आत्मा को विकासमार्ग में प्रतिष्ठित कर सकता है। तालर्य यह है कि यथादवि और यथाशक्ति धर्म का आराधन करने वाला व्यक्ति भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
I
सुबाहुकुमार की भगवदुपदिष्ट अनगारधर्म पर पूरी २ आस्था है, उस पर विश्वास होने के साथ २ वह उसे सर्वश्रेष्ठ भी मानता है परन्तु उसके यथाविधि अनुष्ठान में वह अपने को असमर्थ पाता है, इस लिए उसने अपने आप को श्रावकधर्म में दीक्षित होने की भगवान् से प्रार्थना की और भगवान् ने उसे स्वीकार करते हुए उसे श्रावकधर्म में दीक्षित किया। सारांश यह है व्रतग्रहण करने से पूर्व अपनी शक्ति का ध्यान अवश्य रख लेना चाहेये । यदि किसी विशिष्ट तप के प्राराधन को शक्ति नहीं हैं तो उस से कम भी तप किया जा सकता है, परन्तु इतना ध्यान रहे कि यदि शक्ति है तो उस का धर्मपालन में अधिकाधिक सुदपयोग कर अपना श्रात्मश्रेय अवश्य साधना चाहिये, उमे
छुपाना नहीं चाहिये।
1
७
३ - प्रस्तुत कथा सन्दर्भ में सब से अधिक आकर्षक तो भगवान् का वह कथन है जो कि उन्होंने सुबाहुकुमार को श्रावकधर्म में दीक्षित होने की इच्छा प्रकट करने के सम्बन्ध में किया है | सुबाहुकुमार को उत्तर देते हुए भगवान् कहते हैं " - श्रहासुहं देवाप्पिया ! मा पडिबंधं करोह - " अर्थात् हे भद्र! जैसे तुम को सख हो वैसा करो, परन्तु इस में विलम्भ मत करो । भगवान् के इस उत्तर में दो बातें बड़ी मौलिक ६ - १ – धर्म के ग्रहण में पूरी २ मानसिक स्वतन्त्रता अपेक्षित है, उस के बिना ग्रहण किया हुआ धर्म आत्मप्रगति में सहायक होने के स्थान में उस को अवनति का साधक भी बन जाता है । जो वस्तु इच्छापूर्वक ग्रहण की जाए, ग्रहणकर्ता को उसके संरक्षण का जितना ध्यान रहता है उतना अनिच्छया (किसी प्रकार के दबाव से) गृहीत वस्तु के लिए नहीं होता । सम्भवत: इसी लिए हो जैन शास्त्रों में उपदेशक मुनिराजों के लिए उपदेश तक सीमित रहने और आदेश न देने की मर्यादा रखी गई है।
'अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् । गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥ १ ॥
इस अभियुक्तोक्ति के अनुसार मृत्यु को हर समय सन्मुख रखते हुए श्रविलम्वरूप से धर्म के आराधन
में लग जाना चाहिये । जो मानव व्यक्ति यह सोचते हैं कि अभी तो विषयभोगों के उपभोग करने की अवस्था है, (१) मैं जर हूं, मैं अमर हूँ, ऐसा समझ कर तो मनुष्य विद्या और धन का उपार्जन करे और मृत्यु ने मेरे को केशों से पकड़ कर अभी पटका कि अभी पटका, ऐसा जान कर मनुष्य धर्म का आचरण करे । तात्पर्य यह है कि धर्माचरण में विलम्ब नहीं करना चाहिये ।
For Private And Personal