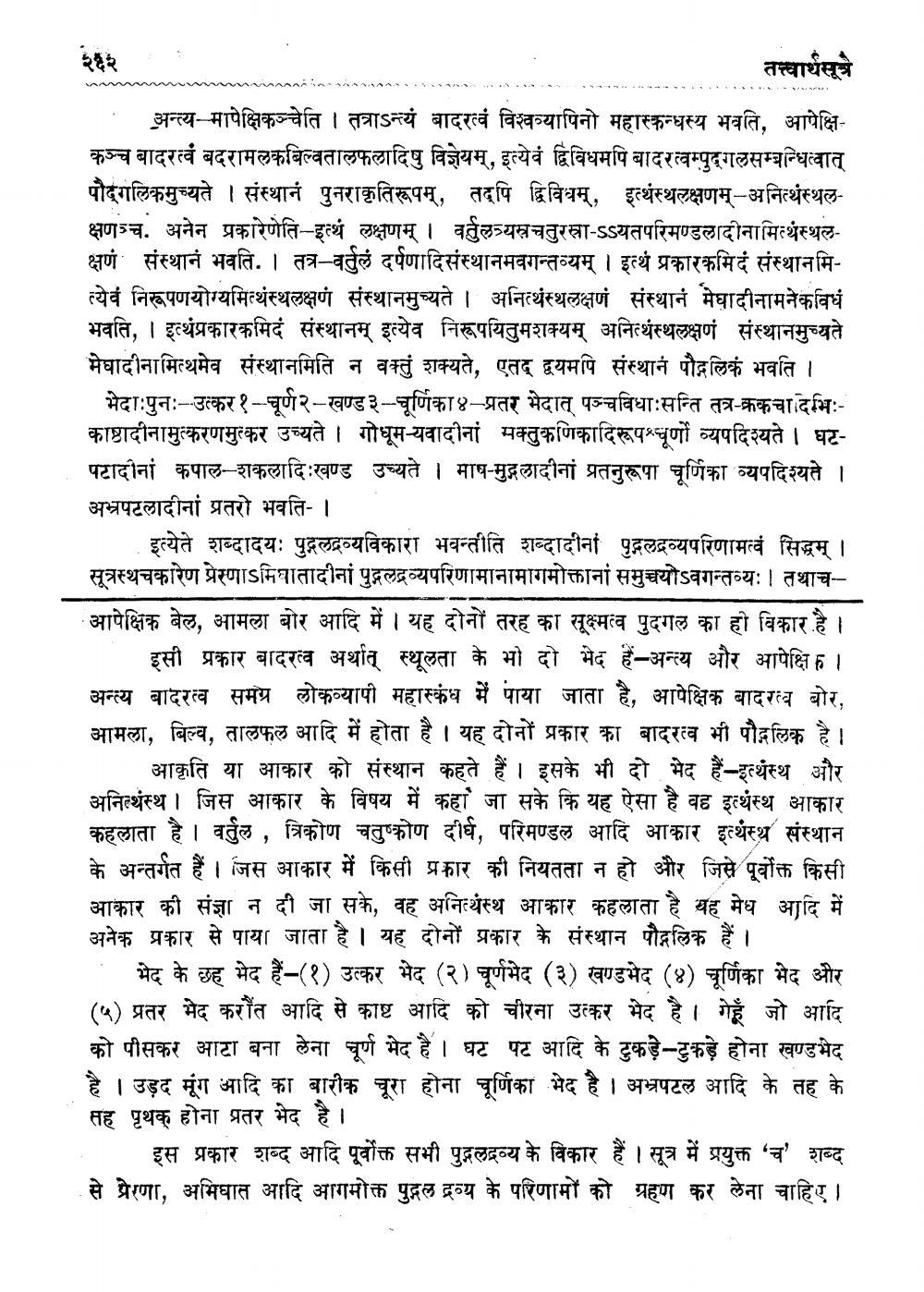________________
तत्त्वार्थसूत्रे - अन्त्य-मापेक्षिकञ्चेति । तत्राऽन्यं बादरत्वं विश्वव्यापिनो महास्कन्धस्य भवति, आपेक्षिकञ्च बादरत्वं बदरामलकबिल्वतालफलादिषु विज्ञेयम्, इत्येवं द्विविधमपि बादरत्वम्पुद्गलसम्बन्धित्वात् पौद्गलिकमुच्यते । संस्थानं पुनराकृतिरूपम्, तदपि द्विविधम्, इत्थंस्थलक्षणम्-अनित्थंस्थलक्षणच. अनेन प्रकारेणेति-इत्थं लक्षणम् । वर्तुलत्र्यसूचतुरस्रा-ऽऽयतपरिमण्डलादीनामित्थंस्थलक्षणं संस्थानं भवति. । तत्र-वर्तुलं दर्पणादिसंस्थानमवगन्तव्यम् । इत्थं प्रकारकमिदं संस्थानमित्येवं निरूपणयोग्यमित्थंस्थलक्षणं संस्थानमुच्यते । अनित्थंस्थलक्षणं संस्थानं मेघादीनामनेकविधं भवति, । इत्थंप्रकारकमिदं संस्थानम् इत्येव निरूपयितुमशक्यम् अनित्थंस्थलक्षणं संस्थानमुच्यते मेघादीनामित्थमेव संस्थानमिति न वक्तुं शक्यते, एतद् द्वयमपि संस्थानं पौद्गलिकं भवति ।
भेदाःपुनः--उत्कर १-चूर्ण२-खण्ड३-चूर्णिका ४-प्रतर भेदात् पञ्चविधाःसन्ति तत्र-क्रकचा देभिःकाष्ठादीनामुत्करणमुत्कर उच्यते । गोधूम-यवादीनां मक्तुकणिकादिरूपश्चूर्णो व्यपदिश्यते । घटपटादीनां कपाल-शकलादिःखण्ड उच्यते । माष-मुद्गलादीनां प्रतनुरूपा चूर्णिका व्यपदिश्यते । अभ्रपटलादीनां प्रतरो भवति- ।
. इत्येते शब्दादयः पुद्गलद्रव्यविकारा भवन्तीति शब्दादीनां पुद्गलद्रव्यपरिणामत्वं सिद्धम् । सूत्रस्थचकारेण प्रेरणाऽमिघातादीनां पुद्गलद्रव्यपरिणामानामागमोक्तानां समुच्चयोऽवगन्तव्यः । तथाचआपेक्षिक बेल, आमला बोर आदि में । यह दोनों तरह का सूक्ष्मत्व पुदगल का हो विकार है।
इसी प्रकार बादरत्व अर्थात् स्थूलता के भो दो भेद हैं-अन्त्य और आपेक्षिक । अन्त्य बादरत्व समग्र लोकव्यापी महास्कंध में पाया जाता है, आपेक्षिक बादरत्व बोर, आमला, बिल्व, तालफल आदि में होता है । यह दोनों प्रकार का बादरत्व भी पौद्गलिक है। ___आकृति या आकार को संस्थान कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं-इत्थंस्थ और अनित्थंस्थ। जिस आकार के विषय में कहाँ जा सके कि यह ऐसा है वह इत्थंस्थ आकार कहलाता है। वर्तुल , त्रिकोण चतुष्कोण दीर्घ, परिमण्डल आदि आकार इत्थंस्थ संस्थान के अन्तर्गत हैं। जिस आकार में किसी प्रकार की नियतता न हो और जिसे पूर्वोक्त किसी आकार की संज्ञा न दी जा सके, वह अनित्यंस्थ आकार कहलाता है यह मेध आदि में अनेक प्रकार से पाया जाता है । यह दोनों प्रकार के संस्थान पौद्गलिक हैं। - भेद के छह भेद हैं-(१) उत्कर भेद (२) चूर्णभेद (३) खण्डभेद (४) चूर्णिका भेद और (५) प्रतर भेद करौंत आदि से काष्ट आदि को चीरना उत्कर भेद है। गेहूँ जो आदि को पीसकर आटा बना लेना चूर्ण भेद है। घट पट आदि के टुकड़े-टुकड़े होना खण्डभेद है । उड़द मूंग आदि का बारीक चूरा होना चूर्णिका भेद है । अभ्रपटल आदि के तह के सह पृथक् होना प्रतर भेद है।
इस प्रकार शब्द आदि पूर्वोक्त सभी पुद्गलद्रव्य के विकार हैं। सूत्र में प्रयुक्त 'च' शब्द से प्रेरणा, अमिघात आदि आगमोक्त पुद्गल द्रव्य के परिणामों को ग्रहण कर लेना चाहिए ।