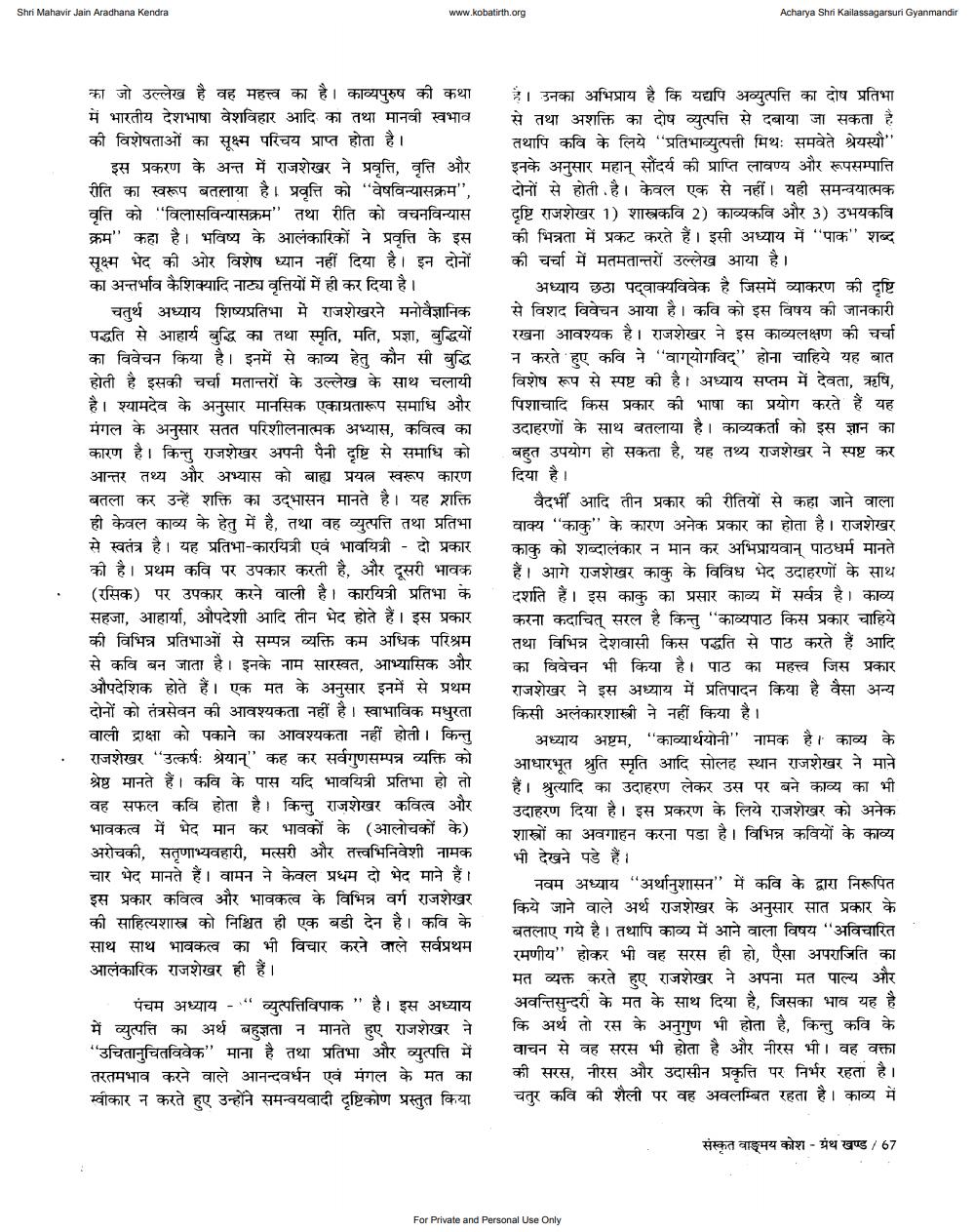________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
का जो उल्लेख है वह महत्त्व का है। काव्यपुरुष की कथा में भारतीय देशभाषा वेशविहार आदि का तथा मानवी स्वभाव की विशेषताओं का सूक्ष्म परिचय प्राप्त होता है ।
इस प्रकरण के अन्त में राजशेखर ने प्रवृत्ति, वृत्ति और रीति का स्वरूप बतलाया है। प्रवृत्ति को "वेषविन्यासक्रम ", वृत्ति को "विलासविन्यासक्रम तथा रीति को वचनविन्यास क्रम" कहा है। भविष्य के आलंकारिकों ने प्रवृत्ति के इस सूक्ष्म भेद की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। इन दोनों का अन्तर्भाव कैशिक्यादि नाट्य वृत्तियों में ही कर दिया है।
चतुर्थ अध्याय शिष्यप्रतिभा में राजशेखरने मनोवैज्ञानिक पद्धति से आहार्य बुद्धि का तथा स्मृति, मति, प्रज्ञा, बुद्धियों का विवेचन किया है। इनमें से काव्य हेतु कौन सी बुद्धि होती है इसकी चर्चा मतान्तरों के उल्लेख के साथ चलायी है। श्यामदेव के अनुसार मानसिक एकाग्रतारूप समाधि और मंगल के अनुसार सतत परिशीलनात्मक अभ्यास, कवित्व का कारण है। किन्तु राजशेखर अपनी पैनी दृष्टि से समाधि को आन्तर तथ्य और अभ्यास को बाह्य प्रयत्न स्वरूप कारण बतला कर उन्हें शक्ति का उद्भासन मानते है। यह शक्ति ही केवल काव्य के हेतु में है, तथा वह व्युत्पत्ति तथा प्रतिभा से स्वतंत्र है। यह प्रतिभा - कारयित्री एवं भावयित्री - दो प्रकार की है। प्रथम कवि पर उपकार करती है, और दूसरी भावक (रसिक) पर उपकार करने वाली है। कारयित्री प्रतिभा के सहजा, आहार्या, औपदेशी आदि तीन भेद होते हैं । इस प्रकार की विभिन्न प्रतिभाओं से सम्पन्न व्यक्ति कम अधिक परिश्रम से कवि बन जाता है। इनके नाम सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक होते हैं । एक मत के अनुसार इनमें से प्रथम दोनों को तंत्रसेवन की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक मधुरता वाली द्राक्षा को पकाने का आवश्यकता नहीं होती। किन्तु राजशेखर "उत्कर्षः श्रेयान्" कह कर सर्वगुणसम्पन्न व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं । कवि के पास यदि भावयित्री प्रतिभा हो तो वह सफल कवि होता है किन्तु राजशेखर कवित्व और भावकत्व में भेद मान कर भावकों के (आलोचकों के) अरोचकी, सतॄणाभ्यवहारी, मत्सरी और तत्त्वभिनिवेशी नामक चार भेद मानते हैं। वामन ने केवल प्रथम दो भेद माने हैं। इस प्रकार कवित्व और भावकत्व के विभिन्न वर्ग राजशेखर की साहित्यशास्त्र को निश्चित ही एक बडी देन है । कवि के साथ साथ भावकत्व का भी विचार करने वाले सर्वप्रथम आलंकारिक राजशेखर ही हैं।
पंचम अध्याय - " व्युत्पत्तिविपाक " है। इस अध्याय में व्युत्पत्ति का अर्थ बहुशता न मानते हुए राजशेखर ने "उचितानुचितविवेक" माना है तथा प्रतिभा और व्युत्पत्ति में तरतमभाव करने वाले आनन्दवर्धन एवं मंगल के मत का स्वीकार न करते हुए उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
। उनका अभिप्राय है कि यद्यपि अव्युत्पत्ति का दोष प्रतिभा से तथा अशक्ति का दोष व्युत्पत्ति से दबाया जा सकता है तथापि कवि के लिये "प्रतिभाव्युत्पत्ती मिथः समवेते श्रवस्या" इनके अनुसार महान् सौंदर्य की प्राप्ति लावण्य और रूपसम्पात्ति दोनों से होती है। केवल एक से नहीं। यही समन्वयात्मक दृष्टि राजशेखर 1) शास्त्रकवि 2) काव्यकवि और 3) उभयकवि की भिन्नता में प्रकट करते हैं। इसी अध्याय में "पाक" शब्द की चर्चा में मतमतान्तरों उल्लेख आया है।
अध्याय छठा पवाक्यविवेक है जिसमें व्याकरण की दृष्टि से विशद विवेचन आया है। कवि को इस विषय की जानकारी रखना आवश्यक है। राजशेखर ने इस काव्यलक्षण की चर्चा न करते हुए कवि ने "वाग्योगविद्" होना चाहिये यह बात विशेष रूप से स्पष्ट की है। अध्याय सप्तम में देवता, ऋषि, पिशाचादि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं यह उदाहरणों के साथ बतलाया है। काव्यकर्ता को इस ज्ञान का बहुत उपयोग हो सकता है, यह तथ्य राजशेखर ने स्पष्ट कर दिया है।
वैदर्भी आदि तीन प्रकार की रीतियों से कहा जाने वाला वाक्य "काकु" के कारण अनेक प्रकार का होता है। राजशेखर काकु को शब्दालंकार न मान कर अभिप्रायवान् पाठधर्म मानते हैं। आगे राजशेखर काकु के विविध भेद उदाहरणों के साथ दर्शाते हैं । इस काकु का प्रसार काव्य में सर्वत्र है । काव्य करना कदाचित् सरल है किन्तु "काव्यपाठ किस प्रकार चाहिये तथा विभिन्न देशवासी किस पद्धति से पाठ करते हैं आदि का विवेचन भी किया है। पाठ का महत्त्व जिस प्रकार राजशेखर ने इस अध्याय में प्रतिपादन किया है वैसा अन्य किसी अलंकारशास्त्री ने नहीं किया है ।
अध्याय अष्टम, "काव्यार्थयोनी" नामक है। काव्य के आधारभूत श्रुति स्मृति आदि सोलह स्थान राजशेखर ने माने हैं । श्रुत्यादि का उदाहरण लेकर उस पर बने काव्य का भी उदाहरण दिया है। इस प्रकरण के लिये राजशेखर को अनेक शास्त्रों का अवगाहन करना पड़ा है। विभिन्न कवियों के काव्य भी देखने पड़े हैं।
नवम अध्याय " अर्थानुशासन" में कवि के द्वारा निरूपित किये जाने वाले अर्थ राजशेखर के अनुसार सात प्रकार के बतलाए गये है । तथापि काव्य में आने वाला विषय "अविचारित रमणीय" होकर भी वह सरस ही हो, ऐसा अपराजिति का मत व्यक्त करते हुए राजशेखर ने अपना मत पाल्य और अवन्तिसुन्दरी के मत के साथ दिया है, जिसका भाव यह है कि अर्थ तो रस के अनुगुण भी होता है, किन्तु कवि के वाचन से वह सरस भी होता है और नीरस भी। वह वक्ता की सरस, नीरस और उदासीन प्रकृत्ति पर निर्भर रहता है। चतुर कवि की शैली पर वह अवलम्बित रहता है। काव्य में
संस्कृत वाङ्मय कोश ग्रंथ खण्ड / 67
For Private and Personal Use Only