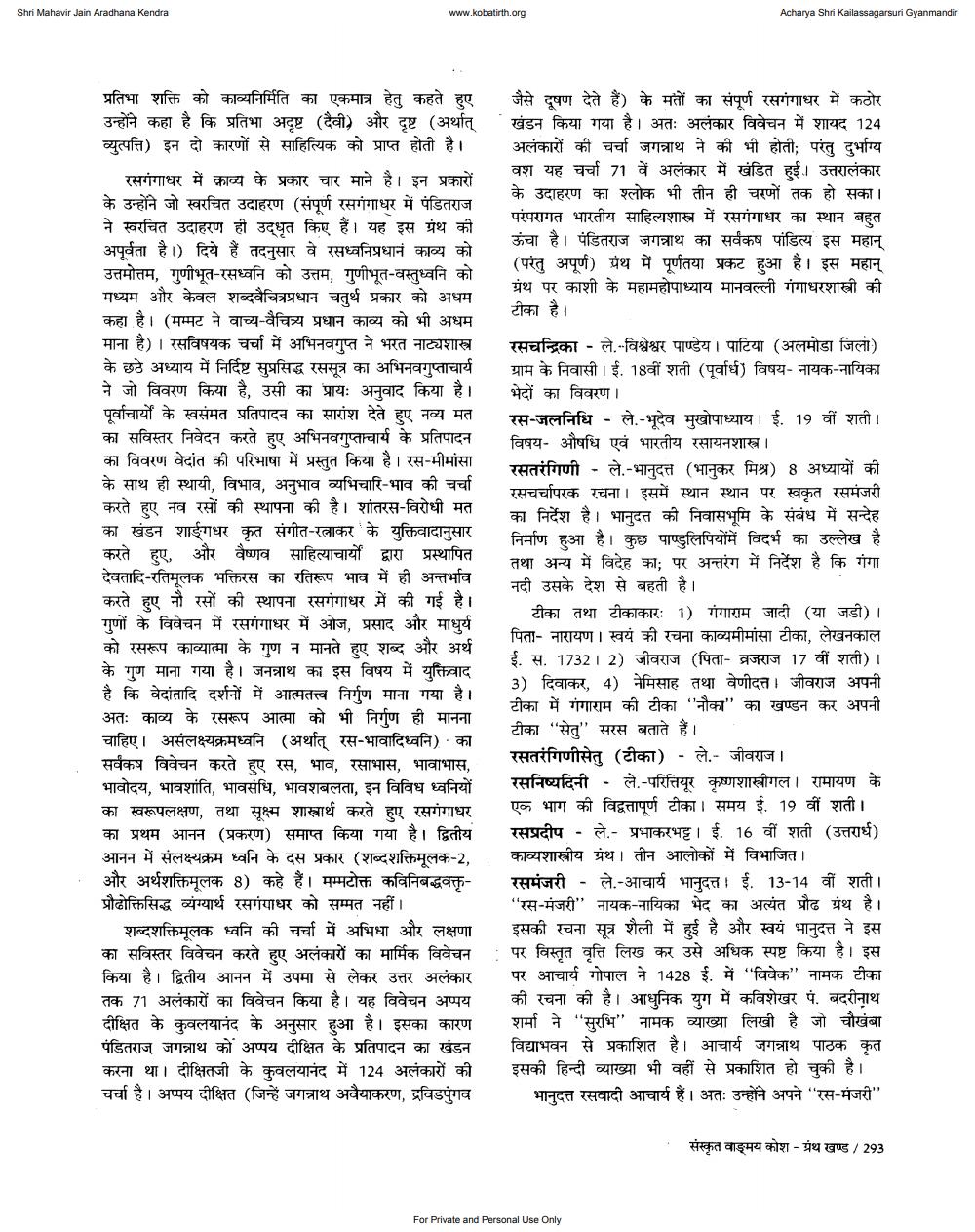________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
प्रतिभा शक्ति को काव्यनिर्मिति का एकमात्र हेतु कहते हुए जैसे दूषण देते हैं) के मतों का संपूर्ण रसगंगाधर में कठोर उन्होंने कहा है कि प्रतिभा अदृष्ट (दैवी) और दृष्ट (अर्थात् खंडन किया गया है। अतः अलंकार विवेचन में शायद 124 व्युत्पत्ति) इन दो कारणों से साहित्यिक को प्राप्त होती है। अलंकारों की चर्चा जगन्नाथ ने की भी होती; परंतु दुर्भाग्य रसगंगाधर में काव्य के प्रकार चार माने है। इन प्रकारों
वश यह चर्चा 71 वें अलंकार में खंडित हुई। उत्तरालंकार
के उदाहरण का श्लोक भी तीन ही चरणों तक हो सका। के उन्होंने जो स्वरचित उदाहरण (संपूर्ण रसगंगाधर में पंडितराज ने स्वरचित उदाहरण ही उद्धृत किए हैं। यह इस ग्रंथ की
परंपरागत भारतीय साहित्यशास्त्र में रसगंगाधर का स्थान बहुत अपूर्वता है।) दिये हैं तदनुसार वे रसध्वनिप्रधान काव्य को
ऊंचा है। पंडितराज जगन्नाथ का सर्वकष पांडित्य इस महान् उत्तमोत्तम, गुणीभूत-रसध्वनि को उत्तम, गुणीभूत-वस्तुध्वनि को
(परंतु अपूर्ण) ग्रंथ में पूर्णतया प्रकट हुआ है। इस महान्
ग्रंथ पर काशी के महामहोपाध्याय मानवल्ली गंगाधरशास्त्री की मध्यम और केवल शब्दवैचित्रप्रधान चतुर्थ प्रकार को अधम
टीका है। कहा है। (मम्मट ने वाच्य-वैचित्र्य प्रधान काव्य को भी अधम माना है)। रसविषयक चर्चा में अभिनवगुप्त ने भरत नाट्यशास्त्र रसचन्द्रिका - ले.-विश्वेश्वर पाण्डेय। पाटिया (अलमोडा जिला) के छठे अध्याय में निर्दिष्ट सुप्रसिद्ध रससूत्र का अभिनवगुप्ताचार्य ग्राम के निवासी। ई. 18वीं शती (पूर्वार्ध) विषय- नायक-नायिका ने जो विवरण किया है, उसी का प्रायः अनुवाद किया है। भेदों का विवरण। पूर्वाचार्यों के स्वसंमत प्रतिपादन का सारांश देते हुए नव्य मत रस-जलनिधि - ले.-भूदेव मुखोपाध्याय। ई. 19 वीं शती। का सविस्तर निवेदन करते हए अभिनवगप्ताचार्य के प्रतिपादन
विषय- औषधि एवं भारतीय रसायनशास्त्र । का विवरण वेदांत की परिभाषा में प्रस्तुत किया है। रस-मीमांसा
रसतरंगिणी - ले.-भानुदत्त (भानुकर मिश्र) 8 अध्यायों की के साथ ही स्थायी, विभाव, अनुभाव व्यभिचारि-भाव की चर्चा
रसचर्चापरक रचना। इसमें स्थान स्थान पर स्वकृत रसमंजरी करते हुए नव रसों की स्थापना की है। शांतरस-विरोधी मत
का निर्देश है। भानुदत्त की निवासभूमि के संबंध में सन्देह का खंडन शागधर कृत संगीत-रत्नाकर के युक्तिवादानुसार
निर्माण हुआ है। कुछ पाण्डुलिपियोंमें विदर्भ का उल्लेख है करते हुए, और वैष्णव साहित्याचार्यों द्वारा प्रस्थापित
तथा अन्य में विदेह का; पर अन्तरंग में निर्देश है कि गंगा देवतादि-रतिमूलक भक्तिरस का रतिरूप भाव में ही अन्तर्भाव
नदी उसके देश से बहती है। करते हुए नौ रसों की स्थापना रसगंगाधर में की गई है।
टीका तथा टीकाकारः 1) गंगाराम जादी (या जडी)। गुणों के विवेचन में रसगंगाधर में ओज, प्रसाद और माधुर्य
पिता- नारायण। स्वयं की रचना काव्यमीमांसा टीका, लेखनकाल को रसरूप काव्यात्मा के गुण न मानते हुए शब्द और अर्थ
ई. स. 1732 1 2) जीवराज (पिता- व्रजराज 17 वीं शती)। के गुण माना गया है। जनन्नाथ का इस विषय में युक्तिवाद
3) दिवाकर, 4) नेमिसाह तथा वेणीदत्त। जीवराज अपनी है कि वेदांतादि दर्शनों में आत्मतत्त्व निर्गुण माना गया है।
टीका में गंगाराम की टीका "नौका" का खण्डन कर अपनी अतः काव्य के रसरूप आत्मा को भी निर्गुण ही मानना
टीका "सेतु" सरस बताते हैं। चाहिए। असंलक्ष्यक्रमध्वनि (अर्थात् रस-भावादिध्वनि) · का सर्वकष विवेचन करते हुए रस, भाव, रसाभास, भावाभास,
रसतरंगिणीसेतु (टीका) - ले.- जीवराज । भावोदय, भावशांति, भावसंधि, भावशबलता, इन विविध ध्वनियों
रसनिष्यदिनी - ले.-परित्तियूर कृष्णशास्त्रीगल। रामायण के का स्वरूपलक्षण, तथा सूक्ष्म शास्त्रार्थ करते हुए रसगंगाधर
एक भाग की विद्वत्तापूर्ण टीका। समय ई. 19 वीं शती। का प्रथम आनन (प्रकरण) समाप्त किया गया है। द्वितीय रसप्रदीप - ले.- प्रभाकरभट्ट। ई. 16 वीं शती (उत्तरार्ध) आनन में संलक्ष्यक्रम ध्वनि के दस प्रकार (शब्दशक्तिमूलक-2, . काव्यशास्त्रीय ग्रंथ। तीन आलोकों में विभाजित। और अर्थशक्तिमूलक 8) कहे हैं। मम्मटोक्त कविनिबद्धवक्तृ- रसमंजरी - ले.-आचार्य भानुदत्त। ई. 13-14 वीं शती। प्रौढोक्तिसिद्ध व्यंग्यार्थ रसगंगाधर को सम्मत नहीं।
"रस-मंजरी" नायक-नायिका भेद का अत्यंत प्रौढ ग्रंथ है। शब्दशक्तिमूलक ध्वनि की चर्चा में अभिधा और लक्षणा इसकी रचना सूत्र शैली में हुई है और स्वयं भानुदत्त ने इस का सविस्तर विवेचन करते हुए अलंकारों का मार्मिक विवेचन : पर विस्तृत वृत्ति लिख कर उसे अधिक स्पष्ट किया है। इस किया है। द्वितीय आनन में उपमा से लेकर उत्तर अलंकार पर आचार्य गोपाल ने 1428 ई. में "विवेक" नामक टीका तक 71 अलंकारों का विवेचन किया है। यह विवेचन अप्पय की रचना की है। आधुनिक युग में कविशेखर पं. बदरीनाथ दीक्षित के कुवलयानंद के अनुसार हुआ है। इसका कारण शर्मा ने "सुरभि" नामक व्याख्या लिखी है जो चौखंबा पंडितराज जगन्नाथ को अप्पय दीक्षित के प्रतिपादन का खंडन विद्याभवन से प्रकाशित है। आचार्य जगन्नाथ पाठक कृत करना था। दीक्षितजी के कुवलयानंद में 124 अलंकारों की इसकी हिन्दी व्याख्या भी वहीं से प्रकाशित हो चुकी है। चर्चा है। अप्पय दीक्षित (जिन्हें जगन्नाथ अवैयाकरण, द्रविडपुंगव भानुदत्त रसवादी आचार्य हैं। अतः उन्होंने अपने "रस-मंजरी"
संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथ खण्ड / 293
For Private and Personal Use Only