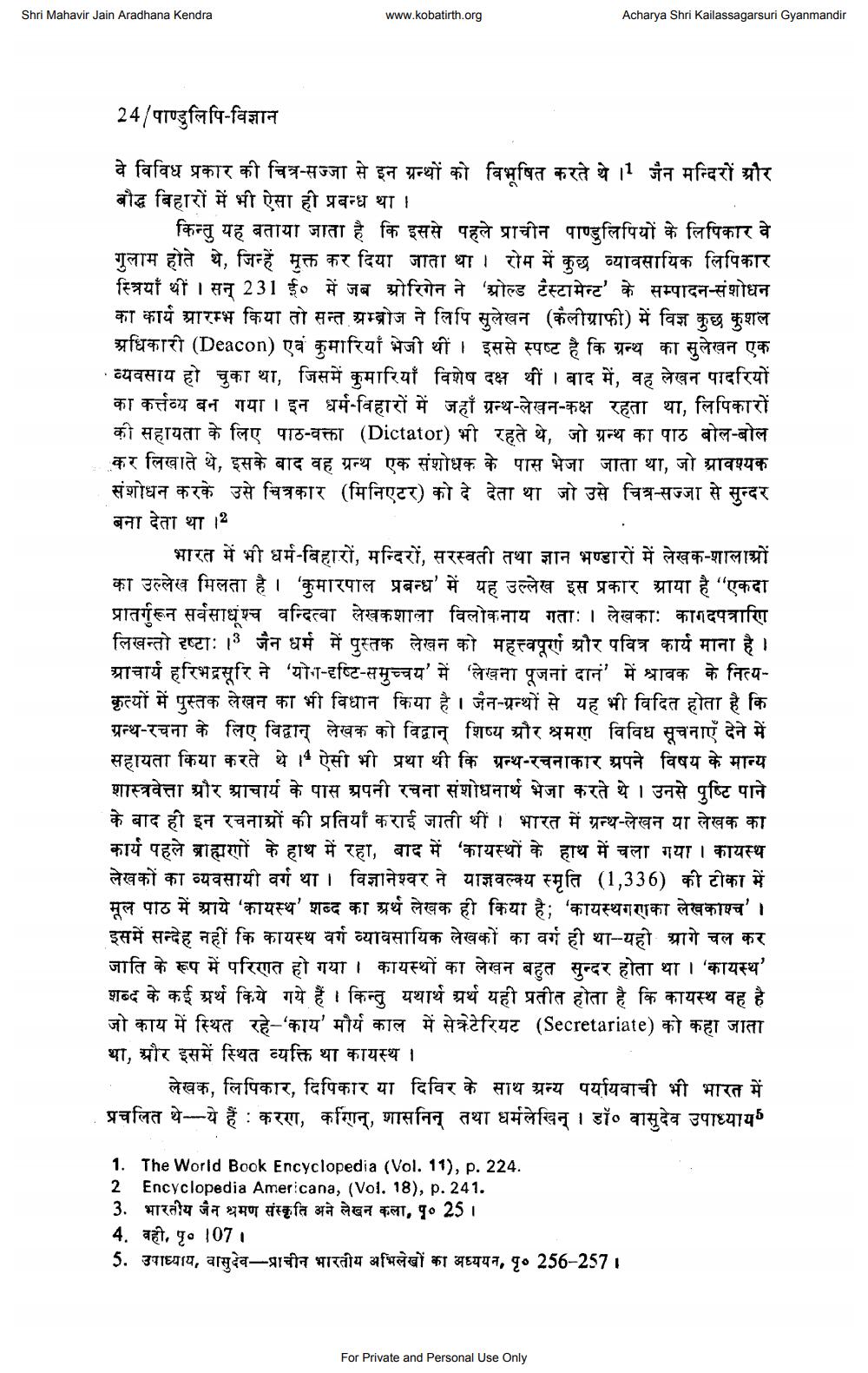________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
24/पाण्डुलिपि-विज्ञान
वे विविध प्रकार की चित्र-सज्जा से इन ग्रन्थों को विभूषित करते थे ।। जैन मन्दिरों और बौद्ध बिहारों में भी ऐसा ही प्रबन्ध था ।
किन्तु यह बताया जाता है कि इससे पहले प्राचीन पाण्डुलिपियों के लिपिकार वे गुलाम होते थे, जिन्हें मुक्त कर दिया जाता था। रोम में कुछ व्यावसायिक लिपिकार स्त्रियाँ थीं । सन् 231 ई० में जब ओरिगेन ने 'ओल्ड टेस्टामेन्ट' के सम्पादन-संशोधन का कार्य प्रारम्भ किया तो सन्त अम्ब्रोज ने लिपि सुलेखन (कैलीग्राफी) में विज्ञ कुछ कुशल अधिकारी (Deacon) एवं कुमारियाँ भेजी थीं। इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थ का सुलेखन एक • व्यवसाय हो चुका था, जिसमें कुमारियाँ विशेष दक्ष थीं। बाद में, वह लेखन पादरियों का कर्तव्य बन गया । इन धर्म-विहारों में जहाँ ग्रन्थ-लेखन-कक्ष रहता था, लिपिकारों की सहायता के लिए पाठ-वक्ता (Dictator) भी रहते थे, जो ग्रन्थ का पाठ बोल-बोल कर लिखाते थे, इसके बाद वह ग्रन्थ एक संशोधक के पास भेजा जाता था, जो अावश्यक संशोधन करके उसे चित्रकार (मिनिएटर) को दे देता था जो उसे चित्र-सज्जा से सुन्दर बना देता था।
भारत में भी धर्म-बिहारों, मन्दिरों, सरस्वती तथा ज्ञान भण्डारों में लेखक-शालाओं का उल्लेख मिलता है । 'कुमारपाल प्रबन्ध' में यह उल्लेख इस प्रकार आया है “एकदा प्रातर्गुरून सर्वसाधूंश्च वन्दित्वा लेखकशाला विलोकनाय गताः । लेखकाः कागदपत्राणि लिखन्तो रष्टाः । जैन धर्म में पुस्तक लेखन को महत्त्वपूर्ण और पवित्र कार्य माना है। आचार्य हरिभद्रसूरि ने 'योग-दृष्टि-समुच्चय' में 'लेखना पूजनां दानं' में श्रावक के नित्यकृत्यों में पुस्तक लेखन का भी विधान किया है । जैन-ग्रन्थों से यह भी विदित होता है कि ग्रन्थ-रचना के लिए विद्वान् लेखक को विद्वान् शिष्य और श्रमण विविध सूचनाएँ देने में सहायता किया करते थे । ऐसी भी प्रथा थी कि ग्रन्थ-रचनाकार अपने विषय के मान्य शास्त्रवेत्ता और आचार्य के पास अपनी रचना संशोधनार्थ भेजा करते थे । उनसे पुष्टि पाने के बाद ही इन रचनाओं की प्रतियाँ कराई जाती थीं। भारत में ग्रन्थ-लेखन या लेखक का कार्य पहले ब्राह्मणों के हाथ में रहा, बाद में 'कायस्थों के हाथ में चला गया । कायस्थ लेखकों का व्यवसायी वर्ग था । विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति (1,336) की टीका में मूल पाठ में आये 'कायस्थ' शब्द का अर्थ लेखक ही किया है; 'कायस्थगणका लेखकाश्च' । इसमें सन्देह नहीं कि कायस्थ वर्ग व्यावसायिक लेखकों का वर्ग ही था-यही आगे चल कर जाति के रूप में परिणत हो गया। कायस्थों का लेखन बहुत सुन्दर होता था । 'कायस्थ' शब्द के कई अर्थ किये गये हैं । किन्तु यथार्थ अर्थ यही प्रतीत होता है कि कायस्थ वह है जो काय में स्थित रहे-'काय' मौर्य काल में सेक्रेटेरियट (Secretariate) को कहा जाता था, और इसमें स्थित व्यक्ति था कायस्थ ।
लेखक, लिपिकार, दिपिकार या दिविर के साथ अन्य पर्यायवाची भी भारत में प्रचलित थे-ये हैं : करण, कगिन्, शासनिन् तथा धर्मलेखिन् । डॉ० वासुदेव उपाध्याय
1. The World Book Encyclopedia (Vol. 11), p. 224. 2 Encyclopedia Americana, (Vol. 18), p. 241. 3. भारतीय जैन श्रमण संस्कृति अने लेखन कला, पृ० 25 । 4. वही, पृ० 107। 5. उपाध्याय, वासुदेव-प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, पृ० 256-2571
For Private and Personal Use Only