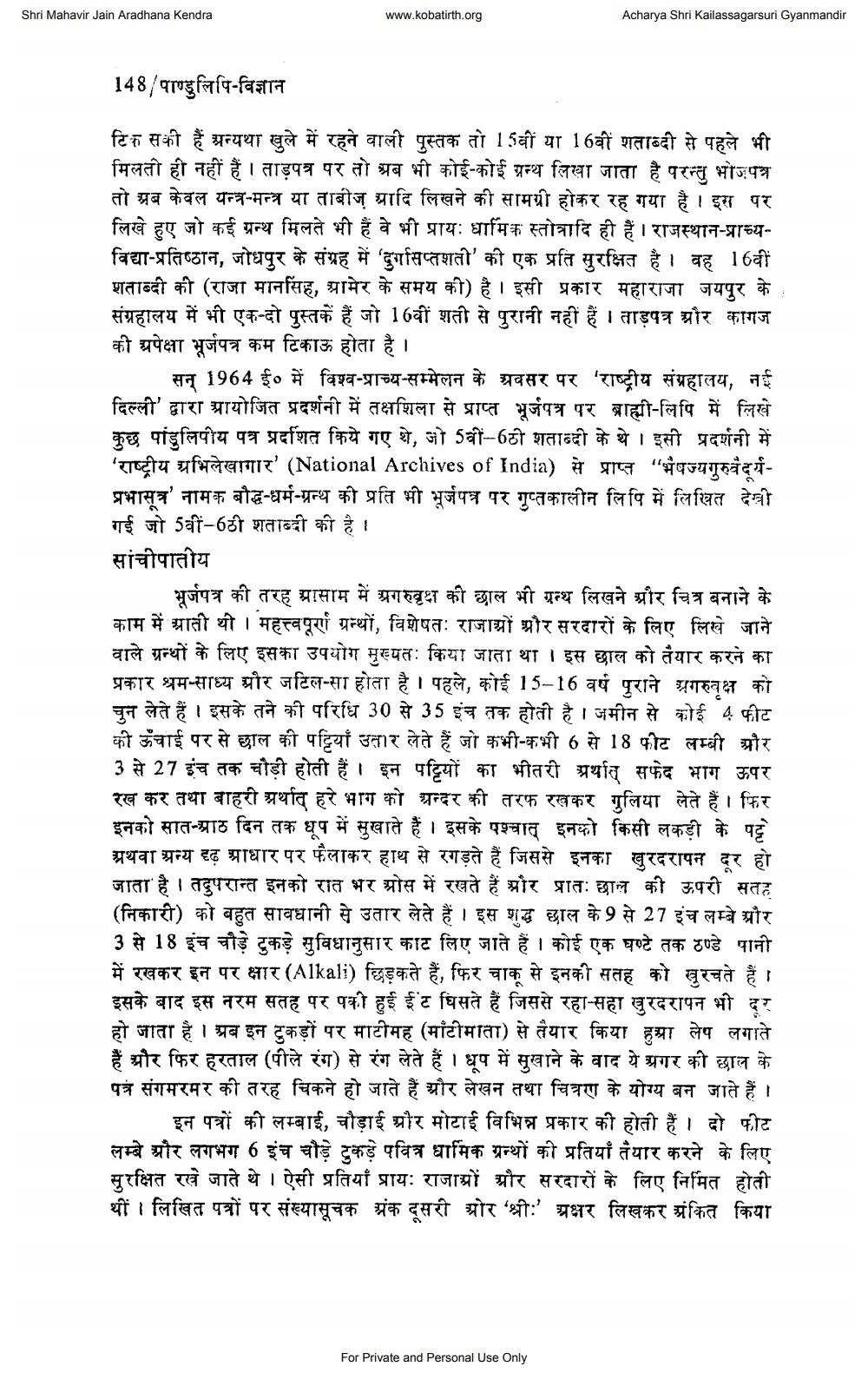________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
148 / पाण्डुलिपि - विज्ञान
टिक सकी हैं अन्यथा खुले में रहने वाली पुस्तक तो 15वीं या 16वीं शताब्दी से पहले भी मिलती ही नहीं हैं । ताड़पत्र पर तो अब भी कोई-कोई ग्रन्थ लिखा जाता है परन्तु भोजपत्र तो अब केवल यन्त्र-मन्त्र या ताबीज़ प्रादि लिखने की सामग्री होकर रह गया है । इस पर लिखे हुए जो कई ग्रन्थ मिलते भी हैं वे भी प्रायः धार्मिक स्तोत्रादि ही हैं। राजस्थान- प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान, जोधपुर के संग्रह में 'दुर्गासप्तशती' की एक प्रति सुरक्षित है। वह 16वीं शताब्दी की ( राजा मानसिंह, आमेर के समय की ) है । इसी प्रकार महाराजा जयपुर के संग्रहालय में भी एक-दो पुस्तकें हैं जो 16वीं शती से पुरानी नहीं हैं । ताड़पत्र और कागज की पेक्षा भूर्जपत्र कम टिकाऊ होता है ।
सन् 1964 ई० में विश्व - प्राच्य सम्मेलन के अवसर पर 'राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली' द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में तक्षशिला से प्राप्त भूर्जपत्र पर ब्राह्मी लिपि में लिखे कुछ पांडुलिपीय पत्र प्रदर्शित किये गए थे, जो 5वीं - 6ठी शताब्दी के थे । इसी प्रदर्शनी में 'राष्ट्रीय अभिलेखागार' (National Archives of India) से प्राप्त "भैषज्यगुरुवैदूर्यप्रभासूत्र' नामक बौद्ध-धर्म-ग्रन्थ की प्रति भी भूर्जपत्र पर गुप्तकालीन लिपि में लिखित देखी गई जो 5वीं - 6ठी शताब्दी की है ।
सांचीपातीय
भूर्जपत्र की तरह आसाम में अगरुवृक्ष की छाल भी ग्रन्थ लिखने और चित्र बनाने के काम में आती थी । महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों, विशेषतः राजाओं और सरदारों के लिए लिखे जाने वाले ग्रन्थों के लिए इसका उपयोग मुख्यतः किया जाता था । इस छाल को तैयार करने का प्रकार श्रम-साध्य र जटिल-सा होता है । पहले, कोई 15-16 वर्ष पुराने श्रगरुवृक्ष को चुन लेते हैं । इसके तने की परिधि 30 से 35 इंच तक होती है। जमीन से कोई 4 फीट की ऊँचाई पर से छाल की पट्टियाँ उतार लेते हैं जो कभी-कभी 6 से 18 फीट लम्बी और 3 से 27 इंच तक चौड़ी होती हैं । इन पट्टियों का भीतरी अर्थात् सफेद भाग ऊपर रख कर तथा बाहरी अर्थात् हरे भाग को अन्दर की तरफ रखकर गुलिया लेते हैं । फिर इनको सात-आठ दिन तक धूप में सुखाते हैं। इसके पश्चात् इनको किसी लकड़ी के पट्ट अथवा अन्य दृढ़ आधार पर फैलाकर हाथ से रगड़ते हैं जिससे इनका खुरदरापन दूर हो जाता है । तदुपरान्त इनको रात भर प्रोस में रखते हैं और प्रातः छाल की ऊपरी सतह (निकारी) को बहुत सावधानी से उतार लेते हैं । इस शुद्ध छाल के 9 से 27 इंच लम्बे और 3 से 18 इंच चौड़े टुकड़े सुविधानुसार काट लिए जाते हैं । कोई एक घण्टे तक ठण्डे पानी में रखकर इन पर क्षार (Alkali) छिड़कते हैं, फिर चाकू से इनकी सतह को खुरचते हैं । इसके बाद इस नरम सतह पर पकी हुई ईट घिसते हैं जिससे रहा-सहा खुरदरापन भी दूर
जाता है । अब इन टुकड़ों पर माटीमह (मांटीमाता) से तैयार किया हुआ लेप लगाते हैं और फिर हरताल (पीले रंग से रंग लेते हैं। धूप में सुखाने के बाद ये अगर की छाल के पत्र संगमरमर की तरह चिकने हो जाते हैं और लेखन तथा चित्ररण के योग्य बन जाते हैं ।
इन पत्रों की लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई विभिन्न प्रकार की होती हैं । दो फीट लम्बे और लगभग 6 इंच चौड़े टुकड़े पवित्र धार्मिक ग्रन्थों की प्रतियाँ तैयार करने के लिए सुरक्षित रखे जाते थे । ऐसी प्रतियाँ प्रायः राजाओं और सरदारों के लिए निर्मित होती थीं । लिखित पत्रों पर संख्यासूचक अंक दूसरी ओर 'श्री' अक्षर लिखकर अंकित किया
For Private and Personal Use Only