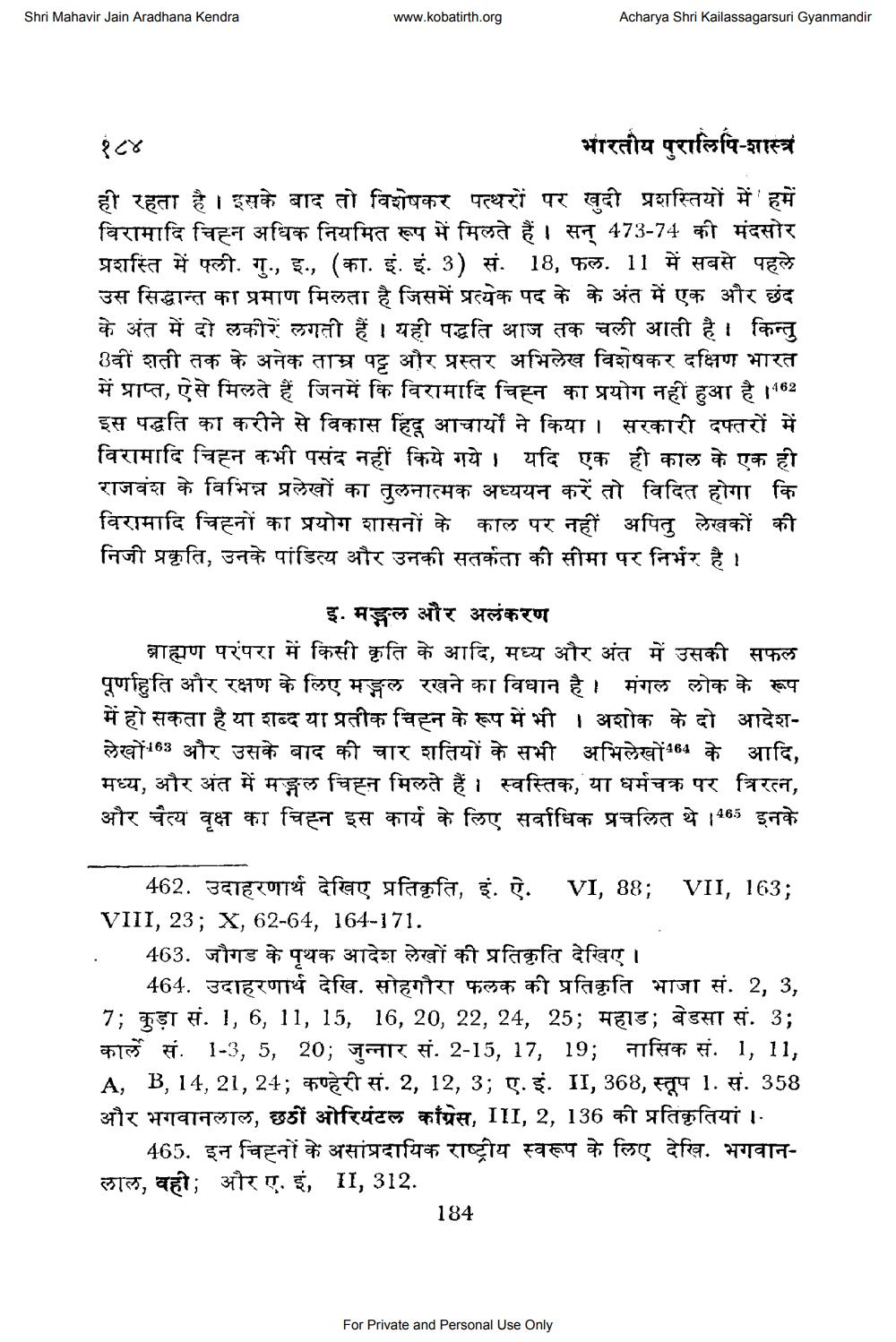________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
१८४
भारतीय पुरालिपि-शास्त्र ही रहता है । इसके बाद तो विशेषकर पत्थरों पर खुदी प्रशस्तियों में हमें विरामादि चिह्न अधिक नियमित रूप में मिलते हैं। सन् 473-74 की मंदसोर प्रशस्ति में पली. गु., इ., (का. इं. इं. 3) सं. 18, फल. 11 में सबसे पहले उस सिद्धान्त का प्रमाण मिलता है जिसमें प्रत्येक पद के के अंत में एक और छंद के अंत में दो लकीरें लगती हैं । यही पद्धति आज तक चली आती है। किन्तु 8वीं शती तक के अनेक ताम्र पट्ट और प्रस्तर अभिलेख विशेषकर दक्षिण भारत में प्राप्त, ऐसे मिलते हैं जिनमें कि विरामादि चिह्न का प्रयोग नहीं हुआ है ।162 इस पद्धति का करीने से विकास हिंदू आचार्यों ने किया। सरकारी दफ्तरों में विरामादि चिह्न कभी पसंद नहीं किये गये। यदि एक ही काल के एक ही राजवंश के विभिन्न प्रलेखों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो विदित होगा कि विरामादि चिह्नों का प्रयोग शासनों के काल पर नहीं अपितु लेखकों की निजी प्रकृति, उनके पांडित्य और उनकी सतर्कता की सीमा पर निर्भर है।
इ. मङ्गल और अलंकरण ब्राह्मण परंपरा में किसी कृति के आदि, मध्य और अंत में उसकी सफल पूर्णाहुति और रक्षण के लिए मङ्गल रखने का विधान है। मंगल लोक के रूप में हो सकता है या शब्द या प्रतीक चिह्न के रूप में भी । अशोक के दो आदेशलेखों163 और उसके बाद की चार शतियों के सभी अभिलेखों के आदि, मध्य, और अंत में मङ्गल चिह्न मिलते हैं। स्वस्तिक, या धर्मचक्र पर त्रिरत्न, और चैत्य वृक्ष का चिह्न इस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रचलित थे ।465 इनके
462. उदाहरणार्थ देखिए प्रतिकृति, इं. ऐ. VI, 88; VII, 163; VIII, 23; X, 62-64, 164-171.
463. जौगड के पृथक आदेश लेखों की प्रतिकृति देखिए।
464. उदाहरणार्थ देखि. सोहगौरा फलक की प्रतिकृति भाजा सं. 2, 3, 7; कुड़ा सं. 1, 6, 11, 15, 16, 20, 22, 24, 25; महाड; बेडसा सं. 3; कार्ले सं. 1-3, 5, 20; जुन्नार सं. 2-15, 17, 19; नासिक सं. 1, 11, A, B, 14, 21, 24; कण्हेरी सं. 2, 12, 3; ए. ई. II, 368, स्तूप 1. सं. 358 और भगवानलाल, छठी ओरियंटल काँग्रेस, III, 2, 136 की प्रतिकृतियां । ___465. इन चिह्नों के असांप्रदायिक राष्ट्रीय स्वरूप के लिए देखि. भगवानलाल, वही; और ए. इं, II, 312.
184
For Private and Personal Use Only