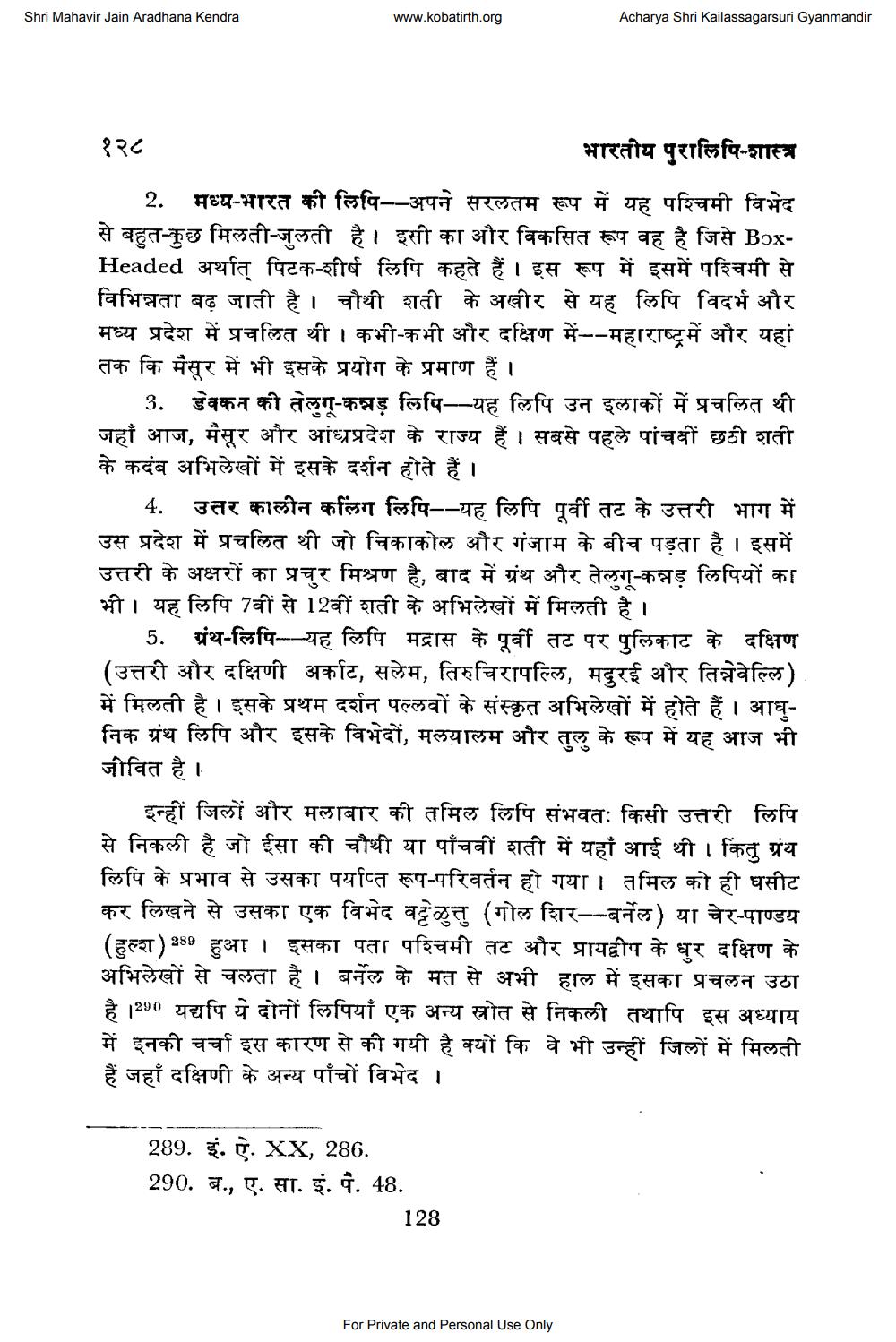________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
१२८
भारतीय पुरालिपि-शास्त्र
2. मध्य-भारत की लिपि--अपने सरलतम रूप में यह पश्चिमी विभेद से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। इसी का और विकसित रूप वह है जिसे Box
Headed अर्थात् पिटक-शीर्ष लिपि कहते हैं । इस रूप में इसमें पश्चिमी से विभिन्नता बढ़ जाती है। चौथी शती के अखीर से यह लिपि विदर्भ और मध्य प्रदेश में प्रचलित थी। कभी-कभी और दक्षिण में--महाराष्ट्र में और यहां तक कि मैसूर में भी इसके प्रयोग के प्रमाण हैं।
3. डेक्कन की तेलग-कन्नड़ लिपि-यह लिपि उन इलाकों में प्रचलित थी जहाँ आज, मैसूर और आंध्रप्रदेश के राज्य हैं। सबसे पहले पांचवीं छठी शती के कदंब अभिलेखों में इसके दर्शन होते हैं ।
4. उत्तर कालीन कलिंग लिपि--यह लिपि पूर्वी तट के उत्तरी भाग में उस प्रदेश में प्रचलित थी जो चिकाकोल और गंजाम के बीच पड़ता है । इसमें उत्तरी के अक्षरों का प्रचुर मिश्रण है, बाद में ग्रंथ और तेलुगू-कन्नड़ लिपियों का भी। यह लिपि 7वीं से 12वीं शती के अभिलेखों में मिलती है।
5. ग्रंथ-लिपि--यह लिपि मद्रास के पूर्वी तट पर पुलिकाट के दक्षिण (उत्तरी और दक्षिणी अर्काट, सलेम, तिरुचिरापल्लि, मदुरई और तिन्नेवेल्लि) में मिलती है। इसके प्रथम दर्शन पल्लवों के संस्कृत अभिलेखों में होते हैं । आधुनिक ग्रंथ लिपि और इसके विभेदों, मलयालम और तुलु के रूप में यह आज भी जीवित है।
इन्हीं जिलों और मलाबार की तमिल लिपि संभवतः किसी उत्तरी लिपि से निकली है जो ईसा की चौथी या पाँचवीं शती में यहाँ आई थी। किंतु ग्रंथ लिपि के प्रभाव से उसका पर्याप्त रूप-परिवर्तन हो गया। तमिल को ही घसीट कर लिखने से उसका एक विभेद वझेळुत्तु (गोल शिर--बर्नेल) या चेर-पाण्डय (हुल्श) 289 हुआ। इसका पता पश्चिमी तट और प्रायद्वीप के धुर दक्षिण के अभिलेखों से चलता है । बर्नेल के मत से अभी हाल में इसका प्रचलन उठा है।200 यद्यपि ये दोनों लिपियाँ एक अन्य स्रोत से निकली तथापि इस अध्याय में इनकी चर्चा इस कारण से की गयी है क्यों कि वे भी उन्हीं जिलों में मिलती हैं जहाँ दक्षिणी के अन्य पाँचों विभेद ।
289. ई. ऐ. XX, 286. 290. ब., ए. सा. इं. पै. 48.
128
For Private and Personal Use Only