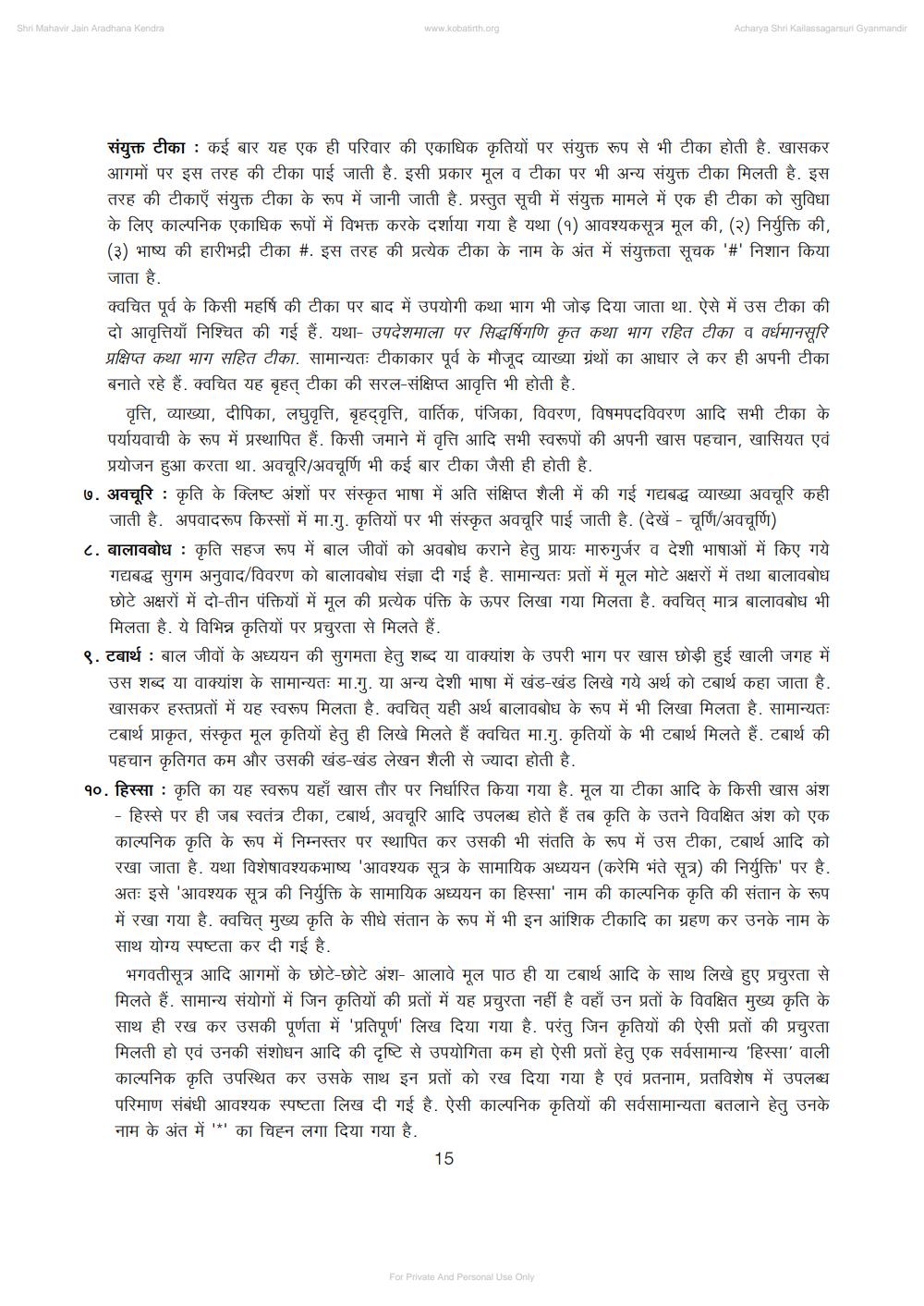________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatith.org
Acharya Shri Kailassagarsur Gyanmandir
संयुक्त टीका : कई बार यह एक ही परिवार की एकाधिक कृतियों पर संयुक्त रूप से भी टीका होती है. खासकर आगमों पर इस तरह की टीका पाई जाती है. इसी प्रकार मूल व टीका पर भी अन्य संयुक्त टीका मिलती है. इस तरह की टीकाएँ संयुक्त टीका के रूप में जानी जाती है. प्रस्तुत सूची में संयुक्त मामले में एक ही टीका को सुविधा के लिए काल्पनिक एकाधिक रूपों में विभक्त करके दर्शाया गया है यथा (१) आवश्यकसूत्र मूल की, (२) नियुक्ति की, (३) भाष्य की हारीभद्री टीका #. इस तरह की प्रत्येक टीका के नाम के अंत में संयुक्तता सूचक '#' निशान किया जाता है. क्वचित पूर्व के किसी महर्षि की टीका पर बाद में उपयोगी कथा भाग भी जोड़ दिया जाता था. ऐसे में उस टीका की दो आवृत्तियाँ निश्चित की गई हैं. यथा- उपदेशमाला पर सिद्धर्षिगणि कृत कथा भाग रहित टीका व वर्धमानसूरि प्रक्षिप्त कथा भाग सहित टीका. सामान्यतः टीकाकार पूर्व के मौजूद व्याख्या ग्रंथों का आधार ले कर ही अपनी टीका बनाते रहे हैं. क्वचित यह बृहत् टीका की सरल-संक्षिप्त आवृत्ति भी होती है.
वृत्ति, व्याख्या, दीपिका, लघुवृत्ति, बृहवृत्ति, वार्तिक, पंजिका, विवरण, विषमपदविवरण आदि सभी टीका के पर्यायवाची के रूप में प्रस्थापित हैं. किसी जमाने में वृत्ति आदि सभी स्वरूपों की अपनी खास पहचान, खासियत एवं
प्रयोजन हुआ करता था. अवचूरि/अवचूर्णि भी कई बार टीका जैसी ही होती है. ७. अवचूरि : कृति के क्लिष्ट अंशों पर संस्कृत भाषा में अति संक्षिप्त शैली में की गई गद्यबद्ध व्याख्या अवचूरि कही
जाती है. अपवादरूप किस्सों में मा.गु. कृतियों पर भी संस्कृत अवचूरि पाई जाती है. (देखें - चूर्णि/अवचूर्णि) ८. बालावबोध : कृति सहज रूप में बाल जीवों को अवबोध कराने हेतु प्रायः मारुगुर्जर व देशी भाषाओं में किए गये
गद्यबद्ध सुगम अनुवाद/विवरण को बालावबोध संज्ञा दी गई है. सामान्यतः प्रतों में मूल मोटे अक्षरों में तथा बालावबोध छोटे अक्षरों में दो-तीन पंक्तियों में मूल की प्रत्येक पंक्ति के ऊपर लिखा गया मिलता है. क्वचित् मात्र बालावबोध भी मिलता है. ये विभिन्न कृतियों पर प्रचुरता से मिलते हैं. ९. टबार्थ : बाल जीवों के अध्ययन की सुगमता हेतु शब्द या वाक्यांश के उपरी भाग पर खास छोड़ी हुई खाली जगह में
उस शब्द या वाक्यांश के सामान्यतः मा.गु. या अन्य देशी भाषा में खंड-खंड लिखे गये अर्थ को टबार्थ कहा जाता है. खासकर हस्तप्रतों में यह स्वरूप मिलता है. क्वचित् यही अर्थ बालावबोध के रूप में भी लिखा मिलता है. सामान्यतः टबार्थ प्राकृत, संस्कृत मूल कृतियों हेतु ही लिखे मिलते हैं क्वचित मा.गु. कृतियों के भी टबार्थ मिलते हैं. टबार्थ की
पहचान कृतिगत कम और उसकी खंड-खंड लेखन शैली से ज्यादा होती है. १०. हिस्सा : कृति का यह स्वरूप यहाँ खास तौर पर निर्धारित किया गया है. मूल या टीका आदि के किसी खास अंश
- हिस्से पर ही जब स्वतंत्र टीका, टबार्थ, अवचूरि आदि उपलब्ध होते हैं तब कृति के उतने विवक्षित अंश को एक काल्पनिक कृति के रूप में निम्नस्तर पर स्थापित कर उसकी भी संतति के रूप में उस टीका, टबार्थ आदि को रखा जाता है. यथा विशेषावश्यकभाष्य 'आवश्यक सूत्र के सामायिक अध्ययन (करेमि भंते सूत्र) की नियुक्ति' पर है. अतः इसे 'आवश्यक सूत्र की नियुक्ति के सामायिक अध्ययन का हिस्सा' नाम की काल्पनिक कृति की संतान के रूप में रखा गया है. क्वचित् मुख्य कृति के सीधे संतान के रूप में भी इन आंशिक टीकादि का ग्रहण कर उनके नाम के साथ योग्य स्पष्टता कर दी गई है.
भगवतीसूत्र आदि आगमों के छोटे-छोटे अंश- आलावे मूल पाठ ही या टबार्थ आदि के साथ लिखे हुए प्रचुरता से मिलते हैं. सामान्य संयोगों में जिन कृतियों की प्रतों में यह प्रचुरता नहीं है वहाँ उन प्रतों के विवक्षित मुख्य कृति के साथ ही रख कर उसकी पूर्णता में 'प्रतिपूर्ण' लिख दिया गया है. परंतु जिन कृतियों की ऐसी प्रतों की प्रचुरता मिलती हो एवं उनकी संशोधन आदि की दृष्टि से उपयोगिता कम हो ऐसी प्रतों हेतु एक सर्वसामान्य 'हिस्सा' वाली काल्पनिक कृति उपस्थित कर उसके साथ इन प्रतों को रख दिया गया है एवं प्रतनाम, प्रतविशेष में उपलब्ध परिमाण संबंधी आवश्यक स्पष्टता लिख दी गई है. ऐसी काल्पनिक कृतियों की सर्वसामान्यता बतलाने हेतु उनके नाम के अंत में '' का चिह्न लगा दिया गया है.
15
For Private And Personal Use Only