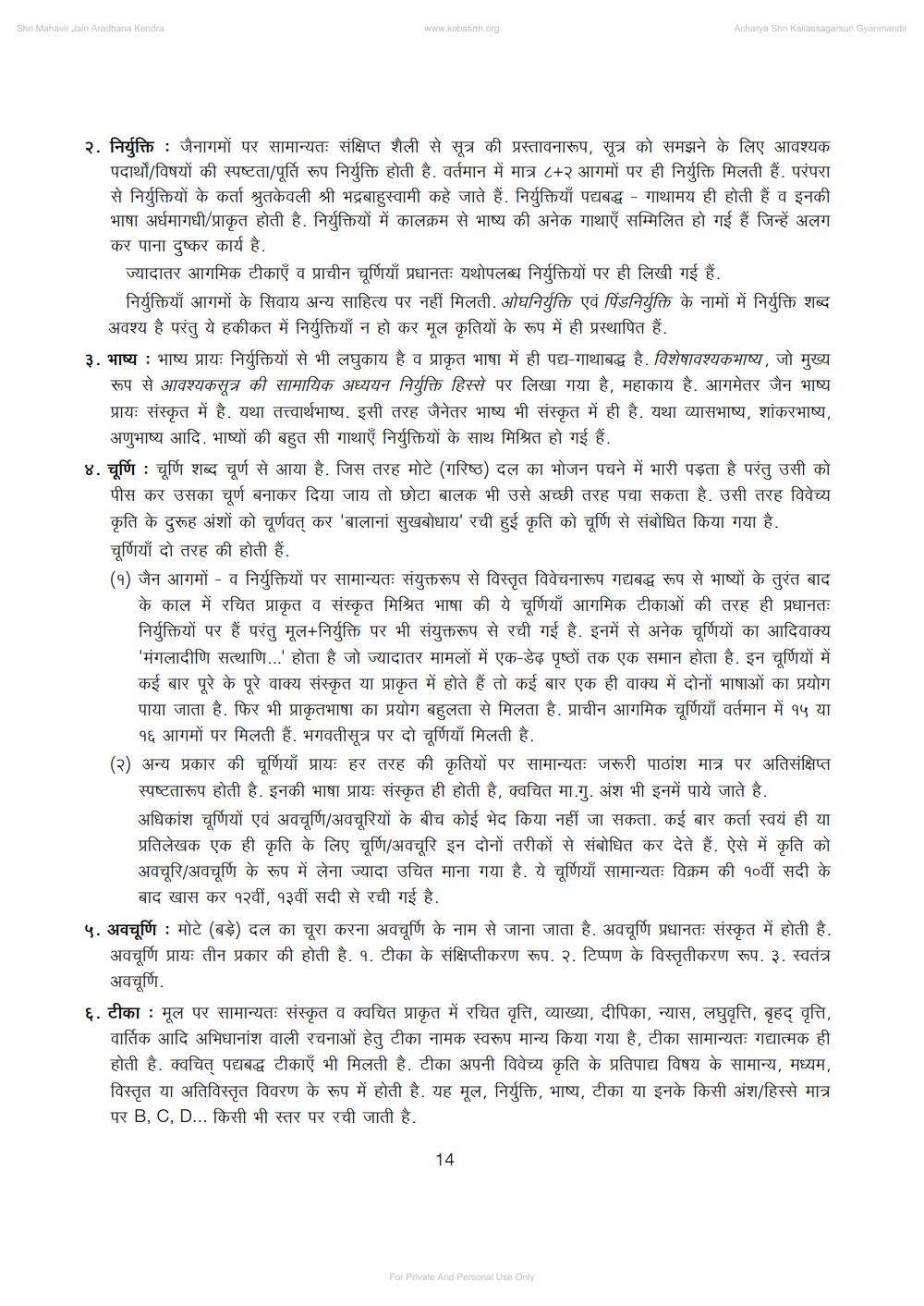________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatith.org
Acharya Shri Kailassagarsur Gyanmandir
२. नियुक्ति : जैनागमों पर सामान्यतः संक्षिप्त शैली से सूत्र की प्रस्तावनारूप, सूत्र को समझने के लिए आवश्यक
पदार्थों/विषयों की स्पष्टता/पूर्ति रूप नियुक्ति होती है. वर्तमान में मात्र ८+२ आगमों पर ही नियुक्ति मिलती हैं. परंपरा से नियुक्तियों के कर्ता श्रुतकेवली श्री भद्रबाहुस्वामी कहे जाते हैं. नियुक्तियाँ पद्यबद्ध - गाथामय ही होती हैं व इनकी भाषा अर्धमागधी/प्राकृत होती है. नियुक्तियों में कालक्रम से भाष्य की अनेक गाथाएँ सम्मिलित हो गई हैं जिन्हें अलग कर पाना दुष्कर कार्य है. ज्यादातर आगमिक टीकाएँ व प्राचीन चूर्णियाँ प्रधानतः यथोपलब्ध नियुक्तियों पर ही लिखी गई हैं. नियुक्तियाँ आगमों के सिवाय अन्य साहित्य पर नहीं मिलती. ओघनियुक्ति एवं पिंडनियुक्ति के नामों में नियुक्ति शब्द अवश्य है परंतु ये हकीकत में नियुक्तियाँ न हो कर मूल कृतियों के रूप में ही प्रस्थापित हैं. ३. भाष्य : भाष्य प्रायः नियुक्तियों से भी लघुकाय है व प्राकृत भाषा में ही पद्य-गाथाबद्ध है. विशेषावश्यकभाष्य, जो मुख्य
रूप से आवश्यकसूत्र की सामायिक अध्ययन नियुक्ति हिस्से पर लिखा गया है, महाकाय है. आगमेतर जैन भाष्य प्रायः संस्कृत में है. यथा तत्त्वार्थभाष्य. इसी तरह जैनेतर भाष्य भी संस्कृत में ही है. यथा व्यासभाष्य, शांकरभाष्य,
अणुभाष्य आदि. भाष्यों की बहुत सी गाथाएँ नियुक्तियों के साथ मिश्रित हो गई हैं. ४. चूर्णि : चूर्णि शब्द चूर्ण से आया है. जिस तरह मोटे (गरिष्ठ) दल का भोजन पचने में भारी पड़ता है परंतु उसी को
पीस कर उसका चूर्ण बनाकर दिया जाय तो छोटा बालक भी उसे अच्छी तरह पचा सकता है. उसी तरह विवेच्य कृति के दुरूह अंशों को चूर्णवत् कर 'बालानां सुखबोधाय' रची हुई कृति को चूर्णि से संबोधित किया गया है. चूर्णियाँ दो तरह की होती हैं. (१) जैन आगमों - व नियुक्तियों पर सामान्यतः संयुक्तरूप से विस्तृत विवेचनारूप गद्यबद्ध रूप से भाष्यों के तुरंत बाद
के काल में रचित प्राकृत व संस्कृत मिश्रित भाषा की ये चूर्णियाँ आगमिक टीकाओं की तरह ही प्रधानतः नियुक्तियों पर हैं परंतु मूल+नियुक्ति पर भी संयुक्तरूप से रची गई है. इनमें से अनेक चूर्णियों का आदिवाक्य 'मंगलादीणि सत्थाणि...' होता है जो ज्यादातर मामलों में एक-डेढ़ पृष्ठों तक एक समान होता है. इन चूर्णियों में कई बार पूरे के पूरे वाक्य संस्कृत या प्राकृत में होते हैं तो कई बार एक ही वाक्य में दोनों भाषाओं का प्रयोग पाया जाता है. फिर भी प्राकृतभाषा का प्रयोग बहुलता से मिलता है. प्राचीन आगमिक चूर्णियाँ वर्तमान में १५ या
१६ आगमों पर मिलती हैं. भगवतीसूत्र पर दो चूर्णियाँ मिलती है. (२) अन्य प्रकार की चूर्णियाँ प्रायः हर तरह की कृतियों पर सामान्यतः जरूरी पाठांश मात्र पर अतिसंक्षिप्त
स्पष्टतारूप होती है. इनकी भाषा प्रायः संस्कृत ही होती है, क्वचित मा.गु. अंश भी इनमें पाये जाते है. अधिकांश चूर्णियों एवं अवचूर्णि/अवचूरियों के बीच कोई भेद किया नहीं जा सकता. कई बार कर्ता स्वयं ही या प्रतिलेखक एक ही कृति के लिए चूर्णि/अवचूरि इन दोनों तरीकों से संबोधित कर देते हैं. ऐसे में कृति को अवचूरि/अवचूर्णि के रूप में लेना ज्यादा उचित माना गया है. ये चूर्णियाँ सामान्यतः विक्रम की १०वीं सदी के
बाद खास कर १२वीं, १३वीं सदी से रची गई है. ५. अवचूर्णि : मोटे (बड़े) दल का चूरा करना अवचूर्णि के नाम से जाना जाता है. अवचूर्णि प्रधानतः संस्कृत में होती है.
अवचूर्णि प्रायः तीन प्रकार की होती है. १. टीका के संक्षिप्तीकरण रूप. २. टिप्पण के विस्तृतीकरण रूप. ३. स्वतंत्र
अवचूर्णि. ६. टीका : मूल पर सामान्यतः संस्कृत व क्वचित प्राकृत में रचित वृत्ति, व्याख्या, दीपिका, न्यास, लघुवृत्ति, बृहद् वृत्ति,
वार्तिक आदि अभिधानांश वाली रचनाओं हेतु टीका नामक स्वरूप मान्य किया गया है, टीका सामान्यतः गद्यात्मक ही होती है. क्वचित् पद्यबद्ध टीकाएँ भी मिलती है. टीका अपनी विवेच्य कृति के प्रतिपाद्य विषय के सामान्य, मध्यम, विस्तृत या अतिविस्तृत विवरण के रूप में होती है. यह मूल, नियुक्ति, भाष्य, टीका या इनके किसी अंश/हिस्से मात्र पर B, C, D... किसी भी स्तर पर रची जाती है.
14
For Private And Personal Use Only