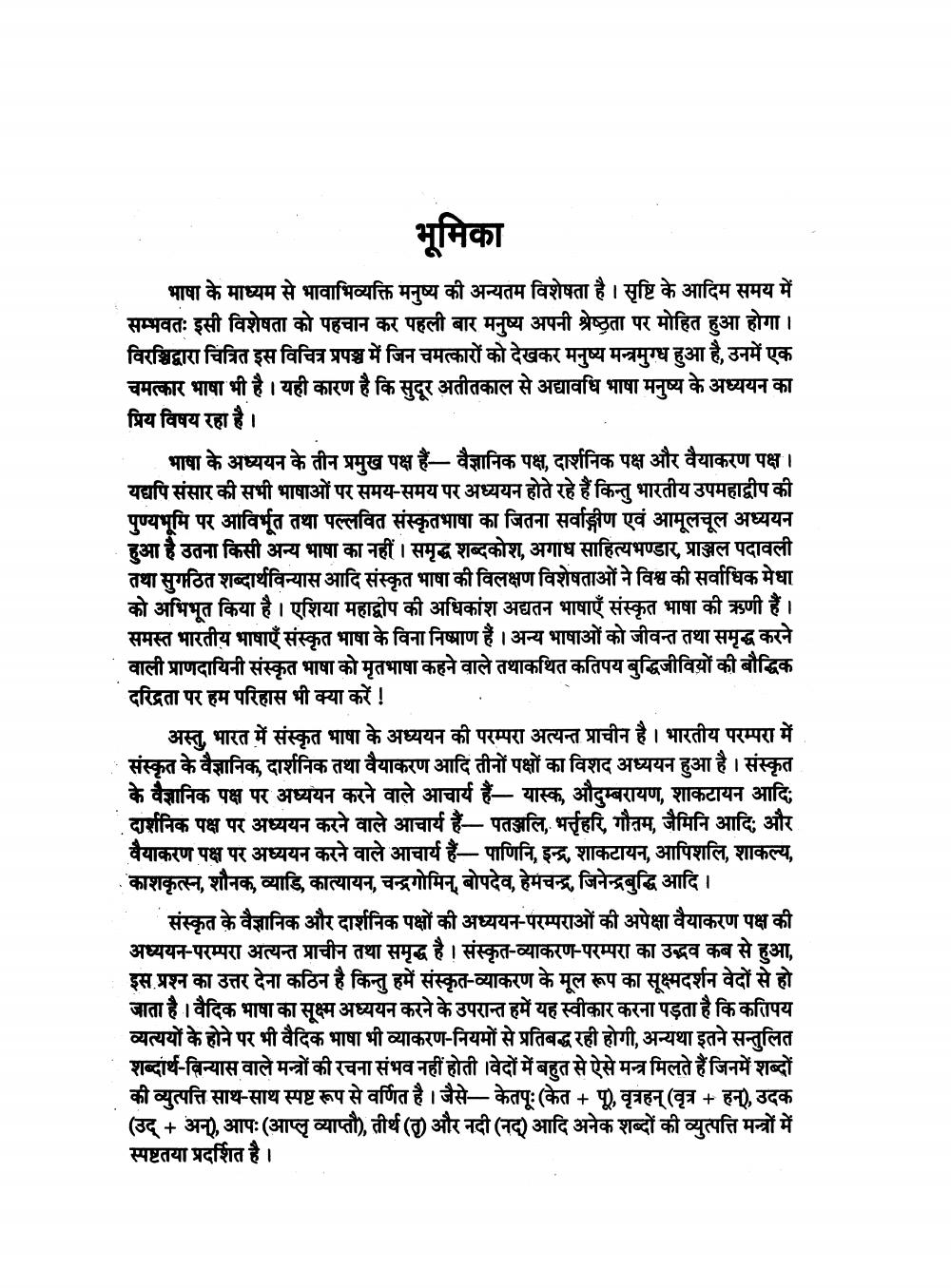________________
भूमिका भाषा के माध्यम से भावाभिव्यक्ति मनुष्य की अन्यतम विशेषता है । सृष्टि के आदिम समय में सम्भवतः इसी विशेषता को पहचान कर पहली बार मनुष्य अपनी श्रेष्ठता पर मोहित हुआ होगा। विरश्चिद्वारा चित्रित इस विचित्र प्रपञ्च में जिन चमत्कारों को देखकर मनुष्य मन्त्रमुग्ध हुआ है, उनमें एक चमत्कार भाषा भी है। यही कारण है कि सुदूर अतीतकाल से अद्यावधि भाषा मनुष्य के अध्ययन का प्रिय विषय रहा है। ___भाषा के अध्ययन के तीन प्रमुख पक्ष हैं- वैज्ञानिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष और वैयाकरण पक्ष । यद्यपि संसार की सभी भाषाओं पर समय-समय पर अध्ययन होते रहे हैं किन्तु भारतीय उपमहाद्वीप की पुण्यभूमि पर आविर्भूत तथा पल्लवित संस्कृतभाषा का जितना सर्वाङ्गीण एवं आमूलचूल अध्ययन हुआ है उतना किसी अन्य भाषा का नहीं । समृद्ध शब्दकोश, अगाध साहित्यभण्डार, प्राञ्जल पदावली तथा सुगठित शब्दार्थविन्यास आदि संस्कृत भाषा की विलक्षण विशेषताओं ने विश्व की सर्वाधिक मेधा को अभिभूत किया है । एशिया महाद्वीप की अधिकांश अद्यतन भाषाएँ संस्कृत भाषा की ऋणी हैं। समस्त भारतीय भाषाएँ संस्कृत भाषा के विना निष्प्राण हैं । अन्य भाषाओं को जीवन्त तथा समृद्ध करने वाली प्राणदायिनी संस्कृत भाषा को मृतभाषा कहने वाले तथाकथित कतिपय बुद्धिजीवियों की बौद्धिक दरिद्रता पर हम परिहास भी क्या करें!
अस्तु, भारत में संस्कृत भाषा के अध्ययन की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। भारतीय परम्परा में संस्कृत के वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा वैयाकरण आदि तीनों पक्षों का विशद अध्ययन हुआ है । संस्कृत के वैज्ञानिक पक्ष पर अध्ययन करने वाले आचार्य हैं- यास्क, औदुम्बरायण, शाकटायन आदि; दार्शनिक पक्ष पर अध्ययन करने वाले आचार्य हैं— पतञ्जलि, भर्तृहरि, गौतम, जैमिनि आदि; और वैयाकरण पक्ष पर अध्ययन करने वाले आचार्य हैं- पाणिनि, इन्द्र, शाकटायन, आपिशलि, शाकल्य, काशकृत्स्न, शौनक, व्याडि, कात्यायन, चन्द्रगोमिन, बोपदेव, हेमचन्द्र, जिनेन्द्रबुद्धि आदि।
संस्कृत के वैज्ञानिक और दार्शनिक पक्षों की अध्ययन-परम्पराओं की अपेक्षा वैयाकरण पक्ष की अध्ययन-परम्परा अत्यन्त प्राचीन तथा समृद्ध है। संस्कृत-व्याकरण-परम्परा का उद्भव कब से हुआ, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है किन्तु हमें संस्कृत-व्याकरण के मूल रूप का सूक्ष्मदर्शन वेदों से हो जाता है । वैदिक भाषा का सूक्ष्म अध्ययन करने के उपरान्त हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि कतिपय व्यत्ययों के होने पर भी वैदिक भाषा भी व्याकरण-नियमों से प्रतिबद्ध रही होगी, अन्यथा इतने सन्तुलित शब्दार्थ-विन्यास वाले मन्त्रों की रचना संभव नहीं होती ।वेदों में बहुत से ऐसे मन्त्र मिलते हैं जिनमें शब्दों की व्युत्पत्ति साथ-साथ स्पष्ट रूप से वर्णित है । जैसे-केतपू: (केत + पू), वृत्रहन् (वृत्र + हन्), उदक (उद् + अन्), आपः (आप्ल व्याप्तौ), तीर्थ (त) और नदी (नद्आदि अनेक शब्दों की व्युत्पत्ति मन्त्रों में स्पष्टतया प्रदर्शित है।