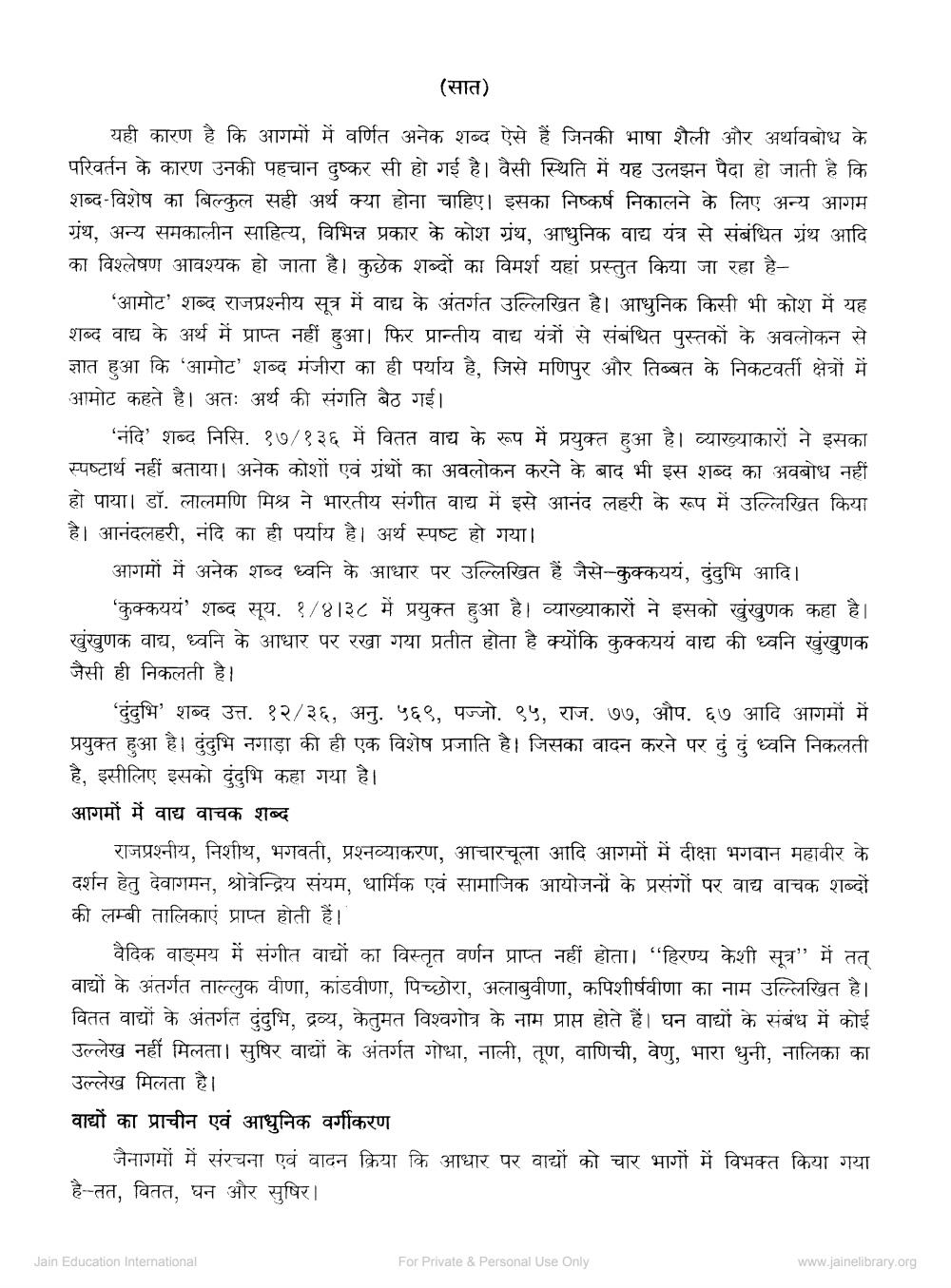________________
(सात)
यही कारण है कि आगमों में वर्णित अनेक शब्द ऐसे हैं जिनकी भाषा शैली और अर्थावबोध के परिवर्तन के कारण उनकी पहचान दुष्कर सी हो गई है। वैसी स्थिति में यह उलझन पैदा हो जाती है कि शब्द-विशेष का बिल्कुल सही अर्थ क्या होना चाहिए। इसका निष्कर्ष निकालने के लिए अन्य आगम ग्रंथ, अन्य समकालीन साहित्य, विभिन्न प्रकार के कोश ग्रंथ, आधुनिक वाद्य यंत्र से संबंधित ग्रंथ आदि का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। कुछेक शब्दों का विमर्श यहां प्रस्तुत किया जा रहा है
_ 'आमोट' शब्द राजप्रश्नीय सूत्र में वाद्य के अंतर्गत उल्लिखित है। आधुनिक किसी भी कोश में यह शब्द वाद्य के अर्थ में प्राप्त नहीं हुआ। फिर प्रान्तीय वाद्य यंत्रों से संबंधित पुस्तकों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि 'आमोट' शब्द मंजीरा का ही पर्याय है, जिसे मणिपुर और तिब्बत के निकटवर्ती क्षेत्रों में आमोट कहते है। अतः अर्थ की संगति बैठ गई। ___'नंदि' शब्द निसि. १७/१३६ में वितत वाद्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है। व्याख्याकारों ने इसका स्पष्टार्थ नहीं बताया। अनेक कोशों एवं ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद भी इस शब्द का अवबोध नहीं हो पाया। डॉ. लालमणि मिश्र ने भारतीय संगीत वाद्य में इसे आनंद लहरी के रूप में उल्लिखित किया है। आनंदलहरी, नंदि का ही पर्याय है। अर्थ स्पष्ट हो गया।
आगमों में अनेक शब्द ध्वनि के आधार पर उल्लिखित हैं जैसे-कुक्कययं, दुंदुभि आदि।
'कुक्कययं' शब्द सूय. १/४।३८ में प्रयुक्त हुआ है। व्याख्याकारों ने इसको खुंखुणक कहा है। खुंखुणक वाद्य, ध्वनि के आधार पर रखा गया प्रतीत होता है क्योंकि कुक्कययं वाद्य की ध्वनि खुंखुणक जैसी ही निकलती है।
'दुंदुभि' शब्द उत्त. १२/३६, अनु. ५६९, पज्जो. ९५, राज. ७७, औप. ६७ आदि आगमों में प्रयुक्त हुआ है। दुंदुभि नगाड़ा की ही एक विशेष प्रजाति है। जिसका वादन करने पर दुं दुं ध्वनि निकलती है, इसीलिए इसको दुंदुभि कहा गया है। आगमों में वाद्य वाचक शब्द
राजप्रश्नीय, निशीथ, भगवती, प्रश्नव्याकरण, आचारचूला आदि आगमों में दीक्षा भगवान महावीर के दर्शन हेतु देवागमन, श्रोत्रेन्द्रिय संयम, धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के प्रसंगों पर वाद्य वाचक शब्दों की लम्बी तालिकाएं प्राप्त होती हैं।
वैदिक वाङ्मय में संगीत वाद्यों का विस्तृत वर्णन प्राप्त नहीं होता। “हिरण्य केशी सूत्र” में तत् वाद्यों के अंतर्गत ताल्लुक वीणा, कांडवीणा, पिच्छोरा, अलाबुवीणा, कपिशीर्षवीणा का नाम उल्लिखित है। वितत वाद्यों के अंतर्गत दुंदुभि, द्रव्य, केतुमत विश्वगोत्र के नाम प्राप्त होते हैं। घन वाद्यों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता। सुषिर वाद्यों के अंतर्गत गोधा, नाली, तूण, वाणिची, वेणु, भारा धुनी, नालिका का उल्लेख मिलता है। वाद्यों का प्राचीन एवं आधुनिक वर्गीकरण
जैनागमों में संरचना एवं वादन क्रिया कि आधार पर वाद्यों को चार भागों में विभक्त किया गया है--तत, वितत, घन और सुषिर।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org