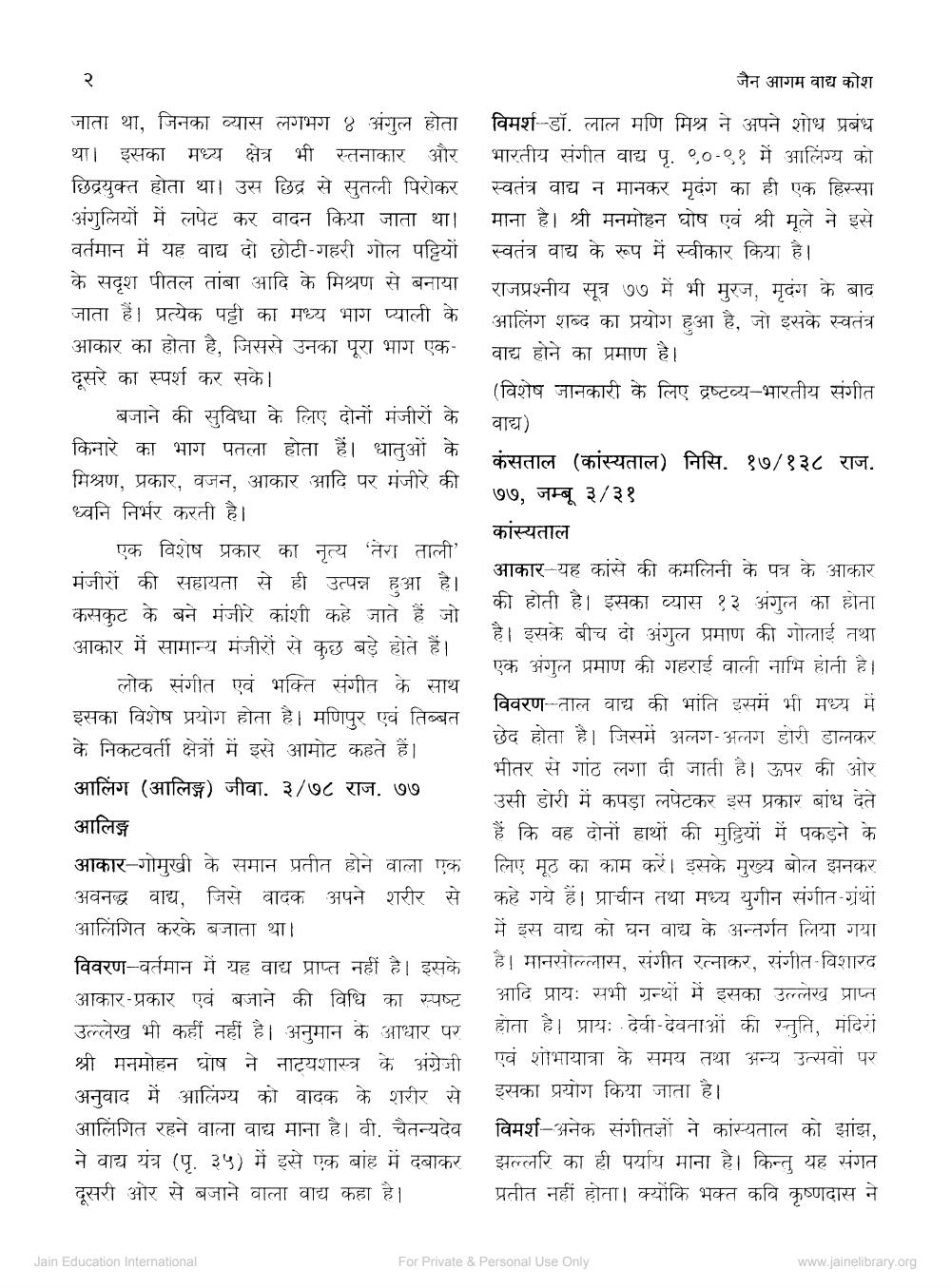________________
२
जाता था, जिनका व्यास लगभग ४ अंगुल होता था। इसका मध्य क्षेत्र भी स्तनाकार और छिद्रयुक्त होता था। उस छिद्र से सुतली पिरोकर अंगुलियों में लपेट कर वादन किया जाता था । वर्तमान में यह वाद्य दो छोटी- गहरी गोल पट्टियों के सदृश पीतल तांबा आदि के मिश्रण से बनाया जाता हैं। प्रत्येक पट्टी का मध्य भाग प्याली के आकार का होता है, जिससे उनका पूरा भाग एकदूसरे का स्पर्श कर सके ।
बजाने की सुविधा के लिए दोनों मंजीरों के किनारे का भाग पतला होता हैं। धातुओं के मिश्रण, प्रकार, वजन, आकार आदि पर मंजीरे की ध्वनि निर्भर करती है।
एक विशेष प्रकार का नृत्य 'तेरा ताली' मंजीरों की सहायता से ही उत्पन्न हुआ है। कसकुट के बने मंजीरे कांशी कहे जाते हैं जो आकार में सामान्य मंजीरों से कुछ बड़े होते हैं।
लोक संगीत एवं भक्ति संगीत के साथ इसका विशेष प्रयोग होता है। मणिपुर एवं तिब्बत के निकटवर्ती क्षेत्रों में इसे आमोट कहते हैं। आलिंग (आलिङ्ग) जीवा. ३ / ७८ राज. ७७ आलिङ्ग
आकार - गोमुखी के समान प्रतीत होने वाला एक अवनद्ध वाद्य, जिसे वादक अपने शरीर से आलिंगित करके बजाता था।
विवरण - वर्तमान में यह वाद्य प्राप्त नहीं है। इसके आकार-प्रकार एवं बजाने की विधि का स्पष्ट उल्लेख भी कहीं नहीं है। अनुमान के आधार पर श्री मनमोहन घोष ने नाट्यशास्त्र के अंग्रेजी अनुवाद में आलिंग्य को वादक के शरीर से आलिंगित रहने वाला वाद्य माना है। वी. चैतन्यदेव ने वाद्य यंत्र (पृ. ३५) में इसे एक बांह में दबाकर दूसरी ओर से बजाने वाला वाद्य कहा है।
Jain Education International
जैन आगम वाद्य कोश
विमर्श - डॉ. लाल मणि मिश्र ने अपने शोध प्रबंध भारतीय संगीत वाद्य पृ. ९०-९१ में आलिंग्य को स्वतंत्र वाद्य न मानकर मृदंग का ही एक हिस्सा माना है। श्री मनमोहन घोष एवं श्री मूले ने इसे स्वतंत्र वाद्य के रूप में स्वीकार किया है 1 राजप्रश्नीय सूत्र ७७ में भी मुरज, मृदंग के बाद आलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, जो इसके स्वतंत्र वाद्य होने का प्रमाण है।
(विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य-भारतीय संगीत वाद्य)
कंसताल (कांस्यताल) निसि. १७/१३८ राज. ७७, जम्बू ३/३१ कांस्यताल
आकार - यह कांसे की कमलिनी के पत्र के आकार की होती है। इसका व्यास १३ अंगुल का होता है। इसके बीच दो अंगुल प्रमाण की गोलाई तथा एक अंगुल प्रमाण की गहराई वाली नाभि होती है। विवरण- ताल वाद्य की भांति इसमें भी मध्य में छेद होता है। जिसमें अलग-अलग डोरी डालकर भीतर से गांठ लगा दी जाती है। ऊपर की ओर उसी डोरी में कपड़ा लपेटकर इस प्रकार बांध देते हैं कि वह दोनों हाथों की मुट्ठियों में पकड़ने के लिए मूठ का काम करें। इसके मुख्य बोल झनकर कहे गये हैं। प्राचीन तथा मध्य युगीन संगीत - ग्रंथां में इस वाद्य को घन वाद्य के अन्तर्गत लिया गया है। मानसोल्लास, संगीत रत्नाकर, संगीत विशारद आदि प्रायः सभी ग्रन्थों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। प्रायः देवी-देवताओं की स्तुति, मंदिरा एवं शोभायात्रा के समय तथा अन्य उत्सवों पर इसका प्रयोग किया जाता
|
विमर्श - अनेक संगीतज्ञों ने कांस्यताल को झांझ, झल्लरि का ही पर्याय माना है। किन्तु यह संगत प्रतीत नहीं होता। क्योंकि भक्त कवि कृष्णदास ने
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org