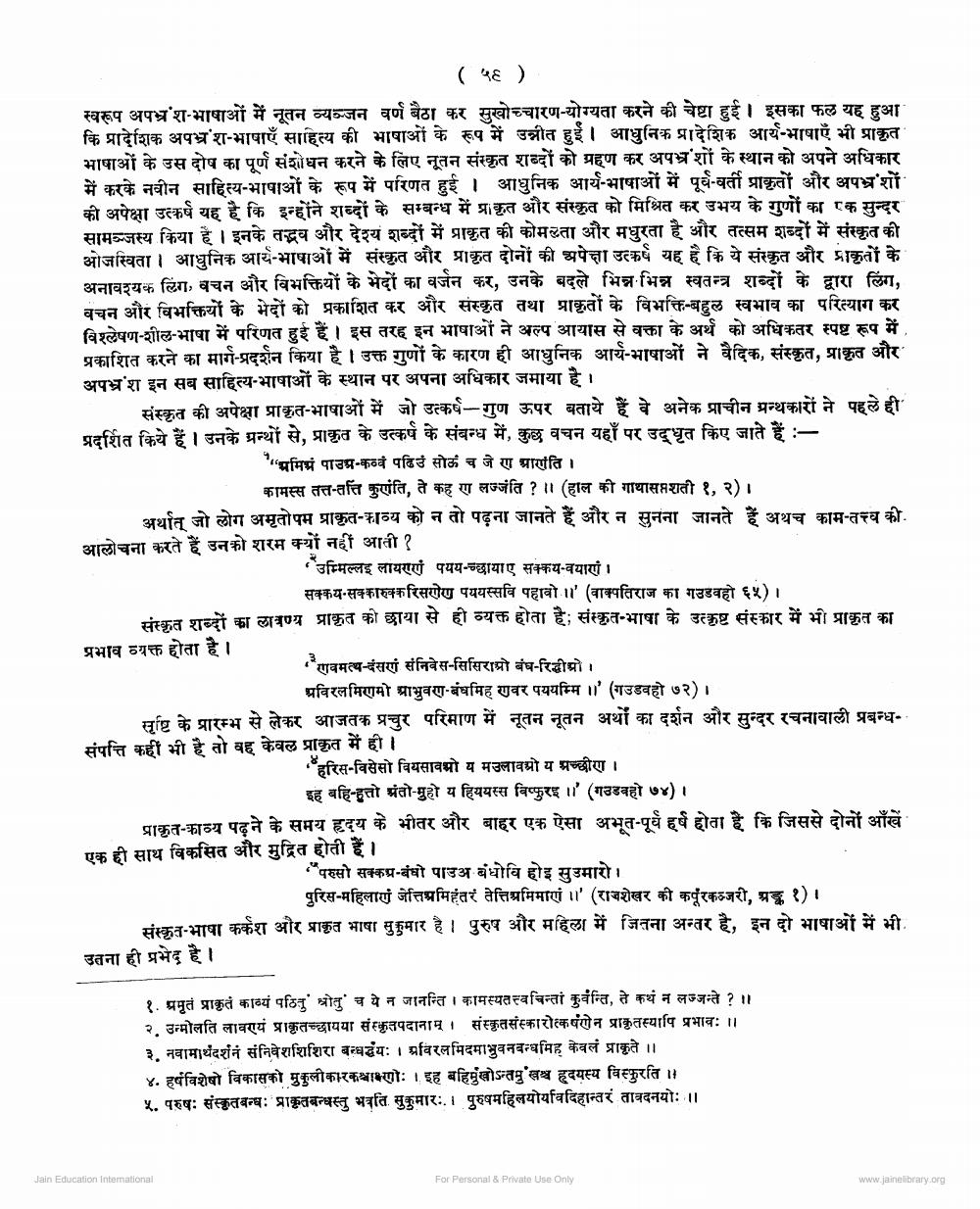________________
( ५६ ) स्वरूप अपभ्रंश-भाषाओं में नूतन व्यञ्जन वर्ण बैठा कर सुखोच्चारण-योग्यता करने की चेष्टा हुई। इसका फल यह हुआ कि प्रादेशिक अपभ्रंश-भाषाएँ साहित्य की भाषाओं के रूप में उन्नीत हुई। आधुनिक प्रादेशिक आर्य-भाषाएँ भी प्राकृत भाषाओं के उस दोष का पूर्ण संशोधन करने के लिए नूतन संस्कृत शब्दों को ग्रहण कर अपभ्रंशों के स्थान को अपने अधिकार में करके नवीन साहित्य-भाषाओं के रूप में परिणत हुई । आधुनिक आर्य-भाषाओं में पूर्व-वर्ती प्राकृतों और अपभ्रशों की अपेक्षा उत्कर्ष यह है कि इन्होंने शब्दों के सम्बन्ध में प्राकृत और संस्कृत को मिश्रित कर उभय के गुणों का एक सुन्दर सामञ्जस्य किया है । इनके तद्भव और देश्य शब्दों में प्राकृत की कोमलता और मधुरता है और तत्सम शब्दों में संस्कृत की ओजस्विता। आधुनिक आर्य-भाषाओं में संस्कृत और प्राकृत दोनों की अपेक्षा उत्कर्ष यह है कि ये संस्कृत और प्राकृतों के अनावश्यक लिंग, वचन और विभक्तियों के भेदों का वर्जन कर, उनके बदले भिन्न भिन्न स्वतन्त्र शब्दों के द्वारा लिंग, वचन और विभक्तियों के भेदों को प्रकाशित कर और संस्कृत तथा प्राकृतों के विभक्ति-बहुल स्वभाव का परित्याग कर विश्लेषण-शील-भाषा में परिणत हुई हैं। इस तरह इन भाषाओं ने अल्प आयास से वक्ता के अर्थ को अधिकतर स्पष्ट रूप में प्रकाशित करने का मार्ग-प्रदर्शन किया है। उक्त गुणों के कारण ही आधुनिक आर्य-भाषाओं ने वैदिक, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश इन सब साहित्य-भाषाओं के स्थान पर अपना अधिकार जमाया है।
संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत-भाषाओं में जो उत्कर्ष-गुण ऊपर बताये हैं वे अनेक प्राचीन ग्रन्थकारों ने पहले ही प्रदर्शित किये हैं। उनके ग्रन्थों से, प्राकृत के उत्कर्ष के संबन्ध में, कुछ वचन यहाँ पर उधृत किए जाते हैं :
"अमिभं पाउप-कव्वं पढिउं सोऊं च जे ण प्राणंति।
कामस्स तत्त-तत्ति कुणंति, ते कह ण लज्जति ? ॥ (हाल की गाथासप्तशती १, २)। अर्थात जो लोग अमृतोपम प्राकृत-काव्य को न तो पढ़ना जानते हैं और न सुनना जानते हैं अथच काम-तत्त्व की. आलोचना करते हैं उनको शरम क्यों नहीं आती?
'उम्मिल्लइ लायएणं पयय-च्छायाए सक्कय-वयाएं।
सक्कय-सक्कारुक्करिसरोण पययस्सवि पहावो ।' (वाक्पतिराज का गउडवहो ६५)। का शब्दों का लावण्य प्राकृत को छाया से ही व्यक्त होता है। संस्कृत-भाषा के उत्कृष्ट संस्कार में भी प्राकृत का प्रभाव व्यक्त होता है।
"णवमत्थ-दसणं संनिवेस-सिसिरानो बंघ-रिद्धीमो।
अविरलमिणमो प्राभुवण-बंधमिह णवर पययम्मि ॥' (गउडवहो ७२)। । सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आजतक प्रचुर परिमाण में नूतन नूतन अर्थों का दर्शन और सुन्दर रचनावाली प्रबन्धसंपत्ति कहीं भी है तो वह केवल प्राकृत में ही।
"हरिस-विसेसो वियसावमो य मउलावनो य अच्छीण।
इह बहि-हुत्तो अंतो-मुहो य हिययस्स विप्फुरइ ।' (गउडवहो ७४) । प्राकृत-काव्य पढ़ने के समय हृदय के भीतर और बाहर एक ऐसा अभूत-पूर्व हर्ष होता है कि जिससे दोनों आँखें एक ही साथ विकसित और मुद्रित होती हैं।
"परुसो सक्का-बंधो पाउअ बंधोवि होइ सुउमारो।
पुरिस-महिलाणं जेत्तिअमिहंतर तेत्तिप्रमिमाणं ।' (राजशेखर की कर्पूरकजरी, अङ्क १)। संस्कृत-भाषा कर्कश और प्राकृत भाषा सुकुमार है। पुरुष और महिला में जितना अन्तर है, इन दो भाषाओं में भी. उतना ही प्रभेद है।
१. प्रमृतं प्राकृतं काव्यं पठितु श्रोतुच ये न जानन्ति । कामस्यतत्त्वचिन्तां कुर्वन्ति, ते कथं न लज्जन्ते ?॥ २. उन्मोलति लावण्यं प्राकृतच्छायया संस्कृतपदानाम् । संस्कृतसंस्कारोत्कर्षणेन प्राकृतस्यापि प्रभावः ।। ३. नवामार्थदर्शनं संनिवेशशिशिरा बन्धद्धयः । अविरलमिदमाभुवनबन्धमिह केवलं प्राकृते ॥ ४. हर्षविशेषो विकासको मुकुलीकारकश्चाक्ष्णोः । इह बहिर्मुखोऽन्तमुखश्च हृदयस्य विस्फुरति ॥ ५. परुषः संस्कृतबन्धः प्राकृतबन्धस्तु भवति. सुकुमारः। पुरुषमहिलयोविदिहान्तरं तावदनयोः ।।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org