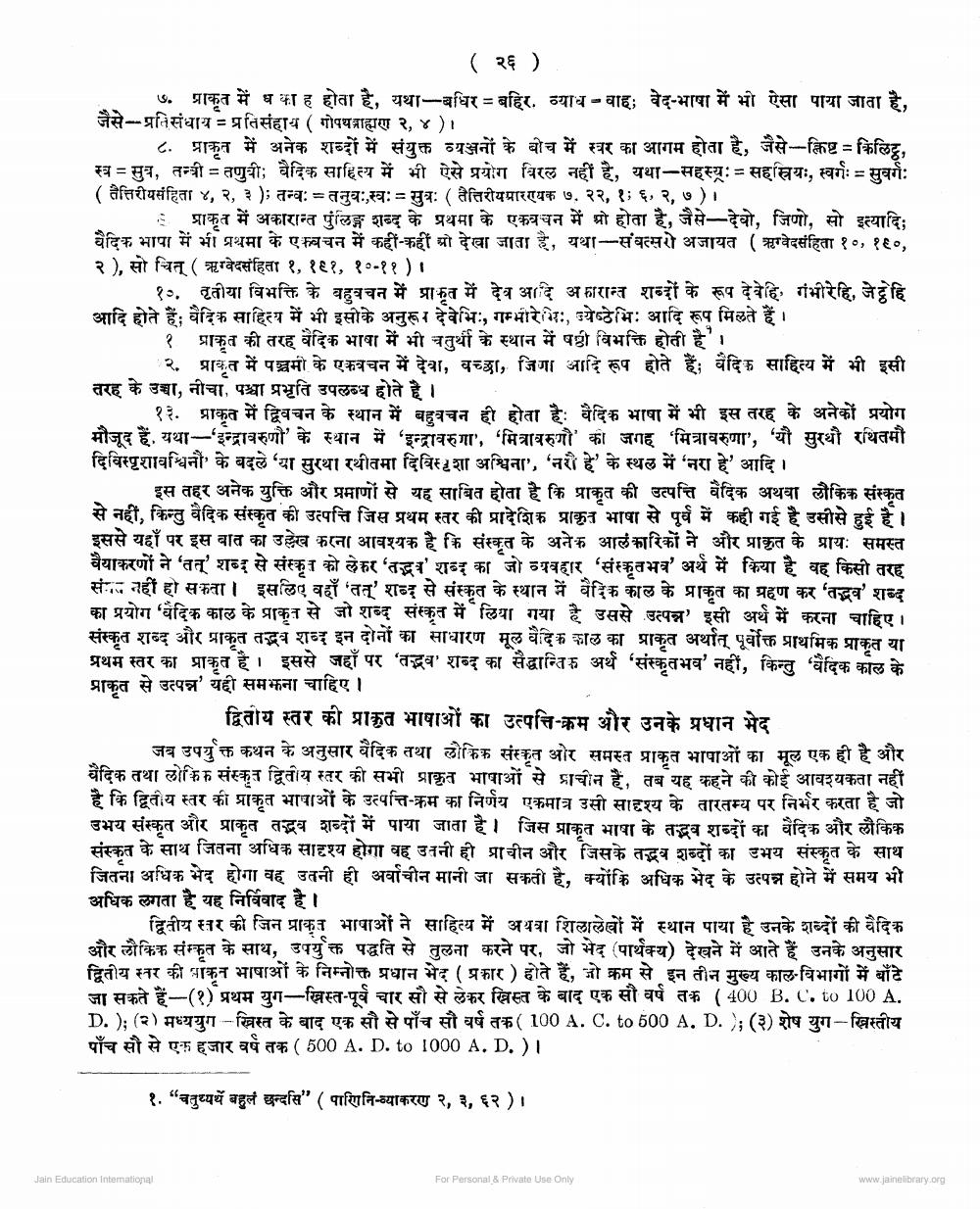________________
( २६ ) ७. प्राकृत में काह होता है, यथा-बधिर = बहिर व्याव - वाह; वेद-भाषा में भी ऐसा पाया जाता है, जैसे -- प्रतिसंधाय = प्रतिसंहाय ( गोपथब्राह्मण २४ ) ।
८. प्राकृत में अनेक शब्दों में संयुक्त व्यञ्जनों के बीच में स्वर का आगम होता है, जैसे- क्लिष्ट = किलिहू, स्त्र = सुत्र, तन्त्री = तणुत्री; वैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग विरल नहीं है, यथा - सहस्य: = सहस्रियः, स्वर्गः = सुवर्ग: ( तैत्तिरीयसंहिता ४, २, ३ ); तन्वः = तनुवः स्वः = सुत्रः ( तैत्तिरीयारण्यक ७. २२, १६, २, ७ ) ।
प्राकृत में अकारान्त पुंलिङ्ग शब्द के प्रथमा के एकवचन में श्रो होता है, जैसे-देवो, जिणो, सो इत्यादि; वैदिक भाषा में भी प्रथमा के एकवचन में कहीं-कहीं ओ देखा जाता है, यथा-संवत्सरो अजायत (ऋग्वेदसंहिता १०, १६०, २ ), सो चित् (ऋग्वेदसंहिता १, १६१, १०-११ ) ।
१०. तृतीया विभक्ति के बहुवचन में प्राकृत देव आदि अन्त शब्दों के रूप देवेहि, गंभीरेहि, जेहि आदि होते हैं; वैदिक साहित्य में भी इसीके अनुरूप देवेभिः, गम्भीरेभिः, ज्येष्ठेभिः आदि रूप मिलते हैं । प्राकृत की तरह वैदिक भाषा में भी चतुर्थी के स्थान में षष्ठी विभक्ति होती है'
१
प्राकृत में पञ्चमी के एकत्रचन में देवा, वच्छा, जिणा आदि रूप होते हैं; वैदिक साहित्य में भी इसी तरह के उच्चा, नीचा, पश्चा प्रभृति उपलब्ध होते है ।
२.
१३. प्राकृत में द्विवचन के स्थान में बहुवचन ही होता है: वैदिक भाषा में भी इस तरह के अनेकों प्रयोग मौजूद हैं, यथा-' इन्द्रावरुणी' के स्थान में 'इन्द्रावरुणा', 'मित्रावरुणौ' की जगह 'मित्रावरुणा', 'यौ सुरथी रथितमौ दिविस्पृशावश्विनौं' के बदले 'या सुरथा रथीतमा दिविस्तृशा अश्विना', 'नरौ हे' के स्थल में 'नरा हे' आदि ।
इस तहर अनेक युक्ति और प्रमाणों से यह साबित होता है कि प्राकृत की उत्पत्ति वैदिक अथवा लौकिक संस्कृत से नहीं, किन्तु वैदिक संस्कृत की उत्पत्ति जिस प्रथम स्तर की प्रादेशिक प्राकृत भाषा से पूर्व में कही गई है उसीसे हुई है । इससे यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि संस्कृत के अनेक आलंकारिकों ने और प्राकृत के प्रायः समस्त वैयाकरणों ने 'तत्' शब्द से संस्कृत को लेकर 'तद्भव' शब्द का जो व्यवहार 'संस्कृतभव' अर्थ में किया है वह किसी तरह
नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ 'तत्' शब्द से संस्कृत के स्थान में वैदिक काल के प्राकृत का ग्रहण कर 'तद्भव' शब्द का प्रयोग 'वैदिक काल के प्राकृत से जो शब्द संस्कृत में लिया गया है उससे उत्पन्न' इसी अर्थ में करना चाहिए । संस्कृत शब्द और प्राकृत तद्भव शब्द इन दोनों का साधारण मूल वैदिक काल का प्राकृत अर्थात् पूर्वोक्त प्राथमिक प्राकृत या प्रथम स्तर का प्राकृत हैं। इससे जहाँ पर 'तद्भव' शब्द का सैद्धान्तिक अर्थ 'संस्कृतभव' नहीं, किन्तु 'वैदिक काल के प्राकृत से उत्पन्न' यही समझना चाहिए ।
द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं का उत्पत्ति-क्रम और उनके प्रधान भेद
जब उपर्युक्त कथन के अनुसार वैदिक तथा लौकिक संस्कृत और समस्त प्राकृत भाषाओं का मूल एक ही है और वैदिक तथा लोकिक संस्कृत द्वितीय स्तर की सभी प्राकृत भाषाओं से प्राचीन हैं, तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं के उत्पत्ति क्रम का निर्णय एकमात्र उसी सादृश्य के तारतम्य पर निर्भर करता है जो उभय संस्कृत और प्राकृत तद्भव शब्दों में पाया जाता है। जिस प्राकृत भाषा के तद्भव शब्दों का वैदिक और लौकिक संस्कृत के साथ जितना अधिक सादृश्य होगा वह उतनी ही प्राचीन और जिसके तद्भव शब्दों का उभय संस्कृत के साथ जितना अधिक भेद होगा वह उतनी ही अर्वाचीन मानी जा सकती है, क्योंकि अधिक भेद के उत्पन्न होने में समय भी अधिक लगता है यह निर्विवाद है ।
द्वितीय स्तर की जिन प्राकृत भाषाओं ने साहित्य में अथवा शिलालेखों में स्थान पाया है उनके शब्दों की वैदिक और लौकिक संस्कृत के साथ, उपर्युक्त पद्धति से तुलना करने पर, जो भेद (पार्थक्य) देखने में आते हैं उनके अनुसार द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं के निम्नोक्त प्रधान भेद ( प्रकार ) होते हैं, जो क्रम से इन तीन मुख्य काल-विभागों में बाँटे जा सकते हैं - (१) प्रथम युग - ख्रिस्त-पूर्व चार सौ से लेकर स्त्रिस्त के बाद एक सौ वर्ष तक ( 400 BC to 100 A D. ); (२) मध्ययुग - ख्रिस्त के बाद एक सौ से पाँच सौ वर्ष तक ( 100 A. C. to 600 A. D. ); (३) शेष युग - ख्रिस्तीय पाँच सौ से एक हजार वर्ष तक ( 500 A. D. to 1000 A. D. ) ।
१. " चतुथ्यर्थे बहुलं छन्दसि " ( पाणिनि व्याकरण २, ३, ६२ ) ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org