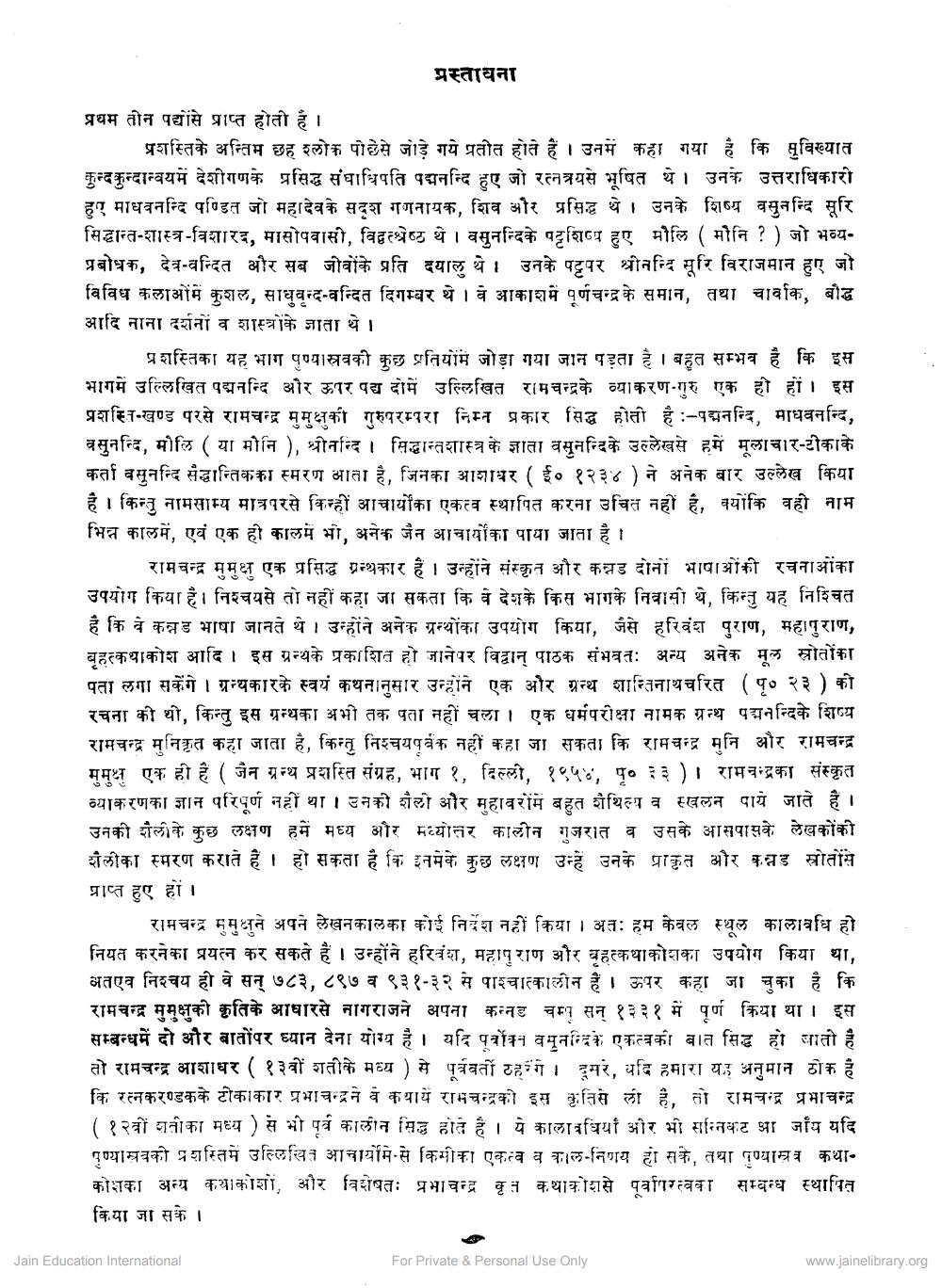________________
प्रस्तावना
प्रथम तीन पद्योंसे प्राप्त होती है।
प्रशस्तिके अन्तिम छह श्लोक पोछेसे जोड़े गये प्रतीत होते हैं । उनमें कहा गया है कि सुविख्यात कुन्दकुन्दान्वयमें देशीगणके प्रसिद्ध संघाधिपति पद्मनन्दि हुए जो रत्नत्रयसे भूषित थे। उनके उत्तराधिकारी हुए माधवनन्दि पण्डित जो महादेवके सदश गगनायक, शिव और प्रसिद्ध थे। उनके शिष्य वसुनन्दि सूरि सिद्धान्त-शास्त्र-विशारद, मासोपवासी, विद्वत्श्रेष्ठ थे। वसुनन्दिके पट्टशिष्य हुए मौलि ( मौनि ? ) जो भव्यप्रबोधक, देव-वन्दित और सब जीवोंके प्रति दयालु थे। उनके पट्टपर श्रीनन्दि सूरि विराजमान हुए जो विविध कलाओं में कुशल, साधुवन्द-वन्दित दिगम्बर थे । वे आकाशमै पूर्णचन्द्र के समान, तथा चार्वाक, बौद्ध आदि नाना दर्शनों व शास्त्रोंके ज्ञाता थे।
प्रशस्तिका यह भाग पण्यास्रवकी कुछ प्रतियोम जोड़ा गया जान पड़ता है । बहुत सम्भव है कि इस भागमें उल्लिखित पद्मनन्दि और कार पद्य दोमें उल्लिखित रामचन्द्रके व्याकरण-गुरु एक हो हों। इस प्रशस्ति-खण्ड परसे रामचन्द्र मुमुक्षकी गुरुपरम्परा निम्न प्रकार सिद्ध होती है :-पद्मनन्दि, माधवनन्दि, वसुनन्दि, मौलि ( या मौनि ), श्रीनन्दि। सिद्धान्तशास्त्र के ज्ञाता बसूनन्दिके उल्लेखसे हमें मूलाचार-टीकाके कर्ता वसुनन्दि सैद्धान्तिकका स्मरण आता है, जिनका आशावर ( ई० १२३४ ) ने अनेक बार उल्लेख किया है । किन्तु नामसाम्य मात्रपरसे किन्हीं आचार्योंका एकत्व स्थापित करना उचित नहीं है, क्योंकि वही नाम भिन्न कालमें, एवं एक ही कालमें भी, अनेक जैन आचार्योंका पाया जाता है।
रामचन्द्र ममक्ष एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार है। उन्होंने संस्कृत और कन्नड दोनों भाषाओं की रचनाओंका उपयोग किया है। निश्चयसे तो नहीं कहा जा सकता कि वे देशके किस भागके निवासी थे, किन्तु यह निश्चित है कि वे कन्नड भाषा जानते थे। उन्होंने अनेक ग्रन्थोंका उपयोग किया, जैसे हरिवंश पुराण, महापुराण, बहत्कथाकोश आदि। इस ग्रन्थके प्रकाशित हो जानेपर विद्वान् पाठक संभवत: अन्य अनेक मूल स्रोतोंका पता लगा सकेंगे। ग्रन्थकारके स्वयं कथनानुसार उन्होंने एक और ग्रन्थ शान्तिनाथचरित ( पृ० २३ ) की रचना की थी, किन्तु इस ग्रन्थका अभी तक पता नहीं चला। एक धर्मपरीक्षा नामक ग्रन्थ पद्मनन्दिके शिष्य रामचन्द्र मुनिकृत कहा जाता है, किन्तु निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि रामचन्द्र मुनि और रामचन्द्र ममक्ष एक ही है ( जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, भाग १, दिल्ली, १९५४, १०३३)। रामचन्द्रका संस्कृत व्याकरणका ज्ञान परिपूर्ण नहीं था। उनकी शैलो और मुहावरोंमें बहुत शैथिल्य व स्खलन पाये जाते है । उनकी शैलीके कुछ लक्षण हमें मध्य और मध्योतर कालीन गजरात व उसके आसपासके लेखकोंकी शैलीका स्मरण कराते हैं। हो सकता है कि इनमेंके कुछ लक्षण उन्हें उनके प्राकृत और कन्नड स्रोतोंसे प्राप्त हुए हा।
रामचन्द्र मुमुक्षने अपने लेखनकालका कोई निर्देश नहीं किया। अतः हम केवल स्थल कालावधि हो नियत करने का प्रयत्न कर सकते हैं। उन्होंने हरिवंश, महापुराण और बहत्कथाकोशका उपयोग किया था, अतएव निश्चय ही वे सन् ७८३, ८९७ व ९३१-३२ से पाश्चात्कालीन हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि रामचन्द्र मुमुक्षुको कृतिके आधारसे नागराजने अपना कन्नड चम्प सन् १३३१ में पूर्ण किया था। इस सम्बन्धमें दो और बातोंपर ध्यान देना योग्य है। यदि पूर्वोक्न वनन्दिक एकत्वकी बात सिद्ध हो जाती है तो रामचन्द्र आशाधर ( १३वीं शतीके मध्य ) से पूर्ववतो ठहरेंगे। दुमर, यदि हमारा यह अनुमान ठीक है कि रत्नकरण्डकके टीकाकार प्रभाचन्द्र ने व कयाये रामचन्द्रको इस कृतिसे ली है, तो रामचन्द्र प्रभाचन्द्र (१२वीं शतीका मध्य) से भी पूर्व कालीन सिद्ध होते है। ये कालावधियां और भी सन्निकट आ जाय यदि पण्यावको प्रशस्तिमें उल्लिखित आचार्योम-से किमीका एकत्व व काल-निणय हो सके, तथा पण्यास्रव कथा. कोशका अन्य कथाकोशों, और विशेषतः प्रभा चन्द्र कृत कथाकोशसे पूर्वापरत्वका सम्बन्ध स्थापित किया जा सके।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org