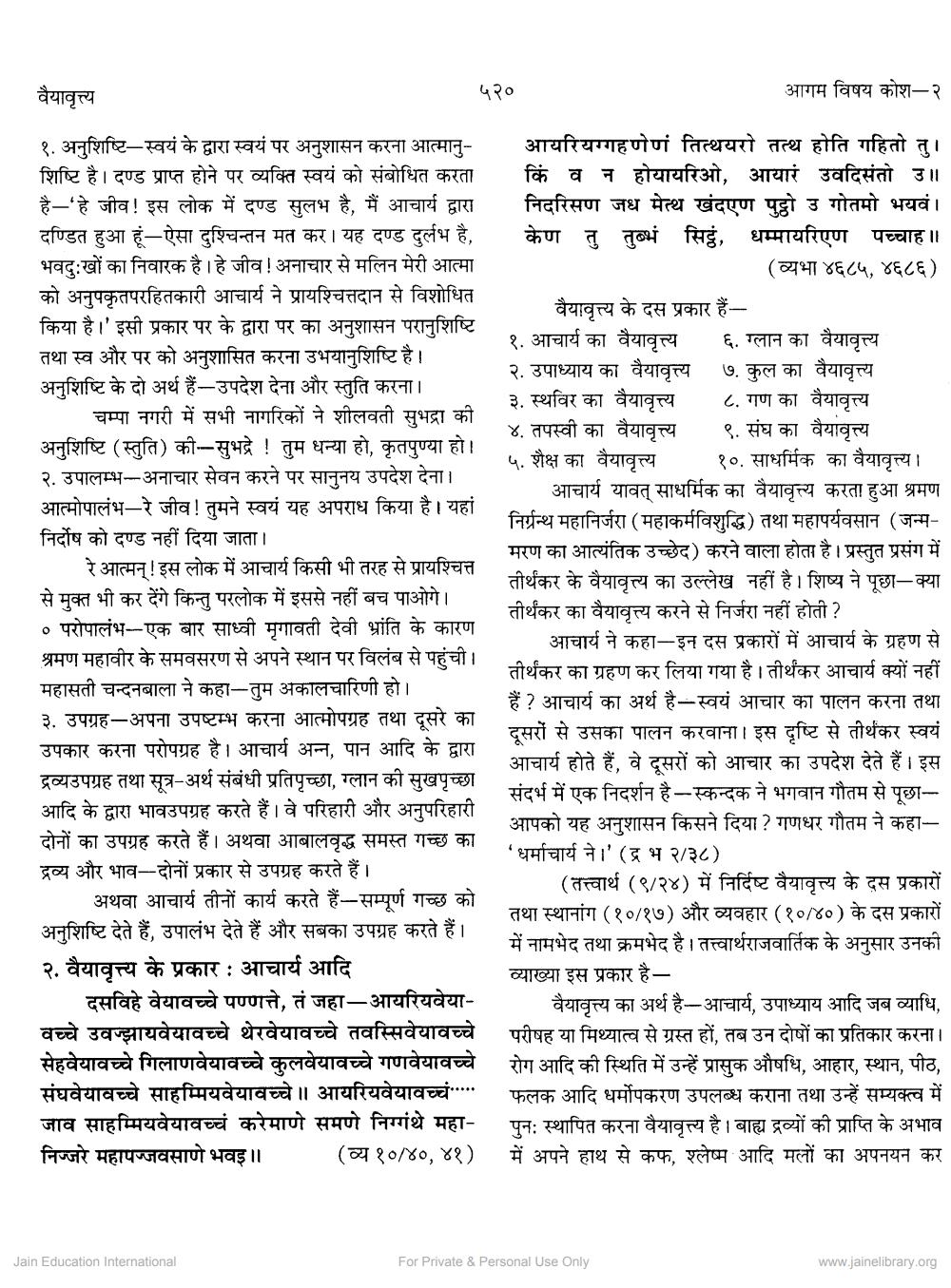________________
वैयावृत्त्य
१. अनुशिष्टि - स्वयं के द्वारा स्वयं पर अनुशासन करना आत्मानुशिष्टि है । दण्ड प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वयं को संबोधित करता है—' हे जीव ! इस लोक में दण्ड सुलभ है, मैं आचार्य द्वारा दण्डित हुआ हूं - ऐसा दुश्चिन्तन मत कर। यह दण्ड दुर्लभ है, भदुःखों का निवारक है। हे जीव ! अनाचार से मलिन मेरी आत्मा को अनुपकृतपरहितकारी आचार्य ने प्रायश्चित्तदान से विशोधित किया है।' इसी प्रकार पर के द्वारा पर का अनुशासन परानुशिष्टि तथा स्व और परको अनुशासित करना उभयानुशिष्टि है । अनुशिष्टि के दो अर्थ हैं - उपदेश देना और स्तुति करना ।
चम्पा नगरी में सभी नागरिकों ने शीलवती सुभद्रा की अनुशिष्टि (स्तुति) की – सुभद्रे ! तुम धन्या हो, कृतपुण्या हो । २. उपालम्भ - अनाचार सेवन करने पर सानुनय उपदेश देना । आत्मोपालंभ-रे जीव ! तुमने स्वयं यह अपराध किया है। यहां निर्दोष को दण्ड नहीं दिया जाता।
से
रे आत्मन् ! इस लोक में आचार्य किसी भी तरह से प्रायश्चित्त मुक्त भी कर देंगे किन्तु परलोक में इससे नहीं बच पाओगे । परोपालंभ - एक बार साध्वी मृगावती देवी भ्रांति के कारण श्रमण महावीर के समवसरण से अपने स्थान पर विलंब से पहुंची। महासती चन्दनबाला ने कहा- तुम अकालचारिणी हो ।
३. उपग्रह — अपना उपष्टम्भ करना आत्मोपग्रह तथा दूसरे का उपकार करना परोपग्रह है। आचार्य अन्न, पान आदि के द्वारा द्रव्यउपग्रह तथा सूत्र - अर्थ संबंधी प्रतिपृच्छा, ग्लान की सुखपृच्छा आदि के द्वारा भावउपग्रह करते हैं। वे परिहारी और अनुपरिहारी दोनों का उपग्रह करते हैं। अथवा आबालवृद्ध समस्त गच्छ का द्रव्य और भाव - दोनों प्रकार से उपग्रह करते हैं।
अथवा आचार्य तीनों कार्य करते हैं- सम्पूर्ण गच्छ को अनुशिष्टि देते हैं, उपालंभ देते हैं और सबका उपग्रह करते हैं । २. वैयावृत्त्य के प्रकार : आचार्य आदि
दसविहे वेयावच्चे पण्णत्ते, तं जहा- -आयरियवेयावच्चे उवज्झायवेयावच्चे थेरवेयावच्चे तवस्सिवेयावच्चे सेहवेयावच्चे गिलाणवेयावच्चे कुलवेयावच्चे गणवेयावच्चे संघवेयावच्चे साहम्मियवेयावच्चे | आयरियवेयावच्चं .... जाव साहम्मियवेयावच्चं करेमाणे समणे निग्गंथे महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवइ ॥ (व्य १०/४०, ४१)
०
Jain Education International
५२०
आगम विषय कोश - २
आयरियरगहणेणं तित्थयरो तत्थ होति गहितो तु । किं व न होयायरिओ, आयारं उवदिसंतो उ ॥ निदरिसण जध मेत्थ खंदएण पुट्ठो उ गोतमो भयवं । केण तु तुब्भं सिहं, धम्मायरिएण पच्चाह ॥ (व्यभा ४६८५, ४६८६ )
वैयावृत्त्य के दस प्रकार हैं१. आचार्य का वैयावृत्त्य २. उपाध्याय का वैयावृत्त्य ३. स्थविर का वैयावृत्त्य ४. तपस्वी का वैयावृत्त्य ५. शैक्ष का वैयावृत्त्य
६. ग्लान का वैयावृत्त्य ७. कुल का वैयावृत्त्य ८. गण का वैयावृत्त्य
९. संघ का वैयावृत्त्य
१०. साधर्मिक का वैयावृत्त्य ।
आचार्य यावत् साधर्मिक का वैयावृत्त्य करता हुआ श्रमण निर्ग्रन्थ महानिर्जरा (महाकर्मविशुद्धि) तथा महापर्यवसान (जन्ममरण का आत्यंतिक उच्छेद) करने वाला होता है। प्रस्तुत प्रसंग में तीर्थंकर के वैयावृत्त्य का उल्लेख नहीं है । शिष्य ने पूछा- क्या तीर्थंकर का वैयावृत्त्य करने से निर्जरा नहीं होती ?
आचार्य ने कहा- इन दस प्रकारों में आचार्य के ग्रहण से तीर्थंकर का ग्रहण कर लिया गया है। तीर्थंकर आचार्य क्यों नहीं हैं ? आचार्य का अर्थ है - स्वयं आचार का पालन करना तथा दूसरों से उसका पालन करवाना। इस दृष्टि से तीर्थंकर स्वयं आचार्य होते हैं, वे दूसरों को आचार का उपदेश देते हैं। इस संदर्भ में एक निदर्शन है - स्कन्दक ने भगवान गौतम से पूछाआपको यह अनुशासन किसने दिया ? गणधर गौतम ने कहा'धर्माचार्य ने।' (द्र भ २ / ३८)
(तत्त्वार्थ (९/२४) में निर्दिष्ट वैयावृत्त्य के दस प्रकारों तथा स्थानांग (१०/१७) और व्यवहार (१०/४०) के दस प्रकारों में नामभेद तथा क्रमभेद है । तत्त्वार्थराजवार्तिक के अनुसार उनकी व्याख्या इस प्रकार है
वैयावृत्त्य का अर्थ है - आचार्य, उपाध्याय आदि जब व्याधि, परीषह या मिथ्यात्व से ग्रस्त हों, तब उन दोषों का प्रतिकार करना । रोग आदि की स्थिति में उन्हें प्रासुक औषधि, आहार, स्थान, पीठ, फलक आदि धर्मोपकरण उपलब्ध कराना तथा उन्हें सम्यक्त्व में पुनः स्थापित करना वैयावृत्त्य है । बाह्य द्रव्यों की प्राप्ति के अभाव में अपने हाथ से कफ, श्लेष्म आदि मलों का अपनयन कर
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org