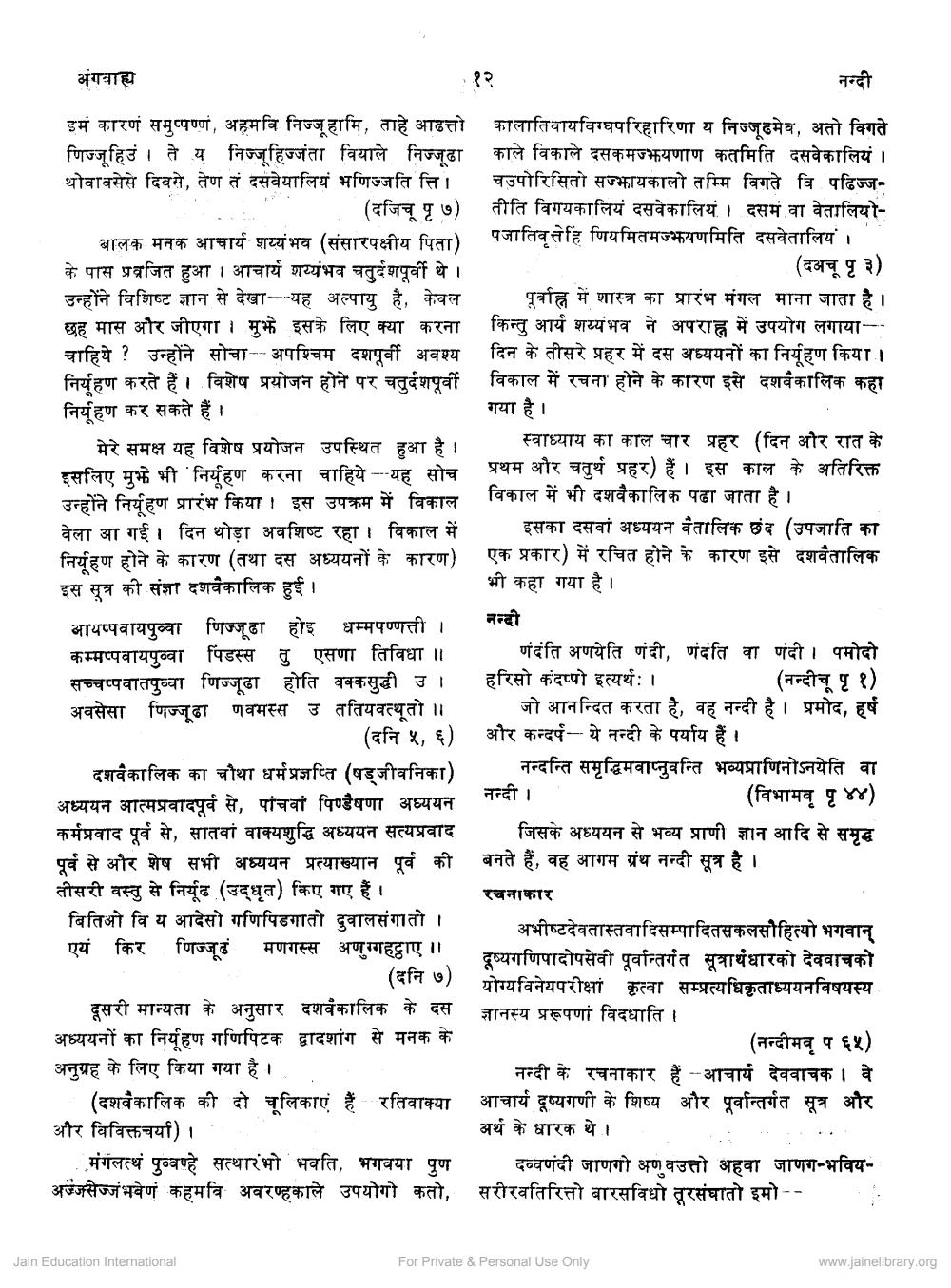________________
अंगवा
इमं कारणं समुप्पण्णं, अहमवि निज्जू हामि, ताहे आढतो णिज्जू हिउं । ते य निज्जू हिज्जता वियाले निज्जूढा थोवावसेसे दिवसे, तेण तं दसवेयालियं भणिज्जति त्ति । ( दजिचू पृ७ ) बालक मनक आचार्य शय्यंभव ( संसारपक्षीय पिता ) के पास प्रव्रजित हुआ । आचार्य शय्यंभव चतुर्दशपूर्वी थे । उन्होंने विशिष्ट ज्ञान से देखा - यह अल्पायु है, केवल छह मास और जीएगा। मुझे इसके लिए क्या करना चाहिये ? उन्होंने सोचा - अपश्चिम दशपूर्वी अवश्य निर्यूहण करते हैं । विशेष प्रयोजन होने पर चतुर्दशपूर्वी निर्यूहण कर सकते हैं ।
मेरे समक्ष यह विशेष प्रयोजन उपस्थित हुआ है । इसलिए मुझे भी निर्यूहण करना चाहिये यह सोच उन्होंने निर्यूहण प्रारंभ किया । इस उपक्रम में विकाल वेला आ गई। दिन थोड़ा अवशिष्ट रहा । विकाल में निर्यूहण होने के कारण ( तथा दस अध्ययनों के कारण ) इस सूत्र की संज्ञा दशवैकालिक हुई।
आयप्पवायपुव्वा णिज्जूढा होइ धम्मपण्णत्ती । कम्मप्पवायपुव्वा पिंडस्स तु एसणा तिविधा || सच्चप्पवातपुव्वा णिज्जूढा होति वक्कसुद्धी उ । अवसेसा णिज्जूढा णवमस्स उ तियवत्थूतो ॥ (दनि ५, ६ )
दशवैकालिक का चौथा धर्मप्रज्ञप्ति (षड्जीवनिका) अध्ययन आत्मप्रवादपूर्व से, पांचवां पिण्डेषणा अध्ययन कर्मप्रवाद पूर्व से, सातवां वाक्यशुद्धि अध्ययन सत्यप्रवाद पूर्व से और शेष सभी अध्ययन प्रत्याख्यान पूर्व की तीसरी वस्तु से निर्यूढ (उद्धृत ) किए गए I बितिओ व आदेसो गणिपिडगातो दुवालसंगातो । एयं किर णिज्जू ढं मणगस्स अणुग्गहट्ठाए । (दनि ७ ) दूसरी मान्यता के अनुसार दशर्वकालिक के दस अध्ययनों का निर्यूहण गणिपिटक द्वादशांग से मनक के अनुग्रह के लिए किया गया है ।
( दशवैकालिक की दो चूलिकाएं हैं रतिवाक्या और विविक्तचर्या) |
मंगलत्थं पुoad सत्थारंभो भवति, भगवया पुण अज्जसेज्जं भवेणं कहमत्रि अवरहकाले उपयोगो कतो,
Jain Education International
नन्दी
कालातिवायविग्धपरिहारिणा य निज्जूढमेव, अतो विगते काले विकाले दसकमज्झयणाण कतमिति दसवेकालियं । चउपोरिसितो सज्झायकालो तम्मि विगते वि पढिज्जतीति विगयकालियं दसवेकालियं । दसमं वा वेतालियोपजातिवृतेहि नियमितमज्झयणमिति दसवेतालियौं । ( दअचू पृ ३ ) पूर्वाह्न में शास्त्र का प्रारंभ मंगल माना जाता है । किन्तु आर्य शय्यंभव ने अपराह्न में उपयोग लगाया -- दिन के तीसरे प्रहर में दस अध्ययनों का निर्यूहण किया । विकाल में रचना होने के कारण इसे दशवैकालिक कहा गया है ।
स्वाध्याय का काल चार प्रहर ( दिन और रात के प्रथम और चतुर्थ प्रहर ) हैं । इस काल के अतिरिक्त विकाल में भी दशवैकालिक पढा जाता है ।
इसका दसवां अध्ययन वैतालिक छंद ( उपजाति का एक प्रकार) में रचित होने के कारण इसे दंशवैतालिक भी कहा गया है ।
नन्दी
गंदंति अणयेति णंदी, गंदति वा गंदी । पमोदो हरिसो कंदप्पो इत्यर्थः । ( नन्दी पृ १ ) जो आनन्दित करता है, वह नन्दी है । प्रमोद, हर्ष और कन्दर्प- ये नन्दी के पर्याय हैं ।
नन्दन्ति समृद्धिमवाप्नुवन्ति भव्यप्राणिनोऽनयेति वा नन्दी | ( विभामवृ पृ ४४ )
जिसके अध्ययन से भव्य प्राणी ज्ञान आदि से समृद्ध बनते हैं, वह आगम ग्रंथ नन्दी सूत्र है ।
रचनाकार
अभीष्टदेवतास्तवादिसम्पादितसकलसौहित्यो भगवान् दूष्यगणिपादोपसेवी पूर्वान्तर्गत सूत्रार्थधारको देववाचको योग्यविनेयपरीक्षां कृत्वा सम्प्रत्यधिकृताध्ययनविषयस्य ज्ञानस्य प्ररूपणां विदधाति ।
( नन्दीमवृप ६५ )
नन्दी के रचनाकार हैं -- आचार्य देववाचक । वे आचार्य दृष्यगणी के शिष्य और पूर्वान्तर्गत सूत्र और अर्थ के धारक थे ।
दवणंदी जागो अणुवउत्तो अहवा जाणग-भवियसरीरवतिरित्तो बारसविधो तूरसंघातो इमो
For Private & Personal Use Only
--
www.jainelibrary.org