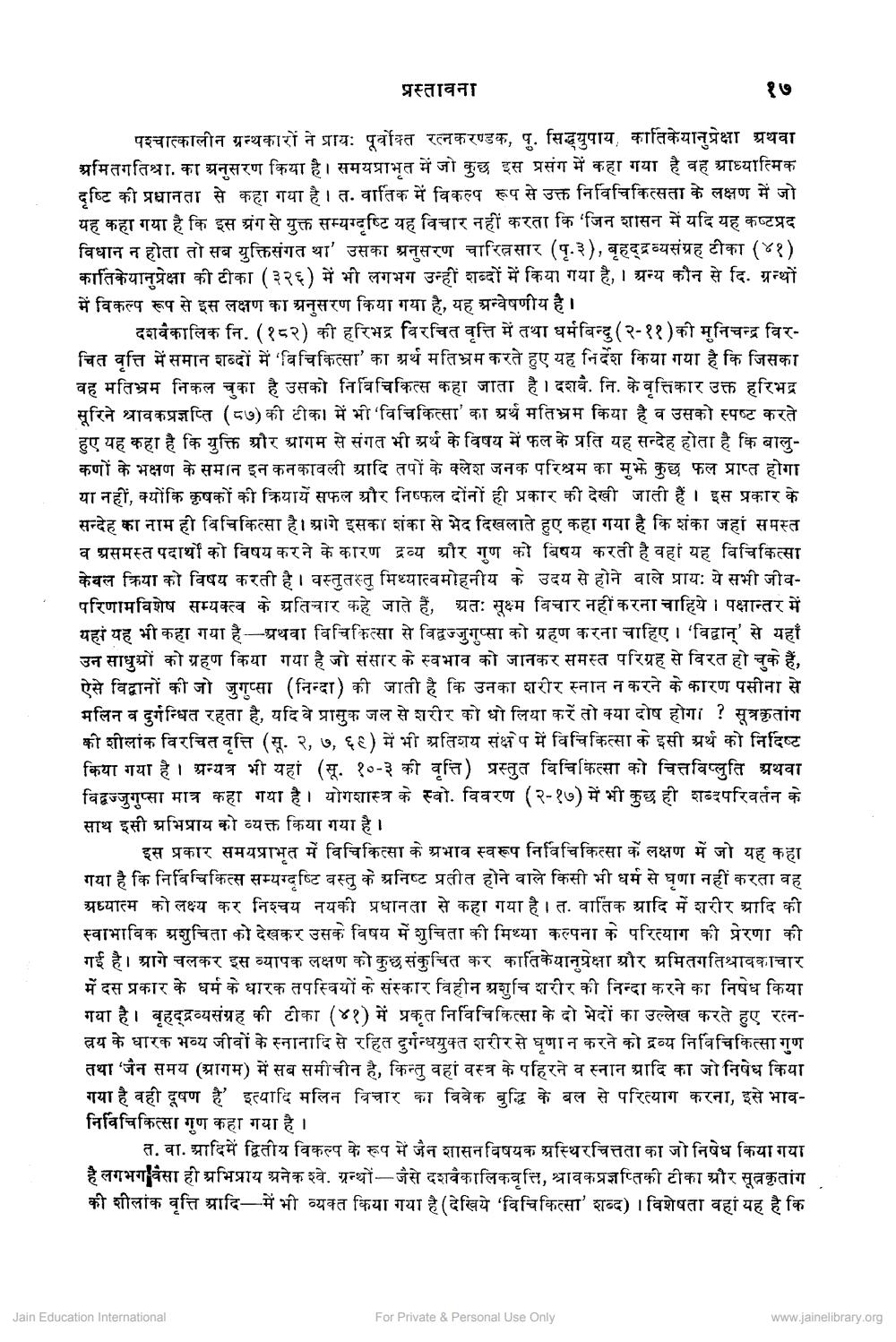________________
प्रस्तावना
पश्चात्कालीन ग्रन्थकारों ने प्राय: पूर्वोक्त रत्नकरण्डक, पु. सिद्धयुपाय, कातिकेयानुप्रेक्षा अथवा अमितगतिश्रा. का अनसरण किया है। समयप्राभत में जो कुछ इस प्रसंग में कहा गया है वह आध्यात्मिक दृष्टि की प्रधानता से कहा गया है। त. वार्तिक में विकल्प रूप से उक्त निविचिकित्सता के लक्षण में जो यह कहा गया है कि इस अंग से युक्त सम्यग्दष्टि यह विचार नहीं करता कि 'जिन शासन में यदि यह कष्टप्रद विधान न होता तो सब युक्तिसंगत था' उसका अनुसरण चारित्रसार (पृ.३), बृहद्रव्यसंग्रह टीका (४१) कार्तिकेयानप्रेक्षा की टीका (३२६) में भी लगभग उन्हीं शब्दों में किया गया है, । अन्य कौन से दि. ग्रन्थों में विकल्प रूप से इस लक्षण का अनुसरण किया गया है, यह अन्वेषणीय है।
दशवकालिक नि. (१८२) की हरिभद्र विरचित वृत्ति में तथा धर्मबिन्दु (२-११)की मूनिचन्द्र विरचित वत्ति में समान शब्दों में विचिकित्सा' का अर्थ मतिभ्रम करते हुए यह निर्देश किया गया है कि जिसका वह मतिभ्रम निकल चुका है उसको निविचिकित्स कहा जाता है । दशवै. नि. के वृत्तिकार उक्त हरिभद्र सरिने श्रावकप्रज्ञप्ति (८७) की टीका में भी 'विचिकित्सा' का अर्थ मतिभ्रम किया है व उसको स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि युक्ति और आगम से संगत भी अर्थ के विषय में फल के प्रति यह सन्देह होता है कि बालुकणों के भक्षण के समान इन कनकावली आदि तपों के क्लेश जनक परिश्रम का मुझे कुछ फल प्राप्त होगा या नहीं, क्योंकि कृषकों की क्रियायें सफल और निष्फल दोनों ही प्रकार की देखी जाती हैं। इस प्रकार के सन्देह का नाम ही विचिकित्सा है। आगे इसका शंका से भेद दिखलाते हुए कहा गया है कि शंका जहां समस्त व असमस्त पदार्थों को विषय करने के कारण द्रव्य और गुण को बिषय करती है वहां यह विचिकित्सा केवल क्रिया को विषय करती है। वस्तुतस्तु मिथ्यात्वमोहनीय के उदय से होने वाले प्रायः ये सभी जीवपरिणामविशेष सम्यक्त्व के अतिचार कहे जाते हैं, अतः सूक्ष्म विचार नहीं करना चाहिये। पक्षान्तर में यहां यह भी कहा गया है -अथवा विचिकित्सा से विद्वज्जुगुप्सा को ग्रहण करना चाहिए । 'विद्वान्' से यहाँ उन साधुओं को ग्रहण किया गया है जो संसार के स्वभाव को जानकर समस्त परिग्रह से विरत हो चुके हैं, ऐसे विद्वानों की जो जुगप्सा (निन्दा) की जाती है कि उनका शरीर स्नान न करने के कारण पसीना से मलिन व दुर्गन्धित रहता है, यदि वे प्रासुक जल से शरीर को धो लिया करें तो क्या दोष होगा ? सूत्रकृतांग की शीलांक विरचित वत्ति (सू. २, ७, ६६) में भी अतिशय संक्षेप में विचिकित्सा के इसी अर्थ को निर्दिष्ट किया गया है। अन्यत्र भी यहां (सू. १०-३ की वृत्ति) प्रस्तुत विचिकित्सा को चित्तविप्लुति अथवा विद्वज्जूगप्सा मात्र कहा गया है। योगशास्त्र के स्वो. विवरण (२-१७) में भी कुछ ही शब्दपरिवर्तन के साथ इसी अभिप्राय को व्यक्त किया गया है।
इस प्रकार समयप्राभत में विचिकित्सा के अभाव स्वरूप निर्विचिकित्सा के लक्षण में जो यह कहा गया है कि निर्विचिकित्स सम्यग्दृष्टि वस्तु के अनिष्ट प्रतीत होने वाले किसी भी धर्म से घृणा नहीं करता वह अध्यात्म को लक्ष्य कर निश्चय नयकी प्रधानता से कहा गया है। त. वार्तिक आदि में शरीर आदि की स्वाभाविक अशुचिता को देखकर उसके विषय में शुचिता की मिथ्या कल्पना के परित्याग की प्रेरणा की गई है। आगे चलकर इस व्यापक लक्षण को कुछ संकुचित कर कार्तिकेयानप्रेक्षा और अमितगतिश्रावकाचार में दस प्रकार के धर्म के धारक तपस्वियों के संस्कार विहीन अशचि शरीर की निन्दा करने का निषेध किया गया है। बहद्रव्यसंग्रह की टीका (४१) में प्रकत निविचिकित्सा के दो भेदों का उल्लेख करते हए रत्नत्रय के धारक भव्य जीवों के स्नानादि से रहित दुर्गन्धयुक्त शरीर से घणान करने को द्रव्य निविचिकित्सा गण तथा 'जैन समय (आगम) में सब समीचीन है, किन्तु वहां वस्त्र के पहिरने व स्नान आदि का जो निषेध किया गया है वही दूषण है' इत्यादि मलिन विचार का विवेक बुद्धि के बल से परित्याग करना, इसे भावनिविचिकित्सा गुण कहा गया है।
त. वा. आदिमें द्वितीय विकल्प के रूप में जैन शासनविषयक अस्थिरचित्तता का जो निषेध किया गया है लगभग वैसा ही अभिप्राय अनेक श्वे. ग्रन्थों-जैसे दशवकालिकवत्ति, श्रावकप्रज्ञप्तिकी टीका और सूत्रकृतांग की शीलांक वत्ति आदि में भी व्यक्त किया गया है (देखिये 'विचिकित्सा' शब्द) । विशेषता वहां यह है कि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org