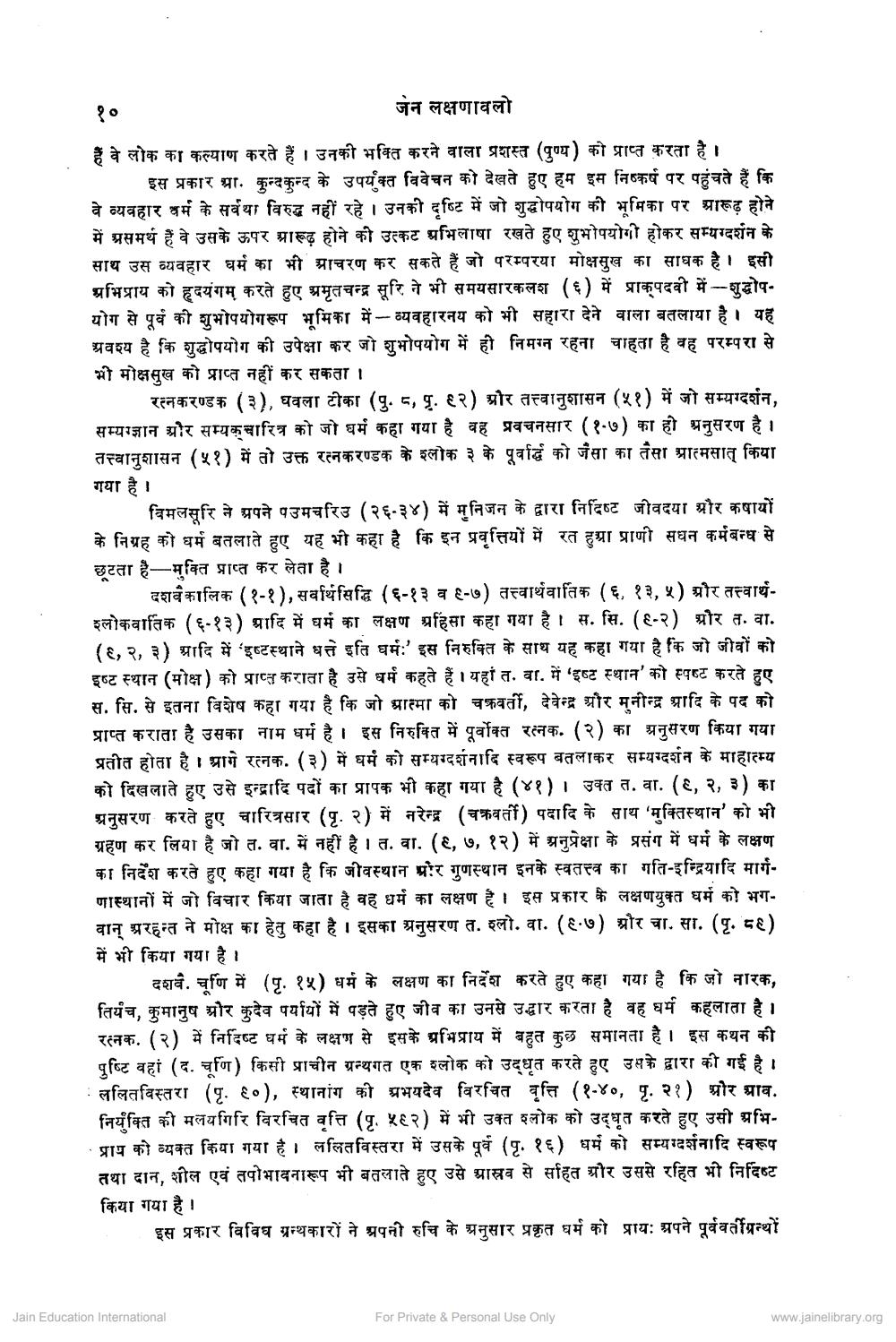________________
१०
जेन लक्षणावलो
हैं वे लोक का कल्याण करते हैं । उनकी भक्ति करने वाला प्रशस्त (पुण्य) को प्राप्त करता है ।
इस प्रकार प्रा. कुन्दकुन्द के उपर्युक्त विवेचन को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे व्यवहार धर्म के सर्वथा विरुद्ध नहीं रहे । उनकी दृष्टि में जो शुद्धोपयोग की भूमिका पर श्रारूढ़ होने में असमर्थ हैं वे उसके ऊपर प्रारूढ़ होने को उत्कट अभिलाषा रखते हुए शुभोपयोगी होकर सम्यग्दर्शन के साथ उस व्यवहार धर्म का भी आचरण कर सकते हैं जो परम्परया मोक्षसुख का साधक है । इसी अभिप्राय को हृदयंगम करते हुए अमृतचन्द्र सूरि ने भी समयसारकलश ( ६ ) में प्राक्पदवी में -- शुद्धोपयोग से पूर्व की शुभोपयोगरूप भूमिका में - व्यवहारनय को भी सहारा देने वाला बतलाया है । यह अवश्य है कि शुद्धोपयोग की उपेक्षा कर जो शुभोपयोग में ही निमग्न रहना चाहता है वह परम्परा से भी मोक्षसुख को प्राप्त नहीं कर सकता ।
रत्नकरण्डक ( ३ ), घवला टीका (पु. ८, पृ. ६२ ) और तत्त्वानुशासन (५१) में जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र को जो धर्म कहा गया है वह प्रवचनसार (१-७) का ही अनुसरण है । तत्वानुशासन (५१) में तो उक्त रत्नकरण्डक के श्लोक ३ के पूर्वार्द्ध को जैसा का तैसा आत्मसात् किया गया है ।
विमलसूरि ने अपने पउमचरिउ (२६-३४) में मुनिजन के द्वारा निर्दिष्ट जीवदया और कषायों के निग्रह को धर्म बतलाते हुए यह भी कहा है कि इन प्रवृत्तियों में रत हुआ प्राणी सघन कर्मबन्ध से छूटता है— मुक्ति प्राप्त कर लेता है ।
कालिक (१-१), सर्वार्थसिद्धि ( ६- १३ व ६-७ ) तत्त्वार्थवार्तिक ( ६, १३, ५) और तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक ( ६-१३) श्रादि में धर्म का लक्षण श्रहिंसा कहा गया है । स. सि. ( ६-२ ) और त. वा. (६, २, ३) आदि में 'इष्टस्थाने धत्ते इति धर्म:' इस निरुक्ति के साथ यह कहा गया है कि जो जीवों को इष्ट स्थान (मोक्ष) को प्राप्त कराता है उसे धर्म कहते हैं। यहां त. वा. में 'इष्ट स्थान' को स्पष्ट करते हुए स. सि. से इतना विशेष कहा गया है कि जो आत्मा को चक्रवर्ती, देवेन्द्र और मुनीन्द्र श्रादि के पद को प्राप्त कराता है उसका नाम धर्म है । इस निरुक्ति में पूर्वोक्त रत्नक ( २ ) का अनुसरण किया गया प्रतीत होता है । प्रागे रत्नक. (३) में धर्म को सम्यग्दर्शनादि स्वरूप बतलाकर सम्यग्दर्शन के माहात्म्य को दिखलाते हुए उसे इन्द्रादि पदों का प्रापक भी कहा गया है ( ४१ ) । उक्त त. वा. (६, २, ३) का अनुसरण करते हुए चारित्रसार (पृ. २) में नरेन्द्र ( चक्रवर्ती) पदादि के साथ 'मुक्तिस्थान' को भी ग्रहण कर लिया है जो त. वा. में नहीं है । त. वा. ( ६, ७, १२) में अनुप्रेक्षा के का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जीवस्थान र गुणस्थान इनके स्वतत्व का णास्थानों में जो विचार किया जाता है वह धर्म का लक्षण है । इस प्रकार के लक्षणयुक्त धर्म को भगवान् अरहन्त ने मोक्ष का हेतु कहा है । इसका अनुसरण त. इलो. वा. ( ६-७ में भी किया गया है ।
)
और चा. सा. (पृ. ८8 )
दशवे. चूर्ण में (पृ. १५) धर्म के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो नारक, तिर्यंच, कुमानुष और कुदेव पर्यायों में पड़ते हुए जीव का उनसे उद्धार करता है वह धर्म कहलाता है । रत्नक. (२) में निर्दिष्ट धर्म के लक्षण से इसके अभिप्राय में बहुत कुछ समानता है । इस कथन की पुष्टि वहां (द. चूर्ण) किसी प्राचीन ग्रन्थगत एक श्लोक को उद्धृत करते हुए उसके द्वारा की गई है । ललितविस्तरा (पृ. ६०), स्थानांग की प्रभयदेव विरचित वृत्ति (१-४०, पृ. २१) और भाव. नियुक्ति की मलयगिरि विरचित वृत्ति (पृ. ५६२ ) में भी उक्त श्लोक को उद्धृत करते हुए उसी अभिप्राय को व्यक्त किया गया है। ललितविस्तरा में उसके पूर्व (पृ. १६) धर्म को सम्यग्दर्शनादि स्वरूप तथा दान, शील एवं तपोभावनारूप भी बतलाते हुए उसे श्रस्रव से सहित और उससे रहित भी निर्दिष्ट किया गया है।
इस प्रकार विविध ग्रन्थकारों ने अपनी रुचि के अनुसार प्रकृत धर्म को प्रायः अपने पूर्ववर्ती ग्रन्थों
Jain Education International
प्रसंग में धर्म के लक्षण गति- इन्द्रियादि मार्ग
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org