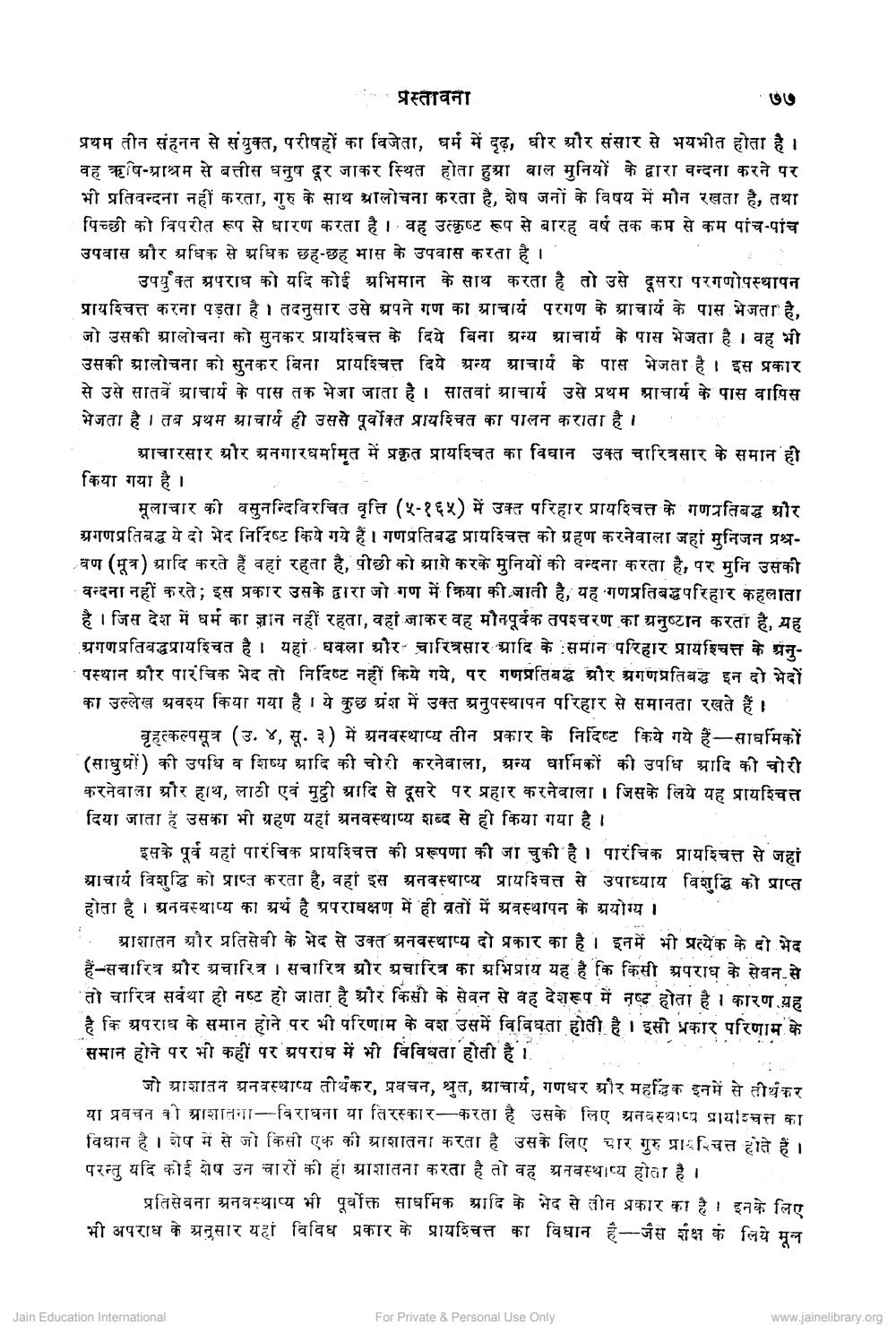________________
प्रस्तावना
प्रथम तीन संहनन से संयुक्त, परीषहों का विजेता, धर्म में दृढ़, धीर और संसार से भयभीत होता है। वह ऋषि-पाश्रम से बत्तीस धनुष दूर जाकर स्थित होता हुआ बाल मुनियों के द्वारा वन्दना करने पर भी प्रतिवन्दना नहीं करता, गुरु के साथ आलोचना करता है, शेष जनों के विषय में मौन रखता है, तथा पिच्छी को विपरीत रूप से धारण करता है। वह उत्कृष्ट रूप से बारह वर्ष तक कम से कम पांच-पांच उपवास और अधिक से अधिक छह-छह मास के उपवास करता है।
उपर्युक्त अपराध को यदि कोई अभिमान के साथ करता है तो उसे दूसरा परगणोपस्थापन प्रायश्चित्त करना पड़ता है। तदनुसार उसे अपने गण का प्राचार्य परगण के प्राचार्य के पास भेजता है, जो उसकी आलोचना को सुनकर प्रायश्चित्त के दिये बिना अन्य प्राचार्य के पास भेजता है । वह भी उसकी आलोचना को सुनकर बिना प्रायश्चित्त दिये अन्य आचार्य के पास भेजता है। इस प्रकार से उसे सातवें आचार्य के पास तक भेजा जाता है। सातवां प्राचार्य उसे प्रथम प्राचार्य के पास वापिस भेजता है। तब प्रथम आचार्य ही उससे पूर्वोक्त प्रायश्चित का पालन कराता है।
प्राचारसार और अनगारधर्मामृत में प्रकृत प्रायश्चित का विधान उक्त चारित्रसार के समान ही किया गया है।
___ मुलाचार की वसूनन्दिविरचित वृत्ति (५-१६५) में उक्त परिहार प्रायश्चित्त के गणप्रतिबद्ध और अगणप्रतिबद्ध ये दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं। गणप्रतिबद्ध प्रायश्चित्त को ग्रहण करनेवाला जहां मुनिजन प्रथवण (मूत्र) आदि करते हैं वहां रहता है, पीछी को आगे करके मुनियों की वन्दना करता है, पर मुनि उसकी वन्दना नहीं करते; इस प्रकार उसके द्वारा जो गण में क्रिया की जाती है, यह गणप्रतिबद्धपरिहार कहलाता है । जिस देश में धर्म का ज्ञान नहीं रहता, वहां जाकर वह मौनपूर्वक तपश्चरण का अनुष्ठान करता है, यह अगणप्रतिबद्धप्रायश्चित है। यहां धवला और चारित्रसार आदि के समान परिहार प्रायश्चित्त के अनुपस्थान और पारंचिक भेद तो निर्दिष्ट नहीं किये गये, पर गणप्रतिबद्ध और अगणप्रतिबद्ध इन दो भेदों का उल्लेख अवश्य किया गया है । ये कुछ अंश में उक्त अनुपस्थापन परिहार से समानता रखते हैं।
बृहत्कल्पसूत्र (उ. ४, सू. ३) में अनवस्थाप्य तीन प्रकार के निर्दिष्ट किये गये हैं-सामिकों (साधुनों) की उपधि व शिष्य आदि की चोरी करनेवाला, अन्य धार्मिकों की उपधि आदि की चोरी करनेवाला और हाथ, लाठी एवं मुट्ठी आदि से दूसरे पर प्रहार करनेवाला। जिसके लिये यह प्रायश्चित्त दिया जाता है उसका भी ग्रहण यहां अनवस्थाप्य शब्द से ही किया गया है।
___ इसके पूर्व यहां पारंचिक प्रायश्चित्त की प्ररूपणा की जा चुकी है। पारंचिक प्रायश्चित्त से जहां प्राचार्य विशुद्धि को प्राप्त करता है, वहां इस अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त से उपाध्याय विशुद्धि को प्राप्त होता है । अनवस्थाप्य का अर्थ है अपराधक्षण में ही व्रतों में अवस्थापन के अयोग्य । '. अाशातन और प्रतिसेवी के भेद से उक्त अनवस्थाप्य दो प्रकार का है। इनमें भी प्रत्येक के दो भेद हैं-सचारित्र और प्रचारित्र । सचारित्र और प्रचारित्र का अभिप्राय यह है कि किसी अपराध के सेवन.से तो चारित्र सर्वथा ही नष्ट हो जाता है और किसी के सेवन से वह देशरूप में नष्ट होता है। कारण यह है कि अपराध के समान होने पर भी परिणाम के वश उसमें विविधता होती है । इसी प्रकार परिणाम के समान होने पर भी कहीं पर अपराध में भी विविधता होती है।
जो अाशातन अनवस्थाप्य तीर्थकर, प्रवचन, श्रुत, आचार्य, गणधर और महद्धिक इनमें से तीर्थकर या प्रवचन को पाशातगा-विराधना या तिरस्कार करता है उसके लिए अनवस्थापय प्रायोचित्त का विधान है। शेष में से जो किसी एक की पाशातना करता है उसके लिए चार गुरु प्रायश्चित्त होते हैं। परन्तु यदि कोई शेष उन चारों की ही पाशातना करता है तो वह अनवस्थाप्य होता है ।
प्रतिसेवना अनवस्थाप्य भी पूर्वोक्त सार्मिक आदि के भेद से तीन प्रकार का है। इनके लिए भी अपराध के अनुसार यहां विविध प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान है--जैस शंक्ष के लिये मूल
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org