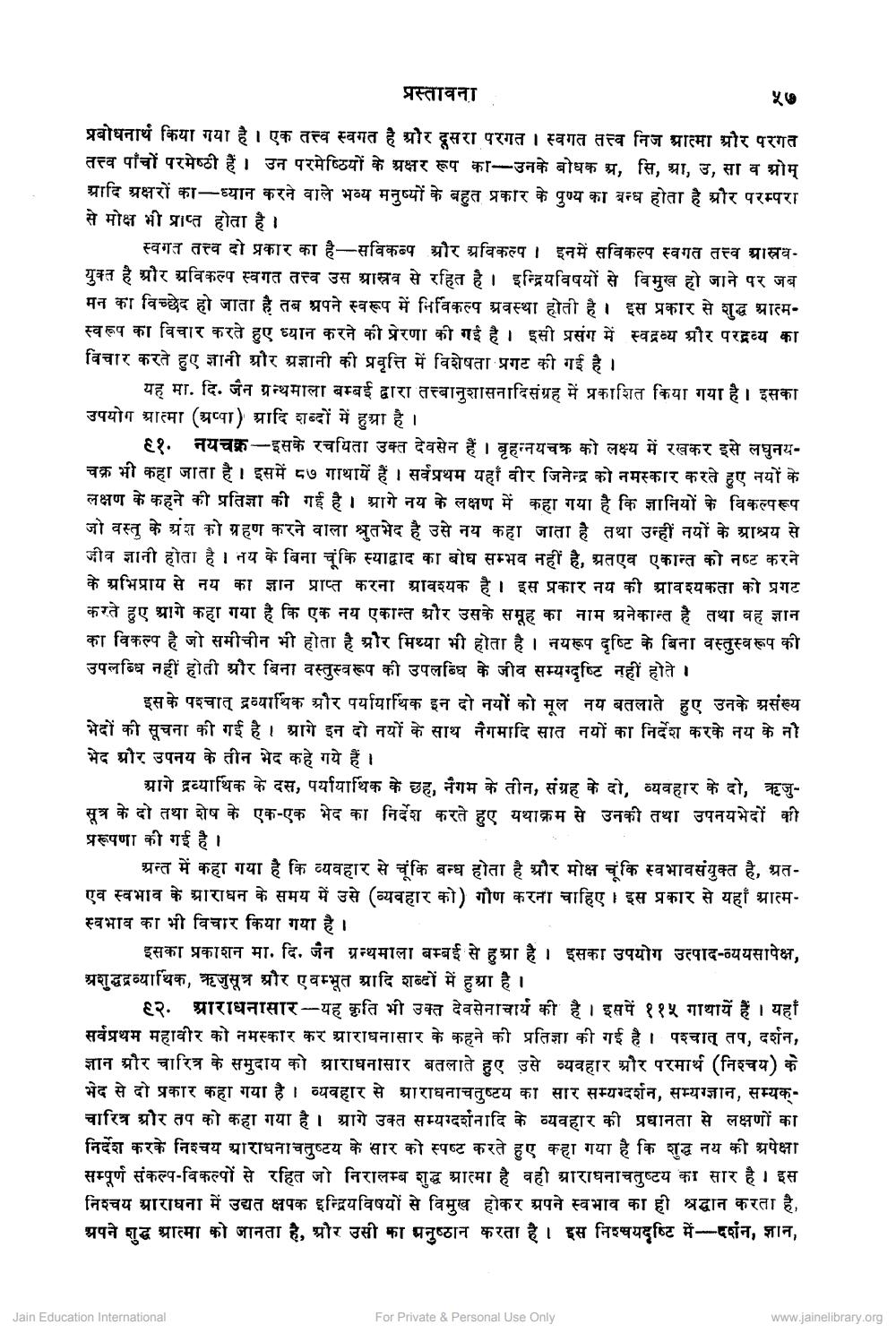________________
प्रस्तावना
प्रबोधनार्थ किया गया है। एक तत्त्व स्वगत है और दूसरा परगत । स्वगत तत्त्व निज प्रात्मा और परगत तत्त्व पाँचों परमेष्ठी हैं। उन परमेष्ठियों के अक्षर रूप का-उनके बोधक अ, सि, पा, उ, सा व प्रोम् प्रादि अक्षरों का ध्यान करने वाले भव्य मनुष्यों के बहुत प्रकार के पुण्य का बन्ध होता है और परम्परा से मोक्ष भी प्राप्त होता है।
स्वगत तत्त्व दो प्रकार का है-सविकप और अविकल्प। इनमें सविकल्प स्वगत तत्त्व प्रास्रव. युक्त है और अविकल्प स्वगत तत्त्व उस प्रास्रव से रहित है। इन्द्रियविषयों से विमुख हो जाने पर जब मन का विच्छेद हो जाता है तब अपने स्वरूप में निर्विकल्प अवस्था होती है। इस प्रकार से शुद्ध प्रात्मस्वरूप का विचार करते हुए ध्यान करने की प्रेरणा की गई है। इसी प्रसंग में स्वद्रव्य और परद्रव्य का विचार करते हुए ज्ञानी और अज्ञानी की प्रवृत्ति में विशेषता प्रगट की गई है।
यह मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई द्वारा तत्त्वानुशासनादिसंग्रह में प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग आत्मा (अप्पा) आदि शब्दों में हया है।
६१. नयचक्र-इसके रचयिता उक्त देवसेन हैं। बृहन्नयचक्र को लक्ष्य में रखकर इसे लघुनयचक्र भी कहा जाता है। इसमें ८७ गाथायें हैं । सर्वप्रथम यहाँ वीर जिनेन्द्र को नमस्कार करते हुए नयों के लक्षण के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। आगे नय के लक्षण में कहा गया है कि ज्ञानियों के विकल्परूप जो वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला श्रुतभेद है उसे नय कहा जाता है तथा उन्हीं नयों के आश्रय से
नी होता है। नय के बिना चंकि स्याद्वाद का बोध सम्भव नहीं है, अतएव एकान्त को नष्ट करने के अभिप्राय से नय का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार नय की आवश्यकता को प्रगट करते हुए आगे कहा गया है कि एक नय एकान्त और उसके समूह का नाम अनेकान्त है तथा वह ज्ञान का विकल्प है जो समीचीन भी होता है और मिथ्या भी होता है। नयरूप दृष्टि के बिना वस्तुस्वरूप की उपलब्धि नहीं होती और बिना वस्तुस्वरूप की उपलब्धि के जीव सम्यग्दृष्टि नहीं होते।
इसके पश्चात् द्रव्यार्थिक और पर्यायाथिक इन दो नयों को मूल नय बतलाते हुए उनके असंख्य भेदों की सूचना की गई है। आगे इन दो नयों के साथ नैगमादि सात नयों का निर्देश करके नय के नौ भेद और उपनय के तीन भेद कहे गये हैं।
आगे द्रव्याथिक के दस, पर्यायाथिक के छह, नैगम के तीन, संग्रह के दो, व्यवहार के दो, ऋजुसूत्र के दो तथा शेष के एक-एक भेद का निर्देश करते हुए यथाक्रम से उनकी तथा उपनयभेदों की प्ररूपणा की गई है।
अन्त में कहा गया है कि व्यवहार से चूंकि बन्ध होता है और मोक्ष चूंकि स्वभावसंयुक्त है, अतएव स्वभाव के अाराधन के समय में उसे (व्यवहार को) गौण करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ आत्मस्वभाव का भी विचार किया गया है।
इसका प्रकाशन मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई से हुआ है। इसका उपयोग उत्पाद-व्ययसापेक्ष, अशुद्धद्रव्यार्थिक, ऋजुसूत्र और एवम्भूत आदि शब्दों में हुआ है।
२. पाराधनासार-यह कृति भी उक्त देवसेनाचार्य की है। इसमें ११५ गाथायें हैं । यहाँ सर्वप्रथम महावीर को नमस्कार कर आराधनासार के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। पश्चात् तप, दर्शन, ज्ञान और चारित्र के समुदाय को आराधनासार बतलाते हए उसे व्यवहार और परमार्थ (निश्चय) के भेद से दो प्रकार कहा गया है। व्यवहार से आराधनाचतुष्टय का सार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तप को कहा गया है। आगे उक्त सम्यग्दर्शनादि के व्यवहार की प्रधानता से लक्षणों का निर्देश करके निश्चय पाराधनाचतुष्टय के सार को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि शुद्ध नय की अपेक्षा सम्पूर्ण संकल्प-विकल्पों से रहित जो निरालम्ब शद्ध आत्मा है वही आराधनाचतुष्टय का सार है। इस निश्चय आराधना में उद्यत क्षपक इन्द्रियविषयों से विमुख होकर अपने स्वभाव का ही श्रद्धान करता है, अपने शुद्ध आत्मा को जानता है, और उसी का अनुष्ठान करता है । इस निश्चयदृष्टि में-दर्शन, ज्ञान,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org