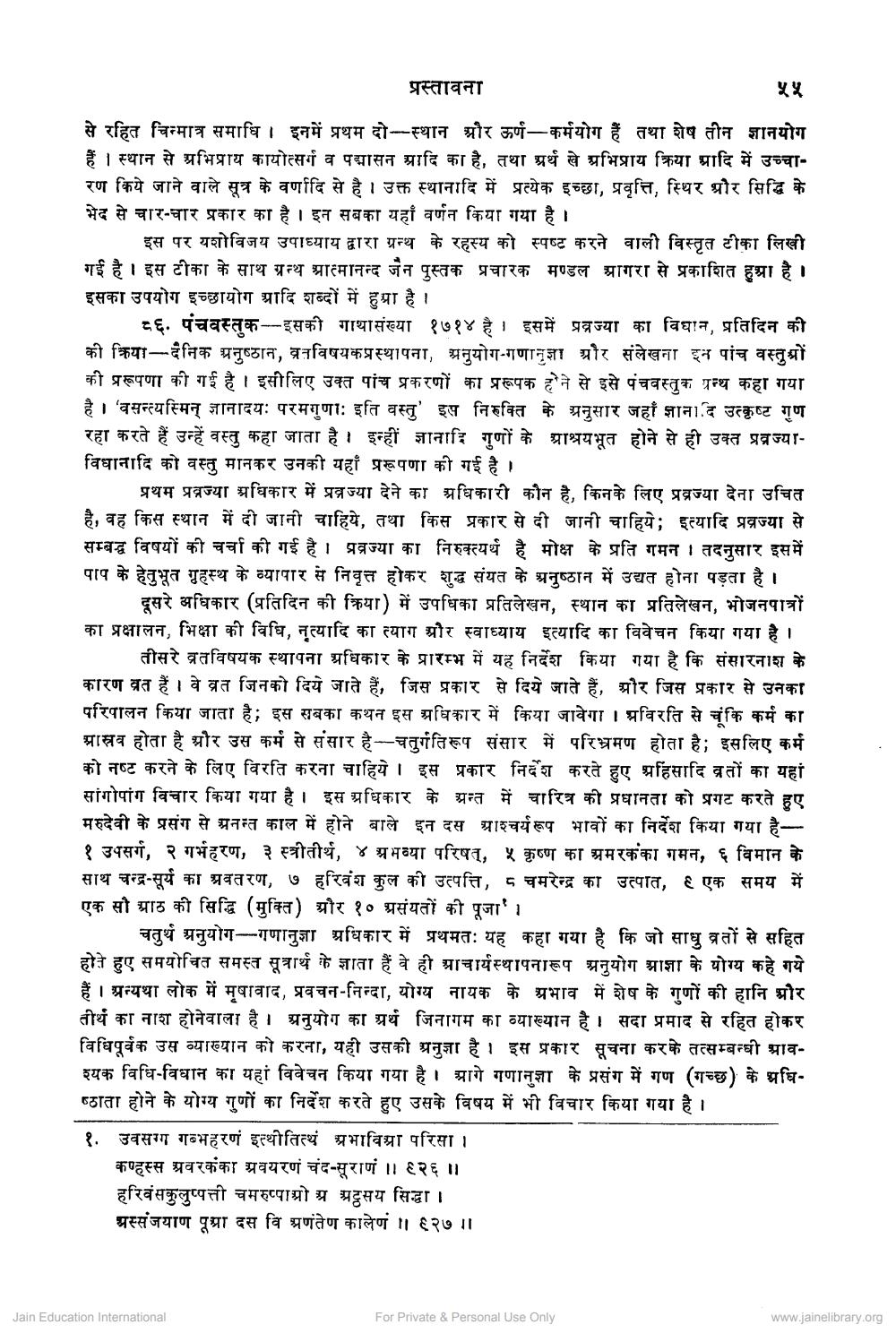________________
प्रस्तावना
से रहित चिन्मात्र समाधि। इनमें प्रथम दो-स्थान और ऊर्ण-कर्मयोग हैं तथा शेष तीन ज्ञानयोग हैं । स्थान से अभिप्राय कायोत्सर्ग व पद्मासन आदि का है, तथा अर्थ खे अभिप्राय क्रिया प्रादि में उच्चारण किये जाने वाले सूत्र के वर्णादि से है। उक्त स्थानादि में प्रत्येक इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिर और सिद्धि के भेद से चार-चार प्रकार का है। इन सबका यहाँ वर्णन किया गया है।
इस पर यशोविजय उपाध्याय द्वारा ग्रन्थ के रहस्य को स्पष्ट करने वाली विस्तृत टीका लिखी गई है । इस टीका के साथ ग्रन्थ प्रात्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल आगरा से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इच्छायोग आदि शब्दों में हुआ है।
८६. पंचवस्तुक-इसकी गाथासंख्या १७१४ है। इसमें प्रव्रज्या का विधान, प्रतिदिन की की क्रिया-दनिक अनुष्ठान, व्रतविषयकप्रस्थापना, अनयोग-गणानज्ञा और संलेखना इन पांच वस्तुओं की प्ररूपणा की गई है। इसीलिए उक्त पांच प्रकरणों का प्ररूपक होने से इसे पंचवस्तुक ग्रन्थ कहा गया है। 'वसन्त्यस्मिन् ज्ञानादयः परमगुणा: इति वस्तु' इस निरूक्ति के अनुसार जहाँ ज्ञानादि उत्कृष्ट गण रहा करते हैं उन्हें वस्तु कहा जाता है। इन्हीं ज्ञानादि गुणों के प्राश्रयभूत होने से ही उक्त प्रव्रज्याविधानादि को वस्तु मानकर उनकी यहाँ प्ररूपणा की गई है।
प्रथम प्रव्रज्या अधिकार में प्रव्रज्या देने का अधिकारी कौन है, किनके लिए प्रव्रज्या देना उचित है, वह किस स्थान में दी जानी चाहिये, तथा किस प्रकार से दी जानी चाहिये; इत्यादि प्रव्रज्या से सम्बद्ध विषयों की चर्चा की गई है। प्रव्रज्या का निरुक्त्यर्थ है मोक्ष के प्रति गमन । तदनुसार इसमें पाप के हेतुभूत गृहस्थ के व्यापार से निवृत्त होकर शुद्ध संयत के अनुष्ठान में उद्यत होना पड़ता है।
दूसरे अधिकार (प्रतिदिन की क्रिया) में उपधिका प्रतिलेखन, स्थान का प्रतिलेखन, भोजनपात्रों का प्रक्षालन, भिक्षा की विधि, नत्यादि का त्याग और स्वाध्याय इत्यादि का विवेचन किया गया है।
तीसरे व्रतविषयक स्थापना अधिकार के प्रारम्भ में यह निर्देश किया गया है कि संसारनाश के कारण व्रत हैं। वे व्रत जिनको दिये जाते हैं, जिस प्रकार से दिये जाते हैं, और जिस प्रकार से उनका परिपालन किया जाता है; इस सबका कथन इस अधिकार में किया जावेगा । अविरति से चूंकि कर्म का प्रास्रव होता है और उस कर्म से संसार है-चतुर्गतिरूप संसार में परिभ्रमण होता है। इसलिए कर्म को नष्ट करने के लिए विरति करना चाहिये । इस प्रकार निर्देश करते हुए अहिंसादि व्रतों का यहां सांगोपांग विचार किया गया है। इस अधिकार के अन्त में चारित्र की प्रधानता को प्रगट करते हुए मरुदेवी के प्रसंग से अनन्त काल में होने बाले इन दस प्राश्चर्यरूप भावों का निर्देश किया गया है१ उपसर्ग, २ गर्भहरण, ३ स्त्रीतीर्थ, ४ अभव्या परिषत्, ५ कृष्ण का अमरकंका गमन, ६ विमान के साथ चन्द्र-सूर्य का अवतरण, ७ हरिवंश कुल की उत्पत्ति, ८ चमरेन्द्र का उत्पात, ६ एक समय में एक सौ पाठ की सिद्धि (मुक्ति) और १० असंयतों की पूजा'।
चतुर्थ अनुयोग-गणानुज्ञा अधिकार में प्रथमत: यह कहा गया है कि जो साधु व्रतों से सहित होते हुए समयोचित समस्त सूत्रार्थ के ज्ञाता हैं वे ही प्राचार्यस्थापनारूप अनुयोग आज्ञा के योग्य कहे गये हैं । अन्यथा लोक में मृषावाद, प्रवचन-निन्दा, योग्य नायक के अभाव में शेष के गुणों की हानि और तीर्थ का नाश होनेवाला है। अनुयोग का अर्थ जिनागम का व्याख्यान है। सदा प्रमाद से रहित होकर विधिपूर्वक उस व्याख्यान को करना, यही उसकी अनुज्ञा है। इस प्रकार सूचना कर के तत्सम्बन्धी प्रावश्यक विधि-विधान का यहां विवेचन किया गया है। आगे गणानज्ञा के प्रसंग में गण (गच्छ) के अधिष्ठाता होने के योग्य गुणों का निर्देश करते हुए उसके विषय में भी विचार किया गया है।
१. उवसग्ग गब्भहरणं इत्थीतित्थं अभाविप्रा परिसा ।
कण्हस्स अवरकंका अवयरणं चंद-सूराणं ।। ६२६ ॥ हरिवंसकुलुप्पत्ती चमरुप्पाम्रो अ अट्रसय सिद्धा। अस्संजयाण पूमा दस वि अणंतेण कालेणं ॥६२७ ।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org