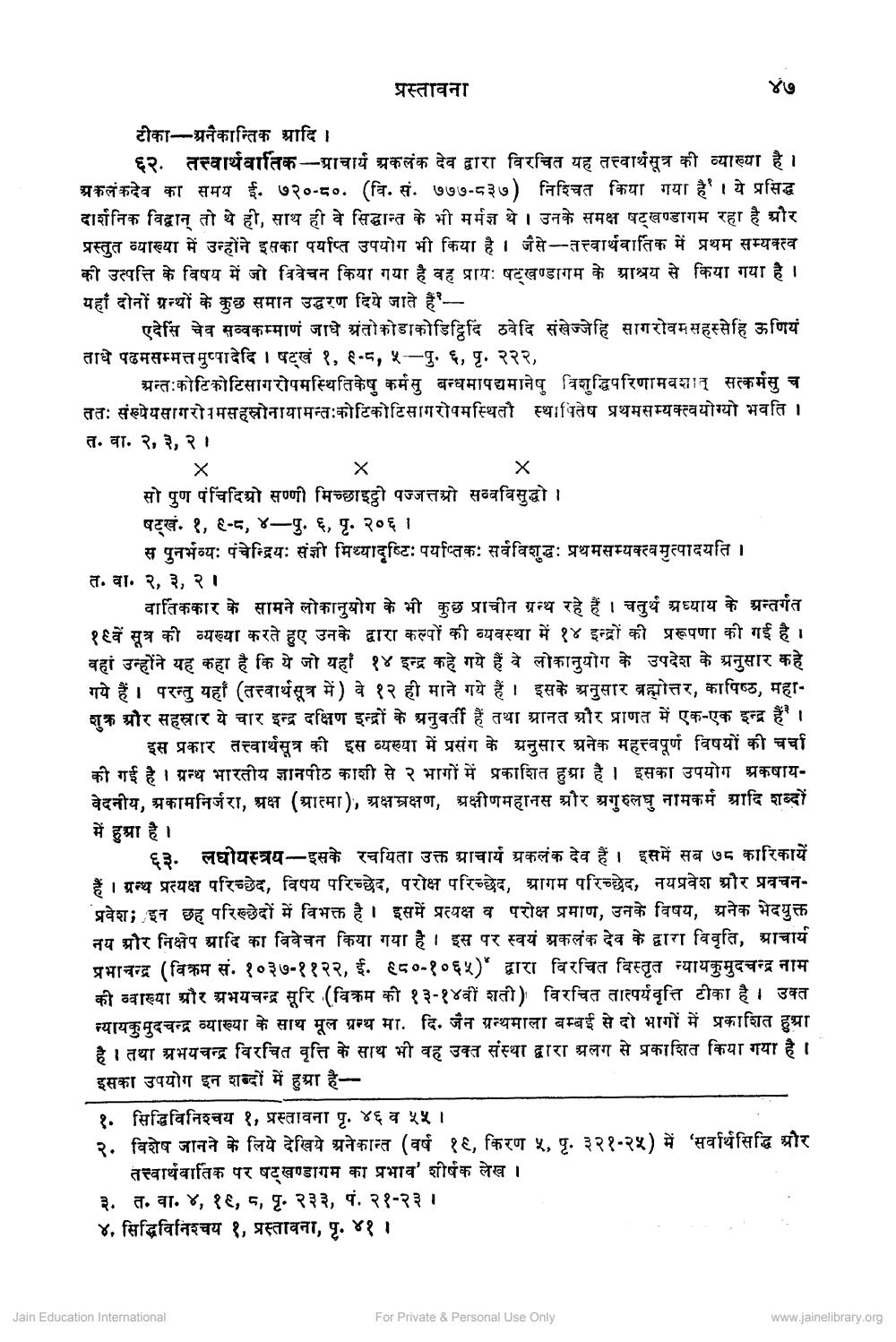________________
प्रस्तावना
टीकाप्रनैकान्तिक आदि ।
६२. तत्वार्थवार्तिक - प्राचार्य अकलंक देव द्वारा विरचित यह तत्त्वार्थ सूत्र की व्याख्या है | कलंकदेव का समय ई. ७२०-८० (वि. सं. ७७७-८३७) निश्चित किया गया है । ये प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् तो थे ही, साथ ही वे सिद्धान्त के भी मर्मज्ञ थे । उनके समक्ष षट्खण्डागम रहा है और प्रस्तुत व्याख्या में उन्होंने इसका पर्याप्त उपयोग भी किया है । जैसे -- तत्त्वार्थवार्तिक में प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति के विषय में जो विवेचन किया गया है वह प्रायः षट्खण्डागम के प्रश्रय से किया गया है । यहाँ दोनों ग्रन्थों के कुछ समान उद्धरण दिये जाते हैं'
देसि चैव सव्वकम्माणं जाघे अंतोकोडा कोडिट्ठिदि ठवेदि संखेज्जेहि सागरोवमसहस्सेहि ऊणियं ता पढमसम्मत्तमुप्पादेदि । षट्खं १, १ ८ ५ – पु. ६, पृ. २२२,
अन्तःकोटिकोटिसागरोपमस्थितिकेषु कर्मसु बन्धमापद्यमानेषु विशुद्धिपरिणामवशात् सत्कर्मसु च ततः संख्ये यसागरोन मसहस्रानायामन्तः कोटिकोटिसागरोपमस्थितौ स्थापितेष प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवति । त. वा. २, ३, २ ।
X
X
X
सो पण पंचिदिसणी मिच्छाइट्ठी पज्जत्तम्रो सव्वविद्धो ।
षट्खं. १, ६-८, ४ – पु. ६, पृ. २०६ |
स पुनर्भव्यः पंचेन्द्रियः संज्ञी मिथ्यादृष्टिः पर्याप्तकः सर्वविशुद्धः प्रथमसम्यक्त्वमुत्पादयति ।
त. वा. २, ३, २ ।
वार्तिककार के सामने लोकानुयोग के भी कुछ प्राचीन ग्रन्थ रहे हैं । चतुर्थ अध्याय के अन्तर्गत १६ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए उनके द्वारा कल्पों की व्यवस्था में १४ इन्द्रों की प्ररूपणा की गई है । वहां उन्होंने यह कहा है कि ये जो यहाँ १४ इन्द्र कहे गये हैं वे लोकानुयोग के उपदेश के अनुसार कहे गये हैं । परन्तु यहाँ (तत्स्वार्थ सूत्र में ) वे १२ ही माने गये हैं । इसके अनुसार ब्रह्मोत्तर, कापिष्ठ, महाशुक्र और सहस्रार ये चार इन्द्र दक्षिण इन्द्रों के अनुवर्ती हैं तथा प्रानत और प्राणत में एक-एक इन्द्र हैं । इस प्रकार तत्त्वार्थसूत्र की इस व्यख्या में प्रसंग के अनुसार अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई है । ग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठ काशी से २ भागों में प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग प्रकषायवेदनीय, अकामनिर्जरा, अक्ष ( आत्मा ), अक्षम्रक्षण, प्रक्षीणमहानस और अगुरुलघु नामकर्म आदि शब्दों में हुआ है।
४७
६३. लघीयस्त्रय - इसके रचयिता उक्त प्राचार्य प्रकलंक देव हैं । इसमें सब ७८ कारिकायें हैं । ग्रन्थ प्रत्यक्ष परिच्छेद, विषय परिच्छेद, परोक्ष परिच्छेद, श्रागम परिच्छेद, नयप्रवेश और प्रवचनप्रवेश; इन छह परिच्छेदों में विभक्त है । इसमें प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाण, उनके विषय, अनेक भेदयुक्त नय और निक्षेप आदि का विवेचन किया गया है। इस पर स्वयं अकलंक देव के द्वारा विवृति, आचार्य प्रभाचन्द्र (विक्रम सं. १०३७-११२२, ई. ६८० - १०६५ ) * द्वारा विरचित विस्तृत न्यायकुमुदचन्द्र नाम की व्याख्या और अभयचन्द्र सूरि (विक्रम की १३-१४वीं शती) विरचित तात्पर्यवृत्ति टीका है । उक्त न्यायकुमुदचन्द्र व्याख्या के साथ मूल ग्रन्थ मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई से दो भागों में प्रकाशित हुना है | तथा अभयचन्द्र विरचित वृत्ति के साथ भी वह उक्त संस्था द्वारा अलग से प्रकाशित किया गया है । इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है
१. सिद्धिविनिश्चय १, प्रस्तावना पृ. ४६ व ५५ ।
२. विशेष जानने के लिये देखिये अनेकान्त ( वर्ष १६, किरण ५, पृ. ३२१-२५) में 'सर्वार्थसिद्धि और तस्वार्थवार्तिक पर षट्खण्डागम का प्रभाव' शीर्षक लेख ।
३. त. वा. ४, १६, ८, पृ. २३३, पं. २१-२३ ।
४, सिद्धिविनिश्चय १, प्रस्तावना, पृ. ४१ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org