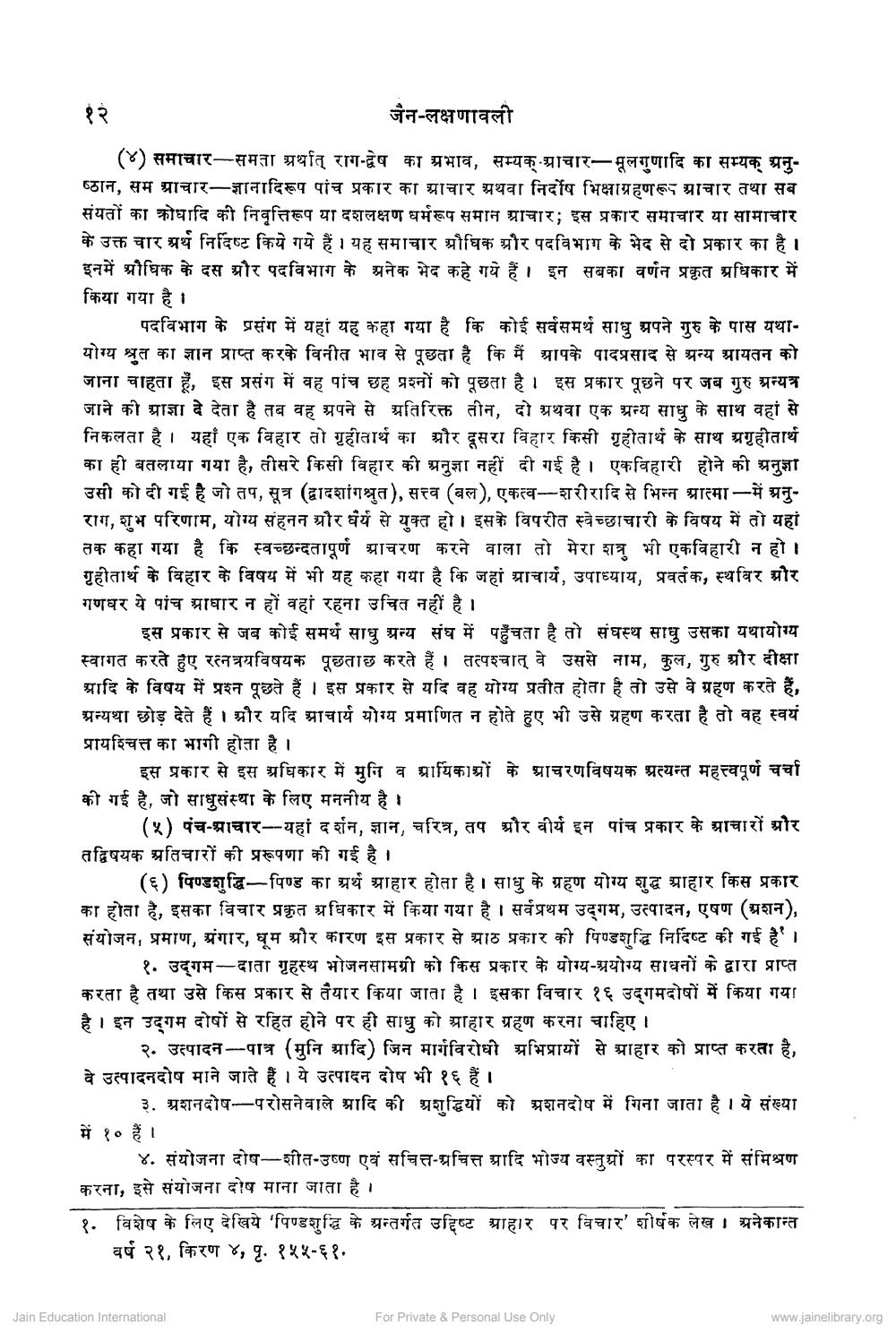________________
१२
जैन-लक्षणावली
(४) समाचार-समता अर्थात् राग-द्वेष का अभाव, सम्यक् प्राचार-मूलगुणादि का सम्यक् अनुष्ठान, सम प्राचार-ज्ञानादिरूप पांच प्रकार का प्राचार अथवा निर्दोष भिक्षाग्रहणरूप प्राचार तथा सब संयतों का क्रोधादि की निवृत्तिरूप या दशलक्षण धर्मरूप समान प्राचार; इस प्रकार समाचार या सामाचार के उक्त चार अर्थ निर्दिष्ट किये गये हैं। यह समाचार औधिक और पदविभाग के भेद से दो प्रकार का है। इनमें औधिक के दस और पदविभाग के अनेक भेद कहे गये हैं। इन सबका वर्णन प्रकृत अधिकार में किया गया है।
पदविभाग के प्रसंग में यहां यह कहा गया है कि कोई सर्वसमर्थ साधु अपने गुरु के पास यथायोग्य श्रुत का ज्ञान प्राप्त करके विनीत भाव से पूछता है कि मैं आपके पादप्रसाद से अन्य आयतन को जाना चाहता हूँ, इस प्रसंग में वह पांच छह प्रश्नों को पूछता है। इस प्रकार पूछने पर जब गुरु अन्यत्र जाने की प्राज्ञा दे देता है तब वह अपने से अतिरिक्त तीन, दो अथवा एक अन्य साधु के साथ वहां से निकलता है। यहाँ एक विहार तो गृहीतार्थ का और दूसरा विहार किसी गृहीतार्थ के साथ अगृहीतार्थ का ही बतलाया गया है, तीसरे किसी विहार की अनुज्ञा नहीं दी गई है। एकविहारी होने की अनुज्ञा उसी को दी गई है जो तप, सूत्र (द्वादशांगश्रुत), सत्त्व (बल), एकत्व-शरीरादि से भिन्न आत्मा-में अनुराग, शुभ परिणाम, योग्य संहनन और धैर्य से युक्त हो। इसके विपरीत स्वेच्छाचारी के विषय में तो यहां तक कहा गया है कि स्वच्छन्दतापूर्ण आचरण करने वाला तो मेरा शत्रु भी एकविहारी न हो। गृहीतार्थ के विहार के विषय में भी यह कहा गया है कि जहां प्राचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर ये पांच प्राधार न हों वहां रहना उचित नहीं है।
इस प्रकार से जब कोई समर्थ साधू अन्य संघ में पहुँचता है तो संघस्थ साधु उसका यथायोग्य स्वागत करते हुए रत्नत्रयविषयक पूछताछ करते हैं। तत्पश्चात् वे उससे नाम, कुल, गुरु और दीक्षा
आदि के विषय में प्रश्न पूछते हैं । इस प्रकार से यदि वह योग्य प्रतीत होता है तो उसे वे ग्रहण करते हैं, अन्यथा छोड़ देते हैं। और यदि आचार्य योग्य प्रमाणित न होते हए भी उसे ग्रहण करता है तो वह स्वयं प्रायश्चित्त का भागी होता है।
इस प्रकार से इस अधिकार में मुनि ब प्रायिकाओं के प्राचरणविषयक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चर्चा की गई है, जो साधुसंस्था के लिए मननीय है।
(५) पंच-प्राचार-यहां दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप और वीर्य इन पांच प्रकार के प्राचारों और तद्विषयक अतिचारों की प्ररूपणा की गई है।
(६) पिण्डशुद्धि-पिण्ड का अर्थ आहार होता है। साधु के ग्रहण योग्य शुद्ध आहार किस प्रकार का होता है, इसका विचार प्रकृत अधिकार में किया गया है । सर्वप्रथम उद्गम, उत्पादन, एषण संयोजन, प्रमाण, अंगार, धूम और कारण इस प्रकार से पाठ प्रकार की पिण्डशुद्धि निर्दिष्ट की गई है।
१. उद्गम-दाता गृहस्थ भोजनसामग्री को किस प्रकार के योग्य-अयोग्य साधनों के द्वारा प्राप्त करता है तथा उसे किस प्रकार से तैयार किया जाता है। इसका विचार १६ उद्गमदोषों में किया गया है। इन उद्गम दोषों से रहित होने पर ही साधु को आहार ग्रहण करना चाहिए।
२. उत्पादन-पात्र (मुनि आदि) जिन मार्गविरोधी अभिप्रायों से आहार को प्राप्त करता है, वे उत्पादनदोष माने जाते हैं । ये उत्पादन दोष भी १६ हैं।
३. प्रशनदोष-परोसनेवाले आदि की प्रशद्धियों को प्रशनदोष में गिना जाता है। ये संख्या
४. संयोजना दोष-शीत-उष्ण एवं सचित्त-अचित्त प्रादि भोज्य वस्तुओं का परस्पर में संमिश्रण करना, इसे संयोजना दोष माना जाता है। १. विशेष के लिए देखिये 'पिण्डशुद्धि के अन्तर्गत उद्दिष्ट आहार पर विचार' शीर्षक लेख । अनेकान्त
वर्ष २१, किरण ४, पृ. १५५-६१.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org